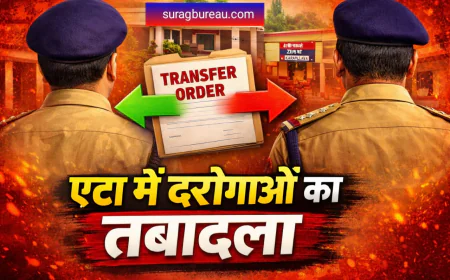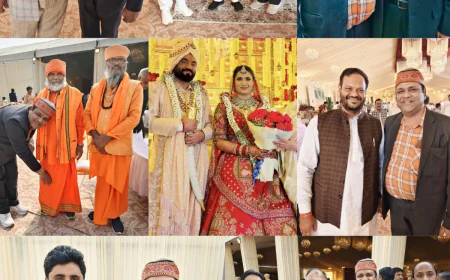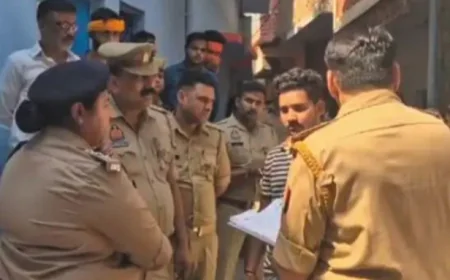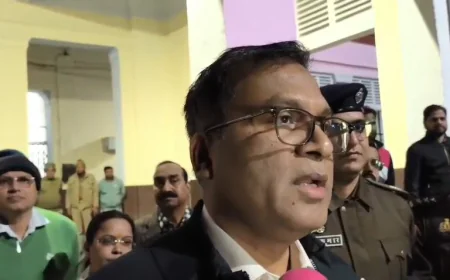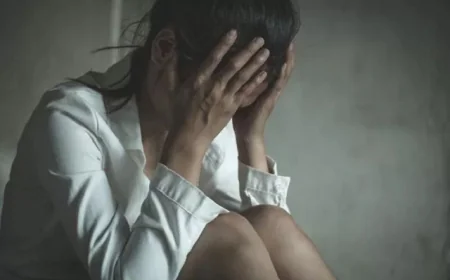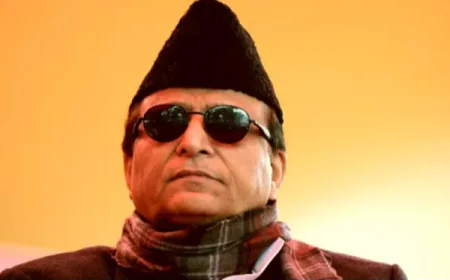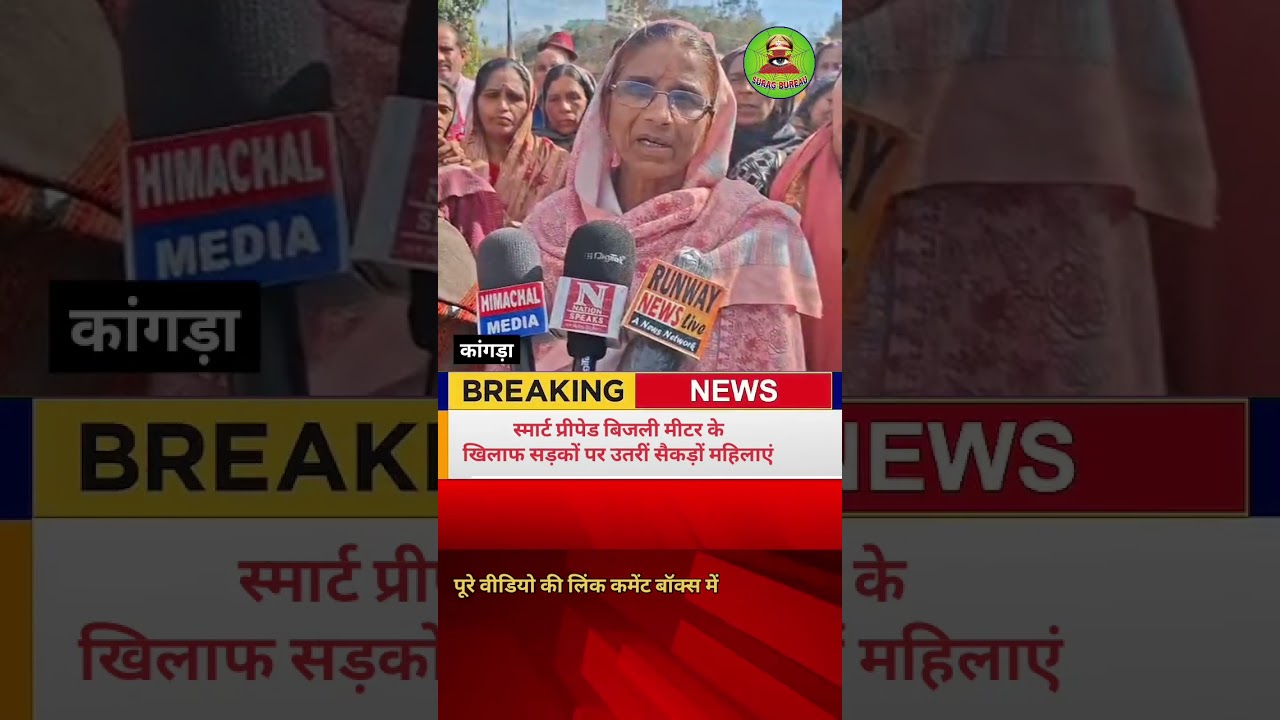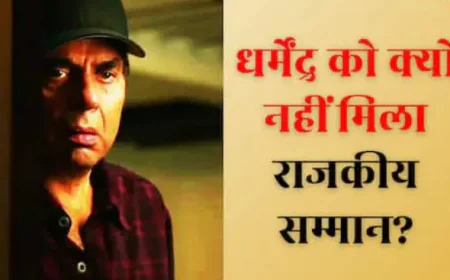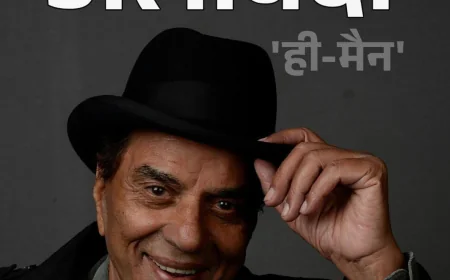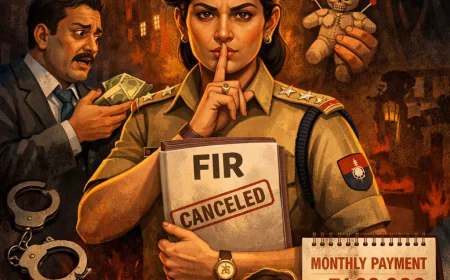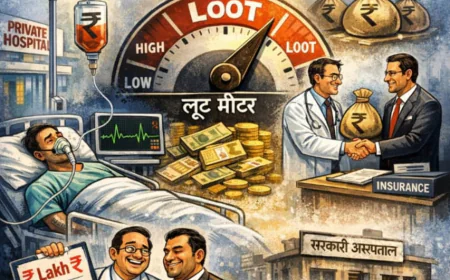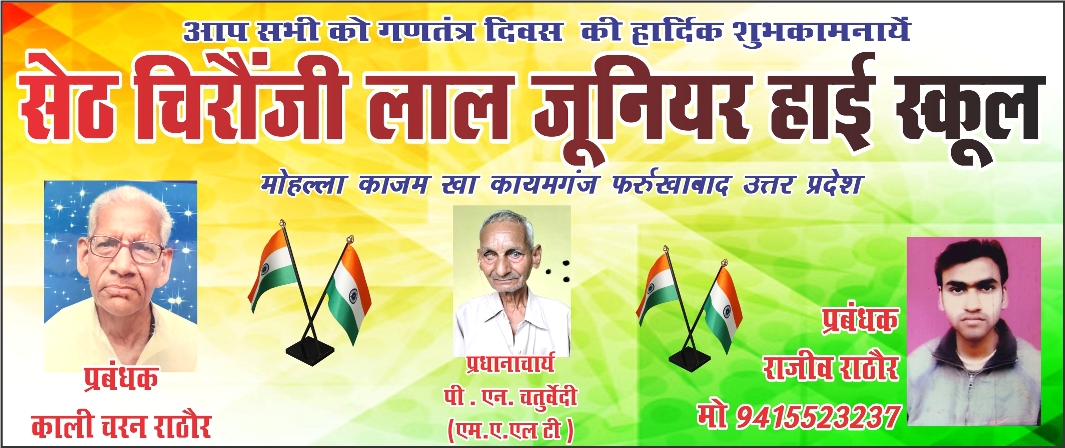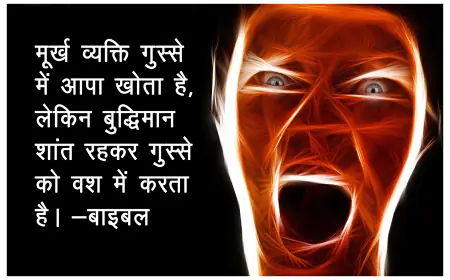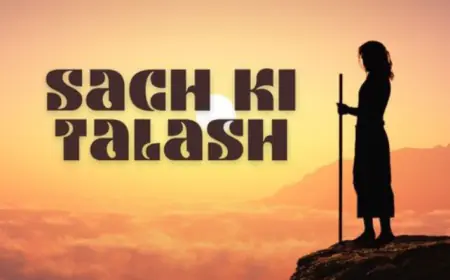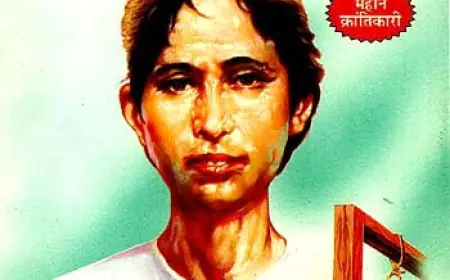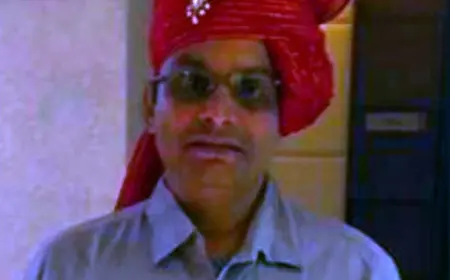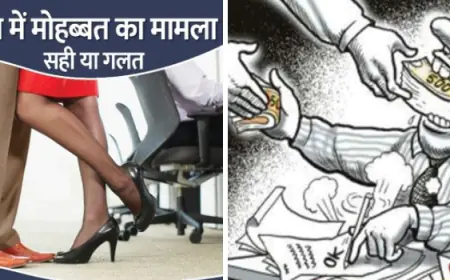78 साल का शैक्षिक सुधार: स्वतंत्रता के बाद से देश की शिक्षा प्रणाली की उल्लेखनीय यात्रा
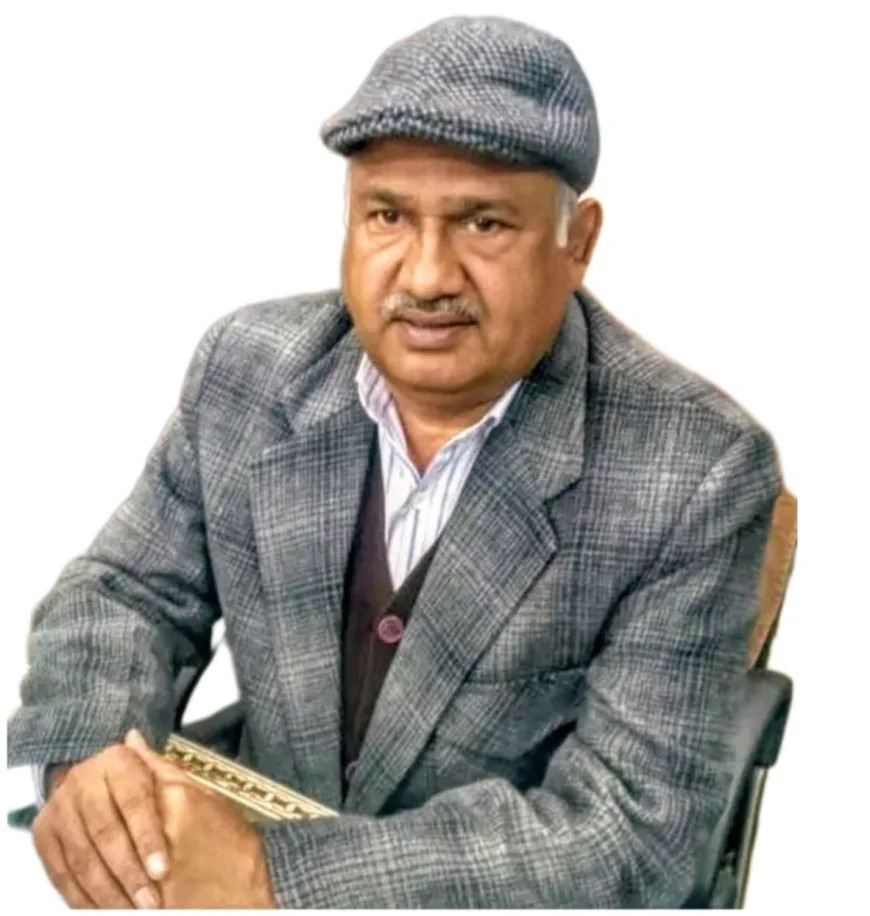
78 साल का शैक्षिक सुधार: स्वतंत्रता के बाद से देश की शिक्षा प्रणाली की उल्लेखनीय यात्रा
भारत आजादी के 78 साल मनाता है, यह देश की शिक्षा प्रणाली की उल्लेखनीय यात्रा पर विचार करने का एक उपयुक्त क्षण है। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों से लेकर वर्तमान दिन तक, भारत ने शिक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तनकारी परिवर्तन देखे हैं, जो अधिक समावेशी और प्रगतिशील समाज के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से, भारत ने शैक्षिक सुधार की एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की है, जो औपनिवेशिक अभिजात वर्ग में निहित एक से अधिक समावेशी, न्यायसंगत और विकास-उन्मुख ढांचे में अपनी प्रणाली को बदल रही है। इस 78 वर्ष के विकास को कई प्रमुख नीतियों, आयोगों और पहलों के माध्यम से पता लगाया जा सकता है जिन्होंने शैक्षिक परिदृश्य को आकार दिया है।
प्रारंभिक वर्ष: नींव रखना (1947-1968) स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने और पहुंच का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 1950 में अपनाए गए भारत के संविधान में 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का निर्देश शामिल था। विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रमुख कमीशन नियुक्त किए गए थे: ** विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-1949): डॉ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इस आयोग ने तीन साल के डिग्री कोर्स की सिफारिश की और ट्यूटोरियल आधारित सीखने और ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना के महत्व पर जोर दिया। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-1953): मुदलियार आयोग के रूप में भी जाना जाता है, इसका उद्देश्य आदर्श नागरिकों का उत्पादन करना, व्यावसायिक कौशल विकसित करना और नेतृत्व गुणों को बढ़ावा देना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (1953): उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित, विश्वविद्यालयों के विस्तार में यूजीसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आईआईटी और आईआईएम का जन्म: शेपिंग तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा स्वतंत्रता के बाद के युग में सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान ( आईआईएम) की स्थापना थी। पहला आईआईटी 1951 में खड़गपुर में स्थापित किया गया था, उसके बाद मुंबई, कानपुर, मद्रास और दिल्ली में अन्य लोग थे। ये संस्थान जल्दी से उत्कृष्टता के केंद्र बन गए, विश्व स्तरीय इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों का उत्पादन किया जो भारत के औद्योगिक और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कोठारी आयोग (1964-1966) एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो शिक्षा के पूरे क्षेत्र की व्यापक समीक्षा प्रदान करता था।
इसकी सिफारिशों ने 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) का आधार बनाया। नीति में शिक्षा प्रणाली के "कट्टरपंथी पुनर्गठन" का आह्वान किया गया है, इस पर जोर दिया गया है: राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए समान शैक्षिक अवसर। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक, स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक संचार आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए तीन-भाषा सूत्र। राष्ट्रीय आय के 6% तक शिक्षा खर्च में वृद्धि। आधुनिकीकरण और विस्तार (1986-2009) 1986 का एनपीई आधुनिक सुधारों का खाका बन गया, जिसमें असमानताओं को दूर करने और शैक्षिक अवसरों को समान करने पर विशेष जोर दिया गया। इसने कई प्रमुख पहलें पेश कीं: ** ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड (1987): आवश्यक शिक्षण सहायक उपकरण और प्रशिक्षित शिक्षक प्रदान करके प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने का लक्ष्य। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ( आईजीओयु ) की स्थापना के साथ खुली विश्वविद्यालय प्रणाली का विस्तार। रोजगार को बढ़ाने के लिए ग्रेड 11-12 में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर। एक्शन का कार्यक्रम (पीओए) 1992: 1986 की नीति का पालन, इसने कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए, गुणवत्ता में सुधार, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और व्यावसायिक प्रशिक्षण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। मील का पत्थर विधान और सार्वभौमिकता (2009-2020) इस अवधि में विधायी कार्रवाई के माध्यम से शैक्षिक अधिकारों का समेकन देखा गया। 2009 के बच्चों को नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (आरटीई) का अधिकार एक स्मारकीय कदम था, जिससे शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बन गया।
आरटीई अधिनियम में यह भी कहा गया है कि निजी स्कूल वंचित बच्चों के लिए अपनी 25% सीटें आरक्षित करते हैं, जो समावेशिता के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 सबसे हालिया और दूरगामी सुधार का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से ओवरहाल करना है। यह कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ सीखने के लिए एक लचीला और समग्र दृष्टिकोण प्रस्तावित करता है: नई 5 + 3 + 3 + 4 पाठयक्रम संरचना: यह समग्र सीखने को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत, तैयारी, मध्य और माध्यमिक चरणों के साथ कठोर 10 + 2 प्रणाली की जगह लेता है। रटने की याद से अनुभवात्मक सीखने में बदलाव: नीति परियोजना-आधारित आकलन और परीक्षाओं के बोझ में कमी पर जोर देती है। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना: प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्वीकार करते हुए, एनईपी 2020 का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पाटना और प्रौद्योगिकी को सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत करना है। उपलब्धियां और लगातार चुनौतियां पिछले 78 वर्षों में, भारत के शैक्षिक सुधारों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जन्म दिया है: साक्षरता दर में वृद्धि: 1947 में महज 12% से लेकर आज 77% से अधिक, साक्षरता में नाटकीय सुधार देखा गया है। शिक्षा प्रणाली का विस्तार: भारत अब लाखों स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक का दावा करता है। लिंग अंतर में कमी: महिला साक्षरता और नामांकन दरों में सुधार में काफी प्रगति हुई है। हालांकि, महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी रहती हैं, जिनमें शामिल हैं: शिक्षा की गुणवत्ता: उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, एक बड़ी चिंता का विषय है। शिक्षक प्रशिक्षण और योग्यता: शिक्षक प्रशिक्षण में अंतराल और निरंतर व्यावसायिक विकास की आवश्यकता चल रही है। डिजिटल विभाजन: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच में असमानता को समान अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। ड्रॉपआउट दरें: प्रगति के बावजूद, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों से छात्रों की एक महत्वपूर्ण संख्या, अभी भी शिक्षा प्रणाली से बाहर है। चुनौतियां और सड़क आगे पिछले 78 वर्षों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, चुनौतियां बनी हुई हैं। गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, और डिजिटल विभाजन उन मुद्दों को दबा रहे हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। कोवड-19 महामारी ने इन विषमताओं को और अधिक उजागर किया, जिसमें कई छात्र ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों तक पहुंचने में असमर्थ थे।
हालांकि, चल रहे सुधारों और नवाचार और समावेशिता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ, भारत की शिक्षा प्रणाली विकसित होने के लिए तैयार है। एनईपी 2020 द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की नींव रखने वाले शुरुआती सुधारों से, भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास देश की व्यापक आकांक्षाओं को दर्शाता है। विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्राचार्य शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद् स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब