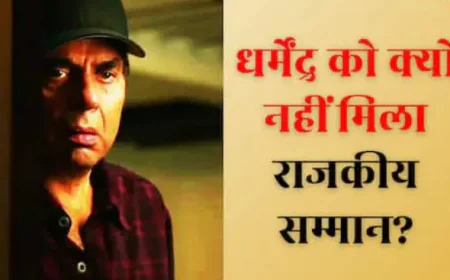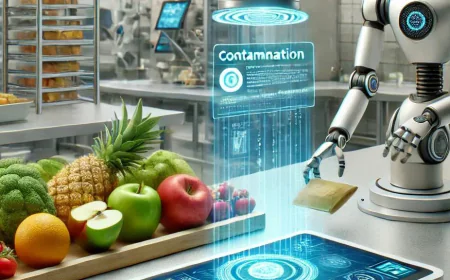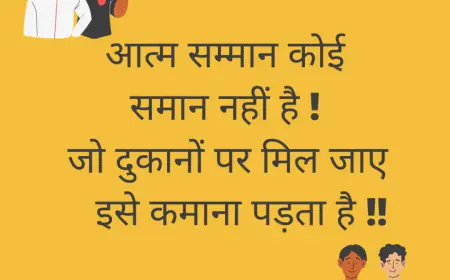प्रलोभन का परिणाम: जब नदियाँ निगलने लगती हैं

प्रलोभन का परिणाम: जब नदियाँ निगलने लगती हैं
भारत में नदियों, पहाड़ों और जल स्रोतों के साथ हो रहा खिलवाड़ अब आपदाओं का कारण बन रहा है। लालचवश लोग नदियों के पाट में मकान और पहाड़ों पर रिसॉर्ट बना रहे हैं। एक टपकता नल प्रतीक है उस सोच का, जो पर्यावरण की उपेक्षा करती है। सेल्फी, पर्यटन और मुनाफ़े की इस भीड़ में प्रकृति दम तोड़ रही है। हमें चेतना की ज़रूरत है—विकास से पहले संवेदना। यदि अब भी नहीं रुके, तो अगली आपदा किसी की संवेदना नहीं देखेगी, बस सबकुछ बहा ले जाएगी। प्रकृति माफ़ नहीं करती, वह वापस लेती है।
✍️ डॉ. प्रियंका सौरभ
यह अजीब विडंबना है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो हम सिर्फ़ मरने वालों पर शोक प्रकट करते हैं — जबकि जिनके लालच, उपेक्षा और मूर्खता से वह आपदा आई, उन पर सवाल उठाने का साहस नहीं करते। एक नदी के बहाव में बहे मकानों और दुकानों को देखकर हम आंसू तो बहाते हैं, लेकिन क्या हम उस कुकर्म पर विचार करते हैं जिसने नदी की गोद में घर बनवा दिए? आज भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, हर जगह मनुष्य का प्रलोभन ही विनाश का बीज बन चुका है। हाल की घटनाएं — उत्तरकाशी, जोशीमठ, केदारनाथ, किन्नौर या हिमाचल की तबाही — सभी हमें याद दिलाती हैं कि जब मनुष्य अपने हित में प्रकृति की रेखाएं मिटा देता है, तो नदी, पहाड़, बादल और धरती एक दिन सबकुछ वापस ले लेते हैं। मेरे घर के पास एक छोटा सा रेस्तरां है। उसके नल से दिन-रात पानी टपकता रहता है।
मैंने कई बार कहा, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा। एक ढीला वॉशर बदलने से समस्या हल हो सकती है, लेकिन सौ-पचास रुपये की मरम्मत उनके लिए बेमतलब है। पानी बहता है, तो बहता रहे। क्या यह एक रेस्तरां तक सीमित लापरवाही है? बिल्कुल नहीं। यह प्रतीक है उस मानसिकता का जो कहती है — "जो हो रहा है, होने दो। हमें क्या फर्क पड़ता है?" इस सोच के कारण हर दिन लाखों लीटर पानी व्यर्थ जाता है, गाड़ियों से निकलती धुआं-संस्कृति जारी रहती है, कचरे में दम तोड़ती गायें खड़ी रहती हैं, और हिमालय की छाती पर रिसॉर्ट्स उगते रहते हैं। भारत का हिमालय क्षेत्र न सिर्फ़ भौगोलिक, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारी धरोहर है। परंतु अब वह पर्यटन का बाजार बन चुका है। पहाड़ों की आत्मा शांति थी, अब वह शोर में डूब चुकी है। दो दिन की छुट्टी मिलते ही लाखों लोग सेल्फी, शराब और शोरगुल की भूख लिए हिमालय पर टूट पड़ते हैं। वे वहां शांति खोजने नहीं जाते, बल्कि वहां भी उसी बाजार को बसाना चाहते हैं जिससे भागने का दावा करते हैं। रिसॉर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, पार्किंग, रोड—हर जगह अतिक्रमण है।
पहाड़ की सीमित सहनशक्ति की कोई चिंता नहीं। जिस ज़मीन को सदियों से पेडों ने थामा हुआ था, वहां अब कंक्रीट की मोटी परतें बिछ गई हैं। जब बरसात आती है, तो वह ज़मीन अपने भीतर पानी को नहीं समेट पाती — परिणामस्वरूप, वही जल वेग बनकर जान लेता है। बादल फटते हैं, बाढ़ आती है, और हम सोशल मीडिया पर दुख प्रकट करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या हम पूछते हैं कि उस बाढ़ ने रास्ता क्यों बदला? क्या वह प्राकृतिक था या उसे रोका गया था? नदियाँ सदियों से बहती आई हैं, उन्होंने अपने लिए रास्ता बनाया है। लेकिन जब हम घाटी में मकान बना लेते हैं, नदी के किनारे होटल ठोक देते हैं, तो वह नदी अपने रास्ते को reclaim करेगी ही। उत्तरकाशी की हालिया त्रासदी में पूरा गांव बह गया। लेकिन वह गांव पहाड़ों की गोद में नहीं था — वह नदी के पाट में बना था। यह कोई आस्था नहीं थी, यह लालच था। और लालच कभी भी सुरक्षित नहीं रहता। कठोर शब्द हैं, लेकिन सच यही है कि हम एक मूर्ख और संवेदनहीन समाज में तब्दील हो चुके हैं। हम आपदाओं को रोकने के बजाय उनका इंतज़ार करते हैं ताकि मीडिया को दृश्य मिलें और सरकारें मुआवज़े का तमाशा कर सकें। हमने पर्यावरण को सिर्फ़ एक 'डॉक्युमेंट' बना दिया है।
नीति आयोग से लेकर नगर पंचायत तक, हर स्तर पर विकास का मतलब अतिक्रमण हो गया है। क्या यह दुखद नहीं कि पहाड़ों पर हो रही तबाही के बीच भी लोग 'डील' खोज रहे हैं — “इस सीजन होटल सस्ते मिल जाएंगे”? क्या हमने चेतना खो दी है? दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर पर एक ऑटो चालक ने मुझे बताया कि उसने किसी को यमुना में प्लास्टिक की बोतल फेंकते देखा और बहुत दुखी हुआ। एक छोटे इंसान की बड़ी भावना! लेकिन क्या उस भीड़ को कोई समझा सकता है जो हर नदी, हर घाट, हर पहाड़ को बस ‘घूमने की जगह’ समझती है? हमारी आंतरिक यात्रा कभी शुरू ही नहीं होती। हम गाड़ी में बैठकर पहाड़ तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर का इंसान वहीं के वहीं मैदान में पड़ा रहता है — लालची, उपभोगी और शोरगुल में डूबा। रेस्तरां का टपकता नल भले ही प्रतीकात्मक हो, लेकिन यह उसी उपेक्षा का प्रतीक है जो हमने हिमालय और पर्यावरण के साथ बरती है। हम जिस संसाधन को रोज़ टपकने देते हैं — पानी, हवा, हरियाली, मिट्टी, हिमनद — वे एक दिन सूख जाएँगे। फिर नल नहीं टपकेगा, तब शायद उसमें से हवा भी न निकले। हम गाय को कचरा खिला कर भी उससे दूध की उम्मीद रखते हैं। हम पेड़ काटकर भी चाहते हैं कि बारिश हो। हम नदी को नाला बनाकर भी उससे आचमन की कामना करते हैं। क्या यह पाखंड नहीं है? अब समय मौन शोक का नहीं, चेतना का है। अगर हम नहीं चेते, तो अगली बार कोई नदी, कोई पहाड़, कोई हवा, कोई भूचाल हमें बख्शेगा नहीं। हमें पुनर्विचार करना होगा कि: क्या हम अपने छोटे-छोटे प्रलोभनों को तिलांजलि देने को तैयार हैं?
क्या हम पर्यावरणीय संतुलन को विकास की नींव बना सकते हैं? क्या हम ‘घूमने’ की जगह ‘जुड़ने’ की भावना से प्रकृति के पास जा सकते हैं? क्या हम एक नल टपकने से पहले उसे ठीक कर सकते हैं — ताकि एक पहाड़ गिरने से रोका जा सके? मैं हिमालय नहीं जाती, न ही अपनी यात्राओं को पहाड़ों पर थोपती हूँ। यह कोई त्याग नहीं, सिर्फ़ समझदारी है। मैं विंध्याचल और अरावली की छोटी पहाड़ियों से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हिमालय की छाती पहले ही विदीर्ण है — उसे और कष्ट देना अब पाप है। जब तक हम विकास को सिर्फ़ भवनों और दुकानों में मापते रहेंगे, तब तक विनाश हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हर बहता नल एक आपदा की दस्तक है। हर रिसता पहाड़, हर भरा हुआ नदी का पाट, हर टूटता पुल हमें चेतावनी देता है — कि प्रलोभन का परिणाम बहुत गहरा होता है। नदियाँ जब निगलने लगती हैं, तब देर हो जाती है।