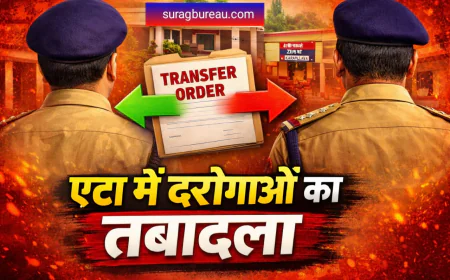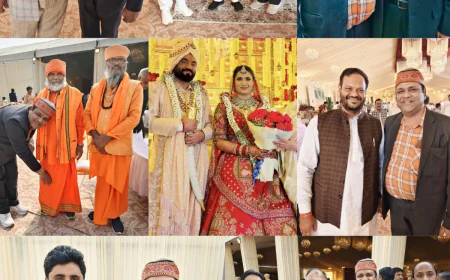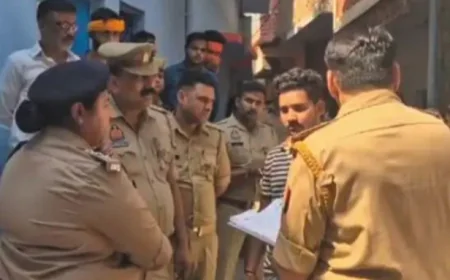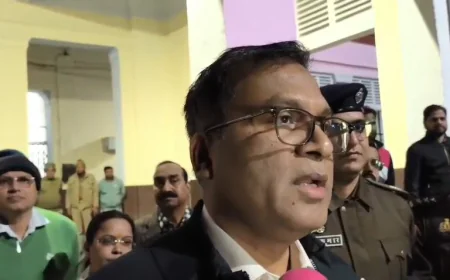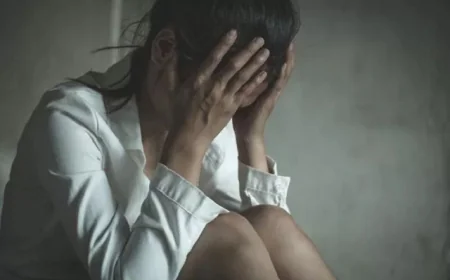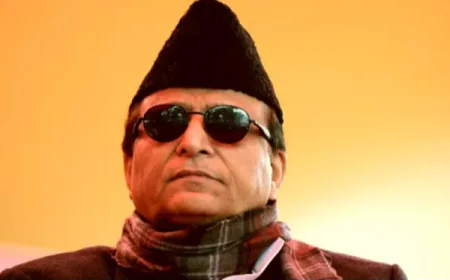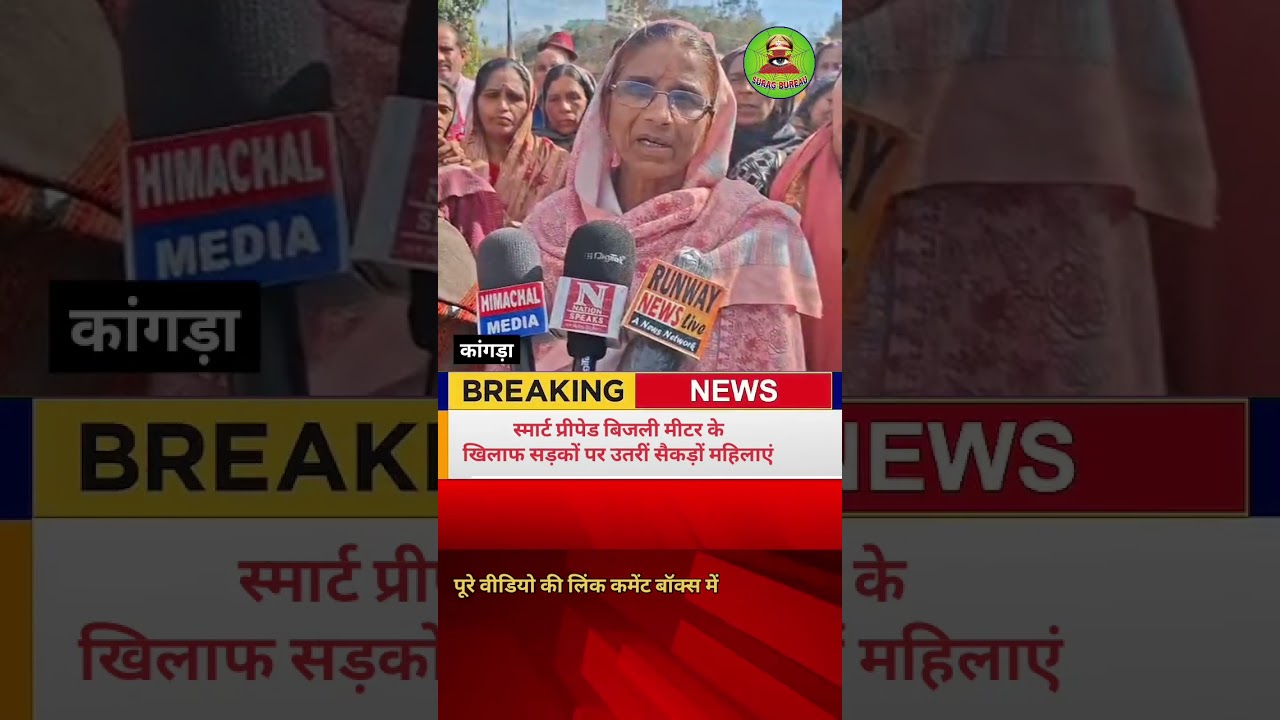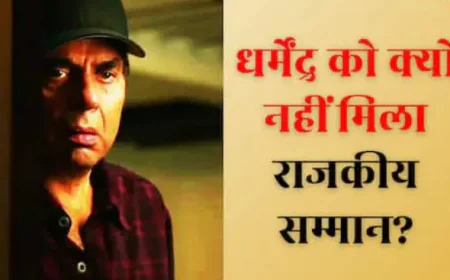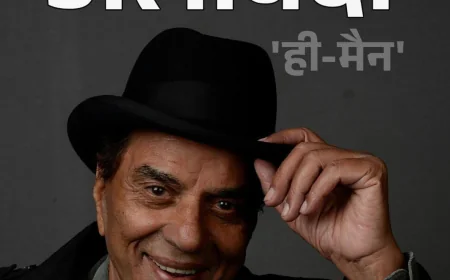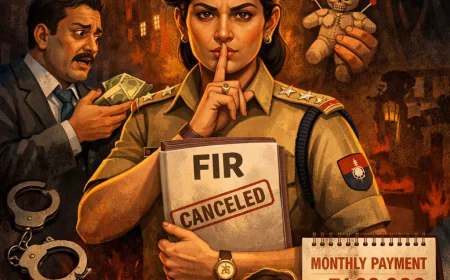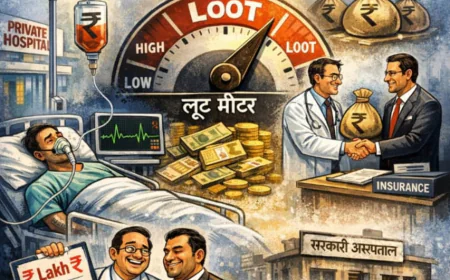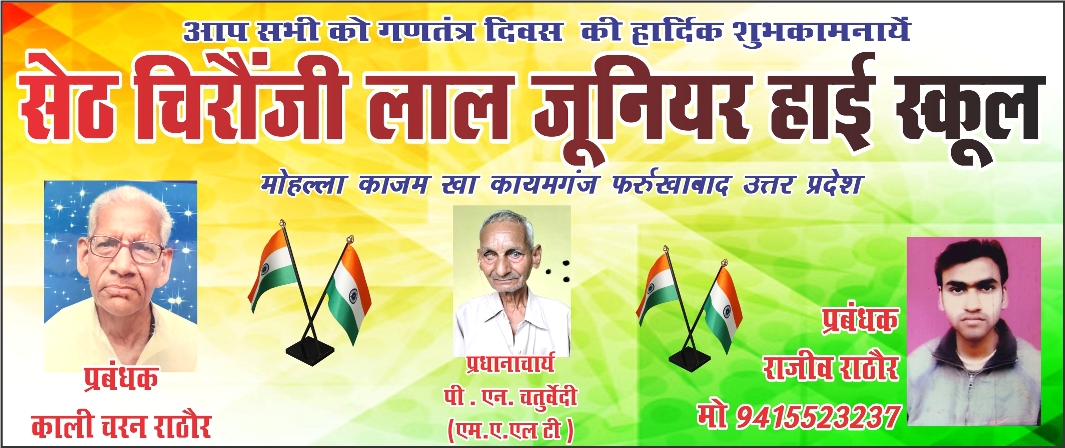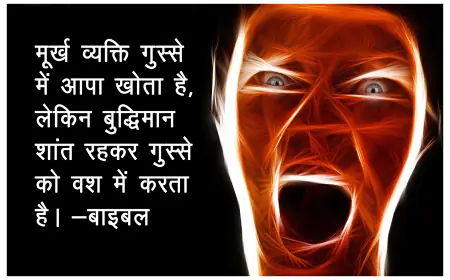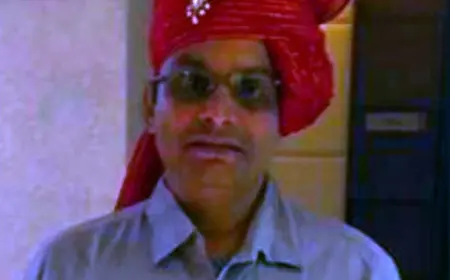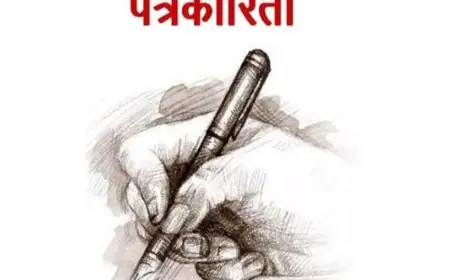एक राष्ट्र, कई आवाज़ें: भारत में भाषाई विविधता

" भारत अपने कई क्षेत्रों में कई प्राचीन और भाषाई रूप से समृद्ध भाषाओं का घर है। एक ही घर में, एक युवा व्यक्ति बोल सकता है, उदाहरण के लिए, ओडिया (ओडिशा के पूर्वी राज्य में बोली जाने वाली भाषा) अपने दादा-दादी के साथ, होमवर्क के लिए अंग्रेजी में स्विच करें, और यूट्यूब पर हिंदी गाने सुनने का आनंद लें। भ्रमित होने से दूर, यह सह-अस्तित्व आवश्यक और प्राकृतिक है। यह एक ऐसे राष्ट्र की पहचान है जहां भाषा विविधता को दूर करने में बाधा बनने के बजाय एक ताकत के रूप में अपनाया जाता है।
उन्होंने कहा, '' [भारतीय भाषाओं] ने हमेशा एक-दूसरे को प्रभावित और समृद्ध किया है। "इस तरह की भ्रांतियों से दूरी बनाना और सभी भाषाओं को गले लगाना और समृद्ध करना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है उनकी टिप्पणी ने एक व्यापक संदेश को मजबूत किया: कि भाषाई विविधता एक बाधा नहीं है, बल्कि एक साझा सांस्कृतिक ताकत है जो भारत को एक साथ जोड़ती है। लेकिन ऐसे विविध देश में भाषा राजनीतिक रूप से विभाजनकारी मुद्दा भी हो सकता है। और भारत के भीतर हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के उपयोग को आकार देने की कोशिश के रूप में देखे गए शब्दों और कार्यों के लिए मोदी और उनकी सरकार के सदस्यों की आलोचना की गई है। देश की भाषाई जटिलता के कारण, स्थिति हमेशा नेविगेट करने के लिए अधिक जटिल होती है क्योंकि यह पहली बार दिखाई दे सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल 19,500 भाषाएँ या बोलियाँ हैं जिन्हें मातृभाषा के रूप में कहा जाता है। उनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के तहत आधिकारिक माना जाता है।
2011 की जनगणना में पाया गया कि 44% भारतीय, लगभग 528 मिलियन लोग, हिंदी को अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते हैं (जिसका अर्थ है कि घर पर क्या बोला जाता है)। इसी तरह, लगभग 57% लोग इसे दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि हिंदी की पूरे क्षेत्रों में व्यापक उपस्थिति है, लेकिन यह मराठी, बंगाली (97 मिलियन), तेलुगु (81 मिलियन), तमिल (69 मिलियन) और मेतेई (1.8 मिलियन) सहित कई अन्य भाषाओं के साथ मौजूद है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में पहली, दूसरी और तीसरी भाषा बोलने वालों को दिखाने वाली तालिका। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में पहला, दूसरा और तीसरा भाषा बोलने वाला। 2011 भारतीय जनगणना, CC BY-NC-SA राष्ट्रीय स्तर पर, भारत की दो आधिकारिक भाषाएँ हैं: हिंदी और अंग्रेजी।
हिंदी का उपयोग केंद्र सरकार के भीतर संचार के लिए किया जाता है, जबकि अंग्रेजी का व्यापक रूप से कानूनी, प्रशासनिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उपयोग किया जाता है। प्रत्येक राज्य राज्य-स्तरीय शासन के लिए अपनी आधिकारिक भाषा चुन सकता है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु तमिल का उपयोग करता है, महाराष्ट्र मराठी का उपयोग करता है, और इसी तरह। लेकिन दैनिक जीवन में, लोग अक्सर भाषाओं के बीच स्विच करते हैं कि वे कहां हैं और वे घर पर, काम पर या सार्वजनिक स्थानों पर किससे बात कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, चार भारतीयों में से लगभग एक ने कहा कि वे कम से कम दो भाषाएं बोल सकते हैं, और 7% से अधिक ने कहा कि वे तीन बोल सकते हैं। भारत ने 1960 के दशक में शिक्षा में तीन भाषा का सूत्र पेश किया था। इस नीति दिशानिर्देश ने छात्रों को तीन भाषाएँ सीखने के लिए प्रोत्साहित किया: उनकी क्षेत्रीय मातृभाषा, हिंदी (यदि यह पहले से ही उनकी पहली भाषा नहीं है) और अंग्रेजी। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों में एक लचीला और समावेशी दृष्टिकोण पैदा करना था। 2020 में, मोदी सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की, जिसने राज्यों को यह चुनने के लिए अधिक लचीलापन दिया कि अंग्रेजी के साथ दो भारतीय भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन सभी राज्यों में सिफारिश को अनिवार्य कर दिया। इससे कई राज्यों में एक प्रतिक्रिया हुई है क्योंकि कुछ लोगों को डर है कि यह प्रभावी रूप से बैकडोर द्वारा हिंदी शिक्षण का परिचय देता है और अन्य भाषाओं के उपयोग को पतला करेगा।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा भारत की आधिकारिक भाषाओं को दिखाने वाला नक्शा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा भारत की आधिकारिक भाषाएँ। विकिमीडिया कॉमन्स के माध्यम से Sbb1413 भारत में अंग्रेजी की भूमिका के बारे में भी काफी बहस हो रही है, जो लगभग 10.6% भारतीय कुछ हद तक बोलते हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि औपनिवेशिक शासन का अवशेष है। मोदी ने खुद सुझाव दिया है कि यह मामला है और अंग्रेजी के आधिकारिक उपयोग को कम करने के लिए कार्रवाई की है, उदाहरण के लिए मेडिकल स्कूलों में। हालांकि, उन्होंने अंग्रेजी के महत्व को भी स्वीकार किया है, विशेष रूप से वैश्विक संचार में, और सभी भारतीय भाषाओं के मूल्य को देश की एकता और प्रगति के लिए लाया गया है। उन्होंने महाराष्ट्र में दर्शकों से कहा, "सभी भाषाओं को गले लगाना हमारा कर्तव्य है," अंग्रेजी सहित भारतीय भाषाओं ने हमेशा एक-दूसरे को समृद्ध किया है और हमारी एकता की नींव बनाई है। कई लोग भाषा को भारत के कई भाषाई समुदायों के बीच एक कड़ी के रूप में देखते हैं। अन्य लोग देखते हैं कि यह सामाजिक गतिशीलता के लिए एक उपकरण है, विशेष रूप से निचली जातियों के लिए। कुछ ने सरकार पर सामाजिक विशेषाधिकारों को बनाए रखने और हिंदी के प्रभुत्व को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी को हतोत्साहित करने का भी आरोप लगाया है। दूसरी ओर, 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंग्रेजी के शिक्षण को अनिवार्य करती है। यह अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों की सिफारिश करता है, और प्राथमिक शिक्षा में मातृ भाषाओं के साथ अंग्रेजी को "जहां भी संभव हो" सिखाया जाना चाहिए।
सरकार डिजिटल दुनिया को लोगों के लिए अधिक समावेशी बनाने के लिए भी कदम उठा रही है, चाहे उनकी भाषा कुछ भी हो। 2022 में मोदी द्वारा शुरू की गई, भाषिनी परियोजना एक राष्ट्रीय एआई पहल है जो सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में भाषण-से-पाठ, वास्तविक समय अनुवाद और डिजिटल पहुंच का समर्थन करती है। इसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक सेवाओं को अधिक समावेशी बनाना है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के समुदायों के लिए। जैसा कि कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने एक बार लिखा था: "अगर ईश्वर ने ऐसा चाहा होता, तो वह सभी भारतीयों को एक भाषा के साथ बोलते ... भारत की एकता रही है और हमेशा विविधता में एकता रहेगी भारत में, बच्चे आज अपनी मातृभाषा बोलते हुए बड़े होते हैं, कई क्षेत्रों में संवाद करने के लिए हिंदी सीखते हैं, और वैश्विक कनेक्शन के लिए अंग्रेजी कौशल प्राप्त करते हैं। भारत का भविष्य एक भाषा को दूसरे के ऊपर चुनने पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उन्हें अगल-बगल पनपने में सक्षम बनाता है। "भाषा सीखने के लिए एक और खिड़की है जिससे दुनिया को देखने के लिए है ऐसी हजारों खिड़कियों से भारत का भविष्य एकता और विविधता दोनों में निहित है।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब