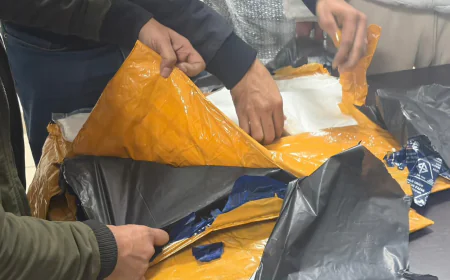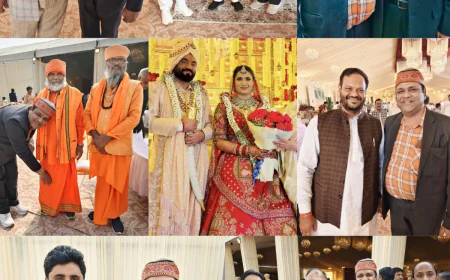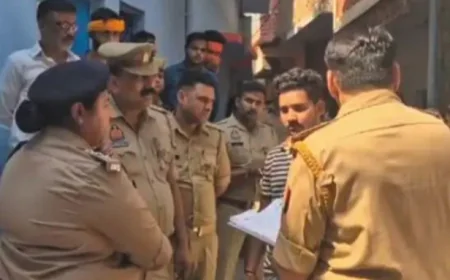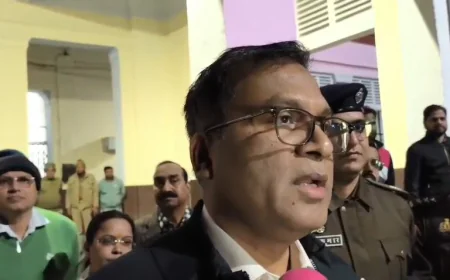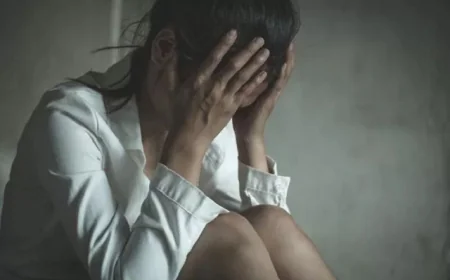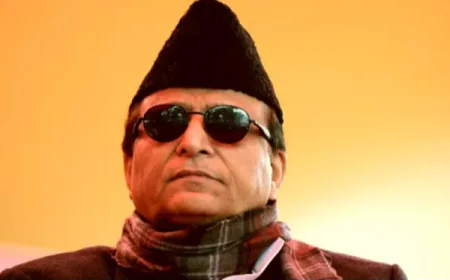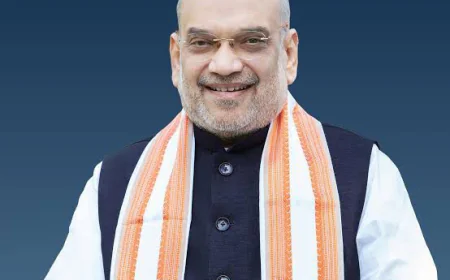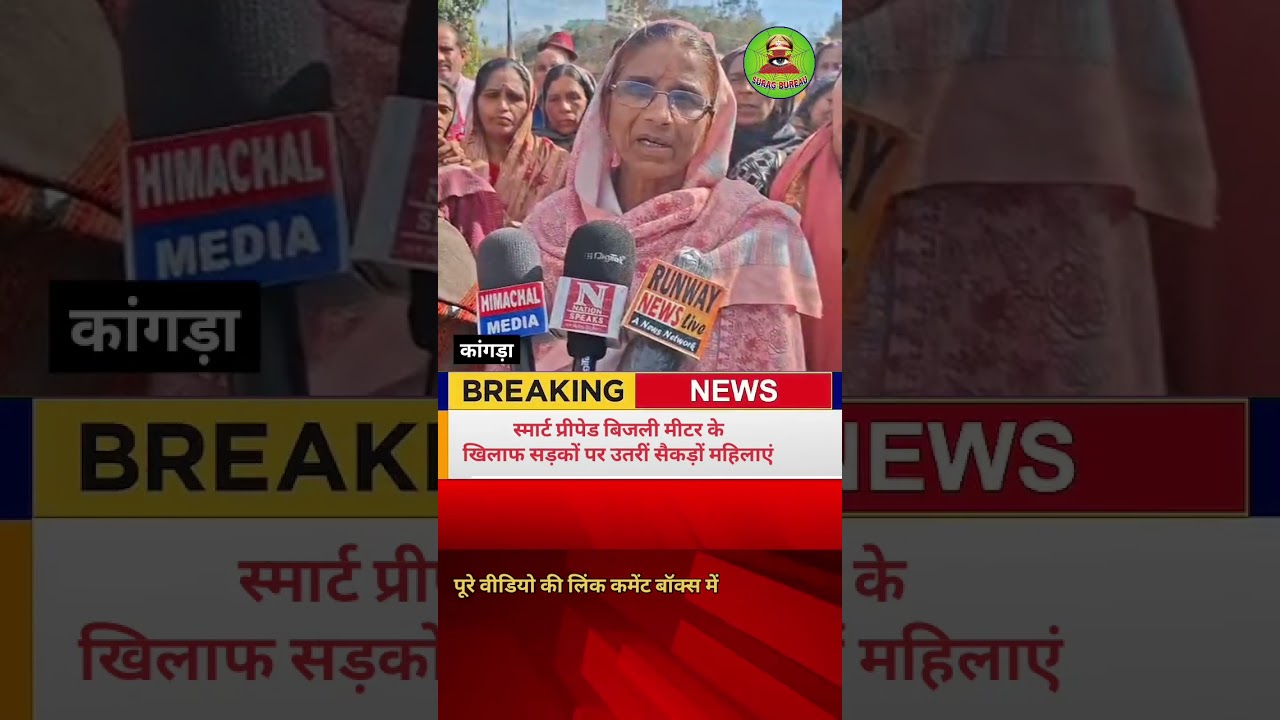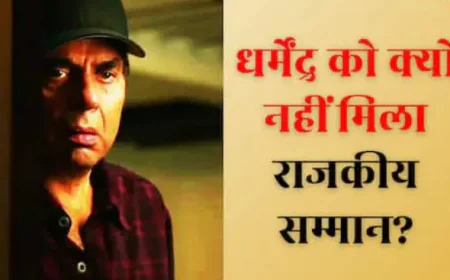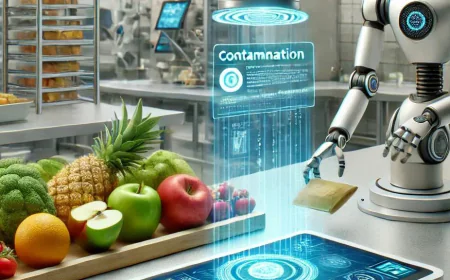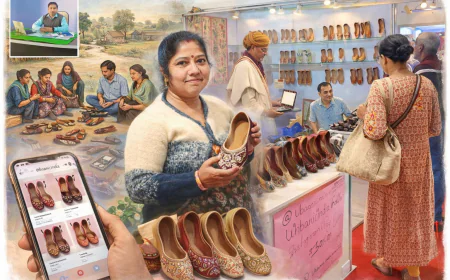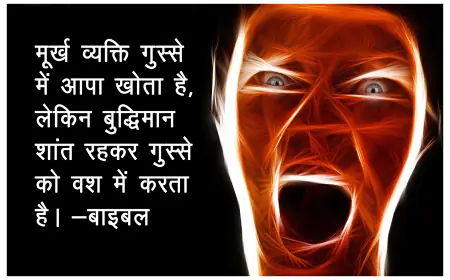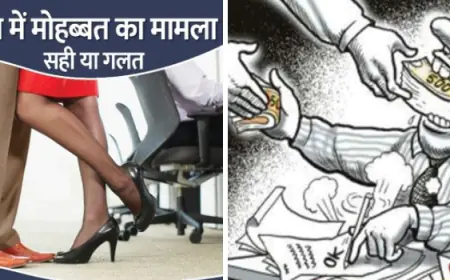सीबीएसई/आईसीएसई/स्टेट बोर्ड 2025: छात्रों को केवल एक महीने में बोर्ड परीक्षा में सफल होने में मदद करने के लिए युक्तियाँ

सीबीएसई/आईसीएसई/स्टेट बोर्ड 2025: छात्रों को केवल एक महीने में बोर्ड परीक्षा में सफल होने में मदद करने के लिए युक्तियाँ
डब्ल्यू बोर्ड परीक्षा समय के खिलाफ एक दौड़ है! यह विस्तृत योजनाओं का समय नहीं है, बल्कि इसके लिए अधिक रणनीतिक मानसिकता की आवश्यकता है, और चरण-वार दृष्टिकोण सभी अंतर ला सकता है चरण 1: एक मजबूत रणनीति बनाना 1. एक यथार्थवादी अध्ययन कार्यक्रम बनाएं अपने दिन की योजना एक स्पष्ट कार्यक्रम के साथ बनाएं जिसमें सभी विषयों के लिए समय आवंटित हो। कमजोर क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दें लेकिन मजबूत विषयों को नजरअंदाज न करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास बर्नआउट से बचने के लिए पर्याप्त ब्रेक हों।
2. परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को समझें आप कहां उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं और कौन से क्षेत्र चुनौती पेश कर सकते हैं, इसकी पहचान करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न की गहन समीक्षा करें। प्रश्नों और समय प्रबंधन से परिचित होने के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। 3. मूल अवधारणाओं में महारत हासिल करें केवल तथ्यों को याद रखने के बजाय मूल अवधारणाओं की गहरी समझ विकसित करें। योग्यता-आधारित प्रश्नों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सीखने को आसान बनाने के लिए निमोनिक्स और विजुअल एड्स जैसे माइंड मैप और फ्लैशकार्ड जैसे अंकी जैसे उपकरणों का उपयोग करें। 4. सक्रिय पुनरीक्षण तकनीकों को शामिल करें सक्रिय पुनरीक्षण आपकी स्मृति में अवधारणाओं को मजबूत करता है। स्व-प्रश्नोत्तरी जैसी तकनीकों का उपयोग करें विषयों को अपने शब्दों में सारांशित करें या बेहतर समझ के लिए किसी और को पढ़ाएं। 5. स्वस्थ और हाइड्रेटेड रहें बर्नआउट को रोकने के लिए पोमोडोरो तकनीक जैसी विधियों का उपयोग करके छोटे, नियमित ब्रेक लेना याद रखें। सुनिश्चित करें कि आप नियमित जलयोजन के साथ स्वस्थ आहार का पालन करें और अपने दिमाग को तेज रखने के लिए कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें। चरण 2: शोधन और पॉलिशिंग (अंतिम 1 महीना)
6. उच्च स्कोरिंग क्षेत्रों पर ध्यान दें वेटेज के आधार पर महत्वपूर्ण अध्यायों को प्राथमिकता दें। ये आपके स्कोर को बढ़ा सकते हैं इसलिए इनमें महारत हासिल करने के लिए समर्पित समय आवंटित करें। 7. परीक्षा स्थितियों का अनुकरण करें मॉक टेस्ट आपको वास्तविक परीक्षा के दबाव के अनुरूप ढलने और अपना समय प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करते हैं। सप्ताह में दो बार समयबद्ध परिस्थितियों में मॉक परीक्षा दें। 8. एक गलती ट्रैकर बनाए रखें अभ्यास परीक्षणों के दौरान की गई गलतियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक जर्नल रखें। अपने शिक्षक के साथ इनकी समीक्षा करें और मुख्य परीक्षा में इन्हें दोहराने से बचने के लिए मॉक टेस्ट दोबारा दें। 9. समय निकालना - किसी ऐसी गतिविधि/शौक/खेल के लिए जिसका आप वास्तव में आनंद लेते हैं (दिन में कम से कम 30-45 मिनट के लिए) चरण 3: फ़ाइन-ट्यूनिंग (अंतिम 2 सप्ताह)
10. अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ डालने से बचें यह थोड़ा धीमा होने का समय है। नई सीख सीमित रखें और जो आप पहले से जानते हैं उसे दोहराने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है और तनाव कम होता है। इस समय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप महत्वपूर्ण विवरण बनाए रखते हैं, संक्षिप्त नोट्स/सारांशों पर ध्यान केंद्रित करें। बोर्ड परीक्षाएँ कठिन लग सकती हैं, लेकिन एक स्पष्ट योजना और निरंतर प्रयास के साथ, छात्र उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं और अपनी अपेक्षाओं को पार कर सकते हैं। याद रखें, ये दो महीने शक्तियों को अधिकतम करने, कमजोरियों को दूर करने और स्वस्थ मानसिकता बनाए रखने के बारे में हैं।
■ विवाह संस्कार के समय पारिवारिक, सामाजिक समरसता, आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाता है
अगर पंजाब में शादी की रस्मों और रीति-रिवाजों की बात करें तो 1965-70 से लेकर 1992 तक शादी के महीने कुछ अलग हुआ करते थे। उस समय पारिवारिक समानता, सामाजिक समरसता, परिवारों की दीर्घकालिक मित्रता, उनकी जाति समुदाय, समान रीति-रिवाज, सामाजिक और आर्थिक स्थिति आदि को ध्यान में रखा जाता था। उस समय लड़का/लड़की एक-दूसरे को जानते थे और एक-दूसरे को दूर से भी नहीं देखते थे। दो अनजान लोगों ने मिलकर एक मजबूत और स्थायी बंधन बना लिया।रचना करते थे समय बदलने के साथ, नब्बे के दशक में लड़का/लड़की दिखने का चलन शुरू हुआ, लेकिन तब भी परिवार ही प्रमुख था, चाहे लड़की कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसे दिखने की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था। समय फिर बदला और लड़कियों के लिए शिक्षा की नई दरें खुलने लगीं आजकल पारिवारिक पृष्ठभूमि का विचार लगभग शून्य है।
अधिकांश युवा अपना जीवनसाथी अपने अध्ययन स्थल या कार्यस्थल पर सहकर्मियों में से चुनते हैं। इसमें अधिकांश शिक्षा एवं विचार हैंसमानता जैसे कारण प्रमुख हैं. नए और अपरिचित रीति-रिवाजों से जुड़ना रुचि का विषय रहा होगा। इसके अलावा, युवा पीढ़ी वर्तमान में बिना शादी के एक-दूसरे के साथ रह रही है। जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है भारतीय संस्कृति इसे मान्यता नहीं देती है। दूसरी ओर, आज पश्चिमी देशों के लोगों ने समाज को बदलने की जिम्मेदारी ले ली है और अब समाज पुरुष और महिला के बजाय पुरुष और महिला के बीच विवाह की ओर बढ़ रहा है। यह एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। बेशक, भारतीय संस्कृति इसकी इजाज़त नहीं देती, लेकिन अदालतें इसकी इजाज़त देती हैंमें हैं अत: भारतीय संस्कृति के अनुसार रीति-रिवाज वैसे ही निभाए जाते हैं, बेशक आज वैसी भावना नहीं है। रोकें/आदेश दें रोका शब्द आज की पीढ़ी के लिए एक नया शब्द है।
पुराने समय में विवाह आमतौर पर मध्यस्थों द्वारा संपन्न होते थे और यदि दोनों पक्ष सहमत होते थे, तो पूरी पंचायत की उपस्थिति में ही विवाह रोका जाता था। लड़के को शगुन देकर रोका जाता है. प्रसाद यह शादी में लड़की के परिवार द्वारा निभाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण रस्म है. चूड़ा आमतौर पर लाल रंग का होता है लेकिन कई लोग सफेद रंग का चूड़ा भी पहनते हैं जिसे शादी के बाद डेढ़ महीने, डेढ़ साल तक भी नहीं बढ़ाया जाता है जिसके कारण यह परिवारों के भावनात्मक बंधन का भी प्रतीक है। लेकिन आजकल टीवी और फिल्मों की वजह से यह खर्च और प्रदर्शन का जरिया बन गया है। जागो जागो समारोह विवाह में एक महत्वपूर्ण समारोह है, आमतौर पर इस समारोह में मायका परिवार शामिल होता है। पहले दौर में जागो का उद्देश्य गांव में विवाह का संदेश देना थाअपने ही समुदाय के लोग हँसते थे और मज़ाक उड़ाते थे। जागरण में शामिल महिलाएँ बाहर के लोगों के बिस्तर धोती थीं।
उस समय कोई नाराज नहीं होता था, लेकिन आज जागो की जगह डीजे ने ले ली है, इस मौके पर ननके के परिवार के सदस्य बोल-बोल कर छज तोड़ते हैं . शादी के समय दूल्हे को अकेला नहीं छोड़ा जाता, दूल्हा कम बोलता है, अगर उसे किसी चीज की जरूरत होती है तो वह सरवले से कह देता है, लेकिन कभी-कभी इसमें छोटा बच्चा भी बना दिया जाता है।उनका सबसे करीबी भाई या मित्र हुआ करता था, जो उनके साथी के रूप में सभी कार्य संभालते थे। नौकर का काम या कर्तव्य मौज-मस्ती के काम या मुलाकातों तक ही सीमित था। श्रेय बांधना सिहर रस्म दूल्हे की सुरक्षा और आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में की जाती है। जैसा कि कहा जाता है कि बहनें हमेशा भाई की लंबी उम्र और खुशी के लिए प्रार्थना करती हैं, इसलिए सिहर रस्म भी बहनों द्वारा की जाती है सभी बहनों को उपहार या शगुन दिया जाता था। इसका दूसरा कारण यह है कि यह दूल्हे को दूसरों से अलग बनाता हैकी तरह लगता है घोड़े की सवारी कुछ समय पहले, शादी से पहले घोड़े की रस्म निभाई गई थी, सड़क के चौराहे पर दूल्हे ने घास भी काटी और उसके बाद दूल्हे की मां ने दूल्हे से मुलाकात नहीं की बहू आ गई।
आज घोड़ों की जगह कारों और सजी-धजी गाड़ियों ने ले ली है। बोलने/गाने का श्रेय यह रस्म शादी से एक दिन पहले घोड़ी के समय निभाई जाती थी। कभी-कभी यह गाना कोई प्रमाणित गायक भी गाता था। लेकिन धीरे-धीरे यह प्रथा भी पूरी तरह बंद हो गई। यह अनुष्ठान मंगलकामना के लिए है। यहदूल्हे की प्रशंसा की जाती है. भ्रमण/आनंद गतिविधियाँ फेरा या आनंद कार्य के साथ विवाह की रस्म पूरी होती है। फेरा और आनंद कार्य के बाद ही विवाह को सामाजिक और कानूनी मान्यता मिलती है। फेरा के दौरान पति-पत्नी अग्नि की परिक्रमा करते हुए सात वचन लेते हैं। सिख पंथ में विवाह आनंद कर्ज के अनुसार किया जाता है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में लावा का पाठ किया जाता है। भेंट करना विवाह में जब कोई लड़का अपने ससुर के घर शादी के लिए पहुंचता है तो सबसे पहले मिलन समारोह आयोजित किया जाता है। इस समारोह का उद्देश्य रिश्तेदारों के लड़के के सम्मान से संबंधित होता हैऔर लड़की को ये नए रिश्ते मिलते हैं।
इस समारोह में दादा/नाना/ताया/चाचा/मामा/फुफड़/जीजा/भाई को भी शामिल किया जाता है हार. वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं. यह रिश्ते को मजबूत करने का एक प्रतीकात्मक समारोह है। शिक्षा बोल रही है प्रदर्शन के बाद लड़की की बहन या उसकी सहेली भाषण देती है। समय के अनुसार कुछ बुद्धिजीवियों ने यह कहकर शिक्षा कहना बंद कर दिया कि गुरु रामदास जी द्वारा दी गई शिक्षा के बाद लावा के रूप में कुछशिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है. अब ये रस्म बंद हो गई है. भुगतान बंद पहले के समय में जब बारात शादी के बाद खाना खाने बैठती थी तो लड़की के रिश्तेदार और समुदाय की महिलाएं कुड़हमों को पीटती थीं, जिन्हें सीठन कहा जाता था। आनंद करजा की रस्म के बाद दोनों परिवार खाना खाते हैं उसके बाद एक या दो रस्में और होती हैं और फिर बारी आती है लड़की की शादी की। पानी का छींटा जब पहले पीरियड में लड़के ने श्रेय बांधाजब के घर से दूर चला गया तो उसकी माँ अपने बेटे से तभी मिलती थी जब वह अपनी बहू लेकर आता था और जब तक बेटा बहू नहीं लाता था तब तक माँ पानी नहीं पीती थी और उसकी इच्छा थी कि अब वह वह अपने दामाद से पानी कभी-कभार ही पिएगी।
गाना बजाना इसका संबंध एक लड़के और लड़की के स्वभाव को परखने से है। लेकिन अब ये रस्म ख़त्म होती नज़र आ रही है. दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे के सिर पर वार करने की रस्म निभाते थे। इसके बाद इस रस्म को देवर-भाभी ने भी निभाया. बंधे हुए लड़के/लड़की का गाना खोलने के लिएयह रस्म शादी के अगले दिन निभाई जाती है। गाना बजाने की रस्म भाभी द्वारा करायी जाती है। हल्दी की बुआई एवं रोपण विवाह में निभाई जाने वाली यह महत्वपूर्ण रस्म लड़के और लड़की दोनों से संबंधित होती है। पुराने समय में आज की तरह लड़के/लड़की को ब्यूटी पार्लर नहीं ले जाया जाता था। शरीर की शुद्धि और सौन्दर्यीकरण के लिए घर पर ही विभिन्न देशी साधनों के साथ हल्दी और वत्तन आदि का मिश्रण किया जाता था। एक लड़के और एक लड़की की शादी की रस्म घर की सुहागन महिलाओं द्वारा निभाई गई। लेकिन आजकल यह रस्म केवल औपचारिक रूप से ही की जाती है क्योंकि लड़का और लड़की सुन्दर होते हैंवे पार्लर जाते हैं और तैयार होते हैं। लड़के/लड़की की शादी से कुछ दिन पहले घर में शादी का माहौल बनाने के लिए गाने गाए जाते हैं। लड़के की शादी के समय लड़की की बहनें गोरी गाती हैं जिसमें भाई की वीरता का वर्णन किया जाता है। लड़कियों की शादी के समय सुहाग गाया जाता है और लड़की को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया जाता है। पुराने समय में जब पानी की कमी होती थी और लड़के/लड़की को स्नान कराने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती थी, तो लड़के/लड़की के मामा-मामी या जीजाजी पानी भरने की इस रस्म को निभाते थे। उनके कंधों पर खरोला। सारशुद्ध पानी पाने के लिए समुदाय एक साथ जाता था। शादी से जुड़े गीत गाती महिलाएं शादी का अद्भुत माहौल बना देती थीं। आजकल यह समारोह नाममात्र का है।
■ लचीलेपन को फिर से परिभाषित किया गया: बिना टूटे झुकने की कला
दर्द से बचना तो दूर, लचीलापन हमें इसे आत्म-खोज और नवीनीकरण के उत्प्रेरक के रूप में अपनाना सिखाता है लचीलेपन को अक्सर एक अटल ताकत के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन इसका असली सार लचीलेपन और विकास में निहित है। यह दर्द या प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के बारे में नहीं है बल्कि साहस और उद्देश्य के साथ उनसे निपटना सीखने के बारे में है। लचीलापन हमारे भीतर की फुसफुसाहट है जो कहती है, "आप पुनर्निर्माण कर सकते हैं।" 36 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रिया (बदला हुआ नाम) को ही लें, जिसका जीवन एक अप्रत्याशित छंटनी के बाद अस्त-व्यस्त हो गया। उसने स्वीकार किया, "मुझे लगा कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है - अपना आत्मविश्वास, अपनी पहचान।" उसके पेशेवर तनाव के नीचे वर्षों का आत्म-सम्मान बाहरी मान्यता से बंधा हुआ था। जर्नलिंग और संज्ञानात्मक रीफ़्रेमिंग के माध्यम से, प्रिया को पता चला कि उसकी योग्यता उपलब्धियों से कहीं अधिक है। छंटनी एक अंत नहीं, बल्कि खुद को फिर से परिभाषित करने का एक अवसर बन गई। मनोवैज्ञानिक एन मास्टेन लचीलेपन को "साधारण जादू" कहते हैं, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि यह कोई असाधारण गुण नहीं है बल्कि एक कौशल है जिसे हम सभी विकसित कर सकते हैं। आज की अप्रत्याशित दुनिया में, लचीलापन अब वैकल्पिक नहीं है - यह आवश्यक है।
लचीलेपन के निर्माण खंड लचीलापन वापस लौटने के बारे में नहीं है, बल्कि चुनौतियों से परिवर्तित होकर आगे बढ़ने के बारे में है। इसकी नींव चार प्रमुख तत्वों पर टिकी है: 1. आत्म-विश्वास: जीवन के तूफानों से निपटने की अपनी क्षमता पर विश्वास करना। 2. भावनात्मक चपलता: भावनाओं से प्रभावित हुए बिना उन्हें स्वीकार करना और संसाधित करना। 3. रिलेशनल एंकर: समर्थन और सुरक्षा के लिए सार्थक कनेक्शन पर भरोसा करना। 4. आशापूर्ण यथार्थवाद: बेहतर परिणामों में विश्वास के साथ कठिनाई की स्वीकृति को संतुलित करना। काम के तनाव से परेशान 50 वर्षीय वकील रोहन (बदला हुआ नाम) पर विचार करें। सचेतन श्वास जैसी ग्राउंडिंग तकनीकों ने उन्हें स्पष्टता हासिल करने में मदद की। उन्होंने साझा किया, "इसने मुझे याद दिलाया कि अराजकता में भी, मैं शांति पा सकता हूं।" ये तत्व हर किसी के लिए सुलभ हैं। लचीलापन असाधारण ताकत के बारे में नहीं है; यह लगातार किए गए सामान्य विकल्पों के बारे में है। लचीलेपन के लिए व्यावहारिक उपकरण लचीलापन का निर्माण छोटे, जानबूझकर किए गए कार्यों से शुरू होता है। जर्नलिंग हमें भावनाओं को संसाधित करने और पैटर्न को उजागर करने की अनुमति देती है। "मेरा डर मुझसे क्या सीखना चाहता है?" जैसे संकेत या "मैं इस पल के बारे में अपने युवा स्वंय को क्या बताऊंगा?" चुनौतियों को विकास के अवसरों में बदला जा सकता है। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में स्थापित करती है।
अदिति (बदला हुआ नाम), एक अकेली मां, को एक साधारण अभ्यास में सांत्वना मिली: अपने दिल पर हाथ रखकर और दोहराते हुए, “मैं सुरक्षित हूं। मैं काफी हूँ।” रचनात्मक अभिव्यक्ति, जैसे कला या आंदोलन, उन भावनाओं को मुक्त करने में मदद करती है जिन्हें शब्द नहीं कर सकते। समायरा (बदला हुआ नाम), एक 19 वर्षीय नर्तकी, ने किसी प्रियजन को खोने के बाद दुःख को व्यक्त करने के लिए एक नृत्यकला को कोरियोग्राफ किया। "यह मेरे शरीर के लिए वह कहानी बताने का एक तरीका बन गया जो मैं बोल नहीं सकती थी," उसने प्रतिबिंबित किया। लचीलेपन का उपहार लचीलापन गहराई से मानवीय है। यह फिर से प्रयास करने के छोटे-छोटे निर्णयों, उन कनेक्शनों में पाया जाता है जो हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, और अनिश्चितता में आशा देखने की क्षमता में पाया जाता है। , "जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होते हैं, तो हमें खुद को बदलने की चुनौती दी जाती है।" लचीलापन अटूट होने के बारे में नहीं है - यह बिना टूटे झुकना सीखने और यह विश्वास करने के बारे में है कि, चाहे हम कितनी भी बार गिरें, हम फिर से उठ सकते हैं।
■ राष्ट्रीय शिक्षा नीति और प्रारंभिक शिक्षा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। ये बातें इस तथ्य को ध्यान में रखकर कही जा रही हैं कि अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा। यदि युवाओं को एक बेहतर मानव संसाधन के रूप में तैयार करना है तो शिक्षा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति में अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया गया है। अभी तक यदि विद्यालयी शिक्षा के प्रारूप को देखें तो उसमें रट कर पढ़ लेने वाली पद्धति हावी थी।
एक बच्चे को कितनी चीजें याद हैं यह हमारे समाज में महत्वपूर्ण रहा, बजाय इसके कि वह किसी विषय को लेकर कितनी समझ रखता है। कई बार केवल बचपन ही नहीं, अपितु बड़ी कक्षाओं की पढ़ाई भी केवल परीक्षा पास कर डिग्री ले लेने भर तक सीमित है । इस प्रक्रिया में केवल परीक्षा के समय पढ़कर पास हो जाना भर उद्देश्य है। यदि सामाजिक मान्यता केवल डिग्री भर लेना है तो शिक्षा की गुणवत्ता में कमी का होना स्वाभाविक है। इसलिए नई नीति में रचनात्मक व तार्किक सोच पर विशेष बल देकर केवल रट कर पास होने वाली प्रणाली को बदलने की कोशिश की गई है। इस नए रूप में नैतिकता, मानवीय व संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाने पर बहुत जोर दिया गया है। विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान का भाव और भारतीय मूल्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। विज्ञानियों एवं चिकित्सकों के अनुसार, एक स्वस्थ बच्चे का मस्तिष्क छह वर्ष तक की आयु में लगभग 85 प्रतिशत तक विकसित हो जाता है।
इसलिए आरंभिक छह वर्ष की अवस्था एक बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है जिसमें उसके मानसिक एवं शारीरिक विकास का ध्यान रखा जाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जिस और इस नीति में ध्यान दिया गया है। बच्चों का कम समय में ही शिक्षा को छोड़ देना एक बड़ी समस्या है। छठी- आठवीं तक 91 प्रतिशत, नौवीं दसवीं में 79 और 11वीं-12वीं में केवल 56 प्रतिशत विद्यार्थी ही आगे जा रहे हैं, यह चिंताजनक है। वर्ष 2030 तक माध्यमिक स्तर तक 100 प्रतिशत दर को कायम रखने की बात कही गई है। इस नए पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण है। मातृभाषा पर बल । जहां तक संभव हो आठवीं तक की पढ़ाई भी मातृभाषा में ही हो। यह न केवल सीखने की क्षमता व गति को बढ़ाएगा, अपितु मातृभाषा के संरक्षण एवं संवर्धन का भी एक बड़ा उपाय है। भाषा की शक्ति व बहुभाषिकता को बढ़ाए जाने पर जोर देने से भारत के सांस्कृतिक वैविध्य को भी सुरक्षित किया जा सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारतीय ज्ञान प्रणाली के आधार पर तैयार करने पर बल दिया। गया है। योजनाएं इस पर आधारित हैं, पर सबसे बड़ा सवाल योजनाओं के क्रियान्वयन पर है। प्रारंभिक शिक्षा के खस्ताहाल हो जाने का एक बड़ा कारण आधारभूत ढांचे का अभाव और बड़ी मात्रा में शिक्षकों के पद रिक्त हैं।
कई जगह शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे। इन सब ने सम्मिलित रूप से सरकारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की छवि को धूमिल किया है। मजबूरी में भले लोग अपने बच्चों का वहां नामांकन करा दें, लेकिन सच्चाई यही है कि सक्षम परिवार उधर रुख नहीं करते। इन सबसे निपटना आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यदि इन व्यावहारिक समस्याओं को सुलझा लिया गया तो निकट भविष्य में हम इस दिशा में बेहतर स्थिति में होंगे।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब