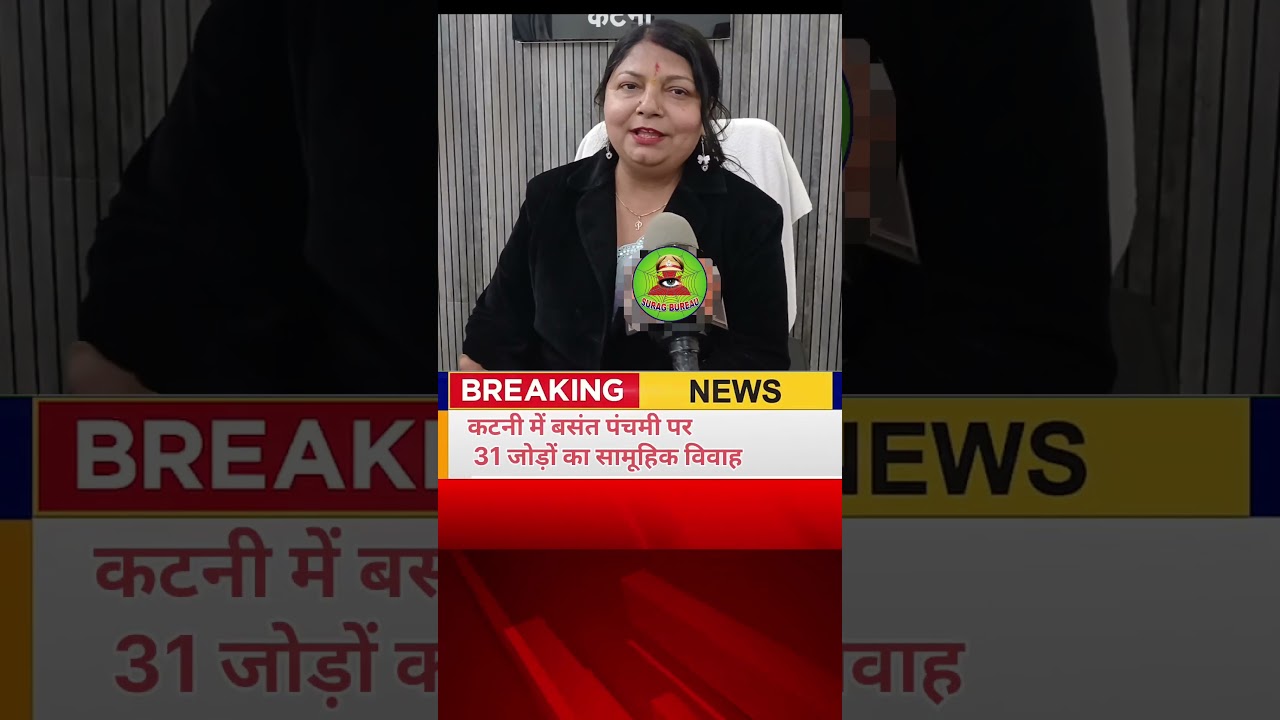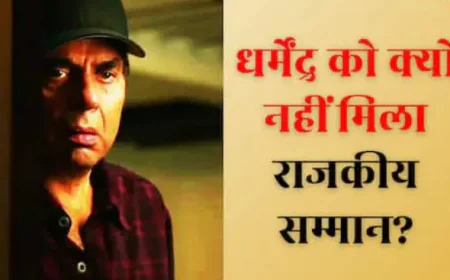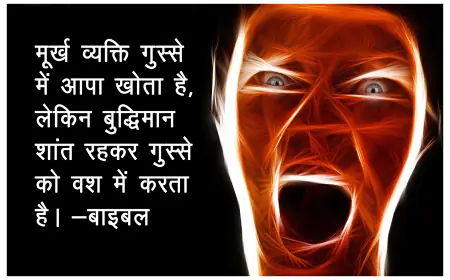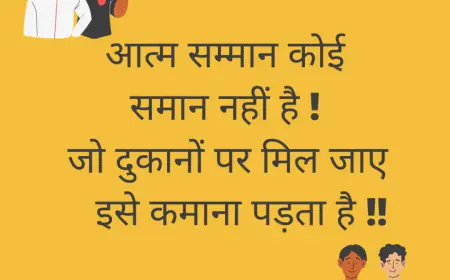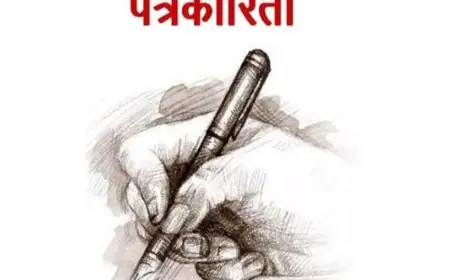फूहड़ शब्दों का ग्लैमर और वर्चुअल समाज की विडंबना

(भाषा के पतन से लोकप्रियता के उत्कर्ष तक की कहानी) फूहड़ शब्दों का ग्लैमर और वर्चुअल समाज की विडंबना
सोशल मीडिया पर अब केवल तस्वीरें या वीडियो नहीं, शब्द भी बिकने लगे हैं। फूहड़ता और अपशब्दों ने अभिव्यक्ति की मर्यादा को पीछे छोड़ दिया है। लाइक, कमेंट और शेयर की भूख ने भाषा को बाजार में बदल दिया है। समाज का वही वर्ग जो संस्कारों की बातें करता है, वही इन पोस्टों पर तालियाँ बजाता है। यह प्रवृत्ति केवल भाषा का पतन नहीं, सोच की गिरावट भी है। सभ्यता की पहली पहचान भाषा होती है—जब भाषा गिरती है, तो समाज भी गिर जाता है।
■ डॉ प्रियंका सौरभ
कुछ समय पहले तक मुझे यह गलतफहमी थी कि सोशल मीडिया पर केवल रील्स और वीडियोज़ में वल्गर या बेहूदा कंटेन्ट ही ज्यादा देखा जाता है। सोचती थी कि शायद यह दृश्य माध्यम का प्रभाव है—जहाँ चमक, शरीर और शोर ही बिकता है। पर हाल के दिनों में कुछ लम्बी पोस्टें पढ़कर भ्रम टूटा। अब केवल दृश्य नहीं, भाषा भी बिकाऊ हो गई है। फूहड़पन अब सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, कलम की नोक पर भी नाच रहा है। इन पोस्टों में विषय तो वही पुराने और ‘ट्रेंडिंग’ हैं—पुरुषों को कोसना, संबंधों में स्त्री की पीड़ा या समाज की संकीर्णता। पर इन सबके बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन विचारों को जिस भाषा में व्यक्त किया जा रहा है, वह भाषा नहीं, गाली का उत्सव लगती है। लाइक्स और कमेंट्स की बरसात होती है, और भीड़ ताली बजाती है—मानो फूहड़ता अब किसी नई ‘साहित्यिक विधा’ का नाम बन चुकी हो। कभी कहा जाता था कि लिखना, दिखने से कठिन होता है। लिखना मतलब सोचना, मनन करना, किसी विषय पर आत्मा से उतरकर बोलना। शब्द कभी भीड़ को लुभाने का नहीं, समाज को सजग करने का माध्यम होते थे।
लेकिन आज इस संतुलन को एक नई भूख ने निगल लिया है—लोकप्रियता की भूख। अब जो सबसे तेज़, सबसे तीखा और सबसे विवादित लिखेगा, वही सबसे ज्यादा देखा जाएगा। ‘क्लिक’ और ‘कमेंट’ की इस दौड़ ने शब्दों की गरिमा को लगभग निचोड़ कर रख दिया है। अब भाषा का अर्थ अभिव्यक्ति नहीं, उत्तेजना रह गया है। और यह प्रवृत्ति केवल अनपढ़ या असंवेदनशील वर्ग तक सीमित नहीं—कई बार वही लोग, जो समाज में सुधार, परिवार में संस्कार और रिश्तों में मधुरता की बातें करते हैं, इन पोस्टों पर टूट पड़ते हैं। वे न केवल इन्हें पढ़ते हैं, बल्कि ‘लाइक’, ‘हार्ट’ और ‘फायर इमोजी’ भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं—जैसे यह कोई सांस्कृतिक आंदोलन हो। यह सवाल सबसे ज्यादा चुभता है—आखिर इस फूहड़ता में आकर्षण क्या है? क्या लोग वास्तव में इन विचारों से सहमत हैं, या बस भीड़ में शामिल हो जाने की मजबूरी है? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सोशल मीडिया ने व्यक्ति को ‘अदृश्य पहचान’ दी है।
अब वह जो कहना, करना या दिखाना असल ज़िंदगी में नहीं कर सकता, उसे वह वर्चुअल दुनिया में निर्भीक होकर कर सकता है। यह आज़ादी धीरे-धीरे अराजकता में बदल गई है। भाषा की मर्यादा, सामाजिक संवेदना और दूसरों की गरिमा—सब पर खुली छूट मिल गई है। किसी का अपमान करना, समूहों को उकसाना, व्यंग्य में विष घोलना—यह सब अब ‘क्रिएटिविटी’ कहलाता है। फूहड़ भाषा को ‘निर्भीक अभिव्यक्ति’ बताया जा रहा है, और सभ्य संवाद को ‘पाखंड’। विचारों की जगह शब्दों का शोर छा गया है। विडंबना यह है कि यही समाज घर में बच्चों को मर्यादा, संस्कार और आदर का पाठ पढ़ाता है, मगर वर्चुअल मंच पर वही लोग अपशब्दों की पोस्ट पर हंसते हुए इमोजी भेजते हैं। यानी हमारी वास्तविक और वर्चुअल नैतिकता में ज़मीन-आसमान का अंतर है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स ने हमें संवाद का अवसर दिया था, पर हम उसे विवाद का अखाड़ा बना बैठे। जहाँ पहले विचारों की टकराहट होती थी, वहाँ अब शब्दों की लाठियाँ चलती हैं। यह प्रवृत्ति केवल भाषा की समस्या नहीं, सामाजिक संस्कृति के क्षरण का संकेत है। क्योंकि जब शब्द दूषित होते हैं, तो विचार भी विकृत हो जाते हैं। और जब विचार विकृत होते हैं, तो समाज में असहिष्णुता पनपती है।
आज यही हो रहा है—हर वर्ग अपने पक्ष को ‘एकमात्र सत्य’ मानने लगा है, और जो असहमत है, उसके लिए अपशब्द तैयार रखे हैं। कला, चाहे लेखन हो या अभिनय—समाज से संवाद का माध्यम है। लेकिन संवाद और प्रहार में फर्क होता है। जो शब्द किसी की गरिमा को चोट पहुँचाएँ, वे अभिव्यक्ति नहीं, आक्रोश का प्रदर्शन हैं। और जब यह आक्रोश लोकप्रियता के रास्ते का शॉर्टकट बन जाए, तब समाज को आत्ममंथन करना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि हम लोकप्रियता और गरिमा के बीच अंतर समझें। लिखना सिर्फ ‘लोग क्या कहेंगे’ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ‘मैं क्या कहना चाहता हूँ’ के लिए होना चाहिए। सच्चा लेखक भीड़ से नहीं, विवेक से संवाद करता है। लेकिन अफसोस, आज सोशल मीडिया ने साहित्य को मनोरंजन और विचार को व्यापार बना दिया है। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर—केवल एक बटन नहीं, एक नैतिक निर्णय है। जब हम किसी फूहड़ पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम अनजाने में उस प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का एल्गोरिदम तो वही दिखाता है जो अधिक देखा जाता है। इसलिए असभ्य कंटेन्ट तभी बढ़ता है जब हम उसे बढ़ाते हैं। दर्शक अगर जिम्मेदार बन जाएँ, तो निर्माता भी सुधरने को मजबूर होंगे। संवेदनशील और सुसंस्कृत समाज वही होता है जहाँ लोकप्रियता का मापदंड शब्दों की गरिमा हो, न कि शब्दों की उत्तेजना। सोशल मीडिया अब किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का दर्पण है। यहाँ जो लिखा, कहा और साझा किया जा रहा है—वही हमारी सामूहिक सोच बन रहा है। अगर हम चाहते हैं कि समाज में शालीनता और संवेदना बनी रहे, तो हमें वर्चुअल व्यवहार में भी वही अनुशासन अपनाना होगा जो वास्तविक जीवन में अपनाते हैं।
फूहड़ शब्दों की लोकप्रियता अल्पकालिक है, पर उनका प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक। विचारों की ताकत शब्दों की मर्यादा में ही बसती है, न कि उनकी अशालीनता में। इसलिए अब वक्त है कि हम ठहरकर सोचें—क्या हम वाकई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं, या बस असभ्यता की स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं? और अगर जवाब दूसरा है, तो हमें याद रखना चाहिए—सभ्यता की पहली पहचान भाषा होती है, और जब भाषा गिरती है, तो समाज भी गिर जाता है।