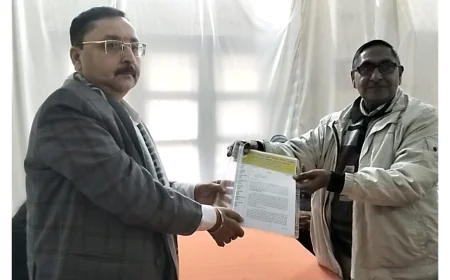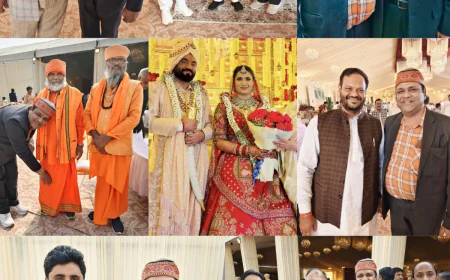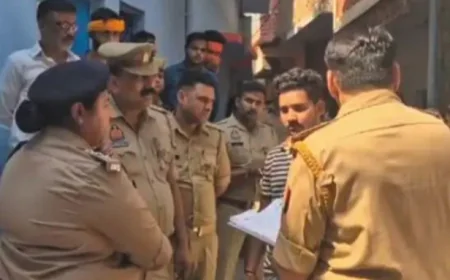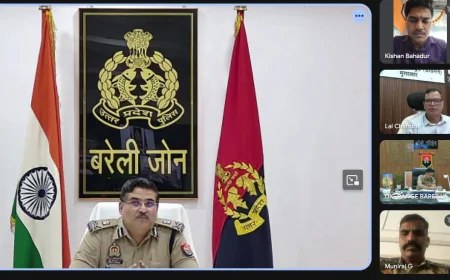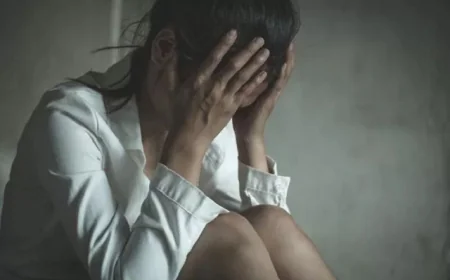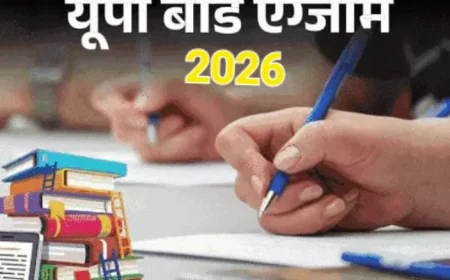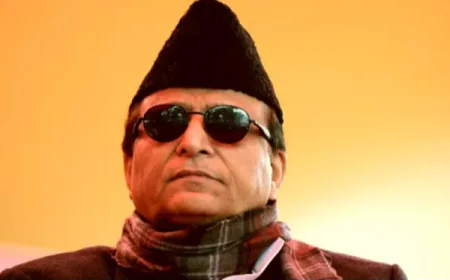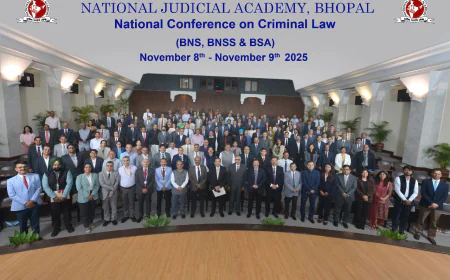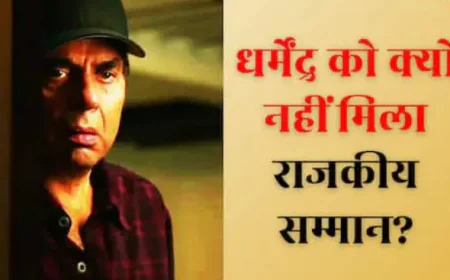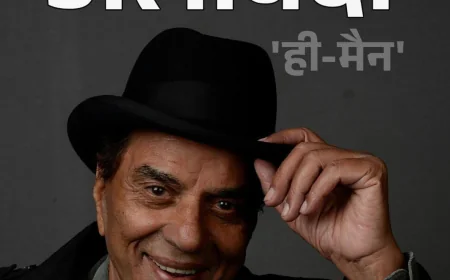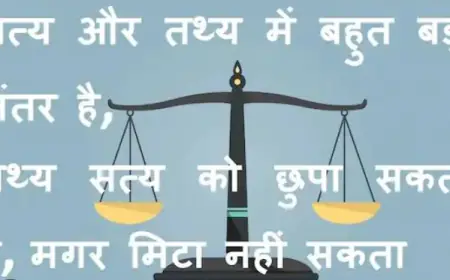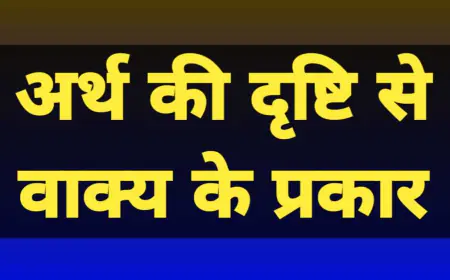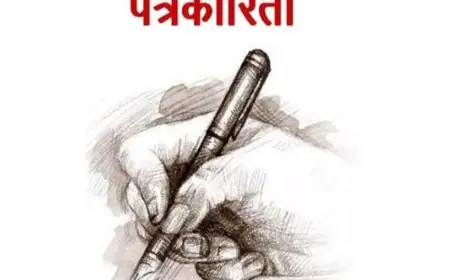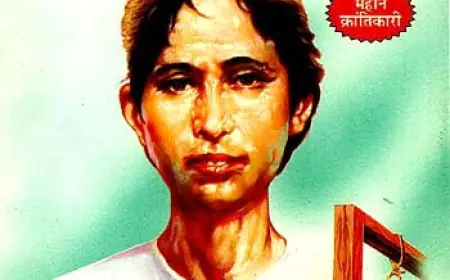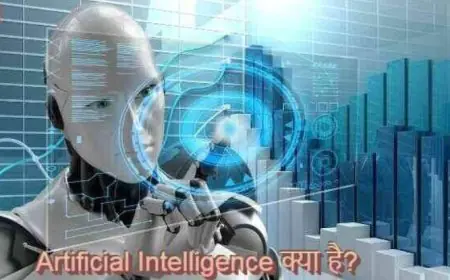देश की भाषिक योजना और हिंदी

देश में आजादी का आंदोलन और हिंदी की स्वीकार्यता दोनों कार्य समांतर चल रहे थे। उस समय अंग्रेजों और अंग्रेजी दोनों के बरक्स हिंदी एक औजार की तरह कार्य कर रही थी। यही कारण था कि बाद में हिंदी स्वतंत्र भारत की भाषिक अभिव्यक्ति बनी। इसके पीछे सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, देशभर के स्वतंत्रता सेनानी इस मत के साथ कार्य कर रहे थे कि देश के लोकतंत्र की भाषा हिंदी होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हिंदी को केंद्रीय स्तर पर राजभाषा का दर्जा दिया गया। हालांकि इसके साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा मिला था, जिसके मूल में अंग्रेजी की विरासत और कुछ छिटपुट हिंदी विरोध था। मगर तब से और आज तक धरातल पर बहुत कुछ बदल चुका है।
वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निकले निष्कर्ष को देखें, तो हिंदी विरोध के गुब्बारे में सुई जमीनी स्तर से चुभाई जा रही है। इसलिए राजनीति में नकारात्मक भाषाई मुद्दों को चुनने का ढर्रा अब बदल देना चाहिए। निराशा की बात है कि ऐसा नहीं रहा और दिनों-दिन इस तरह के मुद्दे उठाए जाने लगे हैं। दरअसल, हिंदी बोलने वालों की जो जनसंख्या वर्ष 2001 में थी, उसमें 2011 तक अखिल भारतीय स्तर पर 25.19 फीसद की वृद्धि हुई, लेकिन यही विस्तार किसी पूर्ण राज्य के रूप में तमिलनाडु में सबसे ऊपर है, जो अब 107.62 फीसद है। आगे यह केरल में 96.80, गोवा में 95.40, गुजरात में 78.53 और कर्नाटक में 49.71 फीसद है। हिंदी- विस्तार का यही आंकड़ा उत्तर प्रदेश 23.86 फीसद, बिहार र में 33.08 और मध्यप्रदेश में 2.15 फीसद है। गौरतलब है कि यह क्षेत्र कथित रूप से हिंदी प्रदेश है और यहां इन दस वर्षों के अंतराल में जनसंख्य के कुल विस्तार वाले फीसद की अवहेलना भी नहीं की जा सकती है। लिहाजा, धारणा से विपरीत हिंदी का मूल विस्तार उन्हीं क्षेत्रों में अधिक हुआ है, जहां जहां परंपरागत रूप हिंदी का प्रभाव नहीं माना गया है और उसमें भी तमिलनाडु सबसे ऊपर है।
गौरतलब है वहां हिंदी को थोपा नहीं गया है, हिंदी- विरोध तो वहां की राजनीति का केंद्रीय तत्त्व है। दरअसल, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज अंतरराज्यीय रोजगार, शिक्षा और मनोरंजन आदि की चाहत में लोगों ने हिंदी सीखी है या इन्हीं कारणों से विस्थापन हुआ है। यदि हिंदी को थोपना होता, तो यह संविधान की मूल मंशा के अनुरूप आज देश की अनिवार्य राजभाषा होती, लेकिन यह सच्चाई किसी से नहीं छिपी है कि स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी सरकारी कामकाज की भाषा स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी ही है। जाहिर है कि हिंदी अपनी जमीन से आगे बढ़ रही है, ऊपर से थोपी नहीं गई है। इस क्रम में हिंदी को लेकर कुछ बने बनाए भ्रम से देश जितना जल्दी जल्दी निकल जाए, तो अच्छा होगा। सर्वप्रथम तो यही कि 'हिंदी पट्टी' जैसी कोई चीज वास्तविक धरातल पर नहीं है। यह सिर्फ ग्रियर्सन (1928) द्वारा प्रस्तावित 'हिंदी बेल्ट' का अनुवाद भर है, जिसे रामविलास शर्मा आदि सरीखे विद्वानों ने हिंदी में जड़भूत कर दिया। जिस बड़े क्षेत्र को ग्रियर्सन ने 'हिंदी बेल्ट' कहा था, उसी में से बिहार को 'बिहारी भाषा' वाला क्षेत्र बताया था। आज अगर इस भाषा को खोजा जाएगा, तो न तो वास्तव में कोई 'बिहारी भाषा' का अस्तित्व है और न ही 'हिंदी बेल्ट' का वास्तव में इस पट्टी में हिंदी से अधिक प्यार पाने वाली दूसरी सैकड़ों भाषाएं हैं और ये सभी लोग हिंदी को उसी व्यावहारिकता के धरातल पर खड़ा होकर स्वीकार करते हैं, जैसे देश के दूसरे हिस्सों के लोग ।
गौरतलब है कि जिस कथित हिंदी पट्टी को हिंदी का ज्ञाता समझ लिया जाता है, वहां हिंदी को अलग से सीखा जाता है। यहां दूर-दराज के क्षेत्रों में आज भी हिंदी उसी तरह है, जैसे बांग्ला, असमिया और गुजराती आदि हो सकती है। यहां तक कि हिंदी का प्रांतीय स्वरूप अपने आप में भिन्न है, जो हिंदी के लोकतांत्रिक चरित्र का सबसे सुंदर उदाहरण है। दूसरी तरफ आज देश में हिंदी 5 नाम पर घोषित सरकारी-गैरसरकारी नौकरियों का अखिल भारतीयकरण तेजी से हुआ है। अब देश को जोड़ने, चलाने और जातीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए संवाहक भाषाओं की जरूरत हमेशा रहेगी और इसमें हिंदी सर्वाधिक उपयोगी है। समाज खैर, लोकतंत्र में किसी को इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए कि वह देश और समाज का एकमेव निर्धारक बन जाए। भाषाएं बहुभाषिक के लोकतंत्र की नियामक होती हैं। अगर अंग्रेजी का शक्तिशाली होना भारतीय रतीय लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है, तो इसकी संभावना हिंदी के साथ भी बनी रहेगी। मगर हिंदी और अंग्रेजी की आपस में हिंदी निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी रही है। इसलिए भी अपने इतिहास से ही हिंदी ने समायोजन पर जोर दिया है, बहिष्कार पर नहीं।
यही कारण है कि इसमें अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी आदि के सैकड़ों शब्द सहज स्वीकृत हैं और यही इसकी शक्ति है, जिससे इसने अपना रास्ता खुद बनाया और आगे भी बनाएगी तथा भारतीय बहुभाषिकता के मूल चरित्र की रक्षा करेगी, जिसमें देश की सभी भाषाएं शामिल हैं।" इसका सबसे उदाहरण आज भोजपुरी को लेकर देखा जा सकता है। हैरत की बात है कि सरकार ने आज तक इसे आठवीं अनुसूची में शामिल करने लायक नहीं समझा, लेकिन गूगल ने इसमें मशीनी अनुवाद को विकसित कर दिया है। इधर डिजिटल मीडिया को लेकर फिक्की द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि वर्ष 2023 में टीवी के दर्शक के रूप में भोजपुरी भाषी न सिर्फ अंग्रेजी, बांग्ला, उड़िया, मलयालम से कई गुना आगे हैं, बल्कि पंजाबी, तेलुगु, मराठी और तमिल के बराबर है। इसका संगीत, फिल्म उद्योग और डिजिटल मीडिया के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रहा है। इसमें देश के सभी भाषा भाषियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। हैं। हिंदी के पास न तो आज शास्त्रीयता के दर्जे की हकदारी है और न ही वह कतार में खड़ी है, लेकिन इसमें एक उदात्त भाव है, जो ईमानदार और शंका से सर्वथा परे है। यह । यह देश की रवानगी की अपनी भाषा है, जो जड़ीभूत न होकर पूर्वाग्रह से मुक्त एक गतिशील भाषा है।
असल में, भारतीय लोक और लोकतंत्र को हिंदी में सबसे सहज ढंग से चरितार्थ किया जा सकता है। अंग्रेजी में न तो तमिलनाडु की आम जनता से संवाद संभव है और न ही कहीं और भाषा एक सामासिक परिसंपत्ति होती है, इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात सोचना भी मूर्खता है। दो अलग-अलग भाषाओं से दो व्यक्ति, दो समाज, दो कमरे बन सकते हैं, जबकि इनमें संवाद के लिए किसी एक भाषा की जरूरत होगी, दो बंद कमरों से निकल कर एक आंगन की जरूरत होगी। हिंदी इसी धरातल पर देश की सभी भाषाओं से सबसे आगे है और रहेगी भी।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब