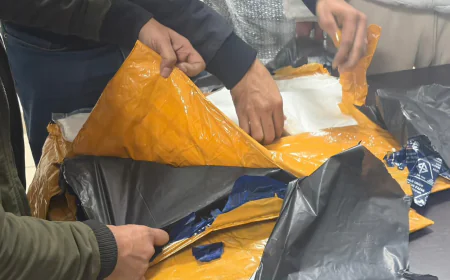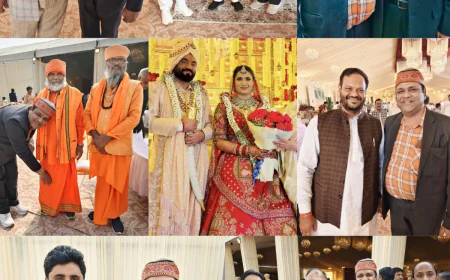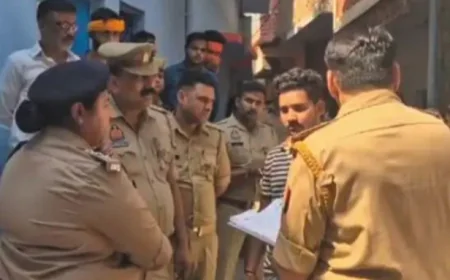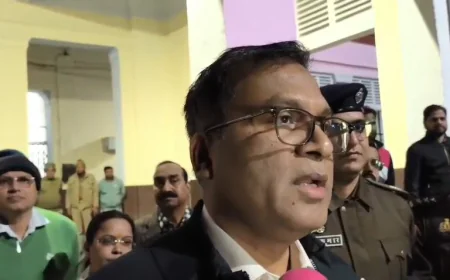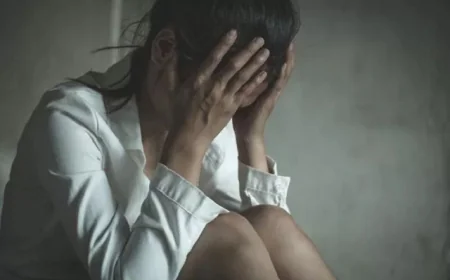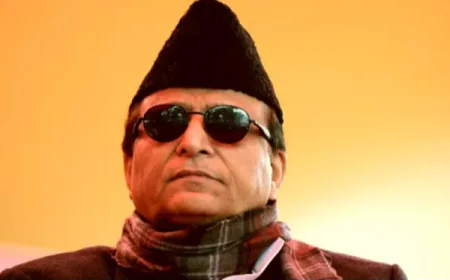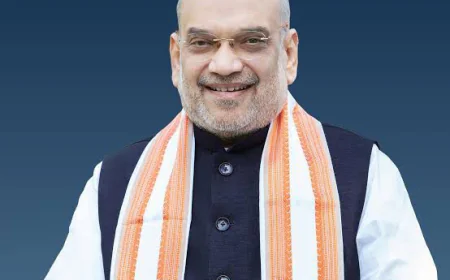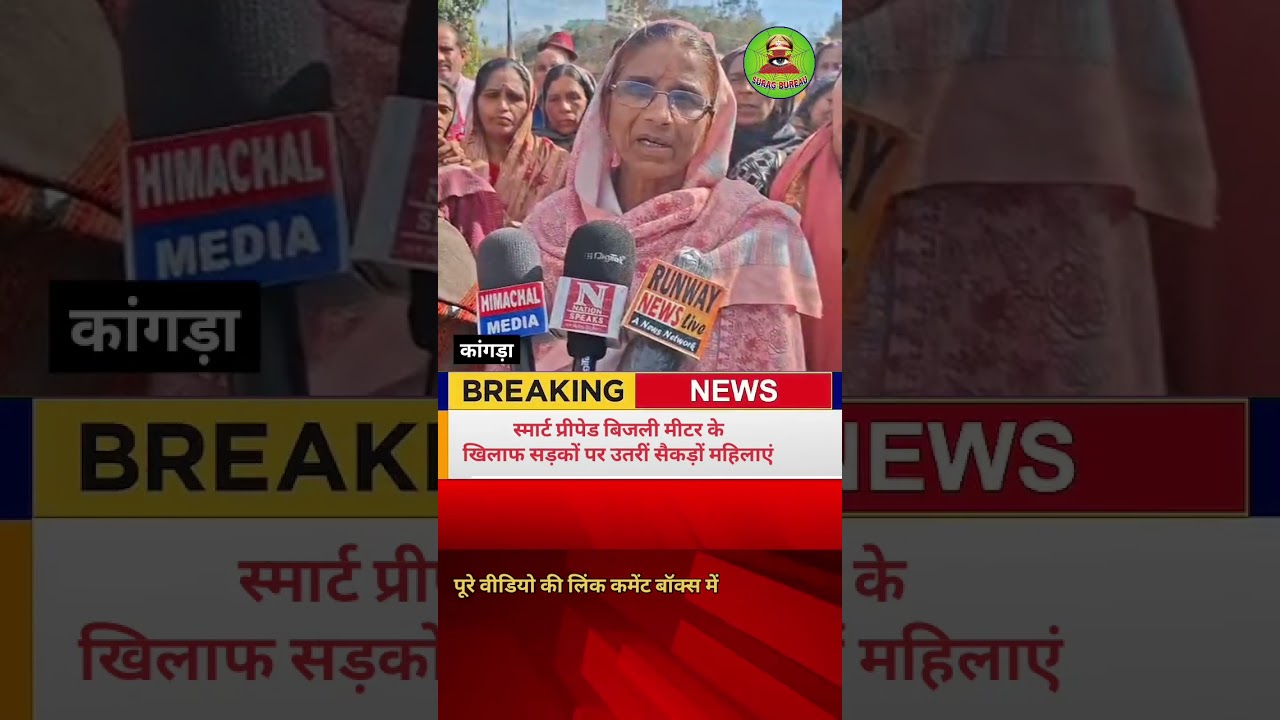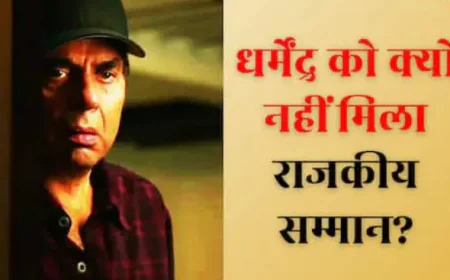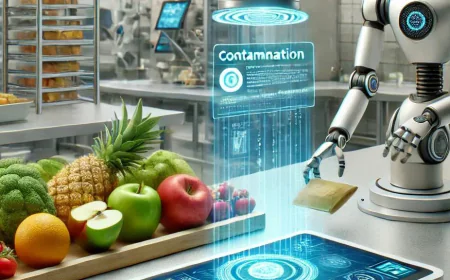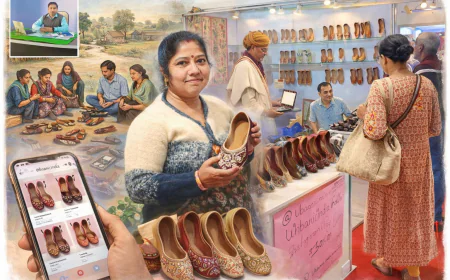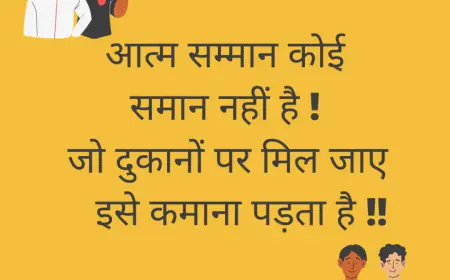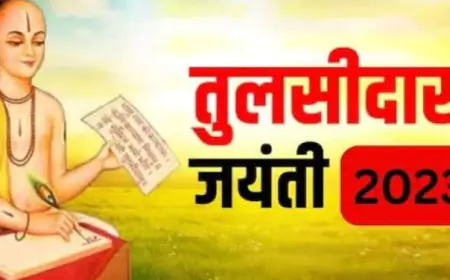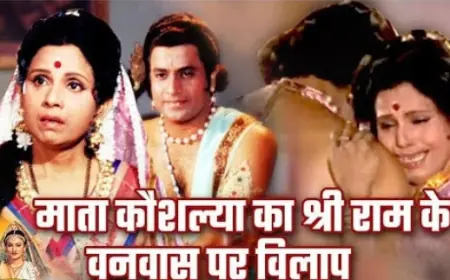विज्ञान में महिलाओं के लिए भविष्य का निर्माण

विज्ञान में महिलाओं के लिए भविष्य का निर्माण
ट्रेलब्लाज़िंग महिला वैज्ञानिकों ने बाधाओं को धता बताते हुए साबित किया कि समावेश केवल निष्पक्षता का मामला नहीं है बल्कि वैज्ञानिक और सामाजिक प्रगति के लिए एक आवश्यकता है 21 वीं शताब्दी में, जहां वैज्ञानिक सफलताएं हमारी दुनिया को आकार देती रहती हैं, विज्ञान में महिलाओं का लगातार अंडरप्रेन्टेशन एक शानदार मुद्दा बना हुआ है। बुनियादी विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक विविध क्षेत्रों में महिलाएं दुनिया भर की कुछ सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में सबसे आगे रही हैं। इन प्रेरक रोल मॉडल के बावजूद, प्रणालीगत बाधाएं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में महिलाओं की भागीदारी को रोकती रहती हैं। यह समय है कि हम इन चुनौतियों का सामना करें और एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां महिलाएं वास्तव में विज्ञान में पनप सकें। यदि हम अपनी आधी आबादी को बाहर करते हैं तो हम किस तरह की वैज्ञानिक दुनिया का निर्माण कर रहे हैं?
महिलाओं की पूरी भागीदारी के बिना, हम प्रतिभा, रचनात्मकता और अभिनव समाधानों के एक विशाल पूल तक पहुंच खो देते हैं जो हमारी कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। कई लड़कियों को रूढ़ियों के कारण कम उम्र से विज्ञान का पीछा करने से हतोत्साहित किया जाता है जो इन क्षेत्रों को "अनुपयुक्त" या "बहुत कठिन" के रूप में फ्रेम करते हैं तथाकथित “टपका हुआ पाइपलाइन” हाई स्कूल के रूप में जल्दी के रूप में अपने टोल लेने के लिए शुरू होता है, कम लड़कियों विज्ञान से संबंधित अध्ययन और कॅरिअर के लिए चुनते हैं । यहां तक कि जो लोग इन प्रारंभिक बाधाओं से गुजरते हैं, उनके लिए भी चुनौतियां उच्च शिक्षा और पेशेवर जीवन में बनी रहती हैं। अनुसंधान में महिलाओं को मेंटरशिप की कमी, फंडिंग और काम पर रखने और पदोन्नति में प्रणालीगत पूर्वाग्रहों तक असमान पहुंच का सामना करना पड़ता है। संख्या अपने लिए बोलती है: यूनेस्को की रिपोर्ट है कि विश्व स्तर पर एसटीईएम के केवल 35 प्रतिशत छात्र ही महिलाएं हैं, और नेतृत्व भूमिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व और भी कम है। भारत में, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) इस बात की पुष्टि करता है कि जहां विज्ञान का पीछा करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है, वहीं शीर्ष अनुसंधान पदों और नेतृत्व भूमिकाओं में उनकी उपस्थिति अभी भी निराशाजनक है। इन बाधाओं के बावजूद, कई भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने यथास्थिति को परिभाषित किया है और उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। डॉ। इंदिरा हिंदुजा ने 1986 में भारत के पहले टेस्ट-ट्यूब बेबी को विकसित करके प्रजनन चिकित्सा में क्रांति ला दी और युग्मक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर (GIFT) तकनीक का नेतृत्व किया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) में मुख्य वैज्ञानिक के रूप में डॉ। सौम्या स्वामीनाथन के नेतृत्व ने वैश्विक स्वास्थ्य नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक कल्पना कालाहस्ती ने भारत के विजयी चंद्रयान -3 मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 2023 में प्रकृति के उल्लेखनीय आंकड़ों की सूची में स्थान अर्जित किया। इन ट्रेलब्लेज़र ने न केवल वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं को धक्का दिया, बल्कि विज्ञान में महिलाओं की भावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए सामाजिक बाधाओं को भी तोड़ दिया। क्या इससे समाज को कोई फर्क पड़ता है? जब महिलाएं वैज्ञानिक नवाचार में सबसे आगे होती हैं तो समाज अधिक समावेशी और व्यापक समाधानों से लाभान्वित होता है। मातृ स्वास्थ्य, लिंग-विशिष्ट चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप जैसे क्षेत्र अक्सर उन महिला वैज्ञानिकों के कारण पनपते हैं जो इन चुनौतियों को पहले से समझते हैं। समावेश सिर्फ निष्पक्षता के बारे में नहीं है - यह विज्ञान को समृद्ध करने के बारे में है। तो, हम कैसे आगे बढ़ते हैं? विज्ञान में महिलाओं के लिए भविष्य बनाने के लिए कई मोर्चों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। हमें महिलाओं की उन्नति में बाधा डालने वाली संरचनात्मक बाधाओं को खत्म करना चाहिए, मेंटरशिप कार्यक्रम प्रदान करना चाहिए और समान भर्ती, धन और कैरियर प्रगति के अवसरों को सुनिश्चित करने वाली नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों को लड़कियों को एसटीईएम क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए, जबकि कार्यस्थलों को लचीले कार्य वातावरण की पेशकश करनी चाहिए जो महिलाओं को व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को संतुलित करने की अनुमति देते हैं।
यह इन बाधाओं को फाड़ने और भविष्य बनाने का समय है जहां हर युवा लड़की जो वैज्ञानिक बनने का सपना देखती है, वह बिना सीमाओं के ऐसा कर सकती है। जब महिलाओं को विज्ञान में योगदान करने के समान अवसर दिए जाते हैं, तो हम सभी लाभ प्राप्त करने के लिए खड़े होते हैं - ग्राउंडब्रेकिंग खोजों से लेकर अधिक समावेशी और समृद्ध दुनिया तक। विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्राचार्य शैक्षिक स्तंभकार गली कौर चंद एमएच मलोट पंजाब [2) आयकर ढांचा बनाम आर्थिक विकास विजय गर्ग आगामी वित्तवर्ष के लिए बजट में सबसे अधिक चर्चा आयकर में दी गई छूट के इर्द-गिर्द ही है। कोई दो मत नहीं कि केंद्र सरकार ने इस बार आयकर सीमा में अप्रत्याशित वृद्धि की है। इस संबंध में यह मांग अरसे से हो रही थी। यह एक दबाव भी था। मगर क्या सरकार का यह कदम आने वाले समय में आर्थिक विकास में तेजी लाएगा या इसे ऐसी आर्थिक नीति के तौर पर जाना जाएगा, जिसमें राजनीतिक दृष्टिकोण बड़ा रुख रखता था, यह अभी स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक तौर पर इसमें यह देखने को मिलता है कि आयकर छूट से नागरिकों के पास वित्तीय तरलता में तो बढ़ोतरी होगी और साथ इसके प्रत्यक्ष तौर पर दो फायदे भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेंगे। पहला, व्यक्तियों की क्रय क्षमता बढ़ेगी और दूसरा, उनकी बचत बढ़ेगी। तीसरा । फायदा यह भी हो सकता सकता है कि कुछ व्यक्तियों को इस वित्तीय बचत से अपने ऋण के भुगतान में भी सहायता मिले, जो पिछले कुछ वर्षों से अपने पास कम वित्तीय तरलता से जूझ रहे थे। यानी संभव है कि क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान या मकान बनाने के लिए उनके द्वारा लिए गए वित्तीय ऋणों की ऋणों की मासिक किस्तों के कारण आर्थिक तरलता में हुई कमी को एक सहारा मिले। इस पक्ष पर अगर सिलसिलेवार समझने की कोशिश की जाए, तो कुछ आंकड़ों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा।
आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य विकास की दर को दस फीसद द के आसपास प्रस्तावित किया है और महंगाई को पांच फीसद से कम । कम इससे स्पष्ट है कि जीडीपी की वास्तविक विकास की दर छह से सात फीसद के बीच ही रहने की संभावना है। इसलिए मोटे तौर पर सभी को यह बात समझनी होगी कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर को बनाए रखने के लिए क्रय क्षमता में तेजी रखना सरकार की प्राथमिकता में है। इसके साथ ही तस्वीर का दूसरा पक्ष एक अलग असलियत को रखता है और वह यह बताता है कि भारत में से आयकर देने वालों की संख्या मात्र आठ करोड़ के आसपास है, जो आबादी का मात्र का मात्र पांच फीसद है। इससे पहले आयकर सीमा सात लाख रुपए थी, जिसे सरकार ने इस बार बजट में बढ़ा कर बारह लाख रुपए कर दिया, लेकिन इस आयकर सीमा के अंतर्गत आने वाले करदाता तीन करोड़ या उससे कम ही हैं। यानी तीन करोड़ करदाता जो औसतन 15 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें ही इस कर मुक्त सीमा का फायदा मिलेगा। तो क्या 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले मुल्क में आर्थिक विकास की जिम्मेदारी चाहे क्रय क्षमता बढ़ाने के संदर्भ में हो या आर्थिक बचत के हिसाब से, मुल्क के इस छोटे से तबके पर ध्यान देना तर्कसंगत है? जबकि भारत जीडीपी के हिसाब से चाहे विश्व में पांचवीं अर्थव्यवस्था का मुकाम रखता है, पर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से विश्व में बहुत पीछे है। आयकर सीमा में बढ़ोतरी का प्रावधान वित्तवर्ष 2025- 26 अप्रैल से लागू होगा।
अब इस संदर्भ में यह बात भी समझनी होगी कि आगामी वित्तवर्ष की पहली दो तिमाहियों तक इस प्रावधान के सकारात्मक असर देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि दिवाली तीसरी तिमाही में आती है और भारत में क्रय क्षमता का असली शक्ति प्रदर्शन उसी दौरान होता है। इस बजट के बाद से एक और चर्चा बहुत आम रही है कि आयकर की इस सीमा में बड़ी वृद्धि को मध्यवर्गीय व्यक्ति और उसके परिवार से प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। भारत में मध्यवर्गीय व्यक्ति आबादी के करीबन 60 फीसद से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि आयकर सीमा में बढ़ोतरी का फायदा मात्र तीन करोड़ परिवारों को होने वाला है, जो कुल जनसंख्या दस फीसद हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस करमुक्त सीमा के प्रावधान को पूर्ण रूप से मध्यवर्गीय व्यक्ति के साथ जोड़ना अनुचित है। क्योंकि ये प्रावधान उच्च मध्यवर्गीय व्यक्ति को ही प्रभावित करते हैं। वित्तवर्ष 2017-18 से वर्ष 2024-25 तक वेतन भोगी व्यक्तियों की आय में छह फीसद से अधिक की कमी देखी गई गई है, "जबकि स्वनियोजित रोजगार वाले लाखों व्यक्तियों की आय में नौ फीसद से अधिक की कमी दर्ज की गई है। यहां यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जिन आयकरदाताओं को इस आयकर सीमा में बढ़ोतरी से फायदा होगा, वे कूल बेतेनी भाबका है, जिनके वेतन में पिछले छह- वेतन भोगियों का मात्र 25 फीसद है, बाकी बचा 75 फीसद वह वेतन सात वर्षों में बहुत अधिक वृद्धि दर्ज नहीं हुई है और इसके अलावा महंगाई दर का चार से पांच फीसद के बीच बने रहना तथा खाद्य पदार्थ की महंगाई का आठ फीसद के स्तर पर पहुंचना, उनके लिए अत्यंत कष्टदायक है, क्योंकि जीएसटी की दरों में किसी भी तरह के परिवर्तन की कोई उम्मीद अभी नहीं दिखती है। सरकार ने बजट प्रस्तुत करते समय आयकर सीमा में इतनी बड़ी राहत देकर एक तरह से तकरीबन एक लाख करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान को भी प्रस्तावित किया है। ज्ञात रहे कि तीन-चार वर्ष पहले जब सरकार ने कंपनियों के करों की दर में कमी की थी, तो उसने एक प्रकार से डेढ़ लाख करोड़ का घाटा प्रस्तावित किया था। जबकि वित्तीय नुकसान उससे दोगुना हुआ था। यह समझना भी अत्यंत आवश्यक है कि इस आयकर सीमा में बढ़ोतरी से प्रति व्यक्ति आय और न्यूनतम आयकर की सीमा के बीच का अंतर छह गुना से अधिक हो गया है। क्या यह पक्ष भारत में गरीबों के पैमाने को अत्यंत प्रभावित नहीं करेगा ?
तनहा करणार आर्थिक विषमता को और अधिक गहरा नहीं करेगा ? नब्बे के दशक के आर्थिक सुधारों के समय भारत में प्रति व्यक्ति आय और न्यूनतम आर्थिक सीमा के बीच का अंतर तीन गुना हुआ करता था। अमेरिका में आज यह अंतर दोगुने से भी कम है। ऐसे समय में भारत में इसका छह आने वाले समय में आर्थिक विकास में किस के स्तर पर पहुंचना, गुना अधिक सुविधाजनक होगा, यह अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। फिर भी, इस कदम के बहुत सकारात्मक पक्ष आने वाले समय में ही दिखेंगे। इससे निजी आर्थिक निवेश को मिलेगा। क्योंकि यह व्यक्ति की आर्थिक क्षमता को यकीनन बढ़ाएगा। इसके अलावा लोगों की इससे बढ़ने वाली आर्थिक बचत का फायदा भी आने वाले दिनों में भारतीय पूंजी बाजार, बैंकिंग क्षेत्र, जमीन-जायदाद कारोबार क्षेत्र आदि में देखने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न वैश्विक परिस्थितियों में हो रहे बदलाव के कारण भी भारत के घरेलू बाजार में आर्थिक तरलता में बढ़ोतरी आवश्यक थी, जिसे राजग सरकार ने समय रहते ही भांप लिया और उन अप्रत्याशित वैश्विक कदमों से निपटने के लिए सरकार का एक महत्त्वपूर्ण कदम समझा जा सकता है।
भारतीय छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ अध्ययन स्थल
जब भारतीय छात्र विदेशी शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो वे उच्च गुणवत्ता वाले सीखने और दुनिया भर में सांस्कृतिक अनुभव को सुरक्षित करते हैं। विदेश में पढ़ाई से जुड़े खर्च भारतीय छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। कई देश छात्रों को उचित लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करते हैं। भारतीय छात्रों के लिए सात कम लागत वाले अध्ययन स्थल इस प्रकार उपलब्ध हैं: 1.। जर्मनी सार्वजनिक जर्मन विश्वविद्यालय किसी भी देश के छात्रों को मुफ्त ट्यूशन की पेशकश करते हुए दुनिया भर में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को जर्मन सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में ट्यूशन फीस का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आमतौर पर न्यूनतम प्रशासनिक शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। रहने का खर्च औसत 70,000 रुपये और 80,000 रुपये प्रति माह के बीच, आवास, भोजन, परिवहन और अन्य आवश्यक चीजों को कवर करता है। डीएएडी छात्रवृत्ति कई छात्रवृत्ति के बीच है जो विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2.। मलेशिया प्रमुख अंतरराष्ट्रीय छात्र मलेशिया को अपने अध्ययन गंतव्य के रूप में चुन रहे हैं क्योंकि यह उचित शिक्षा लागत और जीने के लिए मध्यम खर्च प्रदान करता है। स्नातक कार्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस 1.5 लाख रुपये से लेकर 4 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है, जबकि मास्टर कार्यक्रमों की कीमत 4 लाख रुपये से 9 लाख रुपये सालाना के बीच है। इस स्थान पर प्रत्येक माह जीवित रहने का कुल खर्च 40,000 रुपये और 50,000 रुपये के बीच आता है। शिक्षा की भाषा के रूप में संस्कृतियों और अंग्रेजी की विस्तृत श्रृंखला मलेशिया में अध्ययन करने के लिए कई भारतीय छात्रों को आकर्षित करती है। 3। फ्रांस फ्रांस का हर सार्वजनिक संस्थान एक किफायती शिक्षा कार्यक्रम चलाता है। स्नातक के कार्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस प्रति वर्ष लगभग 2.5 लाख रुपये है, जबकि मास्टर के कार्यक्रम 9 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये सालाना तक हैं। शेष क्षेत्रों की तुलना में पेरिस में शहर के स्थान के परिणामों के आधार पर जीवन में असमानता सबसे महंगी है। फ्रांस में अध्ययन करने की अंतर्राष्ट्रीय छात्र अपील बढ़ जाती है क्योंकि फ्रांसीसी संस्थान विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति के कई अवसर प्रदान करते हैं। 4।
नॉर्वे हर कोई, नागरिकता की परवाह किए बिना, नॉर्वे में मुफ्त सार्वजनिक विश्वविद्यालय नामांकन प्राप्त करता है, जो एक ऐसे राष्ट्र के रूप में एक स्थिति बनाए रखता है जो असाधारण जीवन स्तर प्रदान करता है। स्थानीय रहने की लागत को देखते हुए इस देश में आर्थिक खर्च लगभग 1.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच जाता है। भारतीय छात्रों को नॉर्वे आकर्षक लगता है क्योंकि ट्यूशन फीस मौजूद नहीं है, जबकि अंग्रेजी सिखाने वाले कार्यक्रम सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में उपलब्ध हैं। 5.। आयरलैंड भारतीय छात्र अपने गतिशील सांस्कृतिक वातावरण के साथ-साथ उचित ट्यूशन फीस के कारण आयरलैंड को अपने अध्ययन गंतव्य के रूप में चुनते हैं। स्नातक कार्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस INR 6.3 लाख से INR 10 लाख प्रति वर्ष तक है, जबकि मास्टर कार्यक्रमों की लागत INR 12 लाख और INR 25 लाख सालाना के बीच है। इस स्थान पर मासिक रहने का खर्च INR 70,000 और INR 1 लाख वार्षिक के बीच आता है। जो छात्र स्नातक के बाद काम करने के अवसर चाहते हैं, वे अपने अध्ययन के बाद के कार्य कार्यक्रमों के कारण आयरलैंड को एक आकर्षक गंतव्य पाएंगे। 6। पोलैंड भारतीय छात्र तेजी से अपनी शिक्षा के लिए पोलैंड का चयन करते हैं क्योंकि देश सस्ती शैक्षणिक लागतों को एक साथ रहने और बेहतर शैक्षिक गुणवत्ता की सस्ती लागत प्रदान करता है। स्नातक कार्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस 2 लाख रुपये से लेकर 4 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है, जबकि मास्टर कार्यक्रमों की कीमत 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये सालाना के बीच है। इस स्थान पर मासिक खर्च 40000 रुपये से 60000 रुपये के भीतर आता है। देश अधिक छात्रों को आकर्षित करता है क्योंकि यह ऐतिहासिक मूल्य और एक आदर्श केंद्रीय यूरोपीय स्थिति का संयोजन प्रदान करता है।
7.। मेक्सिको मेक्सिको में किफायती जीवन खर्च के साथ संयुक्त कम ट्यूशन की कीमतें भारतीय छात्रों के लिए एक किफायती शैक्षिक वातावरण बनाती हैं जो वहां अध्ययन करना चाहते हैं। स्नातक कार्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस INR 50,000 से INR 2 लाख प्रति वर्ष तक है, जबकि मास्टर कार्यक्रमों की लागत INR 70,000 और INR 2.5 लाख सालाना के बीच है। मेक्सिको में औसत रहने की लागत प्रति माह 40,000 और 70,000 रुपये के बीच है। मैक्सिकन शिक्षण संस्थानों में स्पेनिश बोलने वाली कक्षाओं में भाग लेते समय छात्र अपनी शिक्षा को जीवंत सांस्कृतिक सेटिंग में खोज सकते हैं। निष्कर्ष विदेश में अध्ययन करने की योजना बनाने वाले छात्रों को अपना निर्णय लेते समय ट्यूशन खर्च और बुनियादी रहने की लागत शामिल करने की आवश्यकता है। जो छात्र स्थानीय रीति-रिवाजों के बारे में सीखने के साथ-साथ छात्रवृत्ति के अवसरों की जांच करते हैं, उन्हें विदेश में अधिक संतुष्टिदायक शैक्षिक अनुभव प्राप्त होगा। ये देश कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं, इस प्रकार भारतीय छात्रों को ऋण मुक्त अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अवसरों के लिए उत्कृष्ट विकल्प प्रदान करते हैं।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्राचार्य शैक्षिक स्तंभकार गली कौर चंद एमएचआर मलोट