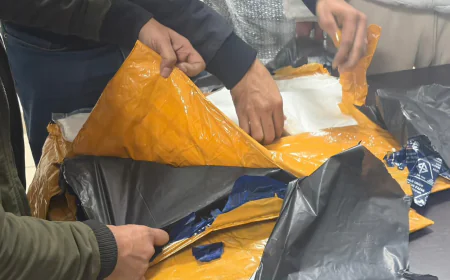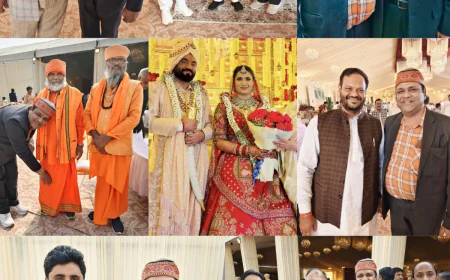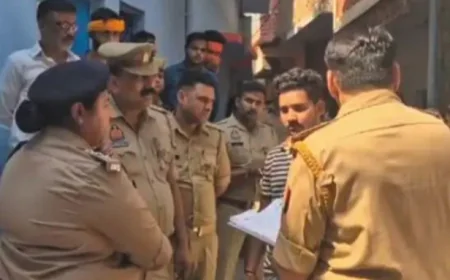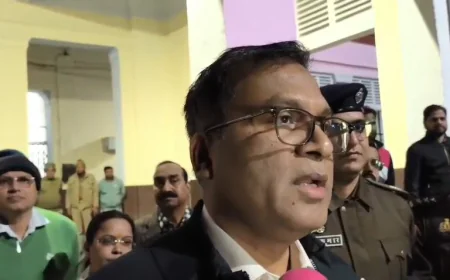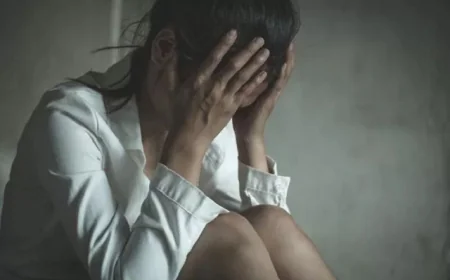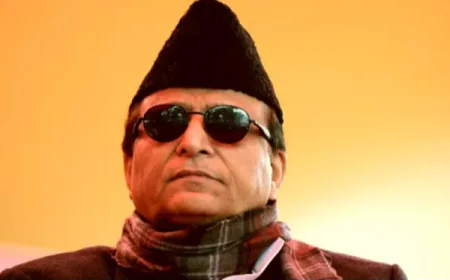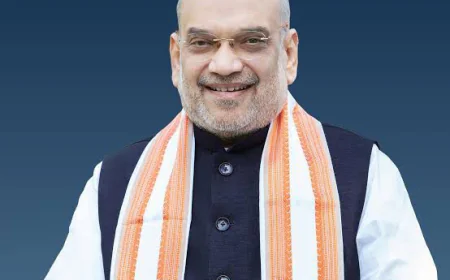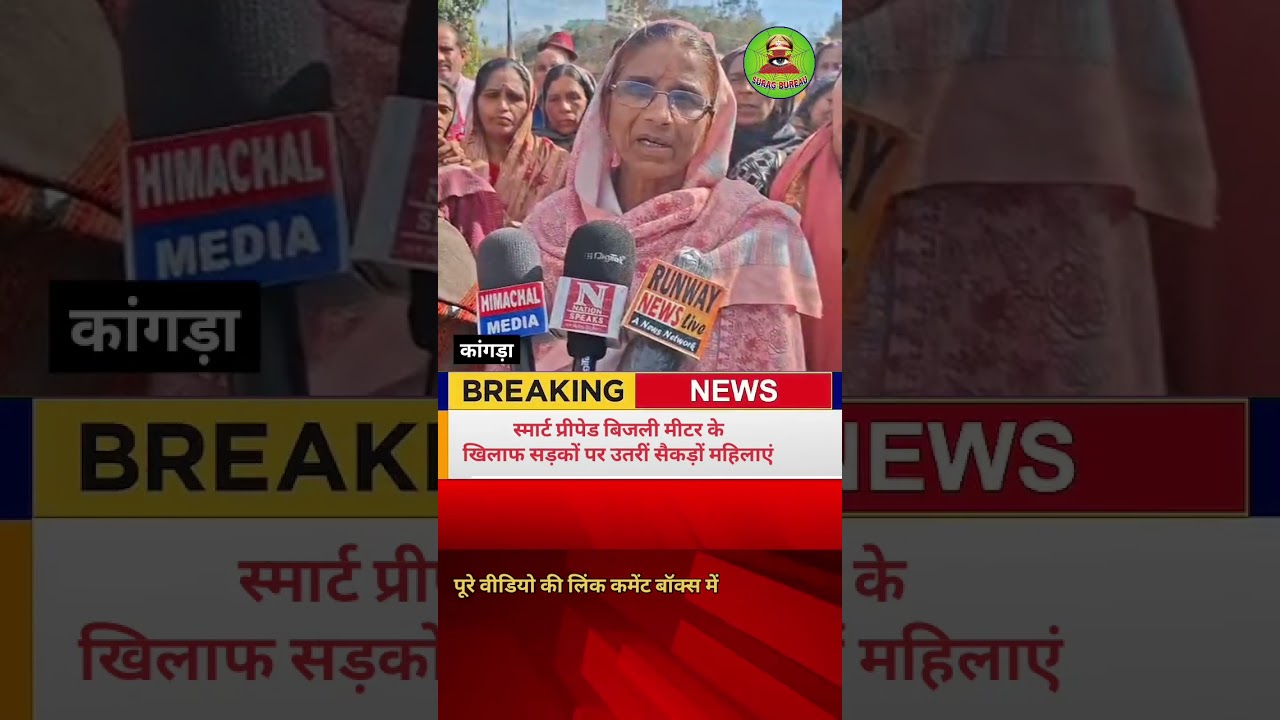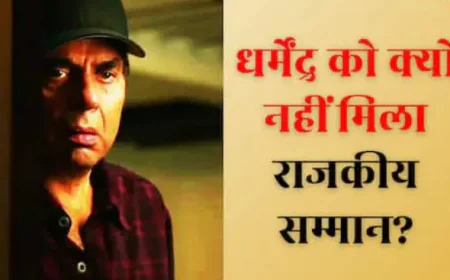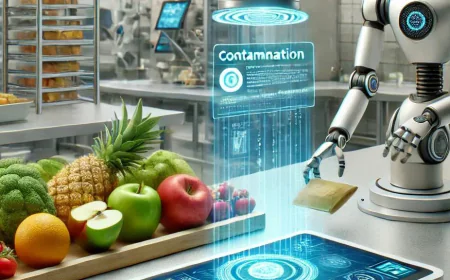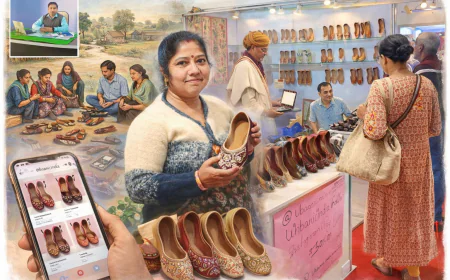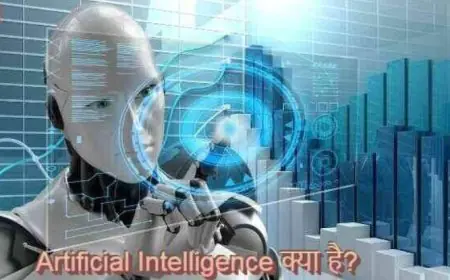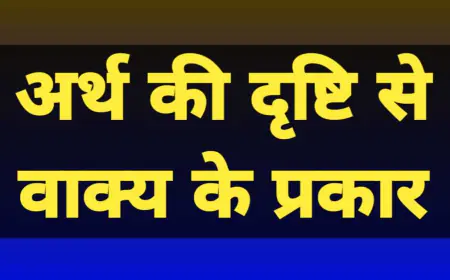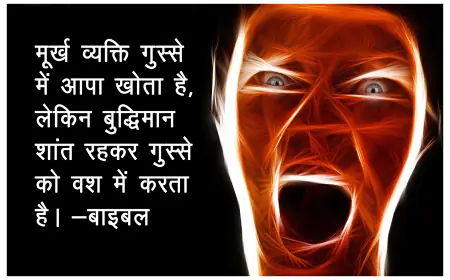राज्यों के लोक सेवा आयोगों में पारदर्शिता का संकट

राज्यों के लोक सेवा आयोगों में पारदर्शिता का संकट
संवैधानिक संस्था होते हुए भी क्यों डगमगा रहा है भरोसा?
राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) भारत की संघीय संरचना में अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं, क्योंकि इन पर लाखों युवाओं के भविष्य और राज्य प्रशासन की गुणवत्ता दोनों निर्भर करते हैं। परंतु हाल के वर्षों में पेपर लीक, अनियमितताओं, देरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्पष्ट प्रक्रियाएँ और त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन जैसे मुद्दों ने इन आयोगों की साख को कमजोर किया है। पारदर्शिता, तकनीक का उपयोग, नियुक्तियों में योग्यता-आधारित मानदंड, नियमित भर्ती कैलेंडर, सुरक्षित परीक्षा अवसंरचना और स्वतंत्र निगरानी तंत्र जैसे सुधार आयोगों को विश्वसनीय बनाने के लिए अनिवार्य हो चुके हैं।
■ डॉ सत्यवान सौरभ
राज्यों के लोक सेवा आयोगों की स्थापना संविधान ने इस उद्देश्य से की थी कि राज्य प्रशासन में प्रतिभा, ईमानदारी और योग्यता को प्राथमिकता मिले। लेकिन विडंबना यह है कि जिन आयोगों पर निष्पक्षता को स्थापित करने की जिम्मेदारी थी, वे स्वयं वर्षों से पारदर्शिता के संकट से जूझ रहे हैं। अनेक राज्यों में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, प्रश्नपत्र त्रुटियाँ, अस्पष्ट आरक्षण गणना और परिणामों की देरी जैसी घटनाओं ने आयोगों के प्रति जनता और युवाओं दोनों का भरोसा डगमगा दिया है। संविधान ने इन संस्थाओं को स्वतंत्र दर्जा दिया, परंतु व्यवहार में राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक सीमाएँ और संस्थागत कमजोरियाँ इनके कार्यों को प्रभावित कर रही हैं। यही कारण है कि आयोगों की प्रक्रियाओं और संरचनाओं की गहन समीक्षा आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। सबसे बड़ी समस्या आयोगों की नियुक्तियों से शुरू होती है। अनेक राज्यों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियाँ योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता के बजाय राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर की जाती हैं।
सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता, आयु, अनुभव या पेशेवर पृष्ठभूमि को लेकर कोई स्पष्ट संवैधानिक मानदंड नहीं है। इसके कारण आयोगों पर पक्षपात व राजनीतिक पक्षधरता के आरोप लगते हैं। इसके विपरीत UPSC में नियुक्तियाँ पेशेवर, अनुभवी और विविध पृष्ठभूमि वाले वरिष्ठ अधिकारियों या शिक्षाविदों के हाथों में रहती हैं, जो उसकी विश्वसनीयता को मजबूत करती हैं। राज्यों में मानव संसाधन नियोजन भी कमजोर कड़ी है। कई बार वर्षों तक अधियाचन नहीं भेजा जाता, पद रिक्त पड़े रहते हैं, आर्थिक कारणों से भर्ती रोक दी जाती है, या अधिसूचनाएँ अचानक जारी होकर फिर रद्द हो जाती हैं। यह अनियमितता पूरे चयन चक्र को बाधित कर देती है। इसके विपरीत केंद्र में 1985 में स्थापित कार्मिक मंत्रालय अधियाचन, सेवा शर्तें और भर्ती चक्र को व्यवस्थित रखता है। राज्यों में ऐसा कोई समर्पित ढाँचा न होने के कारण लोक सेवा आयोगों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। अवसंरचना की कमी भी आयोगों के लिए गंभीर समस्या है। कई राज्यों में सुरक्षित प्रश्नपत्र भंडारण केंद्र, एन्क्रिप्टेड डिजिटल सिस्टम, केंद्रीयकृत परीक्षा केंद्र, आधुनिक स्कैनिंग व्यवस्था और डेटा सुरक्षा तंत्र तक उपलब्ध नहीं हैं।
इस कारण पेपर लीक, ओएमआर गुम होने, मूल्यांकन संबंधी त्रुटियों और तकनीकी विफलताओं जैसी घटनाएँ सामान्य बन गई हैं। उम्मीदवारों में भय व असंतोष का माहौल इसी अव्यवस्था से पैदा होता है। प्रश्नपत्र निर्माण और अनुवाद में त्रुटियाँ व्यापक विवादों को जन्म देती हैं। राज्य आयोग अक्सर स्थानीय शिक्षाविदों के सीमित पैनल पर निर्भर रहते हैं, जिससे प्रश्नों का स्तर, विविधता और सटीकता प्रभावित होती है। कई बार अनुवाद में तथ्यात्मक त्रुटियाँ या अस्पष्टता रहती है, जिससे प्रश्नपत्र रद्द करने तक की नौबत आ जाती है। राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की भागीदारी न होना आयोगों की गुणवत्ता को सीमित रखता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी भी आयोगों की आलोचना का कारण है। कई राज्यों में उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन नहीं होता। अलग-अलग मूल्यांकनकर्ताओं के बीच समरूपता नहीं रहती, मॉडरेशन असमान होता है, और अंकों का निर्धारण स्थिर मानकों पर आधारित नहीं होता। इसके कारण चयन सूची और कट-ऑफ बार-बार विवादों में घिर जाती है, जिससे मामले अदालत तक पहुँचते हैं और भर्ती वर्षों तक लंबित रहती है। आरक्षण गणना की जटिलता भी एक बड़ी चुनौती है। राज्यों में क्षेत्रीय कोटा, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर आरक्षण, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, महिला आरक्षण आदि कई स्तर होते हैं।
मैनुअल गणना में त्रुटियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। छोटी-सी गलती भी पूरी चयन प्रक्रिया को संदिग्ध बना देती है, और कानूनी विवादों के कारण परिणाम अटक जाते हैं। राज्यों के आयोग परीक्षा कैलेंडर का पालन नहीं कर पाते। कुछ राज्यों में पाँच-पाँच वर्षों तक मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं होती। तिथियों का बार-बार बदलना, परिणामों में अत्यधिक देरी, और साक्षात्कार प्रक्रिया का अनिश्चित होना न केवल उम्मीदवारों के करियर को प्रभावित करता है, बल्कि आयु सीमा बढ़ने और मानसिक तनाव जैसी समस्याएँ भी पैदा करता है। इस तरह की अविश्वसनीयता आयोगों की साख पर गहरा प्रश्नचिह्न लगाती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक और दूरगामी सुधारों की आवश्यकता है। सबसे पहले आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति में योग्यता-आधारित मानक अनिवार्य किए जाने चाहिए। न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु, शैक्षणिक योग्यता, प्रशासनिक अनुभव और पेशेवर पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से निर्धारित हों। यह परिवर्तन संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लागू किया जा सकता है। दूसरे, राज्यों में एक पृथक "कार्मिक मंत्रालय" की स्थापना की जानी चाहिए, जो मानव संसाधन योजना, अधियाचन प्रबंधन और भर्ती कैलेंडर को नियंत्रित कर सके। इससे आयोगों को नियमित परीक्षा कार्यक्रम बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह व्यवस्था UPSC की तरह स्थिरता और विश्वसनीयता पैदा करेगी।
तीसरे, आयोगों की परीक्षा प्रक्रिया का संपूर्ण डिजिटलीकरण आवश्यक है। प्रश्नपत्र निर्माण, भंडारण, एन्क्रिप्शन, सीलिंग, डिजिटल मूल्यांकन, ओएमआर स्कैनिंग और परिणाम निर्माण—all तकनीक द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए। इससे पेपर लीक की संभावना कम होगी और मानव त्रुटियाँ भी नियंत्रित होंगी। चौथे, पाठ्यक्रम का नियमित आधुनिकीकरण किया जाए। हर तीन वर्ष में विशेषज्ञ समिति द्वारा पाठ्यक्रम की समीक्षा अनिवार्य हो। आधुनिक प्रशासन, विज्ञान-तकनीक, समसामयिक चुनौतियाँ और नई नीतियाँ पाठ्यक्रम का हिस्सा बनें, ताकि चयनित अधिकारी वर्तमान युग के अनुरूप दक्ष हों। पाँचवें, प्रश्नपत्र निर्माण में राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। अन्य राज्यों के विशेषज्ञ, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और विषय विशेषज्ञों की भागीदारी से प्रश्नपत्रों की गुणवत्ता, संतुलन और विश्वसनीयता बढ़ेगी। अनुवाद में भी प्रमाणित विशेषज्ञों का उपयोग किया जाए ताकि त्रुटियाँ न्यूनतम हों। छठे, मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाना होगा। डिजिटल मूल्यांकन, दो-स्तरीय मॉडरेशन, यूनिफॉर्म स्कोरिंग गाइडलाइन और असंगत अंकों पर स्वतः समीक्षा जैसे उपाय निष्पक्षता को सुनिश्चित करेंगे।
मूल्यांकनकर्ताओं को नियमित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। सातवें, आरक्षण गणना के लिए स्वचालित डिजिटल सॉफ़्टवेयर बनाए जाएँ जिनमें निर्धारित एल्गोरिथ्म त्रुटिरहित गणना करें। इससे विवादों में भारी कमी आएगी। आठवें, राज्य भर में “भर्ती कैलेंडर अधिनियम” लागू होना चाहिए जिसमें प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार और परिणाम की अधिकतम समयसीमा निर्धारित हो। आयोग को वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी चाहिए ताकि जनता को जवाबदेही स्पष्ट हो। नौवें, आयोग के सचिव का पद ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को दिया जाए जिनके पास शैक्षणिक प्रशासन या परीक्षा प्रबंधन का गहन अनुभव हो। इससे परीक्षा लॉजिस्टिक्स, गोपनीयता, सुरक्षा और मूल्यांकन व्यवस्था अधिक पेशेवर होगी। अंत में, उम्मीदवारों की शिकायतों के समाधान के लिए स्वतंत्र डिजिटल ग्रेविएंस पोर्टल बनाया जाए, जिससे उम्मीदवार पारदर्शी तरीके से अपनी समस्या दर्ज कर सकें, स्थिति देख सकें और समयसीमा में समाधान प्राप्त कर सकें। समापन में कहा जा सकता है कि राज्य लोक सेवा आयोगों की मजबूती भारत की प्रशासनिक गुणवत्ता का आधार है। यदि आयोग पारदर्शी, तकनीक-समर्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त और योग्यता-आधारित ढाँचे पर काम करें, तो न केवल युवाओं का विश्वास लौटेगा बल्कि राज्य प्रशासन में दक्ष, ईमानदार और संवेदनशील अधिकारी भी मिलेंगे। सुधारों के बिना आयोगों की साख और देश के भविष्य दोनों पर प्रश्नचिह्न बने रहेंगे।