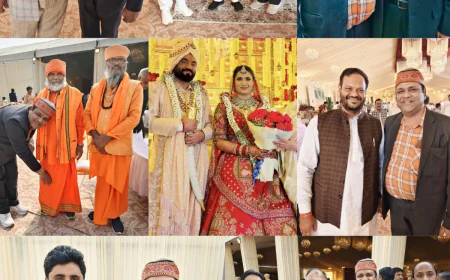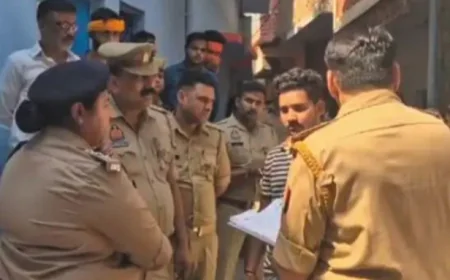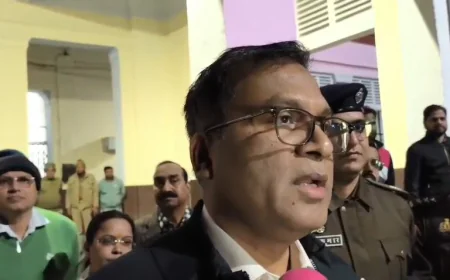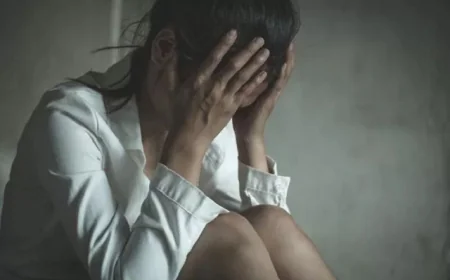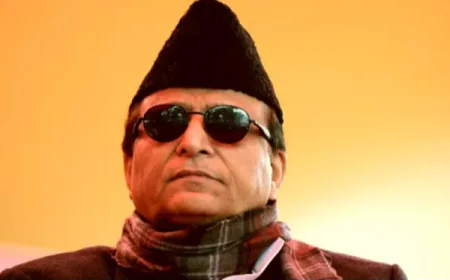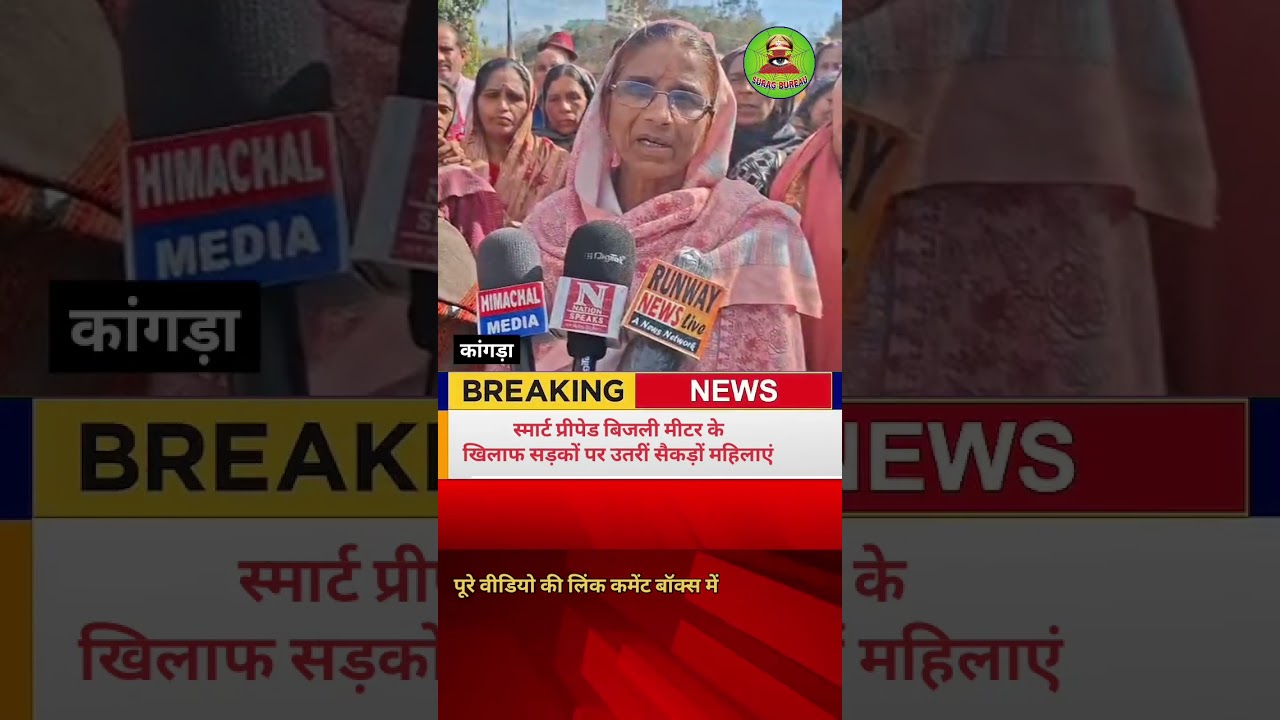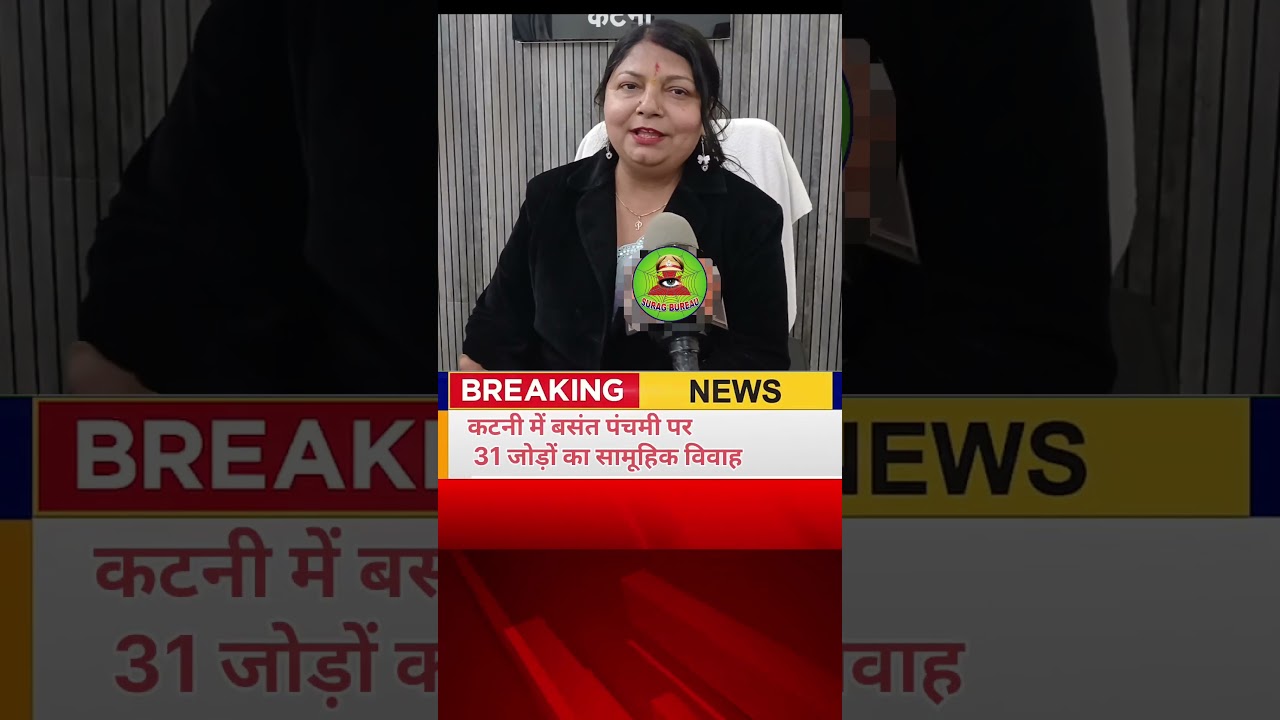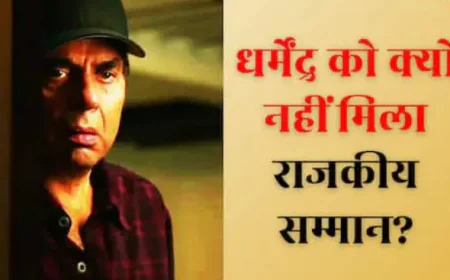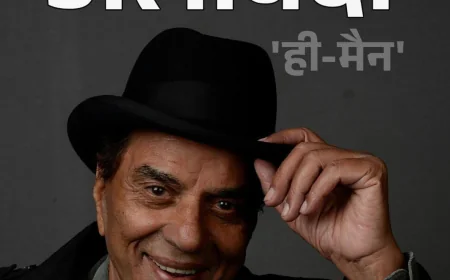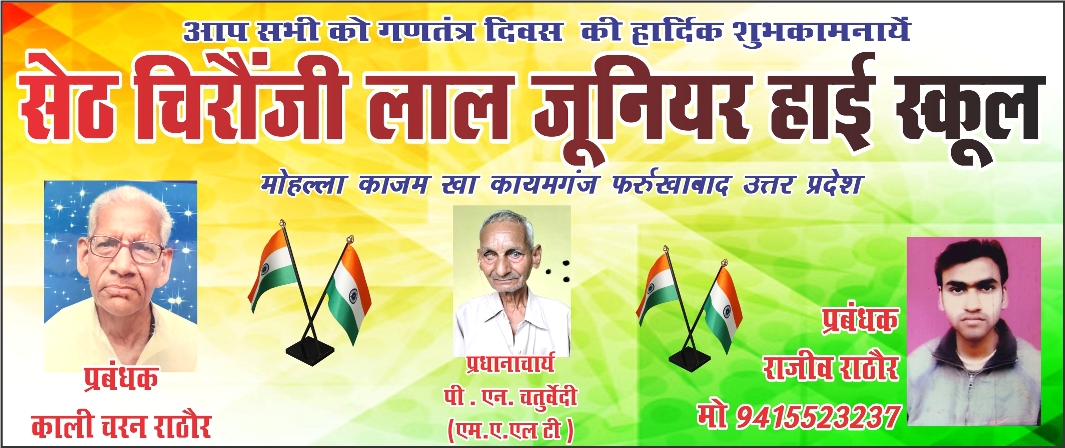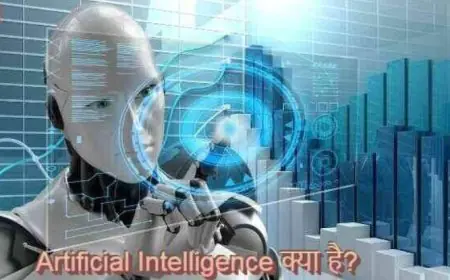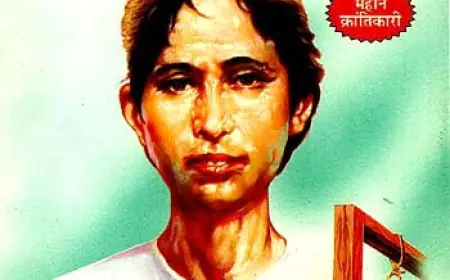भारत में शिक्षा का एक नया पन्ना खुल रहा है

भारत में शिक्षा का एक नया पन्ना खुल रहा है
भारत की शिक्षा प्रणाली में गंभीर कमियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा संबोधित किया गया है। वैश्विक मानकों तक पहुंचने के लिए, इसे अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए भारत शैक्षिक उत्कृष्टता की एक गौरवशाली विरासत का दावा करता है, जो नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन संस्थानों की याद दिलाती है। आज भी, यह दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है, जिसमें लगभग 1.5 मिलियन स्कूल, 40,000 से अधिक कॉलेज और 1,000 से अधिक विश्वविद्यालय शामिल हैं, जो कुल मिलाकर लगभग 300 मिलियन छात्रों को सेवा प्रदान करते हैं। हालाँकि, यह मात्रात्मक लाभ गुणात्मक सफलता में परिवर्तित नहीं हुआ है।
उदाहरण के लिए, जबकि भारत प्राथमिक शिक्षा के लिए 108 प्रतिशत के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) का दावा करता है (यह 100 प्रतिशत से अधिक क्यों है इसके लिए संलग्न ग्राफ़िक की जाँच करें), माध्यमिक शिक्षा के लिए यह लगभग 79 प्रतिशत तक गिर जाता है। इसके विपरीत, चीन प्राथमिक शिक्षा के लिए 100 प्रतिशत और माध्यमिक शिक्षा के लिए 89 प्रतिशत जीईआर बनाए रखता है, जो बेहतर छात्र प्रतिधारण को दर्शाता है। उच्च शिक्षा के लिए भारत का जीईआर और भी निराशाजनक है, जो 27.1 प्रतिशत पर है, यह आंकड़ा चीन का आधा है और अमेरिका के प्रभावशाली 88 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। फ़िनलैंड और दक्षिण कोरिया जैसी अनुकरणीय शिक्षा प्रणालियाँ सभी स्कूल स्तरों पर लगभग 100 प्रतिशत GER हासिल करती हैं। यदि ये आँकड़े शैक्षिक पहुँच में पर्याप्त अंतर को उजागर करते हैं, तो सीखने के परिणामों की गुणवत्ता और भी अधिक चिंताजनक है। शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) से पता चला कि पांचवीं कक्षा के केवल 45 प्रतिशत छात्र दूसरी कक्षा के स्तर पर पढ़ सकते हैं। इसी तरह, 2023 की वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) में पाया गया कि 14-18 आयु वर्ग के एक-चौथाई ग्रामीण छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा में दूसरी कक्षा के स्तर का पाठ धाराप्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं। उच्च शिक्षा में, विस्तारित पारिस्थितिकी तंत्र के बावजूद, कुछ संस्थान वैश्विक रैंकिंग में सम्मानजनक स्थान हासिल कर पाते हैं।
जहां अमेरिका और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों का दबदबा है, वहीं चीनी संस्थान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह असमानता आश्चर्यजनक नहीं है, अनुसंधान उत्पादन में भारत के पिछड़ेपन को देखते हुए, उच्च शिक्षा के भीतर अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) में देश के सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से भी कम निवेश के कारण यह और भी बढ़ गया है। इसके विपरीत, अमेरिका अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटित करता है, और चीन 2 प्रतिशत से अधिक निवेश करता है, जिससे उसके वैश्विक अनुसंधान उत्पादन और नवाचार में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। हालाँकि भारत से शोध प्रकाशनों में वृद्धि हुई है, लेकिन उनका प्रभाव और उद्धरण सूचकांक कम बना हुआ है। कौशल प्रशिक्षण में भी स्थिति उतनी ही परेशान करने वाली है, जहां भारत के कार्यबल का मात्र 4 प्रतिशत ही व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करता है। यह चीन के 24 प्रतिशत और जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड में देखे गए 75 प्रतिशत से बिल्कुल विपरीत है। इसके अलावा, भारतीय स्नातकों की रोजगार योग्यता दर लगभग 48.7 प्रतिशत है, जिससे पता चलता है कि आधे से अधिक स्नातकों में नौकरी बाजार के लिए आवश्यक कौशल का अभाव है। एनईपी दर्ज करें हमारे यहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी 10 से 24 साल के बीच की है। इस जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने और ज्ञान अर्थव्यवस्था में अवसरों को भुनाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास को पुनर्जीवित करना बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का मसौदा तैयार किया गया था।
एनईपी भारतीय शैक्षिक ढांचे में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव करता है, जिसमें 10+2 संरचना को 5+3+3+4 मॉडल के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है जो शैक्षिक चरणों को विकासात्मक चरणों - मूलभूत (आयु 3-8) के साथ संरेखित करता है।प्रारंभिक (उम्र 8-11), मध्य (11-14), और माध्यमिक (14-18)। यह गहन समझ को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम की सामग्री को मुख्य अनिवार्यताओं तक कम करके अनुभवात्मक शिक्षा और आलोचनात्मक सोच पर जोर देता है। नीति का लक्ष्य 2030 तक प्रीस्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100 प्रतिशत जीईआर का लक्ष्य है, जिसमें ड्रॉपआउट को फिर से शामिल करने के लिए विशेष पहल शामिल है। उच्च शिक्षा में, एनईपी अंतर-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़े, बहु-विषयक और अनुसंधान-केंद्रित संस्थानों में परिवर्तन की वकालत करता है, जिसका लक्ष्य हर जिले में कम से कम एक ऐसा संस्थान स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त, नीति संस्थानों के लिए अधिक स्वायत्तता का आह्वान करती है और व्यावहारिक प्रदर्शन के लिए उद्योग के साथ सहयोग बढ़ाने को प्रोत्साहित करती है। नीति का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण से परिचित कराना है। कार्यान्वयन में शैतान हालाँकि, जैसा कि पिछले चार वर्षों से पता चला है, इस व्यापक नीति का राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन चुनौतियों से भरा एक बड़ा काम है। जबकि एनईपी केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया था, इसका सफल कार्यान्वयन काफी हद तक सक्रिय राज्य सहयोग पर निर्भर करता है।
कई विपक्षी शासित राज्यों ने एनईपी के प्रमुख प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर कड़ी आपत्ति जताई है। केंद्र को इन पहलों को लागू करने के लिए सहकारी संघवाद और विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों पर काम करना चाहिए। बजट आवंटन एक और चुनौती है. एनईपी 2020 अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश करता है। हालाँकि, केंद्र और राज्यों द्वारा शिक्षा पर भारत का सार्वजनिक व्यय कभी भी सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा है। इस व्यापक कार्यक्रम को लागू करने के लिए इस फंडिंग अंतर को पाटना महत्वपूर्ण है। कई स्कूल और कॉलेज बुनियादी ढांचे की समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करते हैं। केवल ईंट-और-मोर्टार जोड़ने के बजाय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार करना आवश्यक है। भारत को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप एक विश्व स्तरीय ऑनलाइन शिक्षा मॉडल की आवश्यकता है, जिसमें स्वयं और दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आगे की चुनौती वहां भी बड़ी है; उदाहरण के लिए, भारत में 53 प्रतिशत स्कूलों में कंप्यूटर की कमी है, और 66 प्रतिशत में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी है। जबकि एनईपी अनुसंधान उत्पादन में सुधार पर जोर देती है, न तो केंद्र और न ही राज्यों ने अनुसंधान के लिए धन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग के साथ सहयोग को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एनईपी एक अधिक शिक्षार्थी-केंद्रित संस्कृति की कल्पना करता है, जिसके लिए छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों के बीच मानसिकता में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। इस परिवर्तन में समावेशी शिक्षण और सीखने के तरीकों को अपनाना शामिल है। परिणामस्वरूप, इन मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षकों को नए कौशल में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वैश्विक स्तर पर, छात्रों को भविष्य की मांगों के लिए तैयार करने में एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर आम सहमति बढ़ रही है।
यूनेस्को की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में दुनिया भर में एसटीईएम स्नातकों की संख्या सबसे अधिक है, जिसमें 34 प्रतिशत स्नातक एसटीईएम क्षेत्रों से आते हैं। प्रभावशाली बात यह है कि उनमें से 40 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ हैं। हालाँकि, इनमें से कई स्नातकों के पास भविष्य की नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल का अभाव है। एनईपी छात्रों की आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान कौशल और नवाचार को बढ़ाने के लिए एसटीईएम शिक्षा को पाठ्यक्रम में एकीकृत करने पर जोर देता है। इस कौशल अंतर को संबोधित करने की कुंजी व्यावहारिक सहायता प्रदान करने में निहित हैn सीखने के अनुभव और आधुनिक प्रौद्योगिकी से परिचित होना। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) का अनुमान है कि भारत में कौशल प्रशिक्षण में सुधार से 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में 1 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हो सकता है। कौशल मिशन पिछले महीने केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने कौशल विकास की समस्या को गंभीरता से लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच प्रमुख रोजगार-संबंधी योजनाओं के 'प्रधानमंत्री पैकेज' की घोषणा की, जिसमें 41 मिलियन युवाओं को रोजगार और कौशल प्रदान करने के लिए पांच वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी परिव्यय था। इनमें से दो बड़ी योजनाएं कौशल पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिनमें से सबसे महत्वाकांक्षी योजना पांच वर्षों में 10 मिलियन युवाओं के लिए 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर स्थापित करना है। 21 से 24 वर्ष की आयु के युवा, जो न तो नौकरीपेशा हैं और न ही पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना में 5,000 रुपये का मासिक इंटर्नशिप भत्ता शामिल है; पांच वर्षों में कुल लागत 63,000 करोड़ रुपये है। कौशल पर अन्य प्रमुख पहल हब और स्पोक मॉडल का उपयोग करके 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अपग्रेड करने और कौशल अंतर को दूर करने के लिए उद्योग की जरूरतों के साथ उनकी पाठ्यक्रम सामग्री को संरेखित करने की योजना है। इस योजना में 200 हब और 800 स्पोकन आईटीआई विकसित करना शामिल है, जिसमें पांच वर्षों में कुल 60,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। केंद्र सरकार 30,000 करोड़ रुपये, राज्य सरकारें 20,000 करोड़ रुपये और उद्योग (सीएसआर फंड सहित) 10,000 करोड़ रुपये का योगदान देगा। ये और अन्य पहलें भारत को शिक्षा के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने, देश के विकास और नवाचार को चलाने के लिए कौशल और ज्ञान से सुसज्जित पीढ़ी का पोषण करने का वादा करती हैं।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब