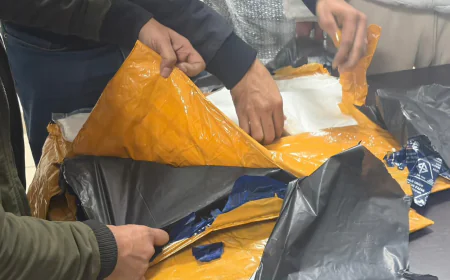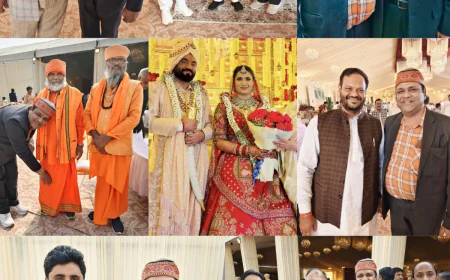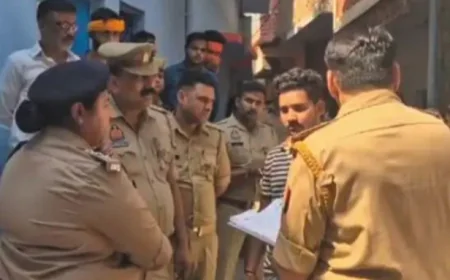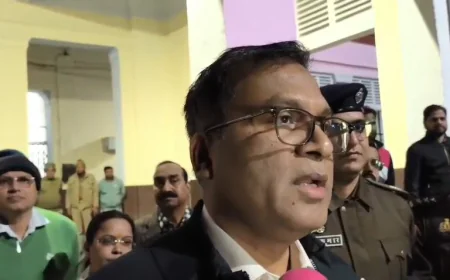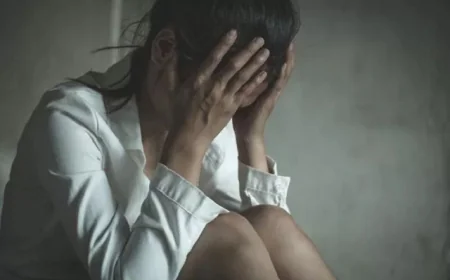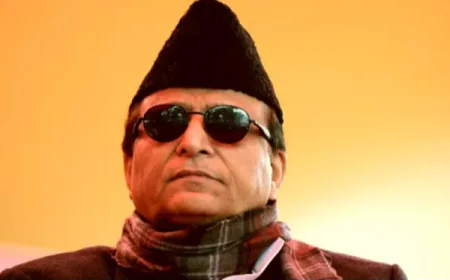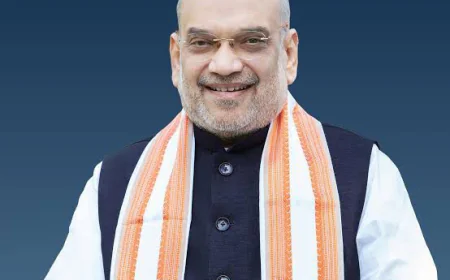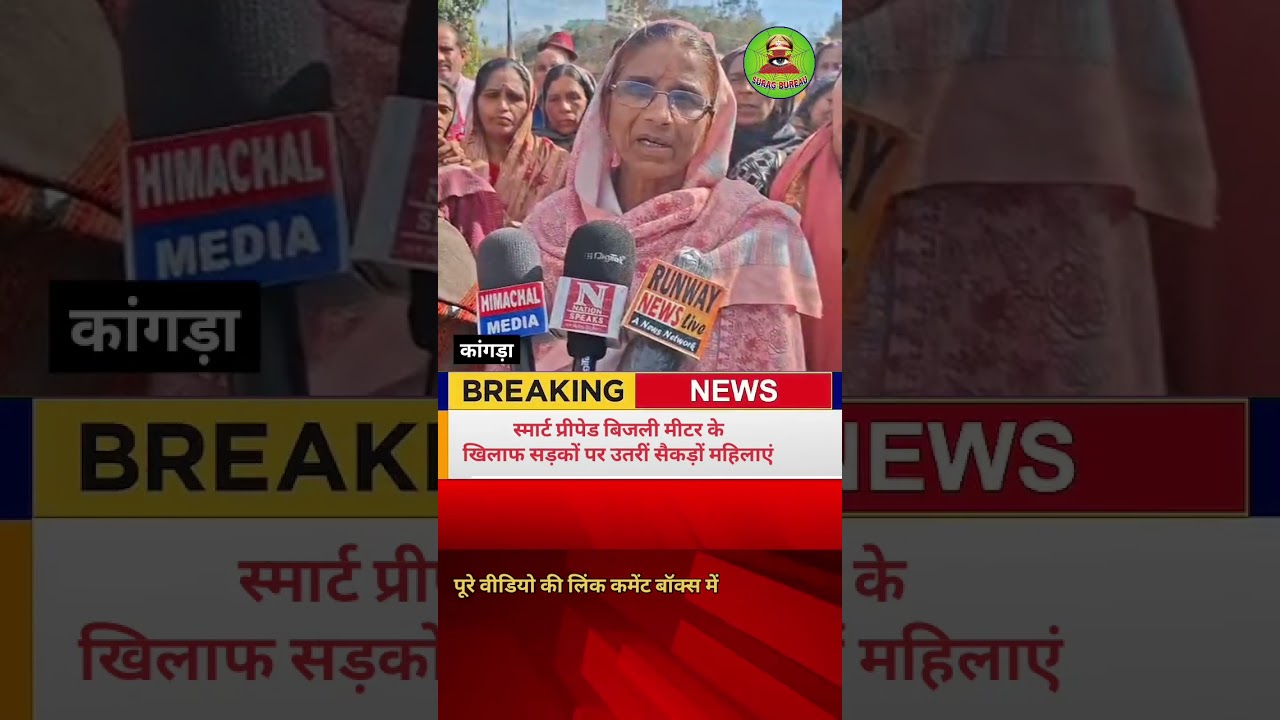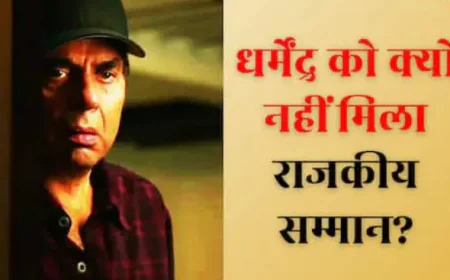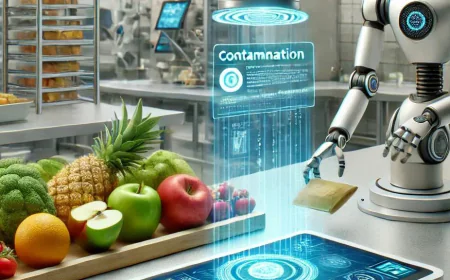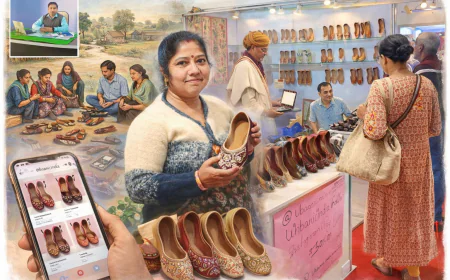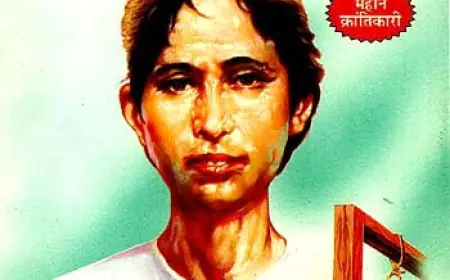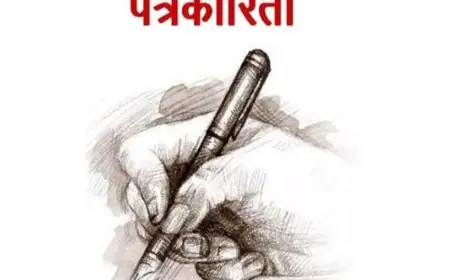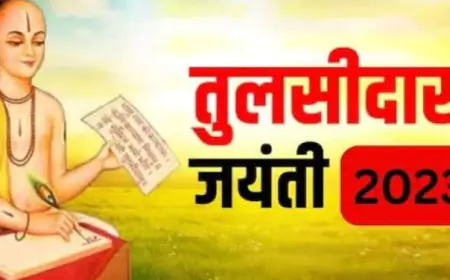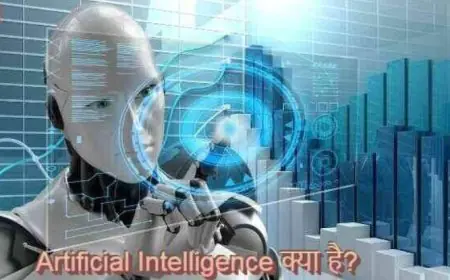खेल शिक्षा की नई दिशा: क्या भारत तैयार है?

खेल शिक्षा की नई दिशा: क्या भारत तैयार है?
भारत में खेल और शारीरिक शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी हैं। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नीतियां बनाई हैं, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में कई चुनौतियां बनी हुई हैं। जब भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी ओर कदम बढ़ा रहा है, खेल शिक्षा को और मजबूत करने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो रही है। कुछ समय पहले तक खेल को शिक्षा और करियर की दृष्टि से गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यह देश की प्राथमिकता सूची में शामिल हो चुका है। सरकार द्वारा खेलों के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, हैं, जिससे खेल न केवल एक प्रतिस्पर्धा का माध्यम बल्कि करियर और राष्ट्र निर्माण का अभिन्न हिस्सा बन गया है।
इसी के साथ, खेल शिक्षा को भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया जा रहा है, ताकि देश में खेल विज्ञान, खेल प्रबंधन और शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों को व्यवस्थित रूप से विकसित किया जा सके। एक सकारात्मक बदलाव यह है कि अब आइआइटी और आइआइएम जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में खेल कोटे की व्यवस्था की गई है, जिससे तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थी भी खेल शिक्षा से जुड़ रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि खेल केवल मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में भी इसका महत्त्वपूर्ण स्थान बनता जा रहा है। इसके बावजूद, भारत में स्पोटर्स इंजीनियरिंग जैसे विषयों पर अब तक बहुत कम काम हुआ है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक, खेल उपकरणों की डिजाइनिंग और प्रदर्शन विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यदि भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनना है, तो स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग पर भी विशेष ध्यान देना होगा, जिससे तकनीकी के माध्यम से खिलाड़ियों का का प्रदर्शन बेहतर किया जा सके और देश को खेल विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा जा सके। खेल शिक्षा का विकास देश के समग्र खेल ढांचे के लिए आवश्यक है।
वर्तमान में देश में खेल शिक्षा के लिए 2 राष्ट्रीय, 9 राज्य स्तरीय खेल विश्वविद्यालय के साथ-साथ 700 से अधिक कॉलेज और विभाग संचालित हैं। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान खेल शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। संस्थानों में खेल विज्ञान, खेल प्रबंधन, खेल पोषण, खेल मनोविज्ञान, खेल चिकित्सा और शारीरिक शिक्षा जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि, भारत में खेल शिक्षा अभी भी वैश्विक 5 मानकों तक नहीं पहुंच पाई है। इसे और प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। भारत में खेल शिक्षा को लेकर सबसे बड़ी चुनौती एकीकृत नियामक निकाय के अभाव की है। इस दिशा में राष्ट्रीय खेल शिक्षा परिषद जैसे निकाय की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है। वर्तमान में, खेल शिक्षा को संचालित करने वाला कोई केंद्रीय संगठन नहीं है, जिससे विभिन्न संस्थान और नियामक निकाय अपने-अपने तरीके से पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मजे बात यह है कि इस परिषद् में शारीरिक शिक्षा के विशेषज्ञ ही नहीं है। वहीं, खेल विज्ञान और खेल प्रबंधन पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अधीन आते हैं, जिससे एक समन्वित और प्रभावी ढांचा विकसित नहीं हो पाता। इस असंगठित व्यवस्था के कारण न केवल पाठ्यक्रमों में एकरूपता की कमी है, बल्कि विद्यार्थी भी सही दिशा में मार्गदर्शन से वचित रह जाते हैं।
इसके अलावा, भारत में खेल शिक्षा अभी भी पारंपरिक पद्धतियों पर आध्यारित हैं, है, जबकि वैश्विक स्तर पर खेल विज्ञान और तकनीक में निरंतर नवाचार हो रहा है। अत्याधुनिक शिक्षण पद्धतियों और डिजिटल नवाचारों को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि खेल शिक्षा को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया सके। यदि भारत को खेल शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना है, तो उसे अपने पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण पद्धतियों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना होगा और यह कार्य एक संगठित नियामक निकाय के माध्यम से ही संभव हो सकता है। भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दिशा में अग्रसर हैं, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खेल शिक्षा को मजबूत करना बेहद आवश्यक हो गया है केवल विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं का निर्माण ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि एक प्रभावी खेल शिक्षा प्रणाली भी विकसित करनी होगी, जो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रबंधकों को तैयार कर सके। यदि खेल शिक्षा को एक केंद्रीकृत नियामक निकाय के तहत लाया जाए, तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत न केवल खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करे, बल्कि खेल विज्ञान और खेल प्रबंधन के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बन सके। अब समय आ गया है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए ताकि 2036 ओलपिक तक भारत खेल शिक्षा के भी दुनिया का नेतृत्व कर सके। खेल शिक्षा को वह सम्मान और प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसका वह लंबे समय से हकदार है, ताकि भारत खेल महाशक्ति बनने के अपने सपने को साकार कर सके। विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब [2) उच्च शिक्षा में महिलाओं का योगदान विजय गर्ग महिलायें आज अकादमिया या शिक्षा, मीडिया, स्वास्थ्यरक्षा, सशस्त्र बलों व अन्य अनेक क्षेत्रों में सामने आ कर नेतृत्व कर रही हैं।
पहले महिला नेतृत्व को स्वीकार करने की तुलना में आज देश में व्यापक परिवर्तन आया है। भारतीय उच्च शिक्षा परिदृश्य भी मजबूत महिला-नीत बल के कारण बदल रहा है। उन्होंने देश की प्रगति की नीव डाली है, सामाजिक-आर्थिक प्रगति के अवसर खोले हैं, तथा आत्मनिर्भरता व जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि की है। कहने की आवश्यकता नहीं कि 'विकसित भारत की यात्रा में महिला सशक्तीकरण हेतु शिक्षा आवश्यक है। शिक्षित महिलायें परिवर्तन लाती हैं, परिवारों को ऊपर उठाती हैं, समुदायों को मजबूत करती हैं तथा राष्ट्रीय प्रगति सुनिश्चित कर भावी पीढ़ियों पर स्थाई प्रभाव छोड़ती हैं। जहां तक नेतृत्व का सवाल है, आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय उच्च शिक्षा में पुरुष प्रभुत्व बना हुआ है, हालांकि महिलायें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। 2021 में भारतीय उच्च शिक्षा में महिला नेतृत्व केवल 9.55 प्रतिशत था, जबकि पुरुष 89.57 प्रतिशत नेतृत्व दे रहे थे। इससे अकादमिक नेतृत्व में महिलाओं का नेतृत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम भारत की तुलना अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से करें तो व्यापक कमी सामने आती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक सर्वोच्च 200 विश्वविद्यालयों में से 25 प्रतिशत का नेतृत्व महिलायें कर रही हैं। अच्छी खबर है कि यह तस्वीर तेजी से बदल रही है। और खासकर पिछले कुछ साल में बदली है। अतीत में भी देश ने अनेक दूरदर्शी महिला नेताओं को देखा है जिनमें सावित्रीबाई फुले जैसी समाजसुधारक हैं।
जिन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिल कर भारत में 1948 में लड़कियों का पहला स्कूल स्थापित किया था और इस प्रकार महिला शिक्षा तथा सामाजिक न्याय की पैरोकारी की थी। उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाली अन्य उल्लेखनीय व व्यावहारिक महिला नेताओं में 'लवली प्रोफेशनल युनिवर्सिटी' की प्रो- चांसलर सुश्री रश्मि मित्तल तथा 'नोयडा इंटरनेशनल युनिवर्सिटी' की उप- कुलपति डा. उमा भारद्वाज, 'चित्कारा युनिवर्सिटी' की प्रो- चांसलर डा. मधु चित्कारा शामिल हैं। 42 साल के व्यापक अनुभव वाली उच्च शिक्षा उद्यमी डा. चित्कारा ने एक सफल विश्वविद्यालय बनाया है। दिल्ली-एनसीआर में 'शिव नाडार युनिवर्सिटी' की उप-कुलपति डा. अनन्या मुखर्जी के संस्थान को 'इंस्टीट्यूशन आफ इमीनेंस' माना गया है। इसके साथ ही बिजनेस और उद्यमिता के क्षेत्र में महिला नेताओं ने उभरते भारतीय युवाओं को प्रेरणा दी है। इनमें किरन मजूमदार शा तथा इंदिरा नूई खासतौर से उल्लेखनीय महिला नेता हैं जिन्होंने खोज एवं समावेशी परिवेशों से भारतीय उच्च शिक्षा में बदलाव किए हैं। नेतृत्वकारी स्थितियों में ज्यादा महिलाओं से विविधता प्रोत्साहित होगी तथा अकादमिक क्षेत्र को नए आयाम मिलेंगे। अपने प्रयासों से वे भारत में भावी पीढ़ियों को ज्यादा प्रगतिशील और समतापूर्ण शिक्षा परिदृश्य विकसित करने की प्रेरणा दे रही हैं। हालांकि, महिलाओं को अकादमिक क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिनमें एक ओर सामाजिक पूर्वाग्रह तथा दूसरी ओर संस्थानों में पैदा बाधायें शामिल हैं। अनेक महिलायें अब भी अपने खिलाफ अनेक पूर्वाग्रहों का सामना कर रही हैं जिनका संबंध खासकर परंपरागत क्षेत्रों में नेतृत्व की उनकी क्षमता से है।
महिलाओं को 'सेंटर' प्राप्त करने तथा अपनी पेशेवर प्रगति के लिए नेटवर्क बनाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दुनिया भर में महिला नेताओं के लिए मुख्य मुद्दों में 'वर्क-लाइफ बैलेंस' तथा वरिष्ठ नेतृत्वकारी स्थितियों में कम उपस्थिति है। भारत ने देश भर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के माध्यम से महिला फैकल्टी के उन्मुखीकरण व प्रशिक्षण के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए तैयार करना तथा उनको उचित कौशलों और ज्ञान से लैस करना है। अन्य देशों में ऐसे कार्यक्रम बनाए गए हैं जिनमें अकादमिक क्षेत्र महिलाओं द्वारा बाधायें तोड़ने के लिए नेतृत्वकारी प्रशिक्षण व समावेशन पर ध्यान दिया गया है कुछ देशों ने अकादमिक क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या में शानदार वृद्धि दर्ज की है, लेकिन इसके बावजूद भारत समेत बाकी दुनिया को इस संबंध में लंबा रास्ता तय करना है। शिक्षा में सशक्तीकरण का अर्थ केवल पहुंच का सवाल न होकर इसमें महिलाओं को शिक्षकों, नेताओं व माडलों की भूमिका देना भी शामिल है। स्कूलों और कालेजों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि लड़कियों के लिए एक प्रेरणादायक बल का काम करती जिससे वे अकादमिक क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ती हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों के नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका के बारे में विविधतापूर्ण विचार एक समावेशी व खोजी परिदृश्य तैयार करते हैं। महिला प्रोफेसरों ने प्रगतिशील शिक्षा नीति तथा शोध की गुणवत्ता में रीढ़ की हड्डी जैसा काम किया है। अब महिलायें अनेक महत्वपूर्ण विभागों तथा शोध संस्थानों का संचालन कर रही हैं जो विश्वविद्यालयों के जीवन में उनके बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है। लड़कियों व महिलाओं के लिए खासकर 'स्टेम' क्षेत्रों में कार्यक्रमों व फेलोशिप ने रचनात्मकता और उत्कृष्टता का संसार बनाने में सहायता की है। वर्तमान समय में भारत के कुछ सर्वाधिक हाई-प्रोफाइल विश्वविद्यालयों व संस्थानों में महिलायें शिखर पर हैं। वे शिक्षा तक ज्यादा पहुंच पैदा करने के साथ ही उसे समतापूर्ण बना रही हैं। महिला नेता अकादमिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग संस्थानों समेत महिला नीत संस्थान हजारों छात्रों को दिशा दे कर उनकी महत्वाकांक्षाओं को स्वरूप दे रहे हैं।
इस प्रकार स्पष्ट है कि महिला नेता शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन कर रही हैं तथा वे अच्छी प्रबंधक हैं। महिलायें शिक्षक तथा परिवर्तन की वाहक हैं। समावेशन को बढ़ावा देने तथा समुदायों को सशक्त बनाने के माध्यम से खाली स्थान भर कर अच्छे नेता की भूमिका अदा कर रही हैं। शक्तिशाली, समाधान केन्द्रित व प्रतिक्रियात्मक कार्यबल के रूप में महिलायें खासकर अपरिहार्य हैं क्योंकि वे न केवल आर्थिक प्रगति, बल्कि सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करती हैं। शिक्षा में महिलाओं की सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका प्रौढ़ साक्षरता तथा कौशल विकास में दिखाई देती है। महिला शिक्षकों ने ग्रामीण व हाशियाकृत समुदायों में साक्षरता दर बढ़ाने के साथ उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियां बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला उद्यमी भी पूरे भारत में सीखने की दिशा में विभिन्न खोजी समाधानों के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं। महिला वित्तपोषकों के 'एडटेक' प्लेटफर्म ने परिवर्तनशील माडलों, डिजिटल क्लासरूम प्रयोगों तथा एआई-आधारित विश्लेषकों को प्रोत्साहित किया है। इससे उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है तथा उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक उनकी पहुंच बढ़ी है। सामाजिक विकास तथा तकनीकी शिक्षा एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। उच्च शिक्षा में महिला नेताओं की संख्या बढ़ाना न केवल उच्च शिक्षा, बल्कि जेंडर समानता के लिए भी जरूरी है जो भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020- एनईपी में अकादमिक क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता का महत्व समझ कर अनेक सुधारों का प्रस्ताव किया गया है। उच्च शिक्षा में नेतृत्व प्रशिक्षण तथा मॅटरशिप सुविधाओं के माध्यम से भारत अकादमिक नेताओं के रूप में महिलाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। 'विकसित भारत' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण तथा भारत के 'जनसंख्या लाभांश' का लाभ उठाने के लिए महिलाओं की उच्च शिक्षा में सहभागिता बढ़ाना जरूरी है। इससे भारत को 'विश्व गुरु बनाने में भी उल्लेखनीय योगदान मिलेगा। विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब [3) भाषाई तनाव को कम करना विजय गर्ग स्कूली शिक्षा में तीन भाषा के फार्मूले पर चल रही पंक्ति - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में एम्बेडेड एक नीति - ने एक बार फिर भावुक बहस को प्रज्वलित किया है। हाल ही में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तमिलनाडु के राजनीतिक नेतृत्व ने राज्य में हिंदी को लागू करने के रूप में माना जाता है, इसके लिए केंद्र की तीखी आलोचना की है। हालांकि, यह संघर्ष अलग-थलग नहीं है; यह कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब जैसे राज्यों में प्रतिध्वनित होता है, प्रत्येक भाषा युद्ध में अपना अध्याय जोड़ता है। वर्तमान हंगामे की जड़ें भारत में भाषा थोपने पर लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक संघर्ष में हैं। तमिलनाडु में, अतीत के हिंदी विरोधी आंदोलनों की यादें अभी भी गूंज रही हैं, क्योंकि राज्य की सत्तारूढ़ डीएमके अपनी भाषाई पहचान को कमजोर करने के लिए एक सूक्ष्म प्रयास के रूप में तीन-भाषा सूत्र पर जोर देने को मानती है।
आलोचकों का तर्क है कि अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी को प्राथमिकता देकर, नीति अनजाने में स्थानीय भाषाओं को दरकिनार कर देती है - एक चिंता जो समृद्ध भाषाई विरासत के साथ दक्षिणी राज्यों में गहराई से गूंजती है। जबकि कुछ लोग हिंदी को एक एकीकृत बल के रूप में देखते हैं, कई लोग इसके प्रचार को क्षेत्रीय संस्कृतियों और पहचान के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। संघर्ष एक व्यापक पैटर्न का प्रतीक है जहां राज्य कथित केंद्रीय आउटरीच के खिलाफ अपनी भाषाई पहचान का दावा करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। तमिलनाडु में स्टालिन और अन्य नेताओं का तर्क है कि एनईपी की भाषा नीति को लागू करना तमिल की प्रधानता को खत्म करने का एक पतला घूंघट प्रयास है। इसी तरह की भावनाओं को कहीं और गूंज दिया गया है: तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में सभी स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र अपनी मातृभाषा सीखें । ऐसा करने में, तेलंगाना न केवल अपनी भाषाई विरासत को संरक्षित कर रहा है, बल्कि आसान समझ के लिए पाठ्यक्रम को सरल बना रहा है। पंजाब के उत्तरी राज्य में भी 2025-26 के शैक्षणिक सत्र के लिए सीबीएसई स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा पाठ्यक्रम से पंजाबी को हटाने से पंजाबियों में आक्रोश फैल गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जैसे राजनीतिक आंकड़ों ने इसे 'हमारी मातृभाषा पर हमला' बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर देकर इन तनावों को शांत करने का प्रयास किया है कि भाजपा हर भारतीय भाषा का सम्मान करे और प्रत्येक भाषा भारतीय संस्कृति की आत्मा को दर्शाती है। वह कहता है कि सभी भाषाई परंपराओं को समृद्ध करना और गले लगाना हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। फिर भी, राय गहराई से विभाजित रहती है।
हिंदी अधिरोपण पंक्ति एक नीतिगत विवाद से अधिक है - यह भारत में गहरे बैठे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक धाराओं का प्रतिबिंब है। कथित भाषाई आधिपत्य के लिए एमके स्टालिन के मजबूत प्रतिरोध को उनके राज्य में व्यापक रूप से साझा किया गया है। भाषा एक भावनात्मक मुद्दा है और अगर ठीक से संभाला नहीं जाता है तो एक बड़े संकट में स्नोबॉल हो सकता है। सबसे अच्छा समाधान एक संतुलित, लचीले दृष्टिकोण में निहित है जो भारत की भाषाई विविधता का सम्मान करता है। केवल सम्मानजनक संवाद, अनुरूप नीतियों और विविधता के उत्सव के माध्यम से भारत इस जटिल भाषाई परिदृश्य को नेविगेट कर सकता है और वास्तव में समावेशी राष्ट्र की ओर बढ़ सकता है।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्राचार्य शैक्षिक स्तंभकार गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब