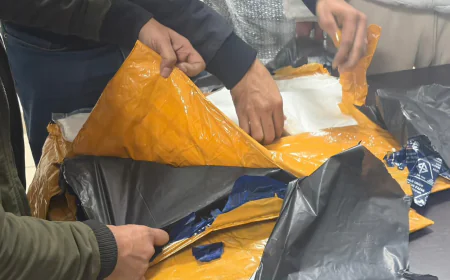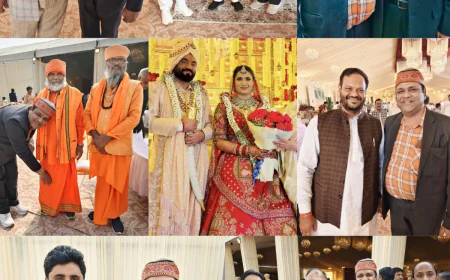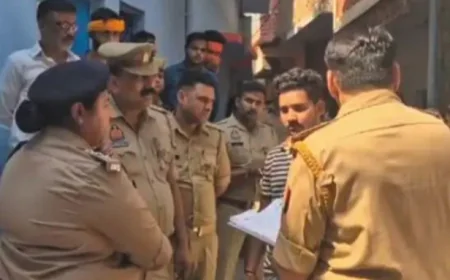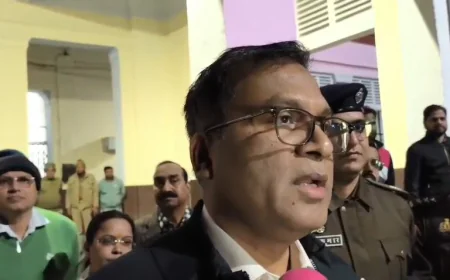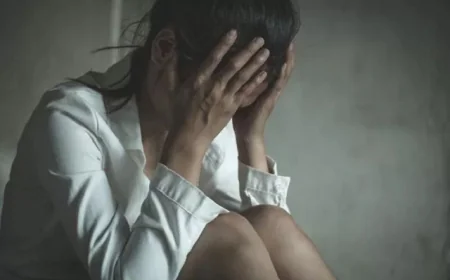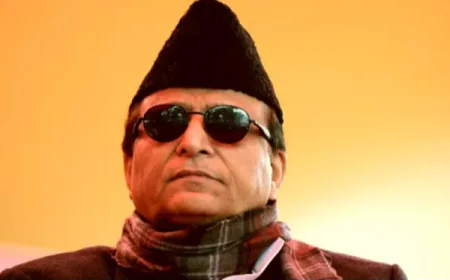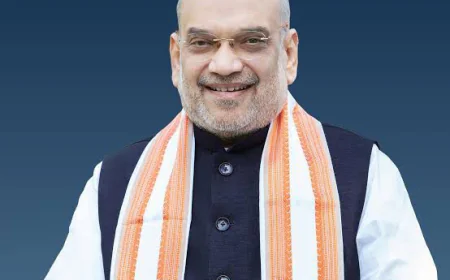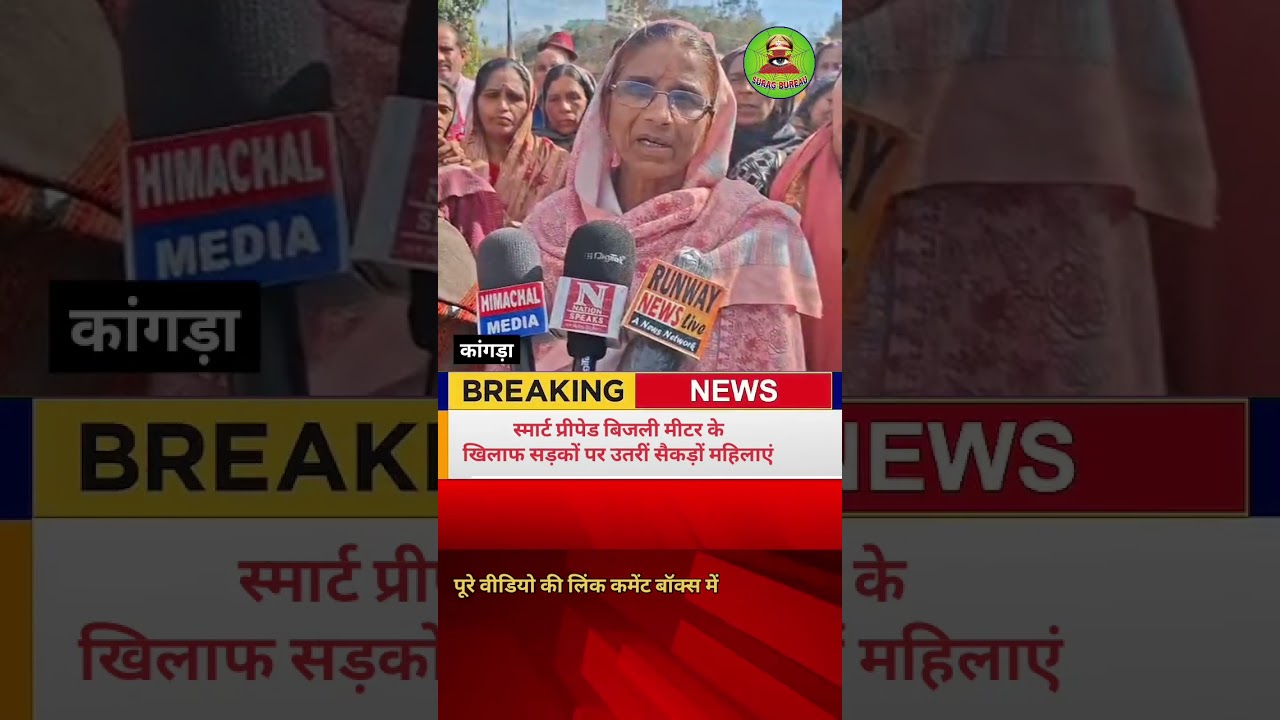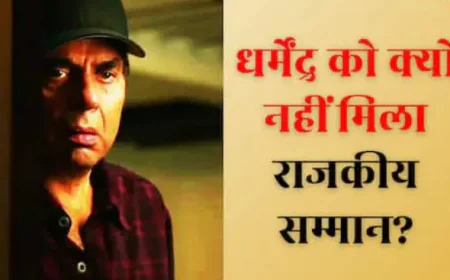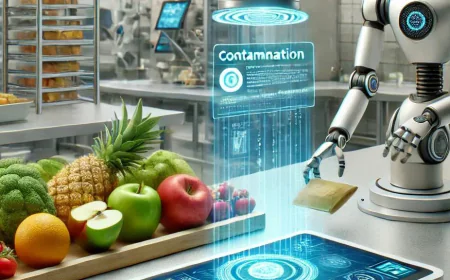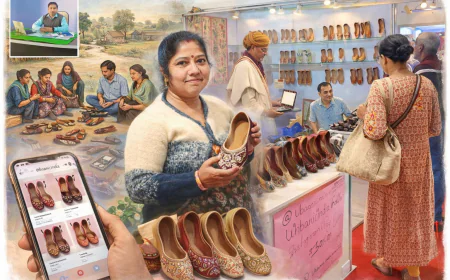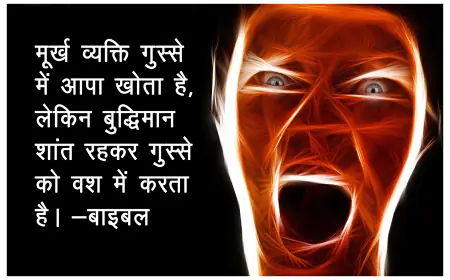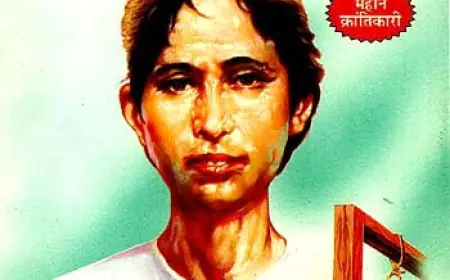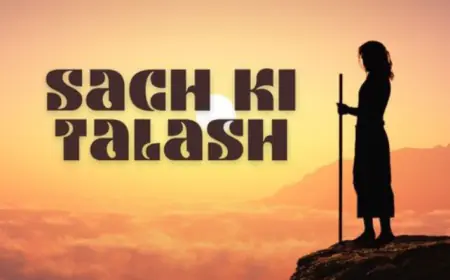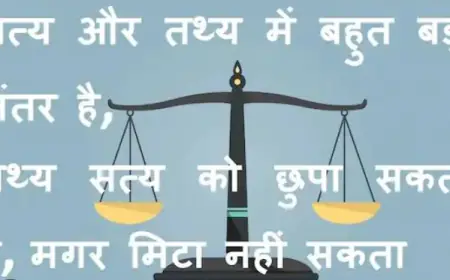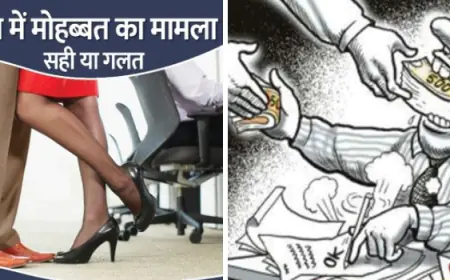प्राथमिक शिक्षा में देश को दोबारा गुरुकुल परंपरा की ओर ले जा सकते हैं।

प्राथमिक शिक्षा में देश को दोबारा गुरुकुल परंपरा की ओर ले जा सकते हैं।
विजय गर्ग
सरकार की प्राथमिकताओं में गुणवत्ता पूर्ण और निशुल्क प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर काफी बातें होती हैं, लेकिन इसमें जुटा सरकारी तंत्र और विद्यालय जो नतीजे दे रहे हैं, वे चिंताजनक हैं। भारत जैसे देश में निजी संस्थाओं को छोड़ दें, तो सरकारी विद्यालय कैसे हैं, यह सर्वविदित है। एक कटु सत्य भी है कि प्राचीन काल में हमारी बाल शिक्षा, जिसे अब प्राथमिक कह सकते हैं, विश्व में सबसे अलग थी। गुरुकुल की सबसे पुरानी परंपरा का उदाहरण आज भी दुनिया देती है। इसी कारण भारत विश्व गुरु कहलाया । गुरुकुलों को पहले मुगलों ने प्रभावित किया, फिर अंग्रेजों ने बंद ही करवा दिया। इस पद्धति में दंड नहीं दिया जाता था, लेकिन मुगलों दौर में बदलाव लाकर शिक्षक को दंड पकड़ा दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने गुरुकुलों को गैर-कानूनी तक घोषित कर दिया। प्राथमिक शिक्षा की गुरुकुल पद्धति कैसी थी, इसके उदाहरण दिए जाते हैं। यह कैसे नष्ट हुई, इस पर विदेशी विद्वानों की भी चिंताएं सामने आईं। अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक, इतिहाकार एवं दार्शनिक विलियम जेम्स डुरांट की किताब 'द स्टोरी आफ सिविलाइजेशन' में बड़ी साफगोई से काफी कुछ लिखा गया है। इसकी कुछ पंक्तियां सच्चाई दर्शाती हैं, 'भारत से ही हमारी सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी।
संस्कृत सभी यूरोपीय भाषाओं की मां है। हमारा समूचा दर्शन संस्कृत से उपजा है। हमारा गणित इसकी देन है। लोकतंत्र और स्वशासन भी भारत से ही उपजा है।' विडंबना देखिए कि आज कि आज उस देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर पीड़ा व्यक्त की जाती है, लेकिन जो सत्य है, वह के सामने है। इसी पुस्तक में वे लिखते हैं कि 'भारत के बारे में पुख्ता ढंग से मामले में मैं के पूर्व और बहुत गरीब सिद्ध हुआ हूँ। लिखने के पहले दो लिखने के पश्चिम की यात्राएं की। उत्तर से लेकर दक्षिण के शहर देखें। पुरानी सभ्यता के सामने मेरा ज्ञान सामने मेरा ज्ञान बहुत तुच्छ और टुकड़ का है। इसके दर्शन, साहित्य, धर्म और कला का विश्व में कोई सानी नहीं है। इस देश की अंतहीन धनाढ्यता इसकी ध्वस्त हो चुकी शान और 'स्वतंत्रता के लिए शस्त्रहीन संघर्ष' से अब भी झांकती है। यहां मेहनतकश स्तकश लोगों को अपने सामने भूख से मरते देखा। ये अकाल या जनसंख्या वृद्धि से नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन की चाल से तिल-तिल कर मर रहे थे। भारतीयों के साथ घिनौना अपराध इतिहास में दर्ज हो चुका है।
अमेरिकी होकर भी मैं ब्रितानियों के इस अत्याचार की निंदा करता है।' जब अंग्रेज भारत आए तो देश में शिक्षा का एक सुगठित ढांचा था। बच्चे गुरुकुल में में पढ़ते थे। अंग्रेजों ने इस प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर व्यावसायिक विद्यालयों को बढ़ावा दिया। उन्होंने प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का आधा हिस्सा तो आते ही तबाह कर दिया। इसके बाद भारत में शिक्षा आमजन के लिए आसान नहीं रही। यहां 1850 तक सात लाख 32 हजार गुरुकुल थे। यानी प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय था, जिसकी शिक्षा व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी। वर्ष 1858 में भारतीय शिक्षा कानून' बनाया गया, जिसका मसविदा मैकाले का था। इस तरह बड़ी साजिश के तहत गुरुकुलों का अस्तित्व समाप्त कर उसे पाश्चात्य रंग में रंगने और फूट डालो शासन करो की नीति के तहत षडयंत्र हुए। गुरुकुलों का दमन कर ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई कि स्वतंत्रता के 77 वर्षों के बाद भी यह भटकी हुई लगती है। भारत के बाद डेनमार्क दुनिया का पहला देश कहलाया, जिसने अनिवार्य सामूहिक शिक्षा की सरकार नियंत्रित प्रणाली शुरू की। यहां 1721 में स्कूल विकसित हुए। वर्ष 1814 में समन्वय आयोग की रपट बाद शिक्षा प्रणाली का आधार बना।
जबकि इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा की अंग्रेजी प्रणाली पश्चिमी यूरोप के दूसरे देशों की तुलना विकसित हुई। उन्नीसवीं सदी में ज्यादातर प्राथमिक शिक्षा चर्च द्वारा मुख्य रूप से गरीब बच्चों को दी जाती थी। शिक्षा के विस्तार में सरकार की रुचि नहीं थी। * 1860 में प्राथमिक विद्यालयों के संगठन से संबंधित नियमों की एक राज्य संहिता तैयार कराई और 1862 2 में इसे समायोजित किया। स्कूली पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता और निरीक्षण की छात्रों के पढ़ने-लिखने के स्तर राष्ट्रीय प्रणाली बनाई गई। इसमें कुछ स्कूलों के लिए वित्तपोषण और गणित कौशल की जांच जांच होती थी। तय होता था। वर्ष 1900 तक उत्तरी अमेरिकी देशों, देशों आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उत्तरी-पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों ने स्कूली शिक्षा के प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाई। उत्तरी यूरोपीय देशों के अधिकांश | देशों में नामांकन 60 से 75 फीसद तक था, जबकि अन्य क्षेत्रों में, विशेषकर एशिया (जापान को छोड़ कर), मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में स्कूली शिक्षा का प्रसार काफी न्यून था। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में जापान की उन्नीसवीं सदी में सबसे उल्लेखनीय स्थिति रही। जापान की तुलना थाईलैंड में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार ज्यादा सफल रहा। समझा जा सकता है कि इसकी प्रेरणा भारतीय गुरुकुल पद्धति से ही से ही मिली।" पूरे विश्व ने भारतीय गुरुकुलों की शिक्षा के महत्त्व को समझा। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि प्राथमिक शिक्षा, "जिसकी सदियों पहले भारत ने गुरुकुल परंपरा से शुरुआत की, वह विश्व का अग्रदूत बना। उसने शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा, पर सबको संदेश दिया।
मगर विद्वेष, आपसी फूट फूट और र गुलामी के चलते इसे समाप्त करने की साजिश हुई। इसमें मैकाले की चाल सफल रही। फिर भी विश्व, बाल शिक्षा के महत्त्व का भारतीय संदेश समझ चुका था। हो भी क्यों न, राष्ट्रों के निर्माण और शक्ति के लिए जन शिक्षा के महत्त्व का अलख भारत ने ही जगाया था। गुलामी से | से मुक्ति के बाद भारत में भी शिक्षा, विशेषकर र प्राथमिक शिक्षा, को लेकर बदलाव होते रहे। यह कैसी विडंबना है कि 1823 में सौ फीस साक्षरता वाला देश 1947 में महज 12 फीसद साक्षरता पर आ गया। इसी चुनौती से निपटने के लिए आज कई प्रयास हो रहे हैं। हो स्वतंत्रता के सतहत्तर वर्षों के बाद भी शिक्षा को लेकर अव्यवस्था, लिंग, भाषाई तथा भौगोलिक अंतर की खाई को नहीं पाटा जा सका। यह प्राथमिक शिक्षा में साफ झलकती है। 2023 की वार्षिक शिक्षा स्थिति रपट के अनुसार, आठवीं कक्षा के तीन में से एक छात्र दूसरी कक्षा के छात्र के स्तर पर नहीं पढ़ सकता है तथा आधे से अधिक बुनियादी विभाजन नहीं कर सकते हैं। 14 से 18 वर्ष की आयु के एक चौथाई अपनी क्षेत्रीय | भाषाओं में दूसरी कक्षा का पाठ धाराप्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं। आज सरकार नियंत्रित प्राथमिक विद्यालयों पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नए दौर में शिक्षकों को ज्यादा सुविधाएं देकर यदि हम अपनी नींव को मजबूत करने की दिशा में बढ़ेंगे, तो पूरे देश में नया वातावरण बनेगा। शिक्षकों को भी पूर्ण समर्पण से जुटना होगा।
शिक्षा में अमीर-गरीब, जात-पात और ऊंच-नीच का भेदभाव समाप्त कर हम देश को दोबारा गुरुकुल परंपरा की ओर ले जा सकते हैं। विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब [2) संचार कौशल में महारत हासिल करने से बेहतर रिश्तों के द्वार खुलते हैं विजय गर्ग प्रभावी संचार एक आवश्यक कौशल है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हों, किसी मीटिंग में भाग ले रहे हों, या दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हों, मजबूत संचार कौशल समझ बढ़ा सकते हैं और बेहतर रिश्तों को बढ़ावा दे सकते हैं। आपके संचार कौशल को बेहतर बनाने में मदद के लिए यहां कुछ व्यावहारिक रणनीतियाँ दी गई हैं: स्फूर्ति से ध्यान देना संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक सुनना है। प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए, आपको यह समझने की ज़रूरत है कि दूसरे क्या कह रहे हैं। वक्ता पर अपना पूरा ध्यान देकर, ध्यान भटकाने से बचते हुए और शारीरिक भाषा के माध्यम से रुचि दिखाकर सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें। स्पष्ट और संक्षिप्त रहें अपने विचार व्यक्त करते समय स्पष्टता और संक्षिप्तता का लक्ष्य रखें। ऐसी शब्दावली या अत्यधिक जटिल भाषा का प्रयोग करने से बचें जो आपके दर्शकों को भ्रमित कर सकती है।
अपने विचारों को तार्किक रूप से व्यवस्थित करें, और उन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप बताना चाहते हैं। संक्षिप्त होने से आपके दर्शकों का ध्यान बनाए रखने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि आपका संदेश समझ में आ गया है। अशाब्दिक संचार का अभ्यास करें आपकी शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव और हावभाव संचार के महत्वपूर्ण घटक हैं। अपने अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान दें, क्योंकि वे या तो आपके बोले गए शब्दों को पुष्ट कर सकते हैं या उनका खंडन कर सकते हैं। आत्मविश्वास और स्वीकार्यता व्यक्त करने के लिए खुली शारीरिक भाषा, जैसे बिना क्रॉस वाली भुजाएं और आरामदायक मुद्रा बनाए रखने का अभ्यास करें। सहानुभूति विकसित करें सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है। सहानुभूति विकसित करने से आपके संचार कौशल में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। दूसरों के साथ बातचीत करते समय, चीजों को उनके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें और समझ के साथ प्रतिक्रिया दें। यह गहरे संबंधों को बढ़ावा देगा और अधिक सार्थक बातचीत को प्रोत्साहित करेगा। प्रतिक्रिया के लिए पूछें अपने संचार कौशल को बढ़ाने के लिए, दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से रचनात्मक प्रतिक्रिया लें। वे इस बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं कि आप स्वयं को कैसे अभिव्यक्त करते हैं और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करते हैं। आलोचना के प्रति खुले रहें और इसे विकास के एक उपकरण के रूप में उपयोग करें।
सार्वजनिक भाषण में व्यस्त रहें सार्वजनिक रूप से बोलने से आपके आत्मविश्वास और संचार क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। समूहों के सामने बोलने का अभ्यास करने के अवसरों की तलाश करें, चाहे वह औपचारिक प्रस्तुतियों, सामुदायिक कार्यक्रमों या यहां तक कि अनौपचारिक समारोहों के माध्यम से हो। अपनी शब्दावली पढ़ें और उसका विस्तार करें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को पढ़ने से आप विभिन्न संचार शैलियों और शब्दावली से परिचित हो सकते हैं। ऐसी किताबें, लेख और निबंध पढ़ने की आदत बनाएं जो आपके लिए चुनौती हों। एक व्यापक शब्दावली आपको अपने विचारों को अधिक सटीक और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की अनुमति देती है, जिससे आपके समग्र संचार कौशल में वृद्धि होती है। प्रौद्योगिकी का बुद्धिमानी से उपयोग करें आज के डिजिटल युग में, संचार अक्सर ईमेल, टेक्स्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। इन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते समय, अपने लहज़े और स्पष्टता का ध्यान रखें। गलतफहमी से बचने के लिए अपने संदेशों को प्रूफरीड करने के लिए समय निकालें। व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ने के लिए वीडियो कॉल को अपनाएं, क्योंकि वे अशाब्दिक संचार की अनुमति देते हैं जिसकी टेक्स्ट में कमी है। नियमित रूप से अभ्यास करें किसी भी अन्य कौशल की तरह, अभ्यास से संचार में सुधार होता है। बातचीत में शामिल हों, चर्चाओं में भाग लें और लगातार अपने विचार व्यक्त करने के अवसर तलाशें। आप जितना अधिक संवाद करेंगे, आप उतने ही अधिक सहज और प्रभावी बनेंगे। खुले दिमाग वाले रहें प्रभावी संचार के लिए नए विचारों और दृष्टिकोणों के प्रति खुलेपन की आवश्यकता होती है।
दूसरों के साथ जुड़ने के लिए तैयार रहें, भले ही उनका दृष्टिकोण आपसे भिन्न हो। विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब [3) भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए अदृश्य लड़ाई विजय गर्ग मानसिक स्वास्थ्य हमारी स्वास्थ्य देखभाल कथा में एक बाद का विचार बना हुआ है। सच्ची चिकित्सा में शरीर और मन दोनों शामिल हैं एक मनोवैज्ञानिक के रूप में, मैंने देखा है कि भारत में स्वास्थ्य केवल शरीर की लड़ाई नहीं है, यह मन का संघर्ष है। हर बीमारी के पीछे एक व्यक्ति होता है जो डर, हताशा और कभी-कभी अकेलेपन से जूझता है। चाहे ग्रामीण इलाकों में, जहां तपेदिक जैसी बीमारियां बनी रहती हैं या शहरी केंद्रों में जहां जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं, भावनात्मक असर अक्सर अदृश्य होता है लेकिन गहराई से महसूस किया जाता है। ग्रामीण भारत में, मरीजों को चिकित्सीय निदान से परे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुझे याद है कि एक छोटे से गांव का एक आदमी तपेदिक से जूझ रहा था, लेकिन जिस चीज ने उस पर सबसे ज्यादा असर डाला वह सिर्फ उसकी बीमारी नहीं थी - वह अलगाव था। वह खुद को भूला हुआ और दुनिया से कटा हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत दूर थीं और उसके परिवार को नहीं पता था कि उसे कैसे सहारा दिया जाए।
यह भावनात्मक अलगाव कई ग्रामीण रोगियों का अनुभव है, और यह उनके शारीरिक लक्षणों जितना ही हानिकारक हो सकता है, जिससे उनमें निराशा की भावना बढ़ जाती है। गुड़गांव जैसे शहरों में संघर्ष अलग-अलग हैं लेकिन उतने ही गहरे भी। मैं चिंता से घिरी एक युवा महिला अंजलि के बारे में सोचता हूं। बाहरी दुनिया को, ऐसा लग रहा था कि उसके पास सब कुछ है - एक शानदार नौकरी, व्यस्त सामाजिक जीवन और एक उज्ज्वल भविष्य। लेकिन अंदर ही अंदर वह हिलोरें ले रही थी। मदद मांगने से पहले वह महीनों तक झिझकती रही, उसे डर था कि अपने संघर्षों को स्वीकार करने से वह कमजोर दिखाई देगी। फैसले का यह डर कई लोगों को मदद मांगने से रोकता है, और यह देखकर दिल दहल जाता है कि शहरी परिवेश में यह कितना आम है। हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य एक बाद का विचार बना हुआ है। हम शारीरिक लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं - हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्थितियों का इलाज - लेकिन लोगों के भावनात्मक भार को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैंने लोगों को वर्षों तक चुपचाप पीड़ा सहते देखा है, उन्हें लगता है कि उनका भावनात्मक दर्द उचित नहीं है क्योंकि इसे शारीरिक बीमारी की तरह नहीं मापा जा सकता है। परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है. भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली इस विभाजन को प्रतिबिंबित करती है। शहरों में, निजी देखभाल विकल्प प्रदान करती है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ अभी भी सीमित और महंगी हैं। ग्रामीण इलाकों में मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा भी कम ही होती है। सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ, विशेषकर महिलाओं के लिए, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच को और भी कठिन बना देती हैं।
महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य - भावनात्मक और शारीरिक दोनों - को ताक पर रख देती हैं और अपने परिवार की ज़रूरतों को अपने ऊपर प्राथमिकता देती हैं। मेरी एक मरीज़, जो दो बच्चों की माँ थी, ने अपनी चिंता के लिए वर्षों तक मदद माँगने में देरी की। वह थक गई थी, अभिभूत थी और अपनी सुध-बुध खो रही थी। लेकिन कई महिलाओं की तरह, वह भी यह सोचने के लिए दोषी महसूस करती थी कि उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह एक आम कहानी है - भारत में बहुत सी महिलाएं चुपचाप मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों को सहन करती हैं, अपनी जरूरतों को महत्वहीन मानकर खारिज कर देती हैं, और इस प्रक्रिया में खुद को अलग कर लेती हैं। हमें इस आख्यान को बदलने की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य कोई विलासिता या कमज़ोरी का प्रतीक नहीं है। यह समग्र कल्याण का एक अभिन्न अंग है। हमें अपनी बातचीत और अपनी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। केवल तभी हम भारत में स्वास्थ्य चुनौतियों के पूर्ण दायरे का समाधान कर सकते हैं - क्योंकि वास्तविक उपचार केवल शरीर के बारे में नहीं है; यह मन के बारे में भी है। विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब [4) सोच बदलने से मिलेगी सफलता विजय गर्ग हमारी सोच वो नींव है, जिसके आधार पर जीवन में हम सफल या असफल होते हैं। आपकी सोच ही आपके यथार्थ को आकार देती है, निर्णयों को प्रभावित करती है और आपके कर्म निर्धारित करती है, जो परिणाम के रूप में आपके सामने आते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते हैं क्योंकि उनके भीतर योग्यता, ज्ञान या अवसरों की कमी होती है। वे इसलिए असफल होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सोच की ताकत के बारे में पता ही नहीं होता है। आइए जानते हैं कि सही सोच कैसे आपकी सफलता में बाधा बननेवाले कारणों को दूर कर सकती है- स्वयं पर संदेह है बाधक 'आपका दिमाग बहुत शक्तिशाली है।
इसलिए जब आप सकारात्मक तरीके से सोचने लगते हैं, तो जीवन में परिवर्तन आने लगता है।' अज्ञात अधिकांश लोग यह समझ ही नहीं पाते कि अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा वह स्वयं हैं। खुद पर संदेह करना आपके दिमाग में गूंजती वो आवाज है, जो आपको यकीन दिलाती है कि आप अच्छे नहीं हैं, आपके अंदर योग्यता की कमी है और आप सफलता के योग्य पात्र नहीं हैं। असल में हारने का डर, अस्वीकृत कर दिए जाने का भय या कोई भी अनजाना डर संकीर्ण और दबी हुई मानसिकता का ही परिणाम है, जो सफलता में बाधक बनता है। लेकिन इससे बचा जा सकता है। एक कागज पर अपने उन विचारों को लिखिए, जो आपकी उन्नति में बाधक हैं। फिर उन्हें चुनौती दीजिए। गौर कीजिए कि आप उन विचारों को कैसे बदल सकते हैं? प्रगतिशील सोच का महत्व उन्नत सोच आपको चुनौतियों से लड़ने का हौसला और हार को सीखने के नए अवसर के रूप में देखने में मदद करती है। खुली सोच रखनेवाले लोग जानते हैं कि वह अपनी मेहनत के बल पर तरक्की के नए रास्ते बना ही लेंगे। निम्न सूत्रों की मदद से अपनी सोच को उन्नत बनाया जा सकता है। चुनौतियों से बचने की बजाय उन्हें स्वीकारिए ।
■ असफल होने पर हार मान लेने की बजाय दोबारा प्रयास करें।
■ अपने प्रयासों को अपनी कमजोरी समझने की बजाय दक्षता हासिल करने का मार्ग समझें।
■ आलोचना की अनदेखी करने की बजाय उससे सबक लें। प्रगतिशील सोच के साथ बाधाएं और असफलता भी सफलता का मंत्र बन जाते हैं। क्योंकि तब आप उन्हें बाधा समझने की बजाय सीखने के नए अवसरों के रूप में स्वीकारने लगते हैं। सोच बदलना है जरूरी जकड़ी हुई सोच को प्रगतिशील विचारधारा में बदलना जरूरी तो है, लेकिन यह सरल नहीं है। निम्न बातें ऐसा करने में सहायक हो सकती हैं। छोटी शुरुआत सबसे पहले किसी एक संकीर्ण विचार को बदल कर उन्नत विचार बनाने के प्रयास करें। हार से सबक: अपनी असफलता को अंतिम परिणाम समझने की बजाय उसे सीखने के एक नए अवसर के रूप में देखें। कृतज्ञता का भाव अपने जीवन की उन बातों पर ध्यान दें, जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। इससे आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ेगी। अच्छी सोचवालों का साथ जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, वह आपकी सोच पर भी बहुत प्रभाव डालते हैं। इसलिए खुली सोचवाले लोगों के सानिध्य में रहें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें।
सफलता भी मिलेगी जीवन में सफलता और आपके बीच सिर्फ आपकी सोच ही खड़ी होती है। इसलिए, अपनी सोच को बेहतर बनाकर आप हर बाधा को पार कर सकते हैं और अपनी मर्जी से अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी पहचान आपके अतीत की गलतियों या वर्तमान की सीमाएं नहीं हैं बल्कि उनसे आप क्या सीखते हैं, इस बात से आपकी पहचान बनती है। प्रयासों से मिलेगी मंजिल सोच में बदलाव रातोरात तो संभव नहीं है लेकिन छोटे- छोटे कदमों से मंजिल तक जरूर पहुंचा जा सकता है। अपने विकास में बाधक विचारों को बदलने का प्रयास कीजिए, ताकि संभावनाओं के मार्ग पर चला जा सके। इसलिए स्वयं से निम्न प्रश्न पूछें- कौन से विचार मेरे आगे बढ़ने में बाधक बन रहे हैं? ■ अपनी असफलता को मैं सीखने के नए अवसर के रूप में कैसे बदल सकता हूं? मेरी कौन-सी आदतें विकसित सोच बनाने में मदद कर सकती हैं? इन सवालों के उत्तर जान लेने के बाद आपके लिए अपनी योग्यता को समझना आसान लगने लगेगा।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब