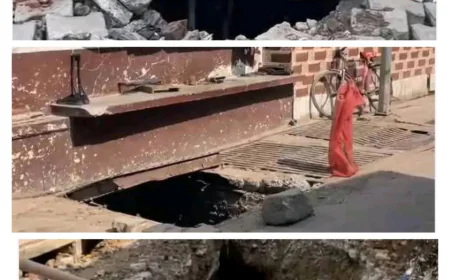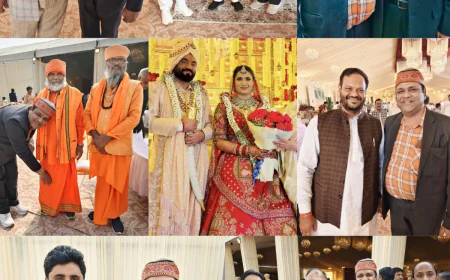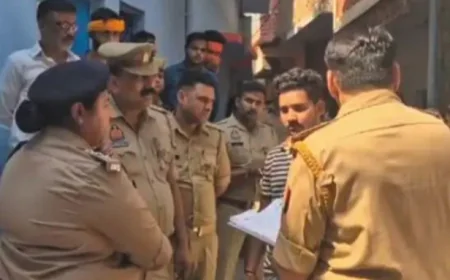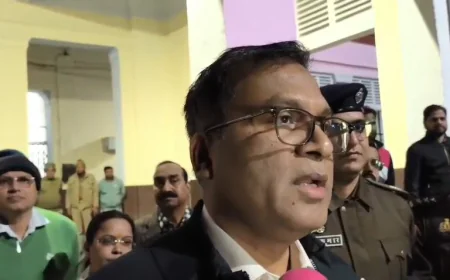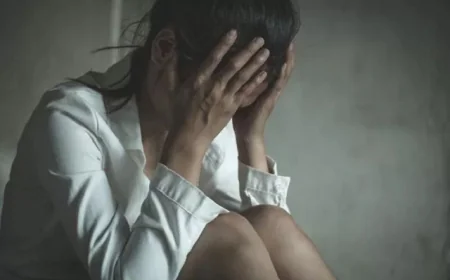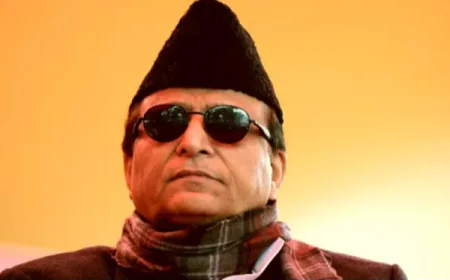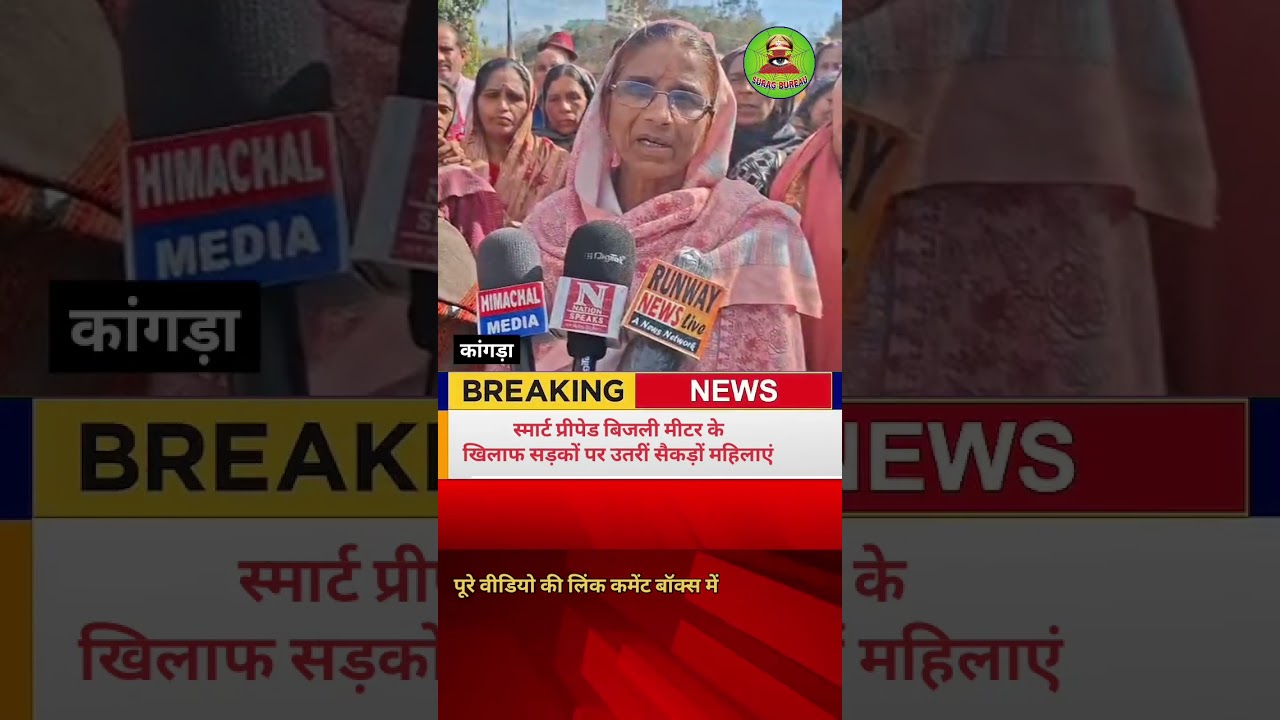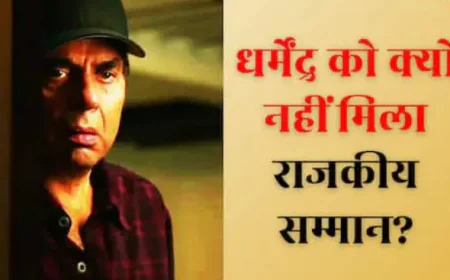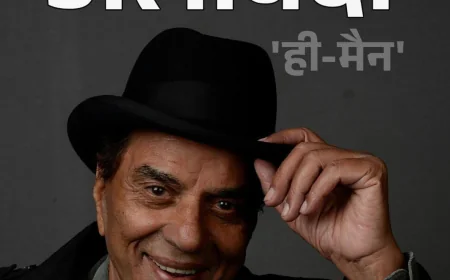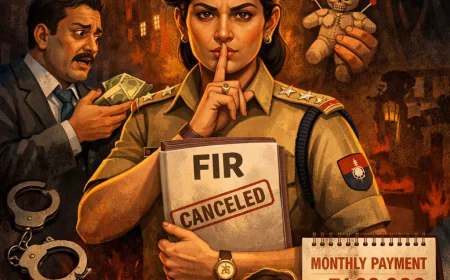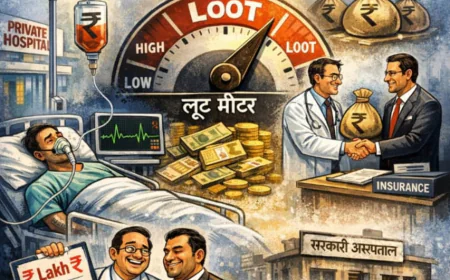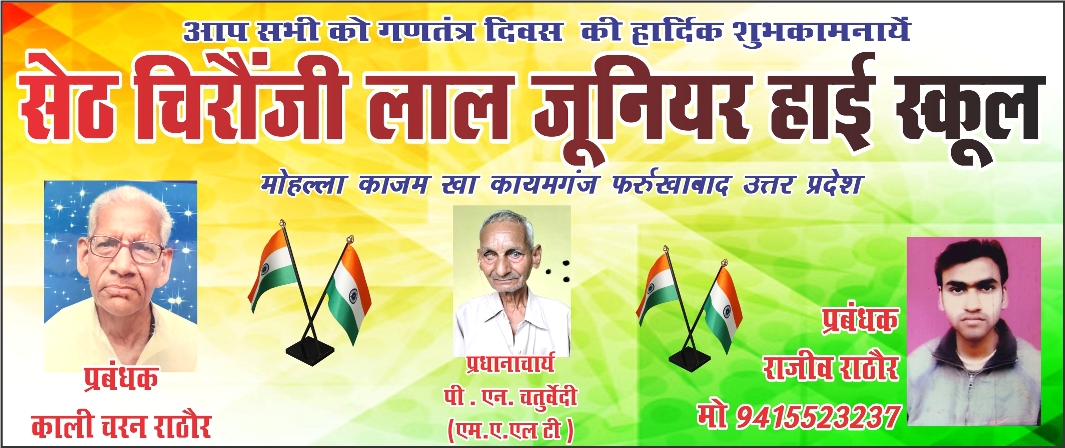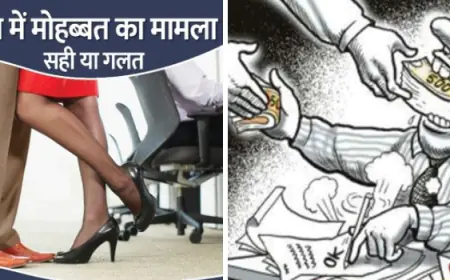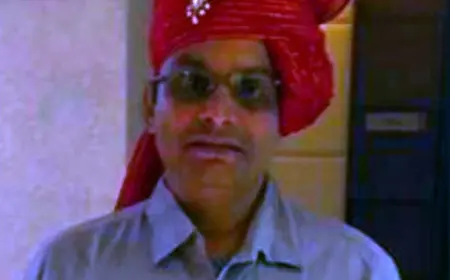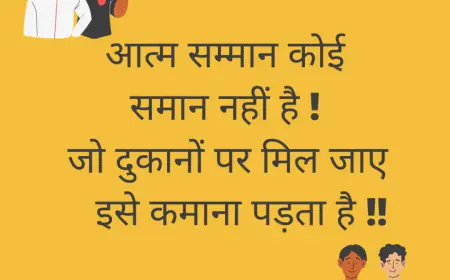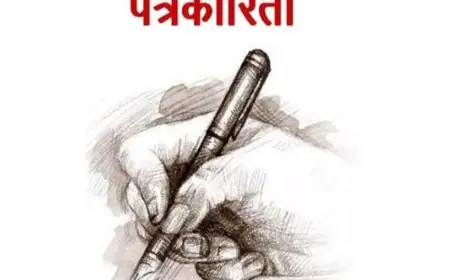कौशल आधारित शिक्षा की ओर ओर बढ़े भारत

कौशल आधारित शिक्षा की ओर ओर बढ़े भारत
अगर आपकी नौकरी की परिभाषा केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित है, तो निश्चित रूप से भारत में नौकरियों का संकट है। डिजिटलीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के नेतृत्व में स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) के बढ़ते उपयोग के साथ, भविष्य में सरकारी नौकरियों की संख्या में और कमी आने की संभावना है। लेकिन अगर नौकरी का मतलब निजी क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार है, तो कोई संकट नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था तीन दशक से लगातार 6 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ रही 1 है, और नौकरियों पैदा हो रही हैं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवाओं का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हिस्सा लगभग 55 प्रतिशत, उद्योग का 27 प्रतिशत और कृषि का 17 प्रतिशत है और पिछले 10 वर्षों में, ये सेवाएं ही हैं जो 7-9 प्रतिशत की दर से बढ़ रही हैं, जबकि उद्योग 4-6 प्रतिशत और कृषि 3-5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, भारत को 2030 तक सालाना लगभग 78.5 लाख नए गैर कृषि रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। यह आंकड़ा स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने और जनसंख्या लाभांश का लाभ उठाने के लिए आवश्यक रोजगार सृजन के विशाल पैमाने को रेखांकित करता है। तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण विनिर्माण क्षेत्र में नए रोजगार सृजन के अवसर सीमित हैं। यही कारण हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 लाख करोड़ रुपये के कुल आवंटन के साथ रोजगार- लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना शुरू की। इस योजना का लक्ष्य दो वर्षों (अगस्त 2025 से जुलाई 2027 के बीच) के भीतर देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। लेकिन सेवा क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा से उतना प्रभावित नहीं होता और इसीलिए उसकी वृद्धि दर उद्योग और कृषि की तुलना में दोगुनी है। सेवा क्षेत्र के प्रमुख चालक आइटी और आइटी-सक्षम व्यवसाय, वित्तीय व्यवसाय, रियल एस्टेट, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार रहे हैं। डिजिटल परिवर्तन ने विशेष रूप से आइटी और संबंधित सेवाओं के विकास को बढ़ावा दिया है। सेवा निर्यात में भी सफलता मिल रही है। इस क्षेत्र में संभावनाएं अत्यधिक हैं। चुनौती यह है कि युवाओं को उन क्षेत्रों में स्किल प्रदान करें जहां उनकी आवश्यकता है और विस्तार की अधिक संभावनाएं हैं। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ( 2023-24 ) की वार्षिक रिपोर्ट स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह सार्वजनिक धारणा है, जो कौशल को उन लोगों के लिए अंतिम उपाय मानती है जो औपचारिक शैक्षणिक प्रणाली में प्रगति नहीं कर पाए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, 20 केंद्रीय मंत्रालय कौशल विकास कार्यक्रम चला रहे हैं लेकिन उनमे समन्वय की कमी है। मांग-आपूर्ति बेमेल है। साथ ही, सीमित गतिशीलता है जो कुशल व्यक्ति को औपचारिक उच्च शिक्षा में जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। हाल ही में, हमने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सकल घरेलू उत्पाद को चारगुना करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन किया और कौशल से संबंधित मुद्दों की जांच की। कालेजों के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समझ और कार्यान्वयन में कमी स्पष्ट थी। कौशल विकास के उद्देश्यों के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में प्रणालीगत चुनौतियां आती हैं, खासकर बुनियादी ढांचे, संसाधन आवंटन और विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण के संबंध में छात्रों और उनके माता-पिता को विभिन्न क्षेत्रों में उभरते हुए नौकरी के अवसरों से अवगत कराना और उन्हें उपयुक्त कौशल प्रदान करने वाले संस्थान का चयन करने में मदद करना बहुत मुश्किल काम नही है। यह प्रत्येक शहर में समय-समय पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को आमंत्रित करके कौशल परामर्श मेलों का आयोजन करके किया जा सकता है। इसलिए, न तो नौकरियों की कमी है और न ही कौशल की, बल्कि आवश्यकता समाज को कौशल आधारित शिक्षा की ओर उन्मुख करने की है ताकि छात्रों को सही प्रकार की नौकरियों के लिए कुशल बनाया जा सके। ऐसा करके ही भारत न सिर्फ अपनी युवा आबादी को उत्पादक बना सकेगा बल्कि इससे देश के आर्थिक विकास को वह गति मिलेगी, जिसकी जरूरत इस समय महसूस की जा रही है। युवाओं को जब नौकरी मिलती है तो वह सैलरी खर्च करते हैं, घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं और जरूरत की दूसरी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं। उनका जीवन स्तर बेहतर होता है। इससे मांग बढ़ती है और अर्थव्यवस्था का चक्का तेजी घूमता है।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब