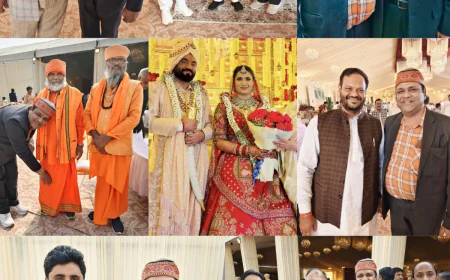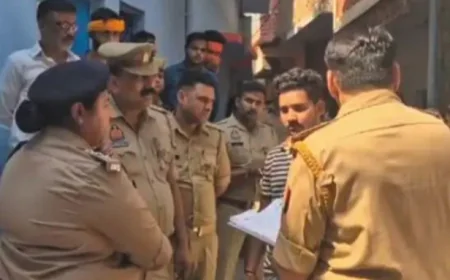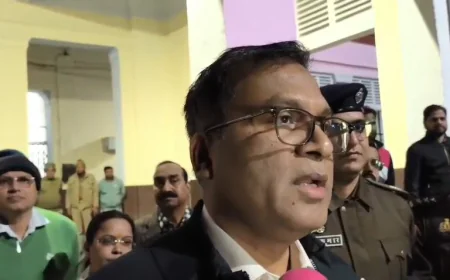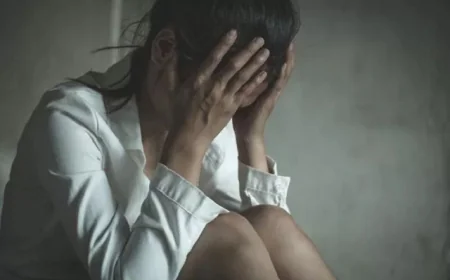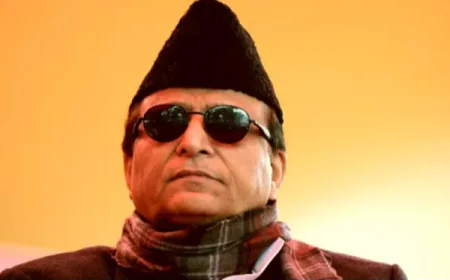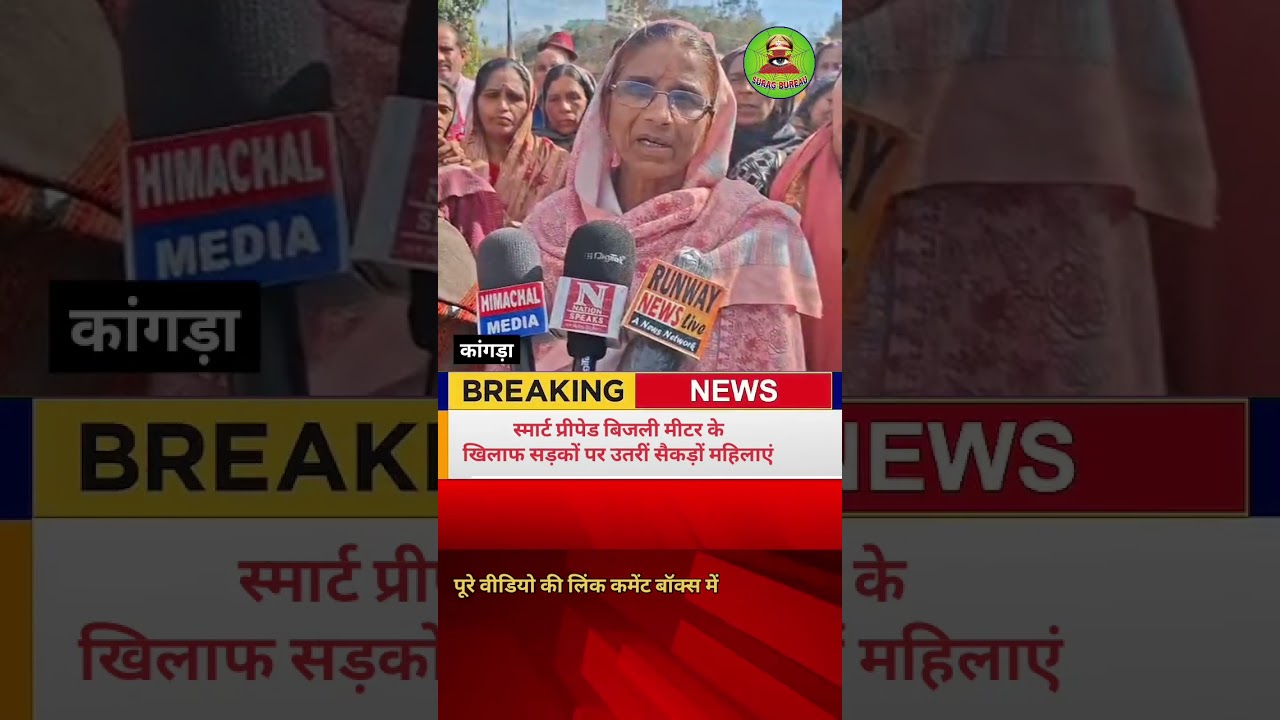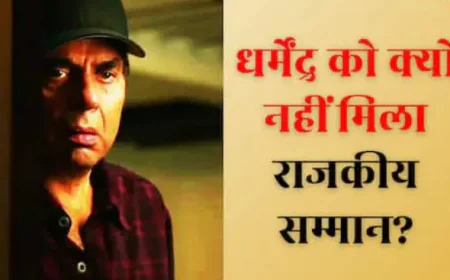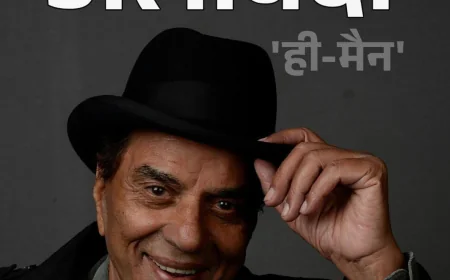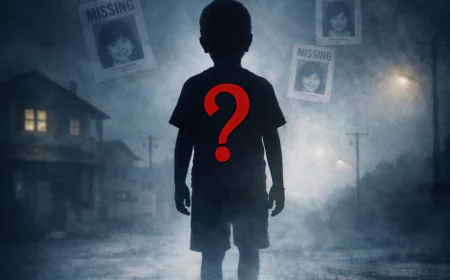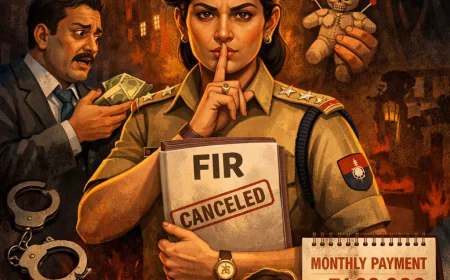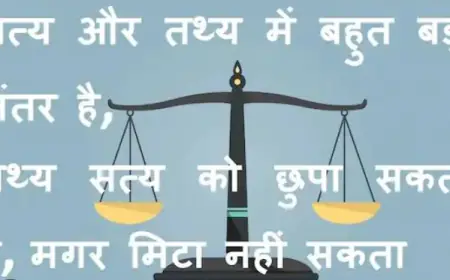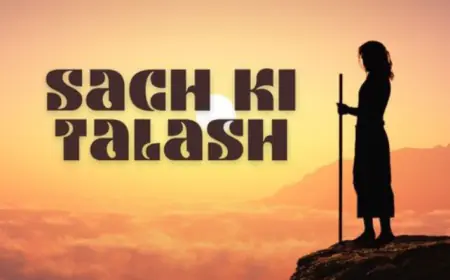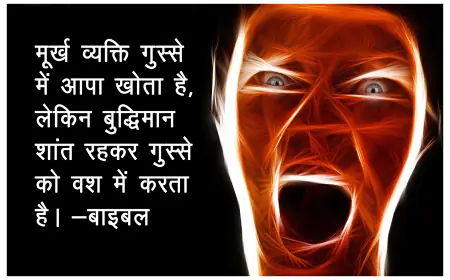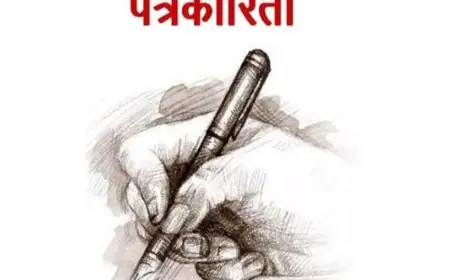किताबें पढ़ने से आपके मस्तिष्क में क्या परिवर्तन होता है

हमारे मस्तिष्क की संरचना, रसायन विज्ञान या भौतिकी के बारे में कोई भी जानकारी पढ़ने से अछूती नहीं रहती। स्पेन के न्यूरोलॉजिस्ट फ्रांसिस्को मोरा के अनुसार, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो किताब या जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसने आपकी रुचि जगाई है या नहीं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने आपकी भावनाओं को कितना प्रभावित किया है।
आठ साल पहले प्रकाशित अपनी पुस्तक "न्यूरोएजुकेशन" में मोरा कहते हैं, "आप केवल वही सीख सकते हैं जो आपको पसंद है।" यह पुस्तक इस बात पर आधारित है कि मस्तिष्क विज्ञान किस प्रकार लोगों के सीखने और सिखाने के तरीके को बेहतर बना सकता है। पिछले वर्ष, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर (मोरा) ने अपनी पिछली सफल पुस्तक के मुख्य विषय पर विस्तार करते हुए, "न्यूरोएजुकेशन एंड रीडिंग" नामक एक अन्य पुस्तक भी प्रकाशित की। इस नई पुस्तक में, उन्होंने पढ़ने की क्षमता को मानवता के लिए एक सच्ची क्रांति के रूप में परिभाषित किया है। पढ़ना एक कृत्रिम और हालिया प्रक्रिया है। मोरा कहते हैं, "हमने लगभग 2 से 3 मिलियन वर्ष पहले आनुवंशिक उत्परिवर्तन के माध्यम से बोलने की क्षमता हासिल की थी।" तब से, मनुष्य बोलने के लिए आवश्यक तंत्रिका सर्किट के साथ पैदा हुआ है, हालांकि बोलना केवल दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। फ्रांसिस्को मोरा ने चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वे तंत्रिका विज्ञान के डॉक्टर हैं।
'न्यूरोएजुकेशन एंड रीडिंग' में वे लिखते हैं, 'हम एक मस्तिष्क डिस्क के साथ पैदा होते हैं जिस पर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। "लेकिन अगर हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो यह खाली ही रहेगा।" दूसरी ओर, पढ़ना लगभग 6,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आया, जब हमें अपनी जनजाति के बाहर संवाद करने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि बोले गए शब्दों की पहुंच सीमित थी। इसके अलावा, इसका आधार आनुवंशिक नहीं बल्कि सीखा हुआ या सांस्कृतिक है। मोरा अपनी पुस्तक में बताते हैं, "पढ़ना एक ऐसी प्रक्रिया है जो वंशानुगत (जीन में) नहीं होती है और इसलिए यह स्वचालित रूप से अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच सकती है।" "यह ऐसी चीज़ है जिसे हर इंसान को स्वयं सीखना होगा, जिसके लिए हर बार सीखने और याद रखने की ज़रूरत होती है।" अच्छी तरह से या अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए प्रयास, ध्यान, स्मृति और स्पष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और यदि आप बहुत अधिक पढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इसके लिए समर्पित करना होगा। हालांकि, वे कहते हैं कि 'महंगा' और 'कड़ी मेहनत' का मतलब यह नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। हालाँकि, जब मोरा चार साल का था, तो उसे पढ़ाई में लापरवाही बरतने के कारण स्कूल से सज़ा मिलनी शुरू हो गई। इसका कारण यह था कि मोरा के शिक्षकों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बच्चे का मस्तिष्क कैसे काम करता है।
तेजी से पढ़ना सीखने से आप अधिक बुद्धिमान नहीं बन जाते। मोरा के अनुसार, बच्चे मां के गर्भ से ही "सीखने की मशीन" होते हैं। बल्कि, "मनुष्य को लगभग सब कुछ सीखना पड़ता है।" पढ़ना सीखना बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसे लेकर कभी-कभी माता-पिता को गर्व होता है तो कभी-कभी चिंता भी होती है। वे कहते हैं, "जब एक माँ को पता चलता है कि उसका 5 साल का बच्चा पढ़ना सीखने में संघर्ष कर रहा है, जबकि उसके पड़ोस में रहने वाला 4 साल का बच्चा अच्छे अंकों से पढ़ रहा है, तो वह माँ स्वयं से पूछ सकती है - क्या मेरा बच्चा इतना मूर्ख है?" तंत्रिका विज्ञान ने दर्शाया है कि मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को पढ़ना सीखने के लिए पहले से परिपक्व होना पड़ता है। यह 3 वर्ष की आयु में भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर 6 या 7 वर्ष की आयु इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इस कारण से, वे लिखते हैं, यह अनुशंसा की जाती है कि औपचारिक पठन निर्देश 7 वर्ष की आयु से शुरू हो, "एक ऐसी आयु जिस पर, लगभग निश्चित रूप से, सभी बच्चों ने पढ़ने के लिए आवश्यक घटकों का विकास कर लिया होगा और वे पढ़ना सीखने के पूर्ण अर्थ और निहितार्थ को समझने में सक्षम हो जाते हैं।" "शिक्षा के मामले में फिनलैंड को बहुत उन्नत माना जाता है और वहां बच्चे इसी उम्र में पढ़ना सीखना शुरू कर देते हैं।" न्यूरोएजुकेशन के महत्व को समझाते हुए मोरा कहते हैं कि शिक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। दूसरा पहलू यह है कि बच्चों को छोटी उम्र में सीखने और अध्ययन करने के लिए मजबूर करने से उन पर अनावश्यक बोझ पड़ता है और वे चिंतित हो जाते हैं। इस मामले में प्रयुक्त 3-4 वर्ष की जल्दबाजी का भविष्य के संदर्भ में कोई विशेष महत्व नहीं है।
सीधे शब्दों में कहें तो, इससे आपकी पढ़ाई में कोई मदद नहीं मिलती और न ही यह आपको अधिक बुद्धिमान बनाता है। मोरा के अनुसार, मस्तिष्क की परिपक्वता में एक मौलिक आनुवंशिक घटक होता है, लेकिन एक सांस्कृतिक घटक भी होता है जो घर से जुड़ा होता है। ऐसे माता-पिता के साथ बड़ा होना जो स्वयं पढ़ते हैं या आपके लिए पढ़कर सुनाते हैं, "एक भावनात्मक पहलू होता है जो पढ़ना सीखने में बहुत मदद करता है।" इंटरनेट ध्यान भटकाने वाला है। "न्यूरोएजुकेशन एंड रीडिंग" में मोरा लिखते हैं, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंटरनेट एक सफल क्रांति रही है, जिसने एक ऐसे "डिजिटल युग" की शुरुआत की है, जहां पढ़ने की प्रक्रिया में न केवल तेजी आई है, बल्कि इसमें नाटकीय बदलाव भी आया है।" हालाँकि, एक अध्ययन में कुछ नकारात्मक पहलू भी सामने आए हैं कि इंटरनेट किस प्रकार युवा और बढ़ते बच्चों के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। यह देखा गया है कि इंटरनेट के प्रभाव से बच्चों में सहानुभूति में कमी से लेकर निर्णय लेने की क्षमता में कमी तक के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। "न्यूरोएजुकेशन" में मोरा बताते हैं कि पढ़ाई करते समय हमें मस्तिष्क को अनावश्यक विचारों से बचाना होता है। कभी-कभी आपको अपने 99% विचारों को रोककर सिर्फ 1% पर ध्यान केंद्रित करना होता है। आपके पास पढ़ाई के लिए भी पर्याप्त समय होना चाहिए।
इसकी तुलना में, इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय आपको उतनी मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती। आप इंटरनेट पर अधिकांश चीजों को केवल सरसरी निगाह से देखते हैं। पढ़ना भी योजना बनाने जैसी ही एक प्रक्रिया है, जिसमें आपको कुछ भी याद नहीं रहता। क्या बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजना जरूरी है? फ़िनिश स्कूल किताबों और कक्षाओं से मुक्त मोबाइल लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का विचार कहां से आया? विद्यार्थी इस प्रकार, जबकि हम इंटरनेट पर सरसरी तौर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, पढ़ते समय हमारा ध्यान लंबे समय तक केंद्रित और बना रहता है। ऐसे भी लोग हैं जो ध्यान के एक नए रूप के बारे में बात करते हैं और इसे डिजिटल कहते हैं। मोरा मानते हैं कि आज किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की जन्मतिथि याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गूगल यह कार्य तुरन्त और अधिक सटीकता के साथ कर देता है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि स्मृति केवल कक्षाओं तक ही सीमित है। वे कहते हैं, "आपको बहुत कुछ याद रखना होगा, क्योंकि आपकी यादें ही आपको बनाती हैं।" "क्या किसी याद की हुई कविता या साहित्य की कुछ पंक्तियों से अपनी बात को सजाना बेहतर नहीं होगा?" पढ़ने से आपका मस्तिष्क बदलता है (और आप भी) हालाँकि, हमारा मस्तिष्क आनुवंशिक रूप से पढ़ने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन इस अनोखे अंग में इस कौशल को सीखने के लिए आवश्यक लचीलापन हासिल करने की अद्वितीय क्षमता है। शायद इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि पढ़ने से मस्तिष्क के उस हिस्से में अधिक सक्रियता होती है जो वास्तव में आकृतियों और चेहरों को पहचानने के लिए जिम्मेदार होता है। समय के साथ-साथ वही भाग शब्दों को बनाने और पहचानने भी लगता है। "न्यूरोएजुकेशन" में मोरा लिखते हैं, "बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों में बच्चे के मस्तिष्क की भौतिक, रासायनिक और तंत्रिका संरचना को बदलने की क्षमता होती है।
इसके परिणामस्वरूप नए तंत्रिका सर्किटों का निर्माण होता है जो छात्र के व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देते हैं। बाद में, "न्यूरोएजुकेशन एंड रीडिंग" में, उन्होंने बताया, "एक व्यक्ति न केवल अपने अनुभवों के आधार पर बदलता है, बल्कि वह जो पढ़ता है उसके आधार पर भी बदलता है।" वे आगे कहते हैं, "पढ़ना केवल एक नीरस गतिविधि नहीं है जिसमें किसी विशेष पुस्तक या दस्तावेज़ का पाठ पढ़ा जाता है, बल्कि यह एक सक्रिय गतिविधि है।" यदि आप चाहें तो पढ़ना, पाठ में कही गई किसी भी बात को पुनः रचने की क्रिया है। इसमें "एक संज्ञानात्मक क्षेत्र का निर्माण करना शामिल है जिसमें रुचि, ध्यान, सीखना, याद रखना, भावनाएं, जागरूकता, ज्ञान और परिवर्तन शामिल हैं।
आईआईटी बनाम एनआईटी बनाम आईआईआईटी: क्या अंतर है?
आईआईटी की कोई तुलना नहीं है। आईआईटी- जेईई को दुनिया भर में सबसे कठिन परीक्षा में से एक माना जाता है और इसलिए आईआईटी सबसे अच्छे हैं। अब एनआईटी बनाम आईआईआईटी की तुलना करने के लिए आ रहा है, मेरे विचार में मैंने निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया है: आईआईआईटी (भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) को अक्सर कई कारकों के कारण कंप्यूटर विज्ञान और संबद्ध पाठ्यक्रमों (जैसे आईटी, एआई, डेटा साइंस, आदि) के लिए एनआईटी (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) से बेहतर माना जाता है। 1.। कंप्यूटर विज्ञान और आईटी पर कोर फोकस आईआईआईटी आईटी और सीएस क्षेत्रों के लिए समर्पित हैं, जबकि एनआईटी इंजीनियरिंग विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। इस फोकस के कारण, आईआईआईटी में अक्सर सीएस से संबंधित क्षेत्रों में बेहतर संकाय, अनुसंधान के अवसर और उद्योग सहयोग होते हैं।
कई आईआईआईटी उद्योग-संचालित हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका पाठ्यक्रम एआई, एमएल, ब्लेकचैन और कलोड कऊपिटर जैसी आधुनिक तकनीकों से अपडेट किया गया है। 2.। मजबूत उद्योग कनेक्शन और प्लेसमेंट आईआईआईटी ,विशेष रूप से आईआईआईटी हैदराबाद, आईआईआईटी बैंगलोर और आईआईएम दिल्ली जैसे शीर्ष लोगों के उत्कृष्ट उद्योग संबंध हैं। गुगल, मोकरोसॉफ़्टवेयर एमजोन और एडबर जैसी कंपनियां अपने विशेष प्रशिक्षण के कारण सॉफ़्टवेयर भूमिकाओं के लिए अधिकांश एनआईटी पर आईआईआईटी पसंद करती हैं। उदाहरण के लिए, आईआईआईटी हैदराबाद के पास भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों के बीच सीएसई के लिए उच्चतम औसत पैकेजों में से एक है, यहां तक कि आईआईटी से भी प्रतिस्पर्धा है। 3। सीएस फील्ड्स में बेहतर कोडिंग कल्चर एंड रिसर्च आईआईआईटी में एक बहुत मजबूत कोडिंग संस्कृति है, जिसमें प्रतियोगी प्रोग्रामिंग ( गुगल कोड जैम, एसीएम आईसीपीसी ) और हैकथॉन में उत्कृष्ट छात्र हैं। वे सीएस में अनुसंधान और नवाचार पर भी बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं, दुनिया भर में एआई, एमएल और डेटा साइंस अनुसंधान में योगदान करते हैं। आईआईआईटी हैदराबाद, विशेष रूप से, वैश्विक विश्वविद्यालयों के प्रतिद्वंद्वी अनुसंधान केंद्र ( सीवीआईटी, एमएल लेव, वालक लेव, आदि) हैं। 4। लचीला और आधुनिक पाठ्यक्रम आईआईआईटी में आमतौर पर एक अधिक लचीला पाठ्यक्रम होता है, जिससे छात्रों को ऐआई, साइबरस्पेस और डेटा साइंस जैसे ट्रेंडिंग क्षेत्रों में ऐच्छिक लेने की अनुमति मिलती है।
कुछ आईआईआईटी में कोई सख्त शाखा प्रणाली नहीं है, जिससे छात्र कई सीएस क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इसके विपरीत, एनआईटी एक अधिक पारंपरिक पाठ्यक्रम का पालन करते हैं, जो सीएस नवाचारों के लिए अद्यतन नहीं हो सकता है। 5.। उच्च कोडिंग और प्रतिस्पर्धी प्रोग्रामिंग रैंकिंग आईआईआईटी के छात्र अक्सर गुगल समर ऑफ कोड , एसीएम आईसीपीसी और कोडफोरस रैंकिंग पर हावी होते हैं। आईआईआईटी हैदराबाद, आईआईआईटी इलाहाबाद और आईआईआईटी दिल्ली अपनी मजबूत प्रतिस्पर्धी कोडिंग संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, अक्सर एनआईटी को बेहतर बनाते हैं। जब एनआईटी एक बेहतर विकल्प हो सकता है जबकि आईआईआईटी सीएस के लिए उत्कृष्ट हैं, कुछ मामले हैं जहां एक एनआईटी बेहतर हो सकता है: यदि गैर-सीएस शाखा पर विचार किया जाता है, तो एनआईटी बेहतर हैं क्योंकि आईआईआईटी मुख्य रूप से सीएस और संबंधित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एनआईटी त्रिची, एनआईटी सुरथकल और एनआईटी वारंगल जैसे शीर्ष एनआईटी में सीएसई में उत्कृष्ट प्लेसमेंट हैं, कभी-कभी नए आईआईआईटी से बेहतर होते हैं। एनआईटी में एक मजबूत पूर्व छात्र नेटवर्क है, जो विभिन्न कैरियर के अवसरों में मदद कर सकता है। एनआईटी बेहतर परिसर जीवन और बुनियादी ढांचे की पेशकश करते हैं, क्योंकि आईआईआईटी में अक्सर छोटे परिसर होते हैं। सीएसई और संबद्ध पाठ्यक्रमों के लिए, आईआईआईटी हैदराबाद, आईआईआईटी दिल्ली और आईआईआईटी बैंगलोर जैसे शीर्ष आईआईआईटी आमतौर पर अपनी मजबूत कोडिंग संस्कृति, प्लेसमेंट, अनुसंधान और उद्योग सहयोग के कारण अधिकांश एनआईटी की तुलना में बेहतर विकल्प हैं।
हालांकि, समग्र परिसर जीवन, सरकारी धन और गैर-सीएस शाखाओं के लिए, शीर्ष एनआईटी बेहतर हो सकते हैं। विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्राचार्य शैक्षिक स्तंभकार गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब -----------+-----------+------------------------- [3) मस्तिष्क और मन के बीच अंतर विजय गर्ग मस्तिष्क एक भौतिक अंग है जो सूचना को संसाधित करता है और शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जबकि मन चेतना, विचारों और भावनाओं को शामिल करने वाली एक अमूर्त अवधारणा है। हालांकि परस्पर जुड़े हुए हैं, वे प्रकृति और कार्य में भिन्न होते हैं। इस अंतर को समझने से अनुभूति, धारणा और मानसिक और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं के बीच जटिल संबंध की खोज करने में मदद मिलती है। "मस्तिष्क" और "मन" शब्दों को आमतौर पर पर्यायवाची शब्द माना जाता है, लेकिन वे दो विचार हैं जो लंबे समय से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के बीच तर्क किए जाते हैं। इन दोनों के बीच भेदभाव यह समझने में मदद कर सकता है कि हम अपने आसपास की चीजों को कैसे देखते हैं, प्रक्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। मस्तिष्क: शारीरिक इकाई मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर पाया जाने वाला एक ठोस, भौतिक अंग है। इसमें अरबों तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स होते हैं, जो जानकारी को संसाधित करने और शरीर के विभिन्न कार्यों को विनियमित करने के लिए जटिल नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ आते हैं। मस्तिष्क शरीर की केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के रूप में काम करता है, आंदोलनों को विनियमित करता है, भावनाओं का प्रबंधन करता है, और सीखने और स्मृति जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को सक्षम करता है। इसे कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जैसे कि सेरेब्रम, सेरिबैलम और ब्रेनस्टेम, प्रत्येक एक अलग कार्य के साथ, जैसे मोटर नियंत्रण, संवेदी व्याख्या और स्वायत्त विनियमन।
मन: विचारों, भावनाओं, चेतना और धारणा से जुड़ी एक गैर-भौतिक इकाई। स्मृति, कल्पना, तर्क और निर्णय लेने में शामिल है। मस्तिष्क की तरह सीधे देखा या मापा नहीं जा सकता। अक्सर मनोविज्ञान, दर्शन और संज्ञानात्मक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। सादृश्य: मस्तिष्क एक कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह है, जबकि मन अपने सॉफ्टवेयर की तरह है। मस्तिष्क शारीरिक संरचना प्रदान करता है, लेकिन मन वह है जहां विचार और अनुभव होते हैं। विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्राचार्य शैक्षिक स्तंभकार गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब ----+-------------------+---+++----------;------------ [4) पढ़ते समय क्यों सो जाता हूँ? विजय गर्ग आपने अक्सर माता-पिता को यह शिकायत करते देखा होगा कि उनके बच्चे किताबें खोलते ही सो जाते हैं। ऐसा केवल छात्रों के साथ ही नहीं बल्कि वयस्कों के साथ भी होता है। जैसे ही आप अखबार या किताब पढ़ना शुरू करते हैं, आपकी आंखें नींद से भर जाती हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है... कुछ लोग कम सोते हैं जबकि कुछ लोग ज्यादा सोते हैं। वैसे, जिन लोगों को नींद आने में परेशानी होती है, अगर उन्हें किताबें पढ़ने को दी जाएं तो वे सोने लगते हैं या झपकी लेने लगते हैं। हालाँकि, यह समस्या पढ़ने वाले बच्चों में अधिक आम है। हालांकि माता-पिता बच्चों की इस समस्या पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों की इस समस्या पर ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए जो भी उपाय अपनाए जा सकते हैं, उन्हें अपनाकर नींद न आने की समस्या को खत्म करना जरूरी है, अन्यथा यह आपकी याददाश्त का दुश्मन बन जाएगा। अब बात करते हैं सोते समय नींद आने के विज्ञान की। दरअसल, जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारी आंखों पर अधिक दबाव पड़ता है, जबकि मस्तिष्क कंप्यूटर की मेमोरी की तरह डेटा फीड करता है। ऐसी स्थिति में आंखों की मांसपेशियां शिथिल होने लगती हैं और कुछ ही देर में हमारा मस्तिष्क काम करने से मना करने लगता है और हमें नींद आने लगती है। पढ़ाई करते समय नींद आने से बचने के लिए अध्ययन क्षेत्र में अच्छी रोशनी रखनी चाहिए। पढ़ाई के लिए ऐसा स्थान चुनें जहां बाहरी हवा और रोशनी आती हो, ताकि शरीर तरोताजा रहे। दूसरा कारण यह है कि पढ़ते समय हमारा अधिकांश शरीर आराम की स्थिति में होता है और केवल मस्तिष्क और आंखें ही काम कर रही होती हैं। ऐसी स्थिति में पूरे शरीर को आराम देने से मांसपेशियां शिथिल होने लगती हैं और व्यक्ति को नींद आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक आसन में बैठकर पढ़ना चाहिए। कभी भी बिस्तर पर न पढ़ें, बल्कि कुर्सी या मेज पर बैठकर किताबें पढ़ने का अभ्यास करें। कुर्सी और मेज को देखकर पढ़ाई के लिए मन तैयार होगा और आलस्य रुकेगा।
पढ़ाई करने से पहले हल्का भोजन करें ताकि आपको सुस्ती महसूस न हो क्योंकि खाने के बाद भी आपको नींद आती है। जब भी हमारा शरीर आराम करता है, तो वह नींद की अवस्था में चला जाता है। सिर्फ पढ़ते ही नहीं, आपने लोगों को कार में यात्रा करते समय सोते हुए भी देखा होगा। यहां भी वही विज्ञान काम करता है। इतना ही नहीं, हाईवे पर वाहन चालकों को भी नींद आने लगती है, क्योंकि शरीर आराम करने के साथ-साथ उनका मस्तिष्क और आंखें भी काम कर रही होती हैं।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब