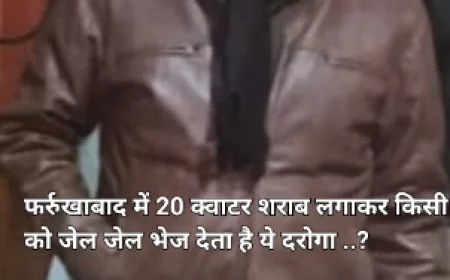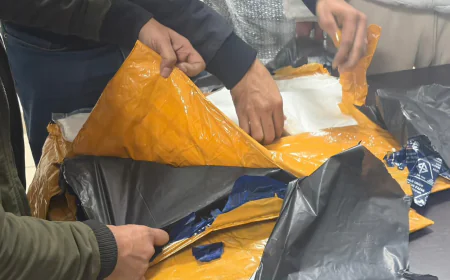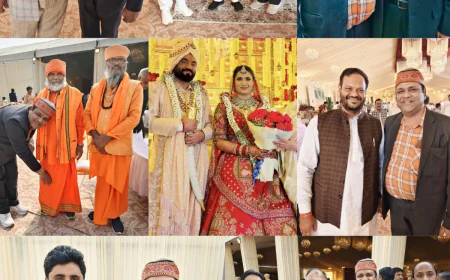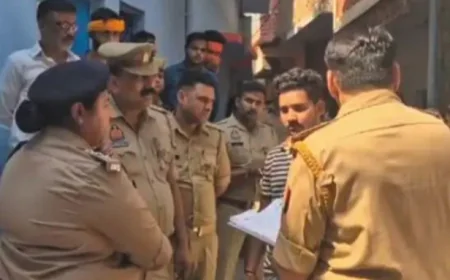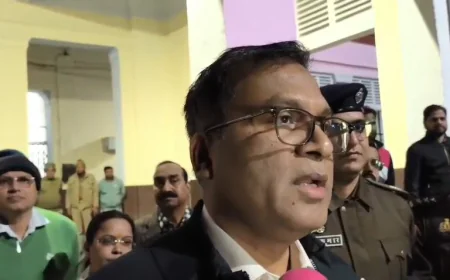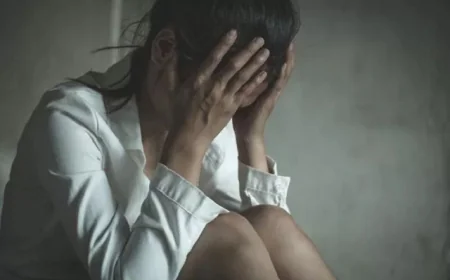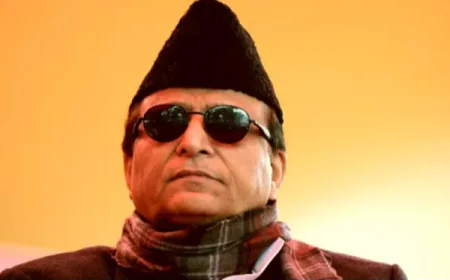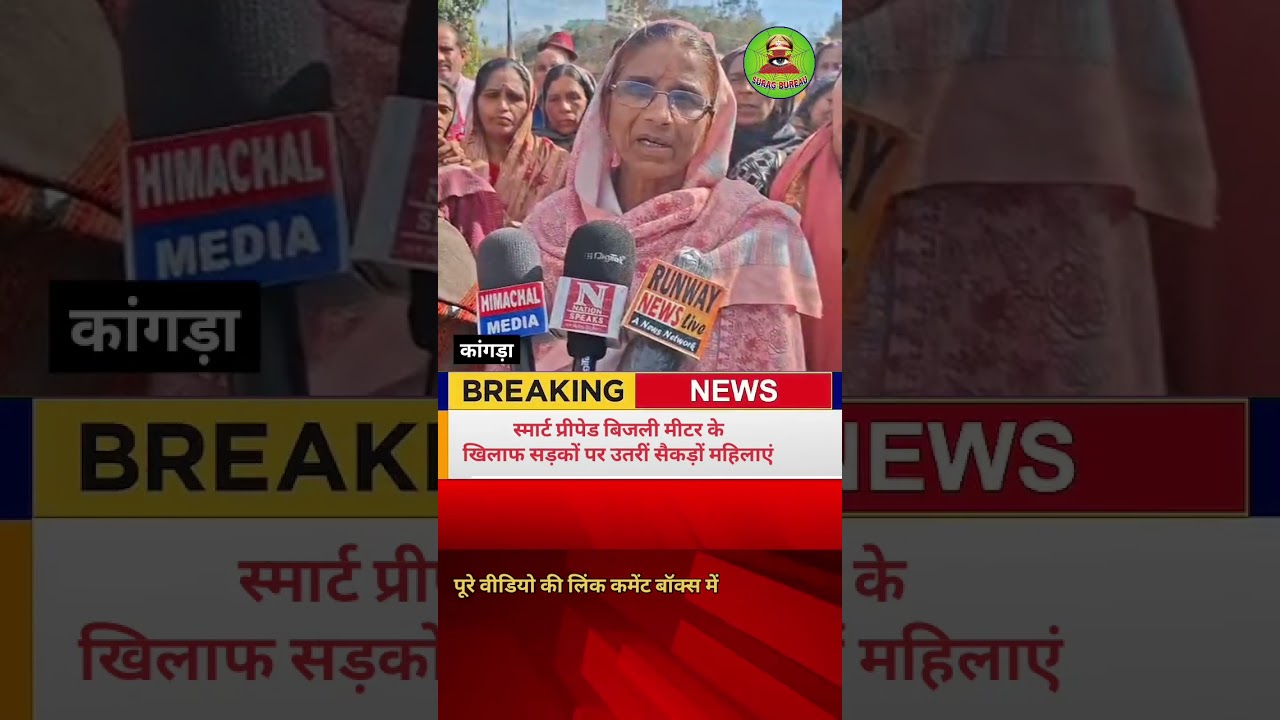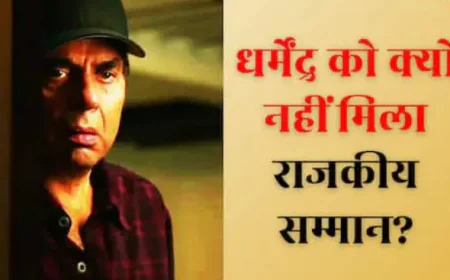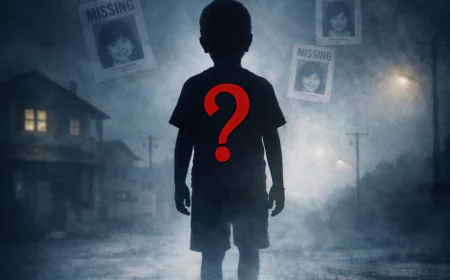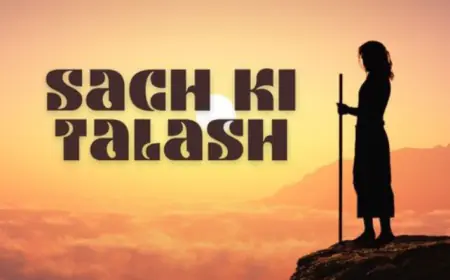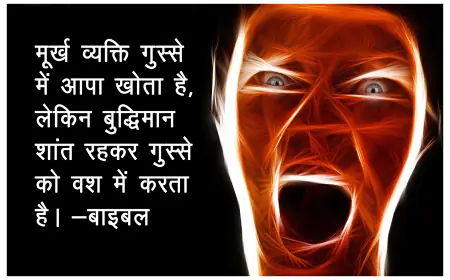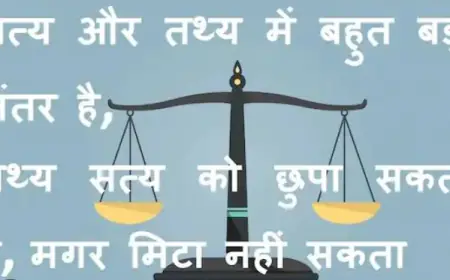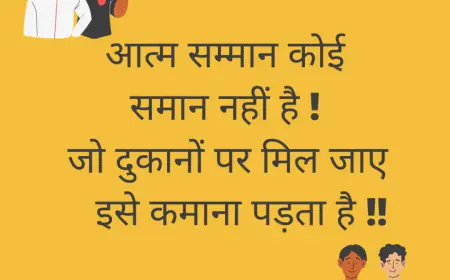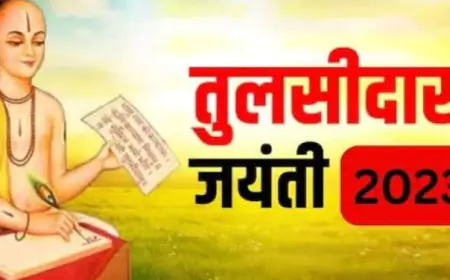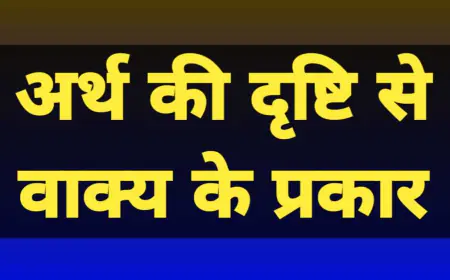प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षणिक संस्कृति में छिपे तनाव पहचानें

हाल ही में, आईआईटी कानपुर ने ‘द आर्ट ऑफ़ लिविंग फ़ाउंडेशन’ के साथ मिलकर एक ‘भलाई कार्यक्रम’ शुरू किया है। रिपोर्ट के अनुसार, फ़ाउंडेशन ने श्वास क्रिया, ध्यान और माईंडफुलनेस अर्थात ‘संचेतना’ (आसपास की घटनाओं के प्रति सजग रहते हुए इनमें बहने से बचना) सहित विशेषज्ञ सत्रों की एक शृंखला आयोजित करने पर सहमति जताई है। इसका उद्देश्य है युवा छात्रों की ‘मानसिक सहनशक्ति एवं तनाव प्रबंधन क्षमताओं’ को बेहतर बनाना।
समझा जा सकता है कि आईआईटी के अधिकारी अपने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं। दरअसल, हाल ही में सूचना के अधिकार से मिली एक जानकारी से पता चला है कि पिछले पांच सालों में 37 विद्यार्थियों ने खुदकशी है, जिसमें 11 छात्र आईआईटी के थे। इसलिए, कोई हैरानी नहीं कि आईआईटी गुवाहाटी ने भी ‘नैदानिक अभ्यासों’ की एक शृंखला चलाने की घोषणा की है – मसलन,परामर्श सत्र, संकाय सदस्यों के साथ सुबह की सैर और ‘तनाव से मुक्ति’ कार्यशालाएं। हालांकि,भारत में समकालीन शैक्षिक परिदृश्य के एक पर्यवेक्षक के रूप में, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अलग-अलग परामर्श सत्र, श्वास क्रिया और संचेतना अभ्यासों का ऐसा कोई समुच्चय इन युवाओँ की बढ़ती दिमागी, मानसिक चिंताओं और अस्तित्वगत पीड़ा से निपटने के लिए अपर्याप्त होगा, जो पहले ही अत्यंत-प्रतिस्पर्धात्मक और सामाजिक डार्विनवाद जनित जीवन-हंता वायरस से बनी मारक 'रण भूमि' में फंसे हुए हैं।
समस्या केवल किसी के 'आहत' हुए स्वः की नहीं है,समस्या समाज की पूरी संरचना है - जिसमें संसाधनों की कमी और असमानता है या फिर किसी की योग्यता केवल प्राप्त किए गए बढ़िया नंबरों से आंकने वाली विचारधारा बनकर रह गई है। उस चूहा-दौड़ में शामिल होना,जिसे तकनीकी-पूंजीपति 'सफलता' का प्रारूप ठहराते हैं। आप अपने 'अशांत' स्वः को बाकी समाज के ताने-बाने से अलग नहीं कर सकते। तीन कारणों के बारे में सोचें कि मानसिक तनाव या अकेलापन आईआईटी के माहौल में अंतर्निहित क्यों है। वास्तव में आप महसूस करेंगे कि किसी भी आईआईटी में प्रवेश पाने की प्रक्रिया ही स्वाभाविक रूप से तनावपूर्ण है। यह किसी महान शिक्षक के साथ चलकर सीखने जैसा न होकर विज्ञान और गणित की गूढ़ता को बनावटी बौद्धिक उत्साह और जिज्ञासा के साथ तलाशने जैसा है। इतना ही नहीं, कोचिंग सेंटरों के अत्याचार से लेकर, कभी न खत्म होने वाले अभ्यास परीक्षा तक की इस यात्रा में कोई रचनात्मक उत्साह या खुशी नहीं है। 'भाग्यशाली' छात्र जब तक बाधाओं से पार पाते हैं - जेईई मुख्य परीक्षा से लेकर जेईई एडवांस उत्तीर्ण करने तक - तब तक उनमें से कई मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तौर से दरिद्र हो चुके होते हैं। दूसरा, यह मानना गलत है कि जब कोई आईआईटी में भर्ती पा लेता है तो उसकी जिंदगी वास्तव में भरपूर बन जाती है, और सब कुछ गुलाबी-गुलाबी हो जाता है।
अतिशयी-प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षणिक संस्कृति में छिपे तनावों का कोई अंत नहीं है। अच्छा ग्रेड पाने की लालसा, बाजार मांग के अनुरूप लगातार बदलते 'कौशल' सीखते रहने का दबाव, और अंतिम नियति को लेकर निरंतर चिंता – जैसे कि, बढ़िया जगह पर नौकरी और वेतन पैकेज। ये सब एक ऐसा सामाजिक माहौल बना देते हैं, जिसमें कोई सच्चा दोस्त नहीं, कोई रचनात्मक उत्साह नहीं होता। हर कोई एक एकाकी व अहंकारी योद्धा भर है! और तीसरा, चूंकि हमारे समाज में आईआईटी में दाखिला पाने का कुछ ज्यादा ही महिमामंडन किया जाता है, जिसकी कीमत में, हमारे अधिकांश कॉलेज और विश्वविद्यालयों का व्यवस्थित रूप से अवमूल्यन हो रहा है। इसलिए आईआईटी विद्यार्थी के लिए लोगों की नज़रों में चढ़ने से बचना बहुत मुश्किल बन जाता है। हम आईआईटी में पढ़ने वाले को एक मिथकीय उत्पाद के रूप में देखना शुरू कर देते हैं: एक अत्यंत-बुद्धिमान प्रौद्योगिकीविद्, वह जो सब कुछ हासिल कर ले, जिसकी 'सफलता' को हम मिथक बनाना पसंद करते हैं।
एक आकर्षक नौकरी, किसी तकनीकी-कॉर्पोरेट उद्यम में एक उच्च पद, लगातार विदेश यात्राएं और निरंतर सामाजिक/आर्थिक गतिशीलता! वास्तव में, हमारा समाज पागलों की तरह 'सफलता की कहानियों' से ग्रस्त है। इसकी वजह से अगर आप एक ‘आईआईटी वाले’ हैं, तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि लोगबाग–आपके माता-पिता सहित - आपको सिर्फ़ एक इंसान के रूप में देखेंगे। आपको लगातार अपने 'अलौकिक' गुणों को साबित करते रहना पड़ेगा। ऐसा लगता है मानो आपका 'आम होना' ही आपका गुनाह है! वास्तव में, यह असंभव अपेक्षा उनमें से कईयों को अमानवीय अवगुण से भर देती है। निस्संदेह, यदि हम इन मुद्दों पर विचार कर हल नहीं निकालते तो हम इन एकाकी व तनावग्रस्त युवा प्रतियोगियों के अंदर केवल ध्यान, श्वास क्रिया और संचेतना अभ्यास करवाकर विवेक पैदा नहीं करवा सकते। भले ही यह किसी प्रकार का अस्थायी राहत देने वाला हो –फील गुड की क्षणिक अवस्था उनके जीवन-पथ में कोई मौलिक परिवर्तन लाने की संभावना नहीं रखती। हालांकि, तात्पर्य यह नहीं है कि संचेतना अभ्यास कोई मायने नहीं रखता। निस्संदेह, अतीत की चोटों और भविष्य की चिंता से विचलित हुए बिना, वर्तमान क्षण में गहराई से और तीव्रता से जीने की क्षमता ही एक बड़ी ध्यान कला है। इसके लिए समर्पित धार्मिकता की भावना होनी चाहिए- शांति, प्रेम परिपूर्ण सहृदयता और करुणा की निरंतर खोज। हालांकि, विडंबना यह है कि तेजी से विकास करते ‘आध्यात्मिक सुपरमार्केट’ वाले हमारे इस समयकाल ने ध्यान व संचेतना के लाभ का भी मजाक बनाकर रख दिया है। इसे फौरी राहत प्रदान करने वाले एक उत्पाद के रूप में बेचा जा रहा है।
इसके अलावा, यह ‘आध्यात्मिक उद्योग’ एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल अब तक नहीं पूछ पाया : संचेतना हो किसके वास्ते? क्या मुझे अपने कॉर्पोरेट लालच को बढ़ाने के लिए संचेतना अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ेगी? क्या अपने विश्वविद्यालय में ‘टॉपर’ बनने के लिए मेरे लिए संचेतना अभ्यास करना जरूरी है? क्या मुझे अहंकार के बोझ से मुक्ति और तनावमुक्ति हेतु संचेतना अभ्यास की आवश्यकता है? वास्तव में, ‘आध्यात्मिक सुपरमार्केट’ के व्यवसाय में रोजाना की तरक्की के साथ, हम अत्यधिक धनाढ्य सेलिब्रिटी बाबाओं और गुरुओं को अपने अमीर ग्राहकों को ‘फौरी मोक्ष’ के नाना प्रकार के पैकेज बेचते हुए देखते हैं –जैसे कि कॉर्पोरेट मालिकों से लेकर वे सभी, जो श्वास-क्रिया और संचेतना अभ्यास करने के वास्ते सात दिन का महंगे ‘रिट्रीट सत्र’ का खर्च उठा सकते हैं। इसलिए, कानपुर आईआईटी और आध्यात्मिक उद्योग के बीच गठबंधन को लेकर बनी अपनी असहजता व्यक्त करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। यदि हम युवा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सचमुच ईमानदार हैं, तो हमें उस समाज की संरचना पर सवाल उठाने की जरूरत है, जिसमें हम जी रहे हैं। इसके अलावा, हमें शिक्षा को पुनः परिभाषित करने, इसकी आत्मा को विशुद्ध रूप से योग्यतावादी व तकनीकी विचारधारा से बचाने और अपने छात्रों को जीवन की एक नई दृष्टि देने की जरूरत है - विशुद्ध ‘कैरियरवादिता’, अति-प्रतिस्पर्धात्मक और भौतिक सफलता से परे।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब