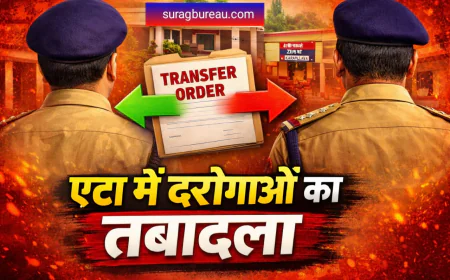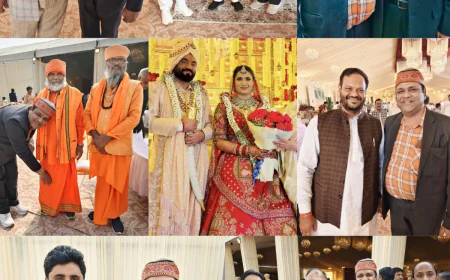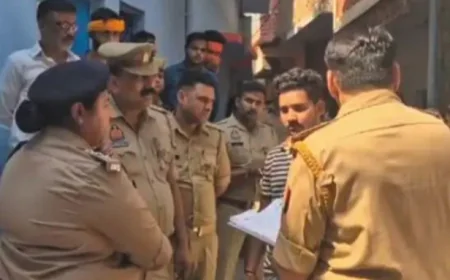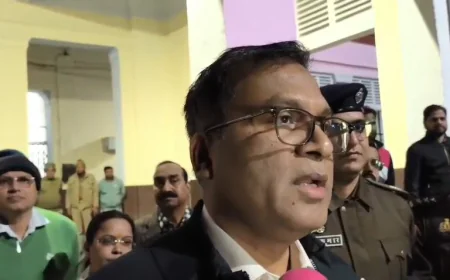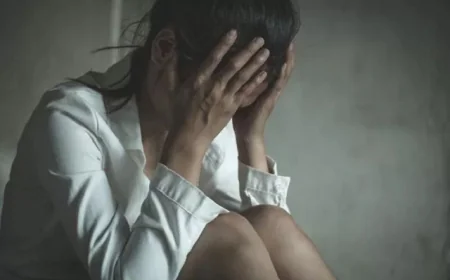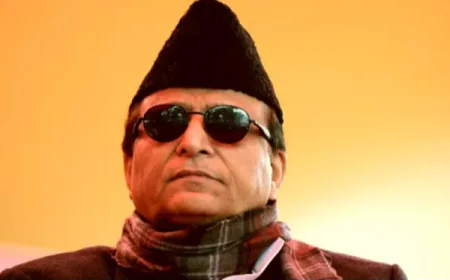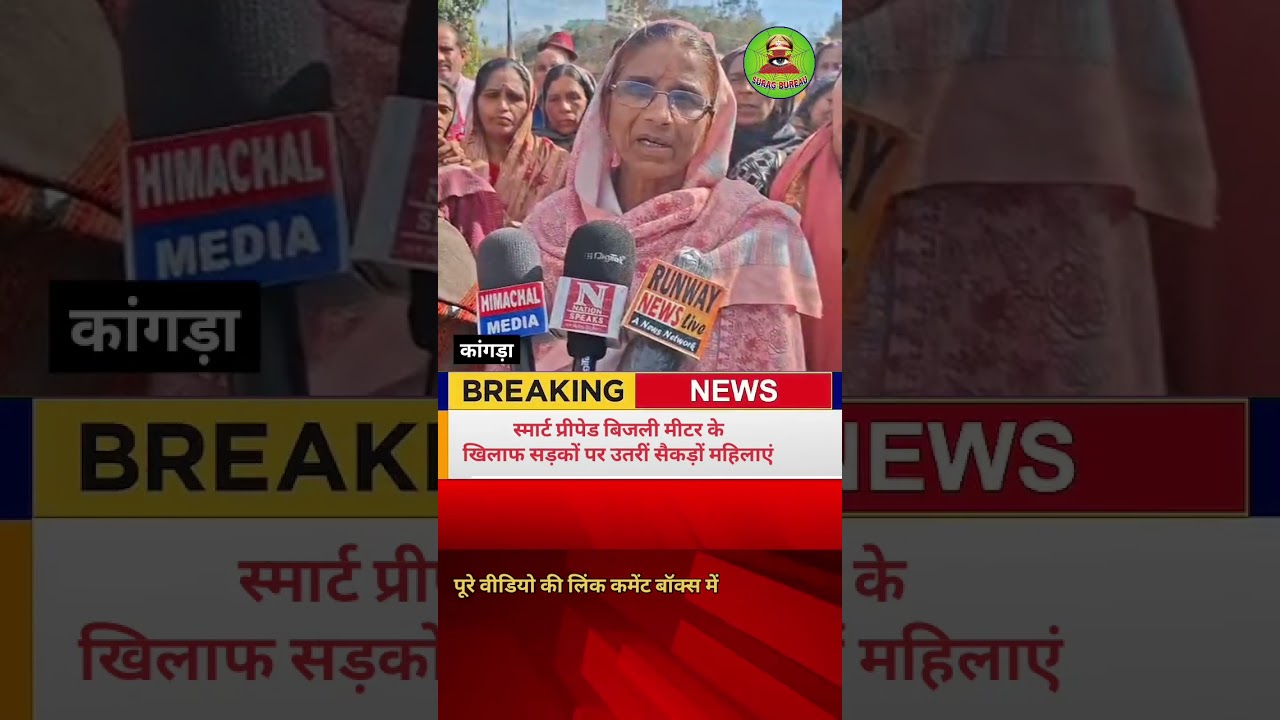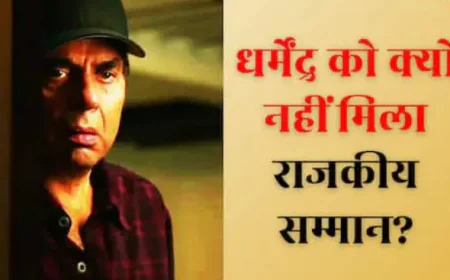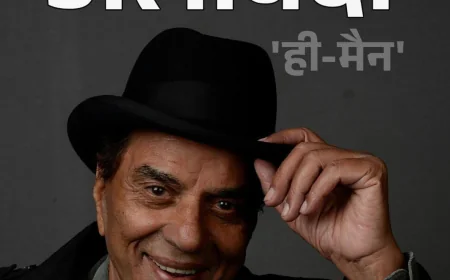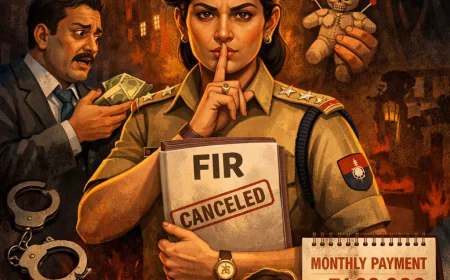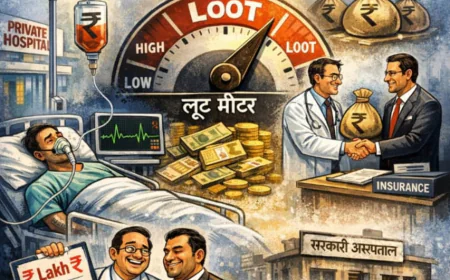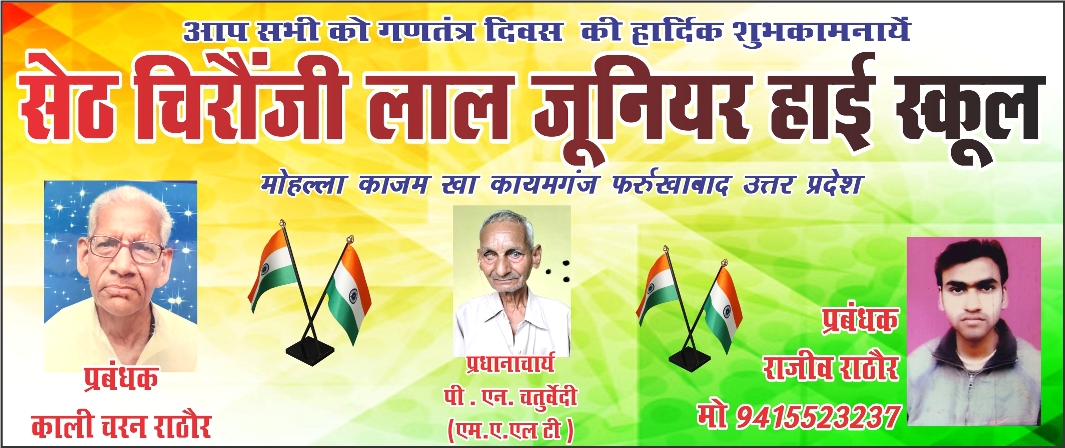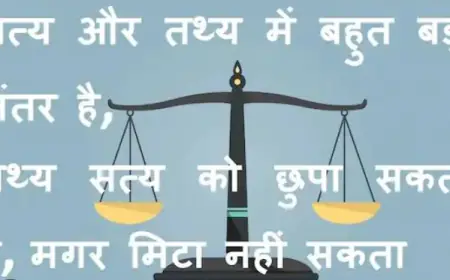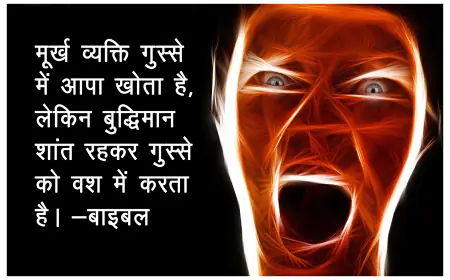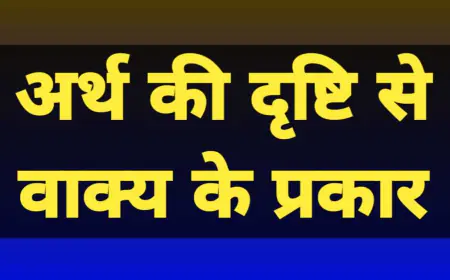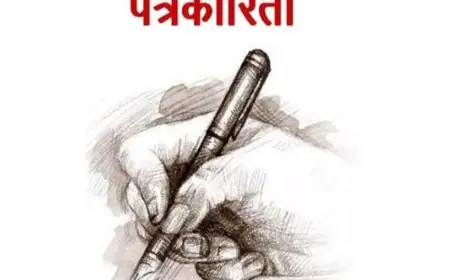विवाह की प्रथा समय, स्थान और सामाजिक संदर्भ के अनुसार बदलती रही है
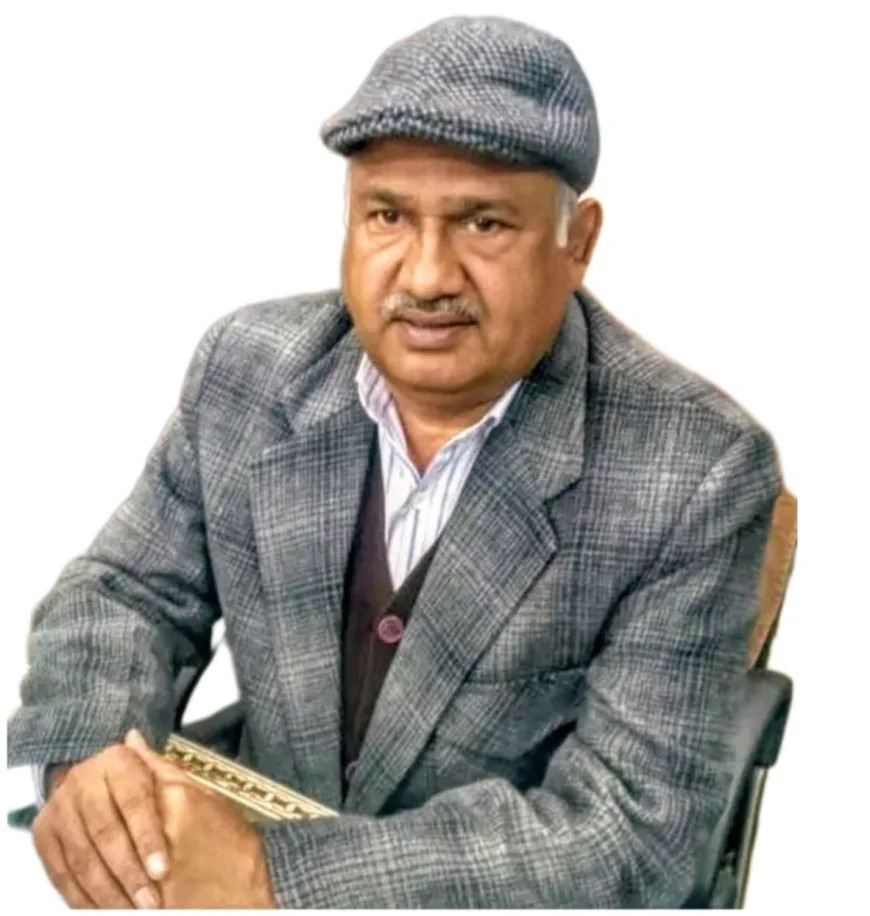
चाहे वह बहुपत्नी विवाह हो या बहुपति विवाह, दोनों ही व्यवस्थाओं को समझने के लिए ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोणों की गहराई में जाना जरूरी है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह सार्वभौमिक एवं सर्वमान्य सत्य है । समाज विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों की एक जटिल संरचना है जिसमें परिवार को एक मूलभूत एवं महत्वपूर्ण संस्था के रूप में समाजशास्त्रियों ने परिभाषित किया है।
परिवार को संस्था के रूप में स्वीकार करना, एक बेहतर, सशक्त और सभ्य समाज के निर्माण में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। मनुष्य अपनी प्रारंभिक सामाजिक शिक्षा परिवार से ही प्राप्त करता है और इसी कारण मां को प्रथम गुरु की संज्ञा दी गई है। इस सामाजिक संरचना में विवाह को भी एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में देखा गया है, जो व्यक्ति को सामाजिक जीवन में प्रवेश का माध्यम प्रदान करती है। विवाह का मूल उद्देश्य संतान-उत्पत्ति और परिवार की स्थापना होता है। इस प्रकार, विवाह समाज की एक अनिवार्य इकाई है जो परिवार रूपी संस्था की नींव रखता है । समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार विवाह और परिवार की अवधारणाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। एक समय में प्रचलित संयुक्त और संगठित परिवार की परंपरा अब धीरे-धीरे एकल परिवार में परिवर्तित हो गई है। यह बदलाव केवल परिवार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समग्र सामाजिक ढांचा भी परिवर्तन की इस धारा से प्रभावित हुआ है।
वास्तव में, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, जो शाश्वत सत्य है। हमारे समाज में विवाह की विभिन्न प्रणालियां प्राचीन काल से विद्यमान रही हैं। समय के साथ इनमें भी अनेक बदलाव आए हैं। एक समय में बहुपति तथा बहुपत्नी विवाह की प्रथा समाज में व्यापक रूप से प्रचलित थी, किंतु धीरे-धीरे सामाजिक चेतना, धार्मिक मूल्यों तथा कानूनी व्यवस्थाओं के प्रभाव से यह स्वरूप बदलता गया और वर्तमान में एक पत्नी तथा एक पति विवाह प्रणाली को ही सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त है। वहीं, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण आज 'लिव इन रिलेशनशिप' जैसी अवधारणाएं भी सामने आई हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बिना विवाह के दो व्यक्ति एक साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं। हालांकि, इसमें भावनात्मक व शारीरिक सहभागिता तो होती है, किंतु वैवाहिक प्रतिबद्धता और सामाजिक मान्यता का अभाव रहता है। ऐसे में यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या लिव इन जैसी व्यवस्थाएं विवाह संस्था के मूल उद्देश्य - सदैव के लिए प्रतिबद्धता, सामाजिक उत्तरदायित्व, परिवार की स्थापना तथा भावनात्मक स्थायित्व इत्यादि को पूर्ण कर पाने में सक्षम हैं? यह एक गूढ़ और जटिल प्रश्न है जिस पर समाज को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो बहुपत्नी विवाह (एक पुरुष की अनेक पत्नियां) के कई उदाहरण सामने आते हैं ।
जहां एक तरफ पटियाला के राजा भूपिंदर सिंह की 10 शादियां होने का उल्लेख मिलता है, वहीं रामायण में राजा दशरथ की तीन पत्नियां थीं, जबकि महाभारत में पांडु की दो पत्नियों- कुंती और माद्री का वर्णन मिलता है । यह विवाह की वह प्राचीन परंपरा थी, जो विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक कारणों से उस काल में प्रचलित रही। हालांकि समय के साथ समाज और कानून दोनों में बदलाव आए । 1955 में लागू हुए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बहुविवाह एवं बहुपत्नी विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। अब एक समय में एक ही वैध पत्नी को मान्यता दी जाती है । यदि किसी विवाहित व्यक्ति ने दूसरा विवाह किया, तो केवल पहली पत्नी को ही कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं । संबंध विच्छेद (तलाक) के उपरांत पुनर्विवाह की स्वतंत्रता भी दी गई है। यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है, लेकिन मुस्लिम, ईसाई या अन्य धर्मावलंबियों पर इसकी बाध्यता नहीं है। जहां एक ओर बहुपत्नी विवाह का इतिहास व्यापक है, वहीं बहुपति विवाह (एक महिला के अनेक पति) भी कुछ क्षेत्रों में प्राचीन परंपरा का हिस्सा रहा है। हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले शिलाई क्षेत्र में इस प्रथा की चर्चा फिर से सामने आई है जिसमें एक महिला ने स्वेच्छा से दो सगे भाइयों के साथ सहर्ष विवाह किया है। यह वाकया हमें पुराने रीति-रिवाजों की तरफ ले जाता है, जबकि नई पीढ़ी के लिए यह हैरत में डालकर सोचने पर विवश करता है।
यद्यपि आज इसका प्रचलन सीमित रह गया है, परंतु यह प्रथा पहले उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कि उत्तराखंड का जौनसार बावर, हिमाचल का शिलाई, किन्नौर और शिमला सहित अन्य इलाकों में सामान्य मानी जाती थी। महाभारत में द्रौपदी का विवाह पांच पांडवों से होना इस परंपरा का प्राचीन उदाहरण है। पांडवों के वनवास काल में इन क्षेत्रों में उनके निवास के संकेत मिलते हैं, जिससे माना जाता है कि बहुपति विवाह की परंपरा वहीं से प्रभावित हो सकती है। आज बहुपति विवाह लगभग विलुप्त हो चुका है, किंतु इस प्रथा के समर्थक और विरोधी दोनों ही अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं । समर्थकों का मानना है कि यह प्रथा नारी को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देती है। कई महिलाएं इसे एक वरदान मानती हैं, वे कहती हैं कि वे ' अक्षय सुहागिन हैं, उन्हें विधवा होने का डर नहीं रहता, और उनके बच्चों के सिर से पिता का साया नहीं उठता। वहीं इसके विरोधी इसे नारी की स्वतंत्रता, सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य के विरुद्ध मानते हैं । उनका मानना है कि यह प्रथा आधुनिक समाज में महिलाओं की गरिमा और समानता के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि न केवल भारत के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में, बल्कि चीन के सिचुआन प्रांत में रहने वाली गियांग जनजाति में भी यह प्रथा आज भी प्रचलन में है। वहां की महिलाएं इसे अपनी संस्कृति का गौरव मानती हैं और इसे स्वेच्छा से अपनाती हैं । विवाह की प्रथा समय, स्थान और सामाजिक संदर्भ के अनुसार बदलती रही है। चाहे वह बहुपत्नी विवाह हो या बहुपति विवाह, दोनों ही व्यवस्थाओं को समझने के लिए ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों की गहराई में जाना आवश्यक है। आज के समय में जहां व्यक्तिगत अधिकार और समानता की बात की जाती है, वहां इन परंपराओं पर पुन: विचार करना एक बौद्धिक विमर्श का विषय बन गया है, क्योंकि कभी-कभी रूढ़िवादी विचार व कार्य भावी पीढ़ी के लिए परंपरा का रूप ले लेती है, जिसको न चाहते हुए भी कभी-कभार निभाना भी पड़ता है । रूढ़िवादी धारणा नहीं, अपितु तार्किक दृष्टिकोण अपन की जरूरत है।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब