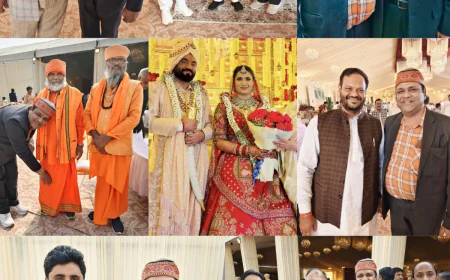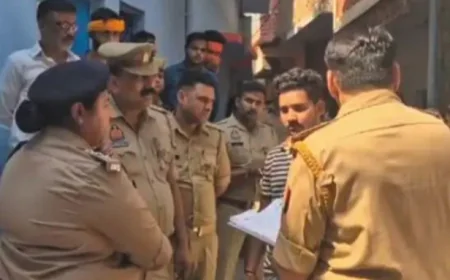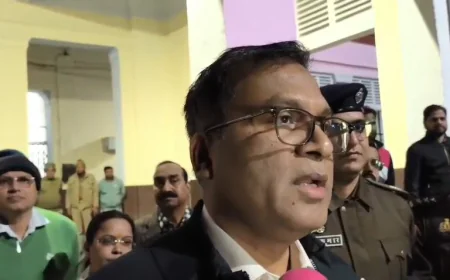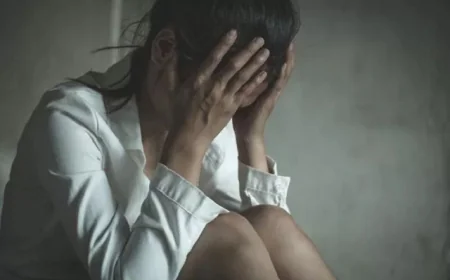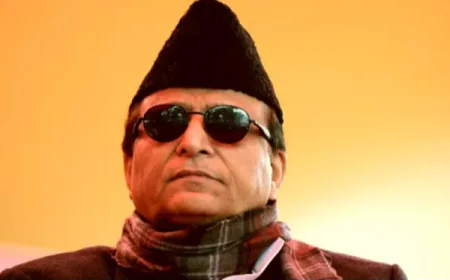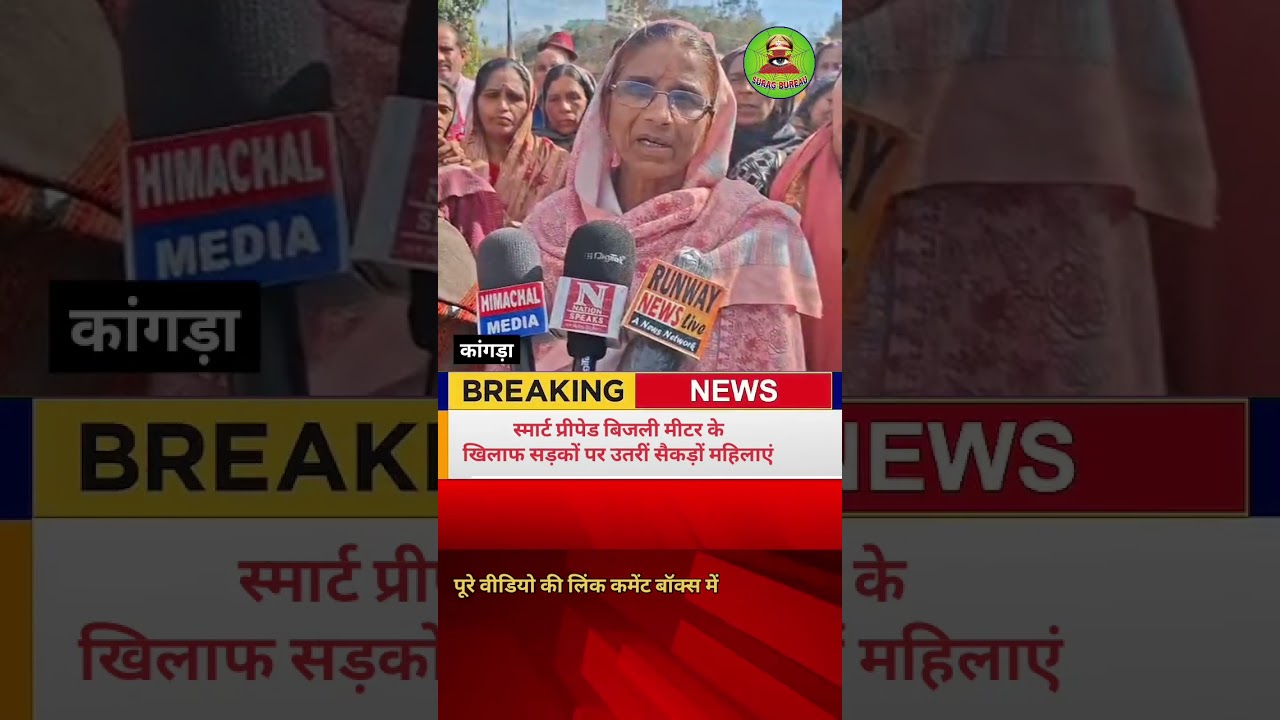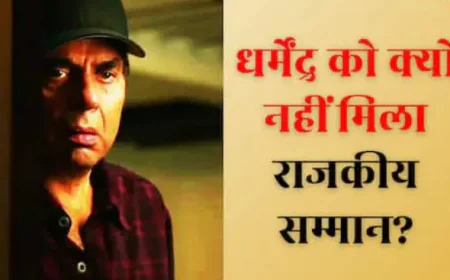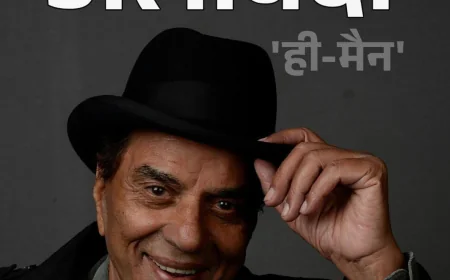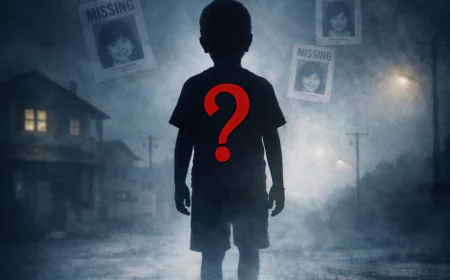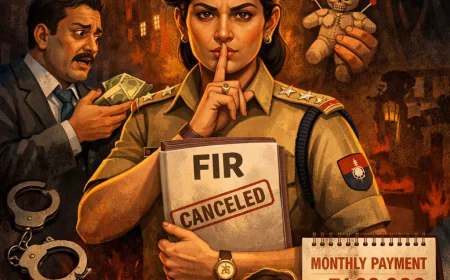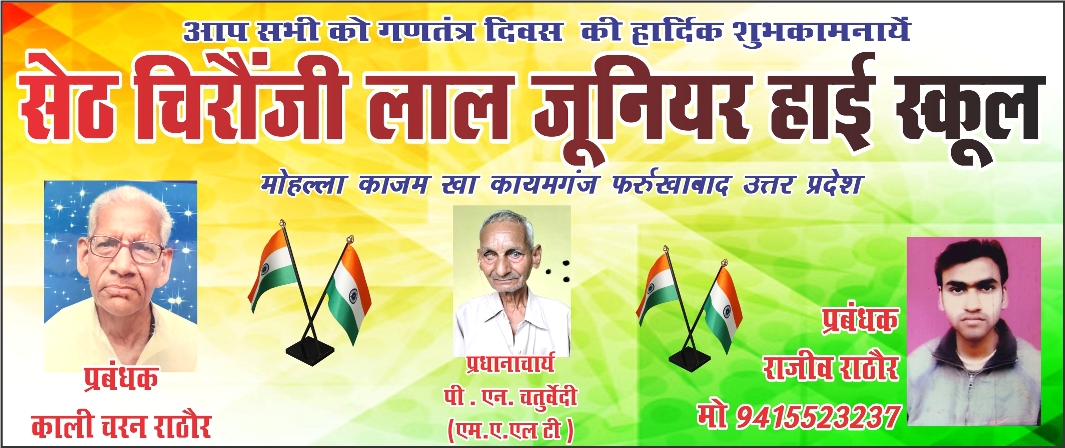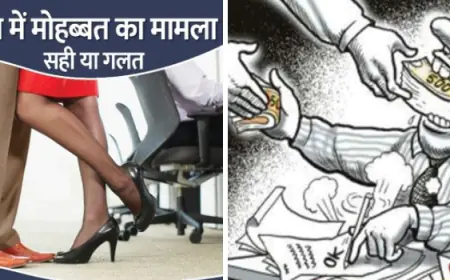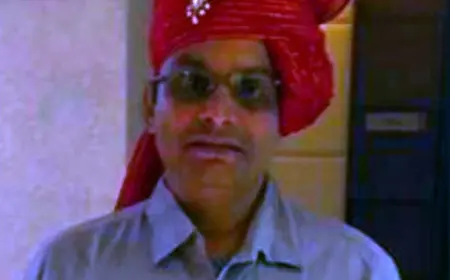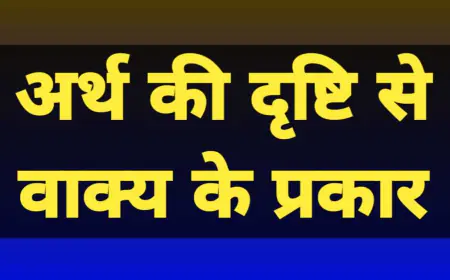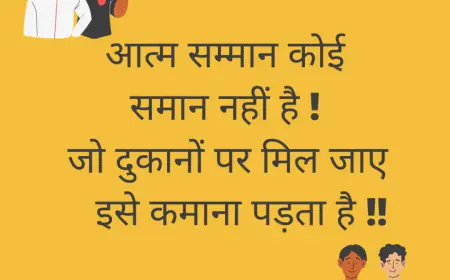आईआईटी और आईआईएम से परे: आश्चर्यजनक पाठ्यक्रम जो आप भारतीय विश्वविद्यालयों में मौजूद नहीं जानते थे

आईआईटी और आईआईएम से परे: आश्चर्यजनक पाठ्यक्रम जो आप भारतीय विश्वविद्यालयों में मौजूद नहीं जानते थे
● विजय गर्ग
एक कैरियर पथ है कि कुछ भी लेकिन साधारण के लिए खोज रहे हैं? संगीत के माध्यम से चिकित्सा से लेकर विज्ञान के साथ जलवायु चुनौतियों को हल करने तक, भारतीय विश्वविद्यालय अब उन पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं जो मोल्ड को तोड़ते हैं। यहां ताजा, भविष्य के लिए तैयार विकल्पों पर एक नज़र है जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा - लेकिन चाहिए। वे दिन गए जब डॉक्टर या इंजीनियर बनना महत्वाकांक्षा का एकमात्र बेंचमार्क था। आज की तेजी से विकसित हो रही दुनिया में, प्रौद्योगिकी और वैश्विक चुनौतियों से प्रेरित, नए कैरियर पथ उभरे हैं, जिससे छात्रों को विशेष और भविष्य के लिए तैयार विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला मिल रही है। यहां कुछ आला और ऑफबीट पाठ्यक्रम हैं जो अब भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए गए हैं जो इस बदलाव को दर्शाते हैं। 1.। पर्यावरण इंजीनियरिंग यह क्या है: सीधे शब्दों में कहें, यह पाठ्यक्रम छात्रों को विकास को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए सुसज्जित करता है। इसका उद्देश्य सक्रिय और प्रतिक्रियाशील दोनों दृष्टिकोणों के माध्यम से पर्यावरणीय प्रणालियों के प्रबंधन में विशेषज्ञता का निर्माण करना है। स्रोत पर प्रदूषण को कम करने और होने पर इसे नियंत्रित करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीकों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
आप इसे कहां पा सकते हैं: बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (बिट्स) पिलानी ने 2023 में पर्यावरण इंजीनियरिंग में चार सेमेस्टर का एमटेक लॉन्च किया। पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातक जल गुणवत्ता विशेषज्ञों और पर्यावरण डिजाइन इंजीनियरों के रूप में काम कर सकते हैं। पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातक जल गुणवत्ता विशेषज्ञ और पर्यावरण डिजाइन इंजीनियरों के रूप में काम कर सकते हैं। चित्र क्रेडिट: कैरोल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन आप इसके साथ क्या पता लगा सकते हैं: यह उन इंजीनियरों के लिए आदर्श है जो स्थिरता के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। यह पाठ्यक्रम दरवाजे खोलता है जैसे: पर्यावरण स्वास्थ्य और सुरक्षा (ईएचएस) प्रबंधक वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंजीनियर पर्यावरण डिजाइन इंजीनियर 2.। साइबर फिजिकल सिस्टम में बीटेक यह क्या है: साइबर-फिजिकल सिस्टम्स (सीपीएस) डिजिटल और भौतिक दुनिया को पाटते हैं - स्वयं ड्राइविंग कारों या एआई-संचालित कारखानों के बारे में सोचें। यह पाठ्यक्रम वास्तविक समय के बुद्धिमान प्रणालियों के निर्माण के लिए कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल सिस्टम और डेटा विज्ञान को एकीकृत करता है आप इसे कहां पा सकते हैं: मणिपाल विश्वविद्यालय, मैंगलोर और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइबर-भौतिक प्रणालियों में चार साल की बीटेक की पेशकश करते हैं।
आप इसके साथ क्या पता लगा सकते हैं: स्नातक बुद्धिमान, वास्तविक दुनिया प्रणालियों के डिजाइन और निर्माण के लिए सुसज्जित हैं जहां कंप्यूटर, सेंसर, मशीनें और नेटवर्क मूल रूप से बातचीत करते हैं। कैरियर पथ में शामिल हैं: साइबर इंजीनियर रोबोटिक्स डेवलपर एंबेडेड सिस्टम आर्किटेक्ट एआई शोधकर्ता ऑटोमेशन इंजीनियर 3। मेडिकल कोडिंग यह क्या है: एक मेडिकल कोडर विश्व स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले मानकीकृत सार्वभौमिक कोड में डॉक्टरों के नोट्स, निदान और प्रक्रियाओं का अनुवाद करता है। यह चिकित्सा बिलिंग प्रक्रिया में पहला कदम है, जो रोगी के इतिहास को ट्रैक करने, अस्पतालों को बीमाकर्ताओं से जोड़ने और बिलिंग संचालन को कारगर बनाने में मदद करता है। मेडिकल कोडर स्वास्थ्य सेवा के व्यावसायिक पक्ष में शामिल हो जाते हैं और अस्पतालों और बीमा एजेंसियों के बीच लिंक को सहज रखने में मदद करते हैं। मेडिकल कोडर स्वास्थ्य सेवा के व्यावसायिक पक्ष में शामिल हो जाते हैं और अस्पतालों और बीमा एजेंसियों के बीच लिंक को सहज रखने में मदद करते हैं। चित्र क्रेडिट: शटरस्टॉक प्रतिनिधि छवि आप इसे कहां पा सकते हैं: दिल्ली में स्वास्थ्य प्रबंधन और अनुसंधान केंद्र स्नातकोत्तर और कार्यकारी डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, अहमदाबाद, एक और तीन महीने के प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रदान करता है।
आप इसके साथ क्या पता लगा सकते हैं: यह स्वास्थ्य सेवा के व्यवसाय या प्रशासनिक पक्ष में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए एकदम सही है। नौकरी की भूमिकाओं में शामिल हैं: चिकित्सा लेखा परीक्षक स्वास्थ्य सूचना तकनीशियन अनुपालन अधिकारी 4। मुसोपैथी यह क्या है: मुसोपैथी चिकित्सा के लिए ध्वनि के सार्वभौमिक गुणों का अध्ययन करके संगीत के चिकित्सीय गुणों की पड़ताल करती है। यह यह आकलन करने के लिए स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मिश्रित करता है कि ध्वनि मानव भलाई को कैसे प्रभावित करती है। जबकि यह संगीत चिकित्सा के साथ ओवरलैप होता है, होम्योपैथी चिकित्सीय परिणामों के लिए ध्वनि के वैज्ञानिक अनुप्रयोग में निहित है। आप इसे कहां पा सकते हैं: IIT मंडी ने 2024 में यह पाठ्यक्रम पेश किया। यह स्नातकोत्तर (एमएस) और पीएचडी कार्यक्रम दोनों प्रदान करता है। आप इसके साथ क्या पता लगा सकते हैं: यह उभरता हुआ क्षेत्र करियर के लिए स्नातक तैयार करता है जैसे: संगीत-आधारित चिकित्सक (मुसोपैथिस्ट) संगीत चिकित्सा में हेल्थकेयर विशेषज्ञ
■ संबंधों के बदलते समीकरण
● विजय गर्ग -
भारत में विवाह सिर्फ एक सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि इसे एक संस्था का दर्जा हासिल है। इससे गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अवधारणा जुड़ी है। विवाह वह संस्था है, जो दो व्यक्तियों को जीवन भर के लिए प्रेम, भरोसे और समर्पण के रिश्ते में बांधती है। विवाह का उद्देश्य केवल एक-दूसरे का साथ निभाना नहीं, बल्कि एक संपूर्ण परिवार की नींव रखना भी होता है। यही वजह है कि विवाह से उत्पन्न होने वाले रिश्ते समाज की रीढ़ माने जाते हैं। हैं। विवाह जैसी संस्था ताउम्र सह- :-जीवन की पैरवी करती है। हमारे देश में विवाह सदियों पुरानी परंपरा है, जिसके बिना सब कुछ अधूरा सा महसूस होता है। हमारा समाज विवाह से उपजे रिश्ते को न केवल स्वीकार करता है, बल्कि इज्जत भी देता है। इतनी समृद्ध परंपरा वाले इस देश में क्षणिक रिश्तों की ओर भागने की कोशिश की जा रही है। क्षणिक रिश्तों के फायदे समाज में प्रचारित किए जा रहे हैं, पर सवाल है कि यह सब किसलिए किया जा रहा है?
क्या फिर पाश्चात्य संस्कृति की यह किसी बाजारवाद से प्रेरित है या कुत्सित त्सित साजिश, जिसकी दिलचस्पी भारतीय संस्कृति को हमेशा कमजोर करने में रही है। इन दिनों परंपराओं में यकीन करने वाले भारत में एक नया शब्द तेजी से उभारा जा रहा है, वह है- 'नैनोशिप' यह शब्द एक 'डेटिंग एप' ने पेश किया है, जिसमें दावा किया गया कि वर्ष 2025 में रूमानी रिश्तों की परिभाषा इसके जरिए बदल जाएगी। 'नैनोशिप' के बारे में भारत में पहले कोई चर्चा नहीं होती थी। यह चर्चा तो तबसे होने लगी, जब डेटिंग एप ने हौले से 'ईयर इन स्वाइप 2024' नामक एक रपट परोस दी। यह एप प्रति वर्ष ऐसी रपट में डेटिंग के अलग-अलग तरीके बताता है। इस बार भी इस रपट में ऐसा ही किया गया, जब 'नैनोशिप' की अवधारणा लोगों सामने रख कर दावा किया गया कि यह एक ऐसा नया तरीका है, वर्ष 2025 में डेटिंग की दुनिया को अलग तरह से प्रभावित कर सकता है और प्यार करने की | परिभाषा 1 को I तरह बदल सकता है। सवाल उठता है। भारतीय समाज में ऐसी अवधारणा का प्रसार क्यों किया रहा है? क्या यह विचार हमारी संस्कृति और मूल्यों के अनुकूल है ? दरअसल, 'नैनोशिप' एक ऐसा रिश्ता है जो बेहद अल्पकालिक होता है। यह यह कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए हो सकता है। अठारह से चौतीस वर्ष के बीच के आठ हजार युवाओं के बीच सर्वे में यह पाया गया कि रोमांस और तात्कालिक जुड़ाव उनके लिए बहुत मायने रखता है।
विशेष रूप से कुंआरे युवाओं के लिए 'नैनोशिप' आकर्षक विकल्प बन क्योंकि इसमें कोई जिम्मेदारी या सामाजिक बंधन नहीं होता। यह रिश्ता सिर्फ 'पल र की खुशी' के लिए होता है। मगर सवाल यह है। क्या आठ हजार लोगों का सर्वेक्षण एक पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है? भारत की 1 करोड़ से अधिक है और उसमें भी युवा वर्ग करोड़ों की संख्या में है। ऐसे में मात्र आठ हजार लोगों के विचारों के आधार पर एक सामाजिक रुख को स्थापित करना न केवल भ्रामक है, बल्कि समाज को गलत दिशा में धकेलने के समान भी है। सवाल यह भी है कि क्या एक सीमित और लक्षित सर्वे से पूरे देश की मानसिकता का अनुमान लगाया जा सकता है ? यह एक विचारणीय प्रश्न है जिसका उत्तर खोजने की जरूरत है। जो लोग इसके महिमामंडन में जुटे हैं, उनका तर्क है कि इस रिश्ते में भावात्मक जुड़ाव शून्य या नाममात्र होता है। इसमें किसी पर कोई दायित्व नहीं। न ही लंबे समय तक किसी का बोझ ढोने की मजबूरी। जिस प्रकार देश में 'नैनोशिप' को बढ़ावा देने की कोशिशें हो रही हैं, उनमें बाजारवाद साफ महसूस होता है। आज 'डेटिंग एप' एक बड़ा उद्योग बन चुका है जो रिश्तों को एक उपभोग की वस्तु के रूप में परोस रहे हैं। इससे बाजार को नए उत्पाद और नए ग्राहक मिलते हैं। सवाल है कि क्या यह प्रेम की तलाश है या मुनाफे का गणित ? बाजार में उपभोक्ताओं को भावात्मक संबंध' नहीं, बल्कि 'संतोषजनक अनुभव' चाहिए, जिसे जब चाहे लिया और जब व चाहे छोड़ा जा सके। यह भारतीय समाज की भावपूर्ण, स्थायित्व और समर्पण की मूल भावना के विपरीत है। हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत उसका पारिवारिक ढांचा है। इसलिए विवाह को केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक संस्था माना गया है। विवाह में सात फेरे जैसी रस्में जीवन भर साथ निभाने का वचन हैं। यह रिश्ता केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच होता है। इसमें समाज की भागीदारी होती है और यही सामाजिक समर्थन एक परिवार को मजबूती देता है हमारी संस्कृति में विवाह को जन्म-जन्मांतर का बंधन माना जाता है। इसमें शारीरिक या तात्कालिक आकर्षण से कहीं अधिक एक गहन भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव होता है। ऐसे में केवल मस्ती और पल भर के संतोष पर आधारित 'नैनोशिप' जैसे रिश्ते क्या हमारे समाज में स्वीकार किए जा सकत सकते हैं? हाल के वर्षों का अनुभव बताता है कि सह-जीवन में धोखा और बिखराव एवं हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। प्रेम के रिश्ते में बंधने का दावा करने वाले लोगों ने किस प्रकार अपने साथी को निर्ममता से मौत के घाट उतारा है, यह कई बार देखा गया है। जब रिश्तों में स्थायित्व और जिम्मेदारी नहीं होती, तब उनका परिणाम अक्सर मानसिक तनाव, अकेलेपन और कभी-कभी अपराध तक पहुंच जाता है। 'नैनोशिप' जैसे रिश्तों में तो भावना और जिम्मेदारी का बिल्कुल अभाव ही है। ऐसे रिश्ते एक अस्थिर सामाजिक वातावरण ही बना सकते हैं जिसमें लोग सिर्फ अपनी तात्कालिक इच्छाओं के लिए जीते हैं। ऐसे लोगों के पास यह सोचने का समय ही नहीं होता कि उनके कर्मों का प्रभाव समाज और अन्य लोगों पर क्या होगा ? सवाल यह नहीं है कि यह नया विचार हमारे समाज को किस कदर प्रभावित कर पाएगा, बल्कि सवाल तो यह है कि हम इसके प्रभावों के प्रति कितने जागरूक हैं? यह समय चुनौतीपूर्ण और सजग होने का है। पश्चिम का अंधानुकरण कर हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। अब हमें बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि रिश्तों में धैर्य, समझदारी, समर्पण और जिम्मेदारी कितनी जरूरी है। हमें बाजार की ओर से से थोपे जा जा रहे 'नए 'चलन' को आंख मूंद कर स्वीकार करने के बजाय अपनी संस्कृति और परंपराओं को ध्यान में रख कर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। संभव है 'नैनोशिप' जैसे रिश्ते पश्चिमी देशों के समाज में फिट बैठते हों। उनके यहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक जिम्मेदारियों से ऊपर है, लेकिन भारत में यह विचार सिर्फ अस्थिरता, निराशा और टूटन ही लाएगा। हमारे देश में रिश्ते सिर्फ निजी नहीं हैं, रिश्तों को सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त है। हमारे पारंपरिक समाज के लिए इस तरह के अल्प अवधि के रिश्ते न केवल अस्वीकार्य हैं, बल्कि यह सांस्कृतिक हमला भी है। यह विवाह बनाम वासना का मामला है, जिसके जरिए रिश्तों की परिभाषा बदलने की कोशिश की जा रही है।