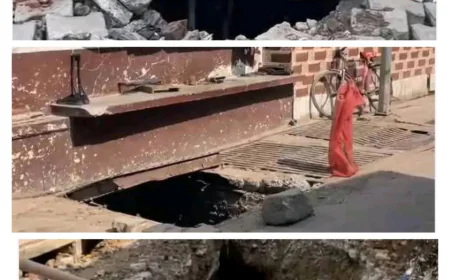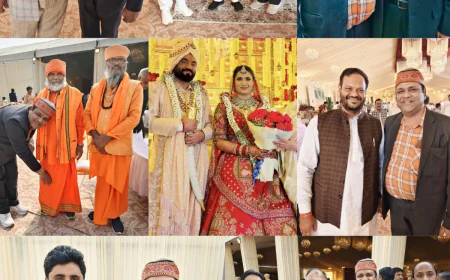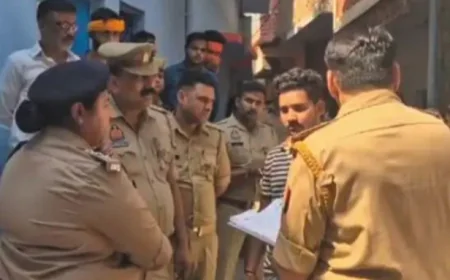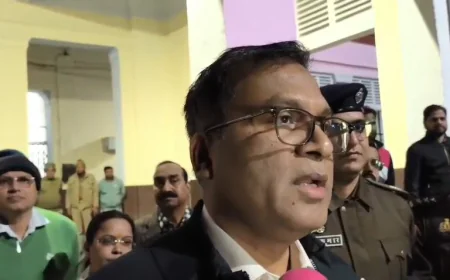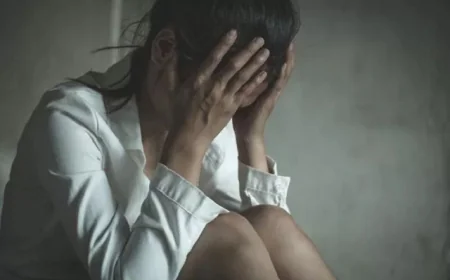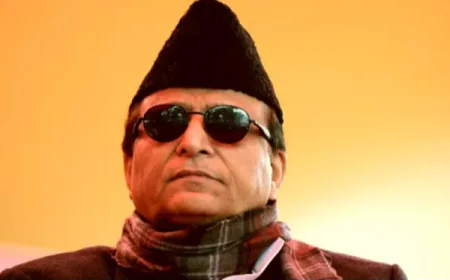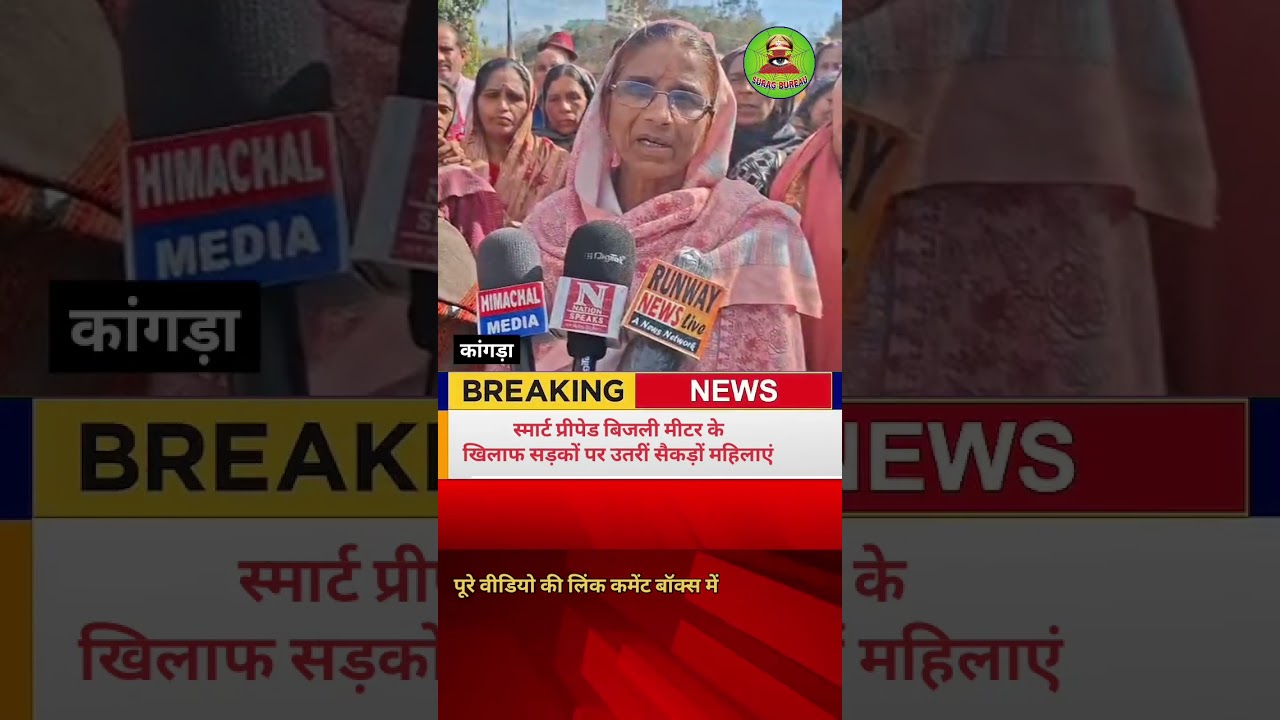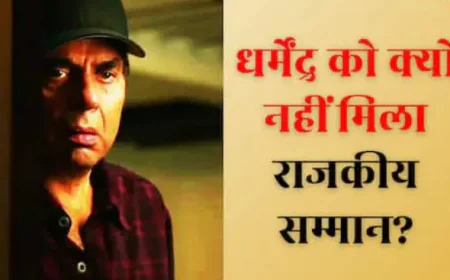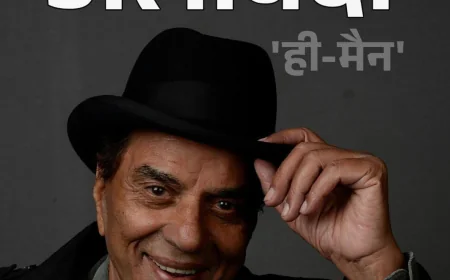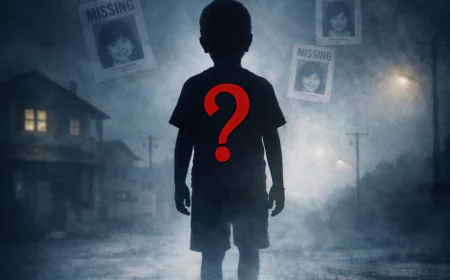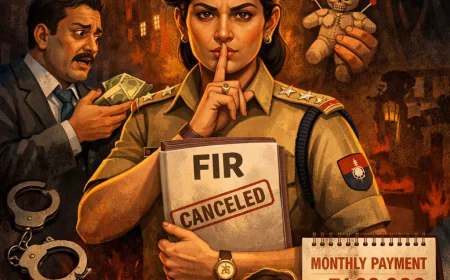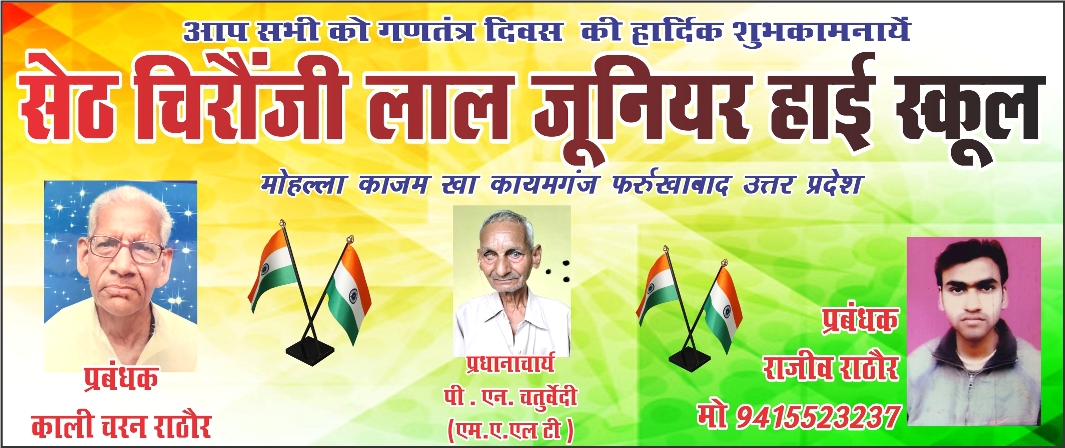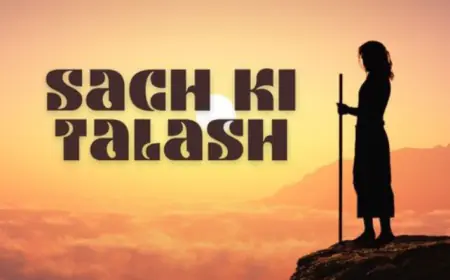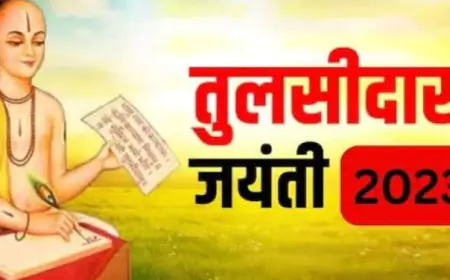भारत में विकलांग बच्चों की शिक्षा

विकलांगता बहुआयामी है और विकलांगता की एक भी सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। न केवल परिभाषाएं देशों में अलग-अलग हैं, बल्कि ये अलग-अलग हैं और विकसित कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक प्रवचनों के साथ बदलते हैं। भारत में विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की प्रभावकारिता, बुनियादी ढांचे, कार्यान्वयन और / या अन्य कारणों में कमी है। इसका एक कारण विकलांग बच्चों के लिए सटीक आंकड़े हैं। भारत में विकलांगता की व्यापकता के बारे में विश्वसनीय डेटा खोजना बहुत मुश्किल है।
सामान्य तौर पर, एकल व्यापकता दर की खोज एक भ्रम है, इसलिए अनुमानों की सीमा और उनकी विविध उत्पत्ति हैं। इससे विकलांग लोगों का एक सटीक आंकड़ा सामने आना मुश्किल हो जाता है। 2001 की जनगणना में पांच प्रकार की विकलांगता को कवर करते हुए, 1028 मिलियन की कुल आबादी में से 2.13 प्रतिशत, या 21.91 मिलियन विकलांग लोगों की व्यापकता दर्ज की गई। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने 58 वें दौर (जुलाई-दिसंबर 2002) के सर्वेक्षण में बताया कि 1.8 प्रतिशत आबादी (18.5 मिलियन) में विकलांगता थी। लेकिन दोनों निकायों द्वारा किए गए उपर्युक्त अनुमान वास्तविकता के निकट और प्रिय हैं; इससे कम या ज्यादा हो सकता है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम भारत में विकलांग बच्चों की शिक्षा: एक अवलोकन विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा: भारत विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने वाले संगठन भारत में विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा: कमियां / अवलोकन भारत में विकलांग बच्चों की बेहतर शिक्षा बनाने के उपाय भारत में विकलांगों के लिए शिक्षा: एक अवलोकन भारत में विशेष शिक्षा की आवश्यकता का पता पूर्व-स्वतंत्र भारत में लगाया जा सकता है। भारतीय इतिहास में कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि विकलांग लोगों के पास शैक्षिक अवसर थे और विकलांगता सीखने के रास्ते में नहीं आई थी। हालांकि, औपनिवेशिक काल के दौरान, भारत ने देश के बाहर मौजूद शैक्षिक मॉडलों को तेजी से देखा। विकलांग बच्चों के माता-पिता ने अपने बच्चों के लिए, मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों से और पश्चिमी देशों में प्रचलित दृष्टिकोण के संपर्क में आने के लिए स्कूल शुरू किए।
चूंकि विकलांग बच्चों की शिक्षा पर सरकार की कोई नीति नहीं थी, इसलिए उसने इन निजी स्कूलों को अनुदान दिया। अलग-अलग स्कूलों की स्थापना का यह दृष्टिकोण, ज्यादातर आवासीय, देश भर में फैला हुआ है, उनमें से अधिकांश शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। एक सदी से अधिक समय तक, इन विशेष स्कूलों ने व्यापक विश्वास के कारण विकलांग बच्चों को उपलब्ध एकमात्र शिक्षा की पेशकश की कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों को दूसरों के साथ शिक्षित नहीं किया जा सकता है। इससे कम संख्या में बच्चों को शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति मिली लेकिन इससे इन बच्चों को शिक्षा पूरी करने के बाद मुख्यधारा के समुदाय में प्रवेश करने में कोई मदद नहीं मिली। ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा: भारत समाज में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों को समान सदस्य के रूप में एकीकृत करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने विकलांग बच्चों (IEDC) के लिए एकीकृत शिक्षा के रूप में जानी जाने वाली योजना के बारे में लाया है। IEDC 1974 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। आईईडीसी कार्यक्रम को 1992 में संशोधित किया गया था जिसके तहत छात्रों को मुख्यधारा की आबादी में एकीकृत करने के लिए 100% वित्तीय सहायता की पेशकश की गई थी। यह आर्थिक रूप से समर्थित परिवहन सुविधा, किताबें, और स्टेशनरी, वर्दी, अनुदेशात्मक सामग्री, सहायक उपकरण, नेत्रहीन विकलांगों के लिए पाठकों की सुविधा, आर्थोपेडिक रूप से विकलांगों के लिए उपस्थिति सुविधा, विशेष शिक्षक सुविधा, स्कूल परिसर में स्थित विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा और वास्तुशिल्प अवरोधों को हटाने आदि। भारत में विकलांग बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने में सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के बीच सामुदायिक भागीदारी और भागीदारी महत्वपूर्ण है।
आईईडीसी कार्यक्रम के तहत एक विकलांग बच्चे को संबंधित राज्य/यूटी में प्रचलित दरों पर निम्नलिखित सुविधाएं दी जा सकती हैं: पुस्तकों और स्टेशनरी पर वास्तविक खर्च 400 रुपये प्रति वर्ष तक। 200 रुपये प्रति वर्ष तक की वर्दी पर वास्तविक खर्च। परिवहन भत्ता 50 रुपये प्रति माह तक। यदि योजना के तहत भर्ती एक विकलांग बच्चा स्कूल परिसर में स्कूल के छात्रावास में रहता है, तो कोई परिवहन शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा। कक्षा V के बाद नेत्रहीन बच्चों के मामले में प्रति माह 50 रुपये का पाठक भत्ता। प्रति माह 75 रुपये की दर से कम चरम विकलांगता के साथ गंभीर रूप से विकलांगों के लिए एस्कॉर्ट भत्ता। पांच साल की अवधि के लिए प्रति छात्र अधिकतम 2000 रुपये के अधीन उपकरणों की वास्तविक लागत। गंभीर रूप से आर्थोपेडिक रूप से विकलांग बच्चों के मामले में, एक स्कूल में 10 बच्चों के लिए एक परिचर की अनुमति देना आवश्यक हो सकता है। अटेंडेंट को संबंधित राज्य/यूटी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए निर्धारित वेतन का मानक पैमाना दिया जा सकता है । जिस संस्थान में वे अध्ययन कर रहे हैं, उसी संस्थान के भीतर स्कूल हॉस्टल में रहने वाले विकलांग बच्चों को भी राज्य सरकार के नियमों / योजनाओं के तहत स्वीकार्य बोर्डिंग और लॉजिंग शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। जहां हॉस्टलर्स को छात्रवृत्ति की कोई राज्य योजना नहीं है, विकलांग बच्चे जिनकी माता-पिता की आय 5,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, उन्हें अधिकतम 200 रुपये प्रति माह के अधीन वास्तविक बोर्डिंग और लॉजिंग शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। हालांकि, विकलांग बच्चों को आम तौर पर हॉस्टल में नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि पास के स्कूलों में आवश्यक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध न हों। स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले गंभीर रूप से आर्थोपेडिक रूप से विकलांग बच्चों को एक सहायक या अयाह की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। हॉस्टल के किसी भी कर्मचारी को प्रति माह 50 रुपये का विशेष वेतन स्वीकार्य है, जो अपने कर्तव्यों के अलावा बच्चों को इस तरह की मदद देने के लिए तैयार है।
विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने वाले संगठन सरकार के साथ साझेदारी में एक गैर सरकारी संगठन सिख युवा सेवा समिति (SYSS) विकलांग बच्चों और DPEP (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) परियोजनाओं के लिए एकीकृत शिक्षा के कार्यान्वयन में भाग लेता है। यह समुदाय-आधारित हस्तक्षेप पहल के माध्यम से कार्यक्रम को भी मजबूत करता है। परियोजनाएं प्रशिक्षित कर्मियों के माध्यम से स्कूलों के लिए भौतिक बुनियादी ढांचा प्रदान करती हैं और सामुदायिक स्कूलों में विकलांग बच्चों के नामांकन के लिए पहुंच सुनिश्चित करती हैं। प्रशिक्षित आंगनवाड़ी (जमीनी स्तर पर) कार्यकर्ता इस गतिविधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सामान्य शिक्षकों को एक समर्थन प्रणाली और फिजियोथेरेपिस्ट की एक बैकअप टीम के रूप में संसाधन शिक्षकों को भी प्रदान करता है। एनजीओ सामान्य शिक्षकों को जागरूकता और अभिविन्यास प्रशिक्षण प्रदान करता है, सामग्री विकसित करता है और विकलांग बच्चों द्वारा सीखने की सुविधा के लिए पाठ्यक्रम के संशोधन में सामान्य शिक्षकों का समर्थन करता है। अन्य सहायक निकाय सर शापुरजी बिलिमोरिया फाउंडेशन है। यह एक शिक्षक विकास पहल है, जो विकलांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य शिक्षकों के लिए इन-सर्विस प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसके अलावा, स्कूल लीवर के लिए तीन साल का पूर्व-सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। प्रशिक्षण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों के सीखने की सुविधा प्रदान करने में सक्षम हों। व्यावहारिक अनुभव, भागीदारी सीखने की पद्धति के संपर्क में आना और कई सेटिंग में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की क्षमता को मानव विकास पर ध्यान देने के साथ एक साथ जोर दिया जाता है। कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन, महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। शिक्षा की अपर्याप्त नीतियां - विभिन्न विकलांगों को अलग-अलग समर्थन की आवश्यकता होती है। समावेशी प्रथाओं का समर्थन करने के लिए कुशल और प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या विभिन्न प्रकार की विकलांगता की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
निरर्थक पाठ्यक्रम - विकलांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक लचीलेपन की कमी है। पारिवारिक दृष्टिकोण - परिवारों को अपने बच्चे की विशेष विकलांगता, इसके प्रभाव और उनके बच्चे की क्षमता पर इसके प्रभाव के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। इससे अक्सर निराशा की भावना पैदा होती है। भारत में विकलांग बच्चों की बेहतर शिक्षा बनाने के उपाय दिसंबर 2002 में संशोधित भारत के संविधान में प्रावधान है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार) के अनुसार, राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और अन्य का एक व्यापक और एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है। यह कार्यक्रम एक 'शून्य अस्वीकृति नीति' को अपनाता है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा प्रणाली से बाहर न रह जाए। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों सहित सभी बच्चों को आठ साल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण, विकल्प और रणनीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का भी समर्थन करता है। इस क्षेत्र में कुछ प्रयास नीचे दिए गए हैं: विकलांग बच्चों के लिए परिवहन सुविधाएं - विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और कम करने के लिए परिवहन सुविधाएं। इस आशय की सुविधाएं नीचे दी गई हैं: अपने बच्चों को परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाले स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकलांग बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त परिवहन की सुविधा भी मिले। इसका मतलब होगा सुविधाओं की उपलब्धता ताकि व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के पास परिवहन तक पहुंच हो और अन्य विकलांग बच्चों ने सेवाओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की। जो स्कूल अपने बच्चों को परिवहन की सुविधा प्रदान नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने स्कूलों में पढ़ने वाले विकलांग बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप परिवहन वाहनों को काम पर रखने / व्यवस्थित करके एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। यदि विकलांग बच्चों के लिए परिवहन सुविधा की व्यवस्था करना संभव नहीं है, तो एसोसिएशन, स्व-सहायता समूहों और नागरिक कल्याण समूहों के गठन के माध्यम से विकलांग बच्चों के माता-पिता की मदद से आवश्यक व्यवस्था की जा सकती है। वास्तु बाधाओं को दूर करना - स्कूलों, कॉलेजों या व्यावसायिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अन्य संस्थानों से वास्तु बाधाओं को हटाना। इस दिशा में प्रयास नीचे दिए गए हैं: निर्माण की जा रही सभी नई स्कूल इमारतों को शहरी मामलों और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा जारी विकलांग और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित रैंप, रेलिंग और अन्य सुविधाओं जैसे बाधा मुक्त सुविधाओं के लिए प्रदान करना चाहिए। ये दिशानिर्देश निर्मित वातावरण में बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करने के लिए मानक निर्धारित करते हैं। सभी मौजूदा स्कूलों को अपने स्कूल भवनों को इस तरह से संशोधित करना चाहिए कि वे बाधा मुक्त हो जाएं।
रैंप आदि के प्रावधान सहित बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण। क्षेत्र में उपयुक्त और उपलब्ध स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री और उपयुक्त तकनीक का उपयोग करके किया जाना चाहिए। योग्य सिविल इंजीनियरों के मार्गदर्शन में संरचनात्मक डिजाइनिंग / संशोधन किया जाना चाहिए। एसएसए, आईईडीसी आदि सहित विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं में उपलब्ध धन। उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। सहायक सामग्री की आपूर्ति- स्कूल में भाग लेने वाले विकलांग बच्चों को पुस्तकों, वर्दी और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति और नीचे उल्लिखित हैं: विकलांग बच्चों को नियमित रूप से स्कूलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें मुफ्त पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जानी चाहिए। आईईडीसी योजना में विकलांग बच्चे के प्रति वर्ष 400 रुपये प्रति वर्ष तक की पुस्तकों और स्टेशनरी पर खर्च करने के लिए अनुदान सहायता का प्रावधान है। इसका उपयोग किया जाना चाहिए। विकलांग बच्चों को भी वर्दी और अन्य सामग्री मुफ्त में प्रदान की जानी चाहिए। विकलांग बच्चों को शिक्षण / शिक्षण सहायता प्रदान की जानी चाहिए जैसे: नेत्रहीन विकलांग बच्चों के लिए- ब्रेल पुस्तकें, टॉकिंग बुक्स, गणित किट, विज्ञान किट, संवेदी प्रशिक्षण किट, गतिशीलता के लिए कैन, टेक्स्ट-टू-स्पीच सॉफ्टवेयर और ब्रेल कीबोर्ड वाले कंप्यूटर हार्डवेयर आदि। विकलांगों को सुनने के लिए - क्लिनिकल ऑडियोमीटर, पोर्टेबल ऑडियोमीटर, स्पीच ट्रेनर, भाषण और श्रवण बाधित, भाषण मान्यता सॉफ्टवेयर और अन्य प्रासंगिक उपकरणों के लिए कान-मोल्ड बनाने के लिए एक माइक्रोमीटर। बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना- विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना नीचे उल्लिखित है: शिक्षा की लागत को निधि देने के लिए छात्रवृत्ति योग्यता के आधार पर विकलांग बच्चों को प्रदान की जाती है। मौद्रिक रूप में विकलांग छात्रों को सीधे या स्कूलों को लिखित लागत के रूप में छात्रवृत्ति दी जा सकती है। छात्रवृत्ति के साथ प्रदान किए जा रहे विकलांग छात्रों की सूची का अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में अलग से उल्लेख और चर्चा की जानी चाहिए। छात्रवृत्ति-धारकों की सूची को नियमित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। शिकायतों के निवारण के लिए उपयुक्त रूप- विकलांग बच्चों के प्लेसमेंट के बारे में माता-पिता की शिकायतों के निवारण के लिए उपयुक्त फॉर्म की स्थापना नीचे दी गई है विकलांग बच्चों के माता-पिता की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रत्येक स्कूल में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना की जानी चाहिए। अभिभावक शिक्षक संघ की नियमित बैठकें सुनिश्चित की जानी चाहिए।
एसएसए के तहत स्थापित स्कूल प्रबंधन समितियों और ग्राम शिक्षा समितियों का उपयोग विशेष जरूरतों वाले बच्चों के माता-पिता की शिकायतों को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। कॉलेजों को भी इसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। ब्लाइंड छात्रों के लिए परीक्षा में संशोधन- कम दृष्टि वाले नेत्रहीन छात्रों और छात्रों के लाभ के लिए विशुद्ध रूप से गणितीय प्रश्नों को समाप्त करने के लिए परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त संशोधन इस क्षेत्र में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा परीक्षाओं में विकलांग बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए गए प्रयास निम्नलिखित हैं: दृश्य इनपुट के आधार पर विशेष कौशल की आवश्यकता वाले प्रश्नों के बदले एक वैकल्पिक प्रश्न गणित और विज्ञान में सेक के लिए प्रदान किया जा रहा है। स्कूल परीक्षा (दसवीं कक्षा)। ब्लाइंड, शारीरिक रूप से विकलांग और डिस्लेक्सिक छात्रों को एक amanuensis (प्रतिलेखक) का उपयोग करने की अनुमति है। amanuensis को उस कक्षा से कम का छात्र होना चाहिए जिसके लिए उम्मीदवार परीक्षा दे रहा है। नेत्रहीन विकलांग छात्रों (कम दृष्टि के साथ) प्रदर्शित होने वाले बढ़े हुए प्रिंट के साथ प्रश्न पत्र प्रदान किए जाते हैं। विकलांग उम्मीदवारों को बाहरी परीक्षा के प्रत्येक पेपर के लिए अतिरिक्त एक घंटे (60) मिनट की अनुमति है। तीसरी भाषा में परीक्षा से छूट दी जाती है। केंद्र अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे जहां तक संभव हो ग्राउंड फ्लोर पर ऐसे उम्मीदवारों की परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था करें। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को विशेष रूप से अपनी श्रेणी का संकेत देना है और यह भी बताना है कि क्या उन्हें मुख्य उत्तर पुस्तिका में दिए गए कॉलम में एक लेखक के साथ प्रदान किया गया है। विकलांग बच्चों को सीबीएसई द्वारा विस्तारित उपरोक्त सुविधाओं के अलावा, नेत्रहीन छात्रों और कम दृष्टि वाले छात्रों के लाभ के लिए विशुद्ध रूप से गणितीय प्रश्नों को खत्म करने का प्रयास किया जाना चाहिए। श्रवण बाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम पुनर्गठन- श्रवण हानि के साथ छात्रों के लाभ के लिए पाठ्यक्रम का पुनर्गठन उन्हें अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में केवल एक भाषा लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए। समावेशी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसलिए बाल केंद्रित शिक्षाशास्त्र पर जोर दिया जाता है।
विकलांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करने का पाठ्यक्रम विशेषज्ञों के परामर्श से उपयुक्त रूप से विकसित किया जाना चाहिए ताकि ये बच्चे नियमित कक्षाओं में अन्य बच्चों के साथ मिलकर सीख सकें। विकलांग बच्चों के लिए सीबीएसई द्वारा किए गए पाठ्यक्रम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। किए गए संशोधन नीचे प्रस्तुत किए गए हैं: विकलांग बच्चों (डिस्लेक्सिया, अंधा, स्पास्टिक और दृश्य हानि वाले उम्मीदवार) के पास दो के मुकाबले एक अनिवार्य भाषा का अध्ययन करने का विकल्प है। उनके द्वारा चुनी गई भाषा बोर्ड द्वारा निर्धारित तीन भाषा फॉर्मूला की समग्र भावना के अनुरूप होनी चाहिए। एक भाषा के अलावा, वे निम्नलिखित विषयों में से किसी भी चार की पेशकश कर सकते हैं: गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, दूसरी भाषा, संगीत, चित्रकारी, गृह विज्ञान और परिचयात्मक सूचना प्रौद्योगिकी। हालांकि ऐसे बच्चों की शिक्षा पश्चिमी दुनिया के प्रयासों के बराबर नहीं है, लेकिन उपर्युक्त पर एक नज़र डालते हुए, भारत में विकलांग बच्चों की शिक्षा में समय बीतने के साथ सुधार हो रहा है। इस क्षेत्र में सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कई प्रयास / नीतियां बनाई और कार्यान्वित की जा रही हैं। ऐसे बच्चों के माता-पिता के नैतिक कर्तव्य पर जोर देना भी भारत में विकलांग बच्चों की शिक्षा के कारण का एक बड़ा कारक है।
[1) सोच का फलसफ
बचपन से ही हम यह सुनते आए हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है। लोग कहते हैं- समय बहुत बदल गया है। लेकिन समय वैसा ही है, जैसा पहले था। साल के वही बारह महीने हैं, दिन के वही चौबीस घंटे, सूरज अब भी पूर्व दिशा से ही निकलता है और चंद्रमा आज भी अपनी तय गति से आसमान में चलता है। प्रकृति ने अपनी लय नहीं बदली, ब्रह्मांड का संचालन यथावत है। बदलाव अगर नहीं आया है, तो वह हमारी सोच में, जीवनशैली में और हमारे दृष्टिकोण में । हमारी मानसिकता आज ऐसी हो गई है कि हम अपनी असफलताओं और कठिनाइयों का उत्तर समय पर मढ़ देते हैं। हमारी यह आदत बन चुकी है कि जब किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती, तो हम तुरंत कह देते हैं- 'अब पहले जैसा समय नहीं रहा।' लेकिन सच्चाई यह है कि समय को दोष देकर हम अपने कर्तव्यों से बच नहीं सकते। समय तो एक मौन साक्षी है, जो न किसी की प्रशंसा करता है, न आलोचना । वह केवल चलता रहता है। हर युग में समय ने किसी को महान बनाया है, तो किसी को नष्ट भी किया है। यह सब उस व्यक्ति की सोच, उसके कर्म और दृष्टिकोण पर निर्भर रहा है। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां तकनीक, संसाधन और अवसर पहले से कहीं अधिक हैं। बावजूद इसके, लोग अधिक तनावग्रस्त हैं, अधिक असंतुष्ट हैं। इसका कारण केवल बाहरी नहीं, आंतरिक है । हमारी सोच नकारात्मकता से भर गई है, हमारी सहनशीलता में कमी आई है और हमने अपने जीवन की बागडोर दूसरों या 'समय' के हाथों में सौंप दी है। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन की दिशा और दशा हमारे ही हाथ में होती है। हम जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसा ही जीवन बनाते हैं। हमारी इस प्रवृत्ति का असर हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र पर भी पड़ता है। जब कोई युवा प्रयास करने से पहले ही यह मान लेता है कि 'अब समय अच्छा नहीं है', तो वह कभी पूरी तरह प्रयास ही नहीं करता । जब कोई बुजुर्ग वर्तमान पीढ़ी की आलोचना करते हुए कहता है कि 'हमारे समय में ऐसा नहीं होता था', तो वह अपनी जिम्मेदारी से बच जाता है। समय को कोसना आसान है, लेकिन आत्ममंथन करना कठिन। और हम आसान रास्ता चुनते हैं। यह प्रवृत्ति केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रही। यह समाज की सोच बन चुकी है। हम अपने आसपास देख सकते हैं कि कैसे ज्यादातर लोग अपनी असफलता, आलस्य और कमजोरी का कारण समय को मानते हैं । लेकिन वह समय किसी अन्य व्यक्ति के लिए अवसर बन जाता है। इतिहास ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा पड़ा है, जब विषम परिस्थितियों में भी कुछ लोगों ने असाधारण कार्य किए। उन्होंने समय को साधन नहीं माना, बल्कि साधना का माध्यम बनाया।
हमें यह समझना होगा कि सोच की शुद्धता ही जीवन में सच्चा परिवर्तन ला सकती है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं होता, लेकिन हर दिन का छोटा प्रयास मिलकर बड़ी सफलता का आधार बनता है। और यह तभी संभव है जब हम समय से भागें नहीं, बल्कि उसका सम्मान करें, इसका उपयोग करें। समय न किसी के पक्ष में है, न विरोध में। वह केवल अवसर देता है - हर व्यक्ति को, हर दिन को । यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस अवसर का क्या करते हैं। जो लोग समय को दोष देने में लगे रहते हैं, वे प्रगति की राह से भटक जाते हैं। वहीं, जो व्यक्ति समय को साधते हैं, अनुशासन में रहते हैं और हर दिन को एक नई शुरुआत मानते हैं, वे अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयां छूते हैं। इसके लिए हमें आत्मचिंतन की आवश्यकता है । हमारी सबसे बड़ी जंग बाहरी हालात से नहीं, हमारी आंतरिक सीमाओं से है। जब तक हम अपनी सोच को परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक कोई भी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं बन सकती । हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि सकारात्मक परिवर्तन केवल सोचने से नहीं आता, उसके लिए निरंतर अभ्यास, अनुशासन और आत्मनियंत्रण चाहिए। हमें खुद को उन आदतों से मुक्त करना होगा जो हमारी प्रगति में बाधा बनती हैं। जैसे टालमटोल की प्रवृत्ति, दूसरों को दोष देना, और निरंतर शिकायत करना । जब हम इन आदतों से ऊपर उठते हैं, तभी हम जीवन की वास्तविक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। परिवर्तन की यात्रा स्वयं से शुरू होती है। अगर हम चाहते हैं कि समाज बदले, देश बदले, तो पहले हमें स्वयं को बदलना होगा। अपने विचारों को ऊंचा करना होगा, अपने कार्यों को उद्देश्यपूर्ण बनाना होगा और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीना होगा। यही वह रास्ता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अपने बच्चों को भी हमें यही सिखाना चाहिए कि समय को दोष देना एक कमजोर सोच है। उन्हें यह सिखाना होगा कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक पाया जा सकता है, अगर दृष्टिकोण सही हो । इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम स्वयं उस सकारात्मकता के उदाहरण बनें। हमारे कर्म, हमारी ईमानदारी और हमारी जीवनशैली ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हो सकती है। समय एक दर्पण की तरह है । वह वही दिखाता है जो हम हैं। अगर हम उसमें सफलता, आशा और ऊर्जा देखना चाहते हैं, तो पहले हमें वह सब अपने भीतर पैदा करना होगा। समय को दोष देना छोड़कर अगर हम हर दिन को अवसर की तरह देखें और अपने विचारों तथा कर्मों को उसकी दिशा में लगाएं, तो वही समय जो हमें अब कठिन लगता है, वही हमारी सफलता की कहानी बन सकता है। समय नहीं बदला है। अगर किसी में बदलाव की जरूरत है, तो वह हम हैं । हमारा दृष्टिकोण, अनुशासन और हमारी कर्मनिष्ठा ही इस जीवन की असली दिशा तय करेंगे । यही सच्ची प्रेरणा है, यही सच्चा आत्मबोध ।
[2) आभासी से ज्यादा कीमती है असली जिंदगी
विजय गर्ग
हाल में एक इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर, मिशा ने आत्महत्या कर ली, जिसका कारण इंस्टाग्राम पर फालोअर्स और लाइक्स की घटती संख्या बताया जा रहा है। उसकी पहचान और आत्मविश्वास पूरी तरह से उसकी वर्चुअल उपस्थिति से जुड़े थे। जब उसका 'डिजिटल आईना' दरका, तो वह खुद को पहचान नहीं पाई। यह घटना एक गंभीर पैटर्न को दर्शाती है, जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं। आज की पीढ़ी 'लाइक्स' और 'फालोअर्स' के जंगल में भटक रही है। बच्चे अब किताबों से नहीं, बल्कि रील्स से दुनिया को समझते हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर घंटे औसतन एक छात्र आत्महत्या कर रहा है। इन आत्महत्याओं का कारण अब केवल परीक्षा या नौकरी नहीं, बल्कि आनलाइन पहचान भी है, जो पल में बनती और मिटती है। हमने बच्चों को 'प्रेजेंटेशन' बनाना सिखाया, लेकिन खुद से बात करने का कौशल नहीं सिखाया। हमने उन्हें 'पब्लिक स्पीकिंग' सिखाई, लेकिन 'आत्म-स्वीकृति' की भाषा नहीं सिखाई। हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर चुके हैं, जहां रील्स पर हंसते हुए युवा वर्ग अंदर ही अंदर घुट रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस के एक अध्ययन के अनुसार, इंटरनेट मीडिया से अत्यधिक जुड़ाव रखने वाले 70 प्रतिशत युवा समय-समय पर डिप्रेशन, चिंता या आत्म-संदेह का सामना करते हैं। आत्मसम्मान का मूल्य अब 'फालोअर्स' की संख्या में मापा जा रहा है। जब आभासी दुनिया से मिलने वाली मान्यता घटती है, तो कई युवा खुद को व्यर्थ मानने लगते हैं। हम केवल यह देखते कि कोई यूट्यूबर एक करोड़ कमा रहा है, लेकिन यह नहीं पूछते कि वह किन तनावों से गुजर रहा है। स्कूलों में 'डिजिटल इथिक्स' की जगह 'कोडिंग' सिखाई जा रही है, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि हम बच्चों को समझाएं कि वर्चुअल दुनिया में खुद को खो देना 'प्रोग्रेस' नहीं, बल्कि 'पतन' है।
सरकार को चाहिए कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स को रेगुलेट करे। फालोअर्स का उतार-चढ़ाव 'जीवन और मृत्यु' का सवाल न बन पाए, इसके लिए एल्गोरिदम से ज्यादा संवेदना की आवश्यकता है। समाज, परिवार और शिक्षा प्रणाली को यह स्वीकार करना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य कोई 'लग्जरी' विषय नहीं है, यह उतना ही अनिवार्य है जितना शारीरिक स्वास्थ्य | स्कूलों में 'डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य' को एक विषय के रूप में शामिल करना चाहिए। बच्चों को यह सिखाना होगा कि उनकी असली पहचान और आत्मसम्मान स्क्रीन पर दिखने वाले आंकड़ों से नहीं जुड़ने चाहिए। हमें अपने बच्चों से कहना चाहिए, "तुम जैसे हो, वैसे ही ठीक हो। तुम्हारी अहमियत किसी स्क्रीन पर नहीं, इस जीवन में है। "