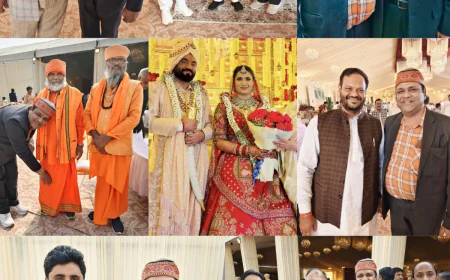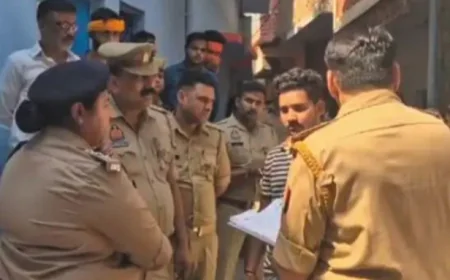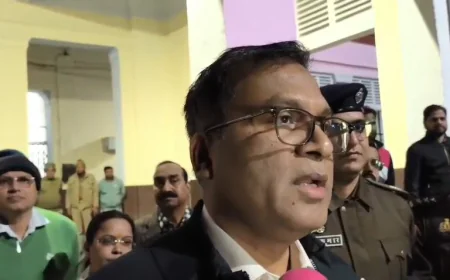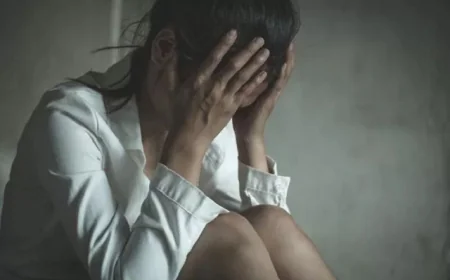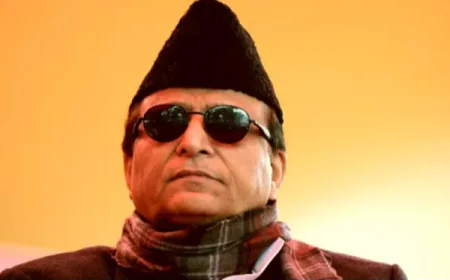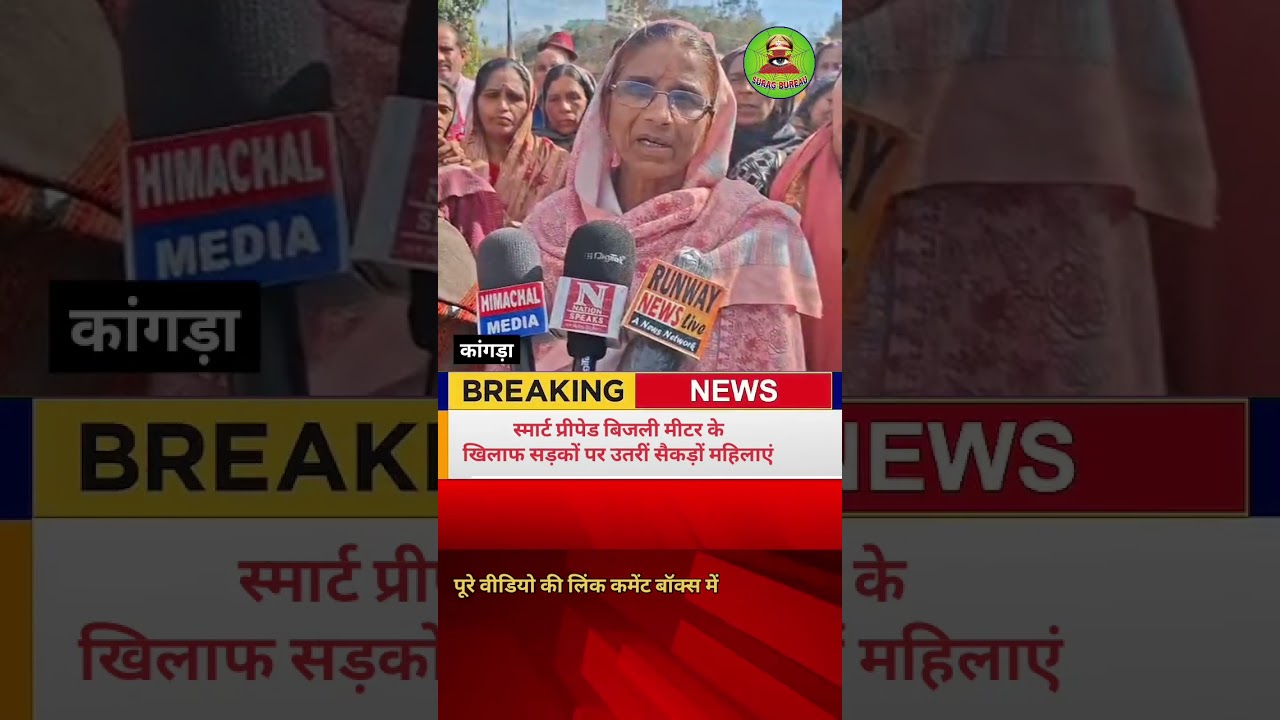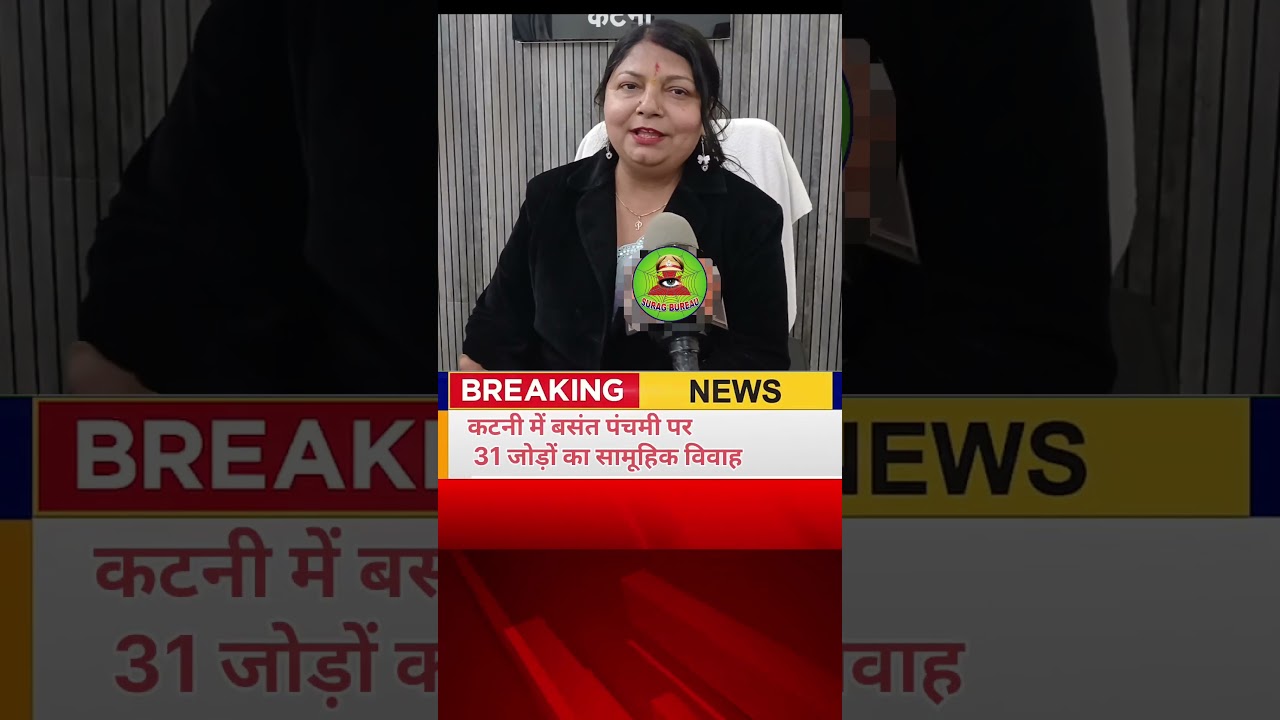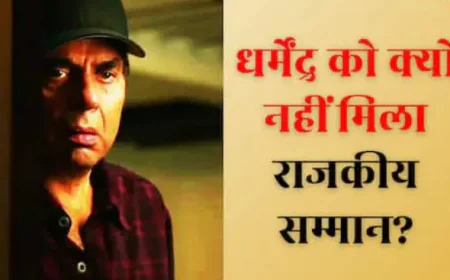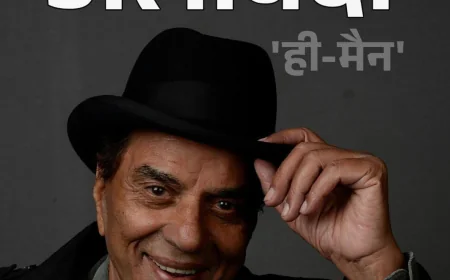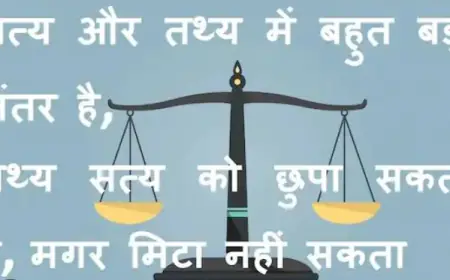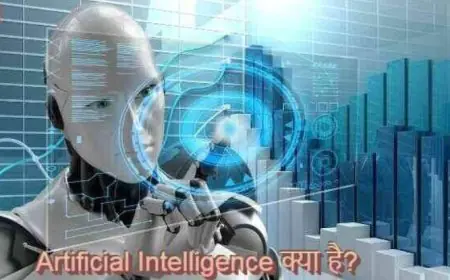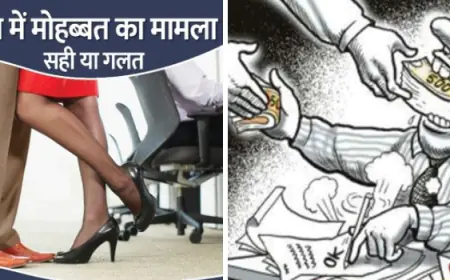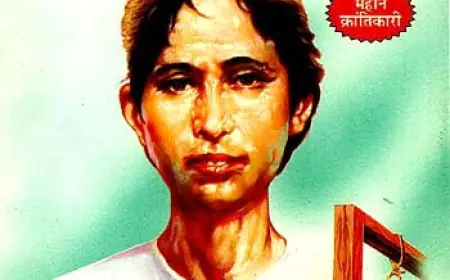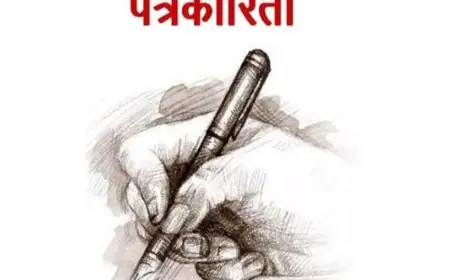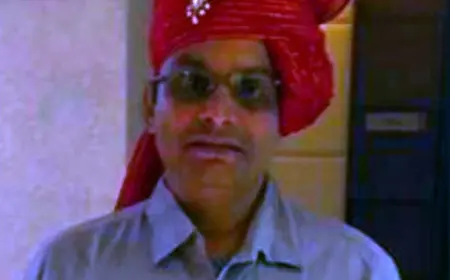डिजिटल युग में स्त्री सशक्तीकरण

डिजिटल युग में स्त्री सशक्तीकरण -
आ ज के डिजिटल युग में इंटरनेट तक महिलाओं की पहुंच में सुधार सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सशक्तीकरण के लिए नहीं, बल्कि यह समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक है। डिजिटल प्रौद्योगिकी महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय स्वतंत्रता के नए अवसर प्रदान कर सकती है, जो समाज में लैंगिक असमानता को कम करने में मदद करती है। हालांकि, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन प्रयासों में महिलाओं की कमजोरियों और सुरक्षा संबंधित समस्याओं का भी समाधान किया जाए। भारत में 'डिजिटल डिवाइड', विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के संदर्भ में, एक प्रमुख समस्या बनकर उभरी है। 'ग्लोबल सिस्टम फार मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन' और 'आक्सफैम ' के 2022 और 2023 के आंकड़ों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की इंटरनेट तक पहुंच सुधार की आवश्यकता है।
मसलन, 2022 में मोबाइल स्वामित्व में लैंगिक अंतर में 11 फीसद की कमी आई है, लेकिन मोबाइल इंटरनेट उपयोग में महिलाओं का हिस्सा 130 1 फीसद पर स्थिर है, जिससे लैंगिक अंतर 40 फीसद तक बढ़ गया है। इसके अलावा, महिलाओं में मोबाइल इंटरनेट जागरूकता 60 फीसद से भी कम है। यह दर्शाता है कि महिलाओं को डिजिटल दुनिया पूरी तरह से समाहित करने के लिए अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। 'महिलाओं के लिए डिजिटल': जुड़ाव की चुनौतियां सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ी हैं। महिलाओं को साइबर दुर्व्यवहार, आनलाइन उत्पीड़न और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासकर जब वे सोशल मीडिया मंचों का उपयोग करती हैं। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को बल्कि उनके डिजिटल जुड़ाव को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
भारत में इंटरनेट, मोबाइल फोन की पहुंच और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि इन इन सुधारों को लैंगिक समानता की दृष्टि से लागू किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के बीच इंटरनेट उपयोग में गहरा अंतर है, जहां पुरुषों द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने की संभावना महिलाओं की तुलना में दोगुनी है। नतीजतन, महिलाओं के लिए डिजिटल अवसरों तक पहुंच में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे उनके आर्थिक अवसरों में समझौता होता है। | डिजिटल साक्षरता की कमी और मोबाइल इंटरनेट उपयोग की जटिलताएं इस अंतर को और बढ़ा देती हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की की गई 'डिजिटल इंडिया' पहल ने डिजिटल पहुंच को बढ़ाने का महत्वपूर्ण किया है, लेकिन इस पहल में महिला केंद्रित मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। गुरुमूर्ति और चामी (2018) के अनुसार, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दस्तावेज में कोई स्पष्ट लिंग-विभाजित प्रशिक्षण लक्ष्यों का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे महिलाओं को डिजिटल दुनिया में समावेशी रूप से शामिल करने में असमर्थता व्यक्त होती है। इसके अलावा, यह पहल यह पहचानने में भी विफल है कि महिलाओं द्वारा इंटरनेट उपयोग की दर में वृद्धि के लिए डिजिटल साक्षरता और कौशल के अवसरों की आवश्यकता है।
डिजिटल प्रौद्योगिकियों का समावेशी विकास समाज में सभी वर्गों को आर्थिक मौके, शिक्षा और गतिशीलता संबंधी बाधाओं को पार करने का अवसर प्रदान कर सकता है। डिजिटल तकनीकें नई नौकरियां पैदा कर, डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को सुगम बना और डिजिटल व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहित कर सकती हैं। इसके अलावा, डिजिटल प्रौद्योगिकी से सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने और नागरिकों की अधिक सहभागिता को बढ़ावा देने में भी मदद मिल सकती है। भारत में इंटरनेट उपयोग तेजी से बढ़ा है, लेकिन इस प्रगति के बावजूद, डिजिटल विभाजन अभी भी एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार भारत में केवल 33 फीसद महिलाओं ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, जबकि 57 फीसद पुरुषों ने इसका उपयोग किया है। स्मार्टफोन के आंकड़े इस असमानता को और स्पष्ट करते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, ग्रामीण भारत में केवल 26 फीसद महिलाओं के पास स्मार्टफोन है, जबकि 49 फीसद पुरुष स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता और गहरी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण भारत पुरुषों द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने की संभावना महिलाओं की तुलना में ल लगभग दोगुनी है। पूरे भार भारत में ऐसा कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जहां महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में इंटरनेट का अधिक उपयोग किया हो।
महिलाओं की डिजिटल कनेक्टिविटी का सीधा असर उनके वित्तीय सशक्तीकरण पर भी पड़ता है। 'डिजिटल बैंकिंग' और 'मोबाइल मनी ट्रांजेक्शन' ने महिलाओं के लिए वित्तीय लेन- देन को अधिक सुविधाजनक और लचीला बना दिया है। 'इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया' की 2022 की रपट' अनुसार, डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी में सुधार से 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सौ अरब डालर की वृद्धि हो सकती है। इस संभावित वृद्धि का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को होगा, क्योंकि डिजिटल मंच उन्हें कौशल विकास, रोजगार और उद्यमशीलता के नए अवसर प्रदान करते हैं। डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या हर साल लगभग 2.5 फीसद की दर से बढ़ रही है। इससे न केवल महिलाएं 'स्टार्टअप्स' में भागीदारी कर रही हैं, बल्कि वे नेतृत्वकारी भूमिका निभाकर तकनीकी नवाचार को भी बढ़ावा दे रही हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ग्रामीण महिलाओं को डिजिटलीकरण के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है। इसने उन्हें आनलाइन मंचों पर अपने छोटे व्यवसायों को विस्तार देने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद द की है। । रपटों के मुताबिक जिन महिलाओं के की पहुंच वे लगभग 140 फीसद अधिक आय अर्जित करती हैं।
इंटरनेट उपभोग बढ़ाने के प्रयासों में 'डिजिटल डिवाइड' खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए, इन प्रयासों में महिलाओं और लड़कियों को इंटरनेट से होने वाली परेशानियों पर भी विचार करना चाहिए। भारत सरकार ने अपने 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के माध्यम से पूरे भारत में डिजिटल पहुंच और बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए एक स्पष्ट प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें गूगल, फेसबुक और अमेजन जैसे उद्योग दिग्गजों द्वारा इस पहुंच में तेजी लाई गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रदान किए गए डेटा इन मुद्दों पर हमारी प्रगति के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन यह भी जांचना महत्त्वपूर्ण है कि अपनाए गए दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक मानदंडों और संरचनाओं को मजबूत नहीं करते, जो असमानताएं बढ़ाते हैं। 'डिजिटल इंडिया' जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य 'डिजिटल डिवाइड' को समाप्त करना है, लेकिन यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि महिलाएं पूरी तरह अवसरों से लाभ उठा सकें। महिलाओं के लिए डिजिटल सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वे इंटरनेट का उपयोग सुरक्षित और सशक्त रूप से कर सकें।
● वृद्ध पशुओं के संरक्षण का महत्व -
जीव-जंतुओं का संरक्षण आज के समय में पर्यावरणीय चिंताओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है। परंतु देखा गया है कि यह चर्चा अक्सर विलुप्तप्राय प्रजातियों और उनके बचाव तक ही सीमित रहती है। वृद्ध जानवरों के संरक्षण का महत्व, जो उनके झुंड या समाज में मार्गदर्शक और संरक्षक की भूमिका निभाते हैं, आमतौर पर उपेक्षित रह जाता है। हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है कि बूढ़े और बुद्धिमान जानवर अपने समूहों एवं पर्यावरण में स्थायित्व बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी यह जरूरी है। मानवीय गतिविधियों के कारण न केवल वृद्ध व बुद्धिमान जीवों की संख्या में गिरावट आ रही है, बल्कि उनके साथ पर्यावरणीय और जैविक जानकारियां भी विलुप्त हो रही हैं। हालिया अध्ययन चार्ल्स डार्विन विवि, आस्ट्रेलिया के नेतृत्व में किया गया है और इसे साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। अध्ययन में बताया गया है कि वृद्ध व बुद्धिमान जानवर जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हाथी, व्हेल, बंदर और अन्य लंबे समय तक जीने वाली प्रजातियां अपने समूह के लिए अनुभवजन्य ज्ञान का स्रोत होते हैं, जो उनकी संतानों और समुदाय के लिए फायदेमंद होता है। उदाहरण के तौर पर, वृद्ध हाथियों (मैट्रियार्क्स) को सूखे के समय जल स्रोतों का पता लगाने और समूह की सुरक्षा का मार्गदर्शन करने में कुशल माना जाता है। इसी तरह वृद्ध व्हेल अपनी संतानों को भोजन प्राप्त करने एवं जटिल समुद्री वातावरण में नेविगेट करने का प्रशिक्षण देती हैं। विशेष रूप से मनुष्यों में, दादी-नानी जैसी संरचनाओं का प्रभाव संतानों के जीवित रहने और उनकी प्रजनन क्षमता पर भी देखा गया है।
इसी तरह मछलियों और ठंडे खून वाले जीवों में वृद्ध और बड़े जीव लंबे समय तक प्रजनन कर सकते हैं और अपनी संतानों की संख्या बढ़ा सकते हैं। कई जानवरों के समूहों में वृद्ध सदस्य नेतृत्व और निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे युवा सदस्यों को प्रशिक्षित करते हैं। वृद्ध जीवों की घटती संख्या के लिए मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। अवैध शिकार और मनोरंजन के लिए जानवरों का शिकार इन प्रजातियों की घटती संख्या का प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवास की कमी और बीमारियां भी इन जीवों की संख्या को प्रभावित कर रही हैं। वृद्ध जीव न केवल अपने समूह के लिए बल्कि मानव समाज और प्रकृति के लिए भी अनमोल हैं। उनके अनुभव और ज्ञान को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हमने अभी कदम नहीं उठाए, तो इसके परिणाम भावी पीढ़ियों के लिए भयावह हो सकते हैं। इसलिए वृद्ध जानवरों को संरक्षित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह प्रकृति और मानवता के हित में भी है।
●सोशल मीडिया के निशान -
आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, खासकर बच्चों और युवा वयस्कों के लिए। हालाँकि ये प्लेटफॉर्म संचार, आत्म-अभिव्यक्ति और सूचना तक पहुंच के लिए ढेर सारे लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन इनके अत्यधिक उपयोग से मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से शरीर की छवि के संदर्भ में। सोशल मीडिया पर सावधानी से तैयार की गई और अक्सर अवास्तविक छवियों की लगातार बाढ़ सुंदरता की विकृत धारणा पैदा करती है, जिससे अपर्याप्तता, असुरक्षा और कम आत्मसम्मान की भावनाएं पैदा होती हैं। युवा व्यक्तियों पर ऐसे संदेशों की बौछार की जाती है जो शारीरिक उपस्थिति को मूल्य के बराबर मानते हैं, जिससे पूर्णता की निरंतर खोज को बढ़ावा मिलता है जिसे कभी भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक अप्राप्य आदर्श की यह निरंतर खोज खाने के विकार, चिंता और अवसाद सहित गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। अवास्तविक सौंदर्य मानकों के अनुरूप होने का दबाव व्यक्तियों को अत्यधिक आहार, व्यायाम और यहां तक कि खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे अस्वास्थ्यकर व्यवहार में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता है। शरीर की छवि पर सोशल मीडिया का प्रभाव इन प्लेटफार्मों में व्याप्त तुलना की संस्कृति से और भी बढ़ गया है।
युवा व्यक्ति लगातार अपनी तुलना अपने साथियों से करते हैं, जिससे अक्सर उनमें ईर्ष्या, असंतोष और बेकार की भावनाएँ पैदा होती हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर गुमनामी और जवाबदेही की कमी व्यक्तियों को साइबरबुलिंग में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे युवा उपयोगकर्ताओं के आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को और नुकसान पहुंच सकता है। नकारात्मक टिप्पणियों और आहत करने वाली टिप्पणियों का लगातार संपर्क स्थायी निशान छोड़ सकता है, जिससे सामाजिक अलगाव, अलगाव और यहां तक कि आत्म-विनाशकारी व्यवहार भी हो सकता है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को मीडिया साक्षरता कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम में एकीकृत करना चाहिए, छात्रों को ऑनलाइन सामने आने वाली छवियों का गंभीर मूल्यांकन करना और सोशल मीडिया चित्रण की अवास्तविक प्रकृति को पहचानना सिखाना चाहिए। माता-पिता और शिक्षकों को आत्म स्वीकृति, शरीर की सकारात्मकता और स्वस्थ आत्म-सम्मान के महत्व के बारे में बच्चों और युवा वयस्कों के साथ खुली और ईमानदार बातचीत में शामिल होना चाहिए। उन्हें उनकी शारीरिक बनावट के बजाय उनकी शक्तियों, मूल्यों और जुनून पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। सरकार को साइबरबुलिंग के खिलाफ सख्त नीतियां भी लागू करनी चाहिए और विविधता और समावेशिता का जश्न मनाने वाले शरीर सकारात्मकता अभियानों को बढ़ावा देना चाहिए।
युवा व्यक्तियों को अपने सोशल मीडिया के उपयोग के प्रति सचेत रहना और आवश्यक होने पर इन प्लेटफार्मों से ब्रेक लेने के लिए प्रोत्साहित करना एक कठिन काम होगा। लेकिन हमें ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो आत्म स्वीकृति को बढ़ावा दें, जैसे शौक पूरा करना, प्रकृति में समय बिताना और आत्म- देखभाल प्रथाओं में संलग्न होना । आत्म-स्वीकृति, आलोचनात्मक सोच और खुले संचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर, हम बच्चों और युवा वयस्कों को लचीलेपन और सकारात्मक आत्म - छवि के साथ डिजिटल दुनिया में नेविगेट करने के लिए सशक्त बना सकते हैं, जिससे लंबे समय में उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा हो सके।
● क्यों ज़रूरी है मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना ?
विवाह के बाद कई दंपती विवाह प्रमाणपत्र नहीं बनवाते। परंतु यह एक कानूनी दस्तावेज़ है जो पति-पत्नी दोनों के विवाह का वैध प्रमाण होता है। यह न केवल विवाह की पंजीकरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है, बल्कि विवाह संबंधी अधिकारों की सुरक्षा भी करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से विवाह पंजीकरण को अनिवार्य घोषित किया। मैरिज सर्टिफिकेट क्यों होना चाहिए ? विवाह के बाद जो लड़कियां अपना सरनेम नहीं बदलतीं, उनके लिए यह दस्तावेज़ विवाह का क़ानूनी सबूत प्रदान करता है। विदेश में वीज़ा और इमिग्रेशन प्रक्रियाओं में पति/पत्नी के रिश्ते को प्रमाणित करने के लिए विवाह प्रमाणपत्र अनिवार्य होता है। बैंक जमा या जीवन बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है, ख़ासकर जब नामांकित व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं हो । पेंशन योजनाओं और अन्य वित्तीय लाभों का दावा करने के लिए भी सर्टिफिकेट आवश्यक है। तलाक़, संपत्ति विवाद और उत्तराधिकार के मामलों में विवाह की वैधता साबित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है।
यदि पति- पत्नी के सरनेम अलग हैं, तो बच्चों की वैधता प्रमाणित करने में यह सहायक होता है । मैरिज सर्टिफिकेट विवाह से संबंधित धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों से महिलाओं की रक्षा करता है और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यदि विवाह प्रमाणपत्र नहीं होगा ... जिन पति-पत्नी की विदेश में साथ रहने या जाने की योजना है उनके लिए विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में वीज़ा और इमिग्रेशन प्रक्रिया में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बैंक जमा, जीवन बीमा या कर्मचारी बीमा पेंशन योजना के तहत, एक विवाहित व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद लाभ के लिए केवल अपनी पत्नी और बच्चों को नामांकित कर सकता है। बिना मैरिज सर्टिफिकेट के इन लाभों का दावा करना मुश्किल हो जाता है। पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति और पैतृक संपत्ति पर महिला के अधिकारों और हितों के दावे को सामान्यतः विवाह की वैधता के आधार पर चुनौती दी जाती है। मैरिज सर्टिफिकेट न होने की स्थिति में महिला अपने अधिकारों का दावा नहीं कर सकेगी। वैवाहिक विवादों या तलाक़ की स्थिति में, मैरिज सर्टिफिकेट न होने के कारण विवाह को अमान्य घोषित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में बिना पंजीकरण और रीति-रिवाजों के किए गए विवाह को अमान्य करार दिया गया था। कई मामलों में, बिना रीति-रिवाजों के विवाह करने या धर्मस्थल में विवाह कर धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में, शिक्षित होने के बावजूद, महिलाएं विवाह प्रमाणपत्र के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब