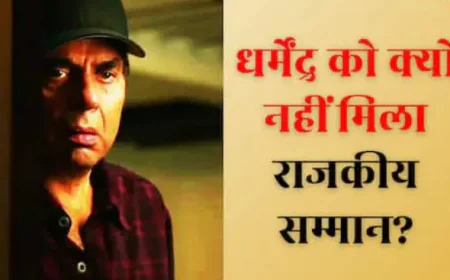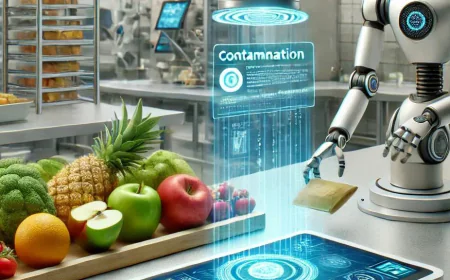विनाश के पाँच तोप: शिक्षा से तहसील तक

विनाश के पाँच तोप: शिक्षा से तहसील तक
शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, थाना और तहसील जैसे पाँच संस्थानों की विफलता गंभीर चिंता का विषय है। शिक्षा अब ज्ञान नहीं, कोचिंग और फीस का बाजार बन चुकी है। स्वास्थ्य सेवाएँ निजीकरण की भेंट चढ़ चुकी हैं, जहाँ इलाज से ज्यादा पैकेज बिकते हैं। चिकित्सा व्यवस्था मुनाफाखोरी का अड्डा बन गई है। थाने न्याय की जगह रिश्वत का केंद्र और तहसील एक कागज़ी भूलभुलैया बनकर रह गई है। इन संस्थाओं को सुधारने की जरूरत हैं।
■ प्रियंका सौरभ
**"शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, थाने औ तहसील। सब मिलकर ताबूत में, ठोंक रहे हैं कील।।" यह दो पंक्तियाँ महज़ अलंकार नहीं, बल्कि उस निराशा का संगीन उद्घोष हैं, जो आम आदमी की उम्मीदों को कुचलकर उसे निराशा की चुम्बक बनाती हैं। ये पाँच स्तंभों से हमारा समाज अपनी नाजुक मिट्टी का संतुलन बनाये रखता है — पर, अफ़सोस, वे स्वयं पत्थर बन चुके हैं।
★ शिक्षा: जहाँ विद्या बिक रही है बचपन से हमें सिखाया गया कि शिक्षा से इंसान का चरित्र बनता है। पर अब चरित्र कहीं बिकता नहीं, बल्कि कोचिंग सेंटर की दीवारों पर टंगा पाया जाता है। दसवीं बोर्ड हो या मेडिकल प्रवेश, सवाल योग्यता का नहीं, पक्षपात और सिफ़ारिश का होता है। वर्दीधारी शिक्षक उस जादुई इकाई में बदल चुके हैं, जहाँ से विद्वता कम, फीस वसूली ज़्यादा जरूरी है। स्मार्ट क्लासरूम में धूल जमी पाठ्यपुस्तकें नहीं, बल्कि अभिभावकों के कष्ट होते हैं। एनआईटी का सपना देखता छात्र, एनपीए (नॉन-परफ़ॉर्मिंग असैट) बन जाता है, क्योंकि रोजगारदाता अब 'डिग्री' नहीं, 'प्रैक्टिकल स्किल्स' मांगते हैं — जिन्हें हासिल करने का रास्ता फीस के अतिरिक्त टेस्ट में दिक्कतें है। वह कोचिंग सेंटर जहाँ प्रवेश परीक्षा की तैयारी होती थी, वह अब नक़दी की परीक्षा लेता है। हर साल लाखों अभिभावक 'अब्ज़ॉर्ब' हो जाते हैं — एक कोचिंग सेंटर की माला में पिरोकर, दूसरा सेंटर की रस्सी से लटका दिए जाते हैं। नतीजा? शिक्षा की किरणें फीकी पड़ चुकी हैं।
★स्वास्थ्य: सेवा नहीं, सेवा शुल्क स्वास्थ्य सेवा का नाम सुनते ही सरकारी अस्पतालों के मरघट जैसे माहौल की याद ताज़ा हो जाती है। जहाँ प्रतीक्षा कक्ष में पंखे हवा नहीं, बल्कि बीमारी फैलाने की तैयारी करते हैं। डॉक्टर गिनती में कम, प्राइवेट विभागीकरण में ज़्यादा। मरीज तो बस एक ‘कैश-काउंटर’ बन कर रह गया है। निजी अस्पतालों ने बीमार ग्राहक को ‘लक्षित बाजार’ मान लिया है। जांच-परीक्षण, एमआरआई, सर्जरी — सब कुछ पैकेज में बिका जाता है। एक छोटी सी खांसी के लिए भी प्रोसिज़र चार्ज लगता है, जबकि कमरे में बिताई एक रात का बिल हृदयाघात से कम नहीं। अगर ग़रीब मौत को गले लगा लेता है, तो उसे सकुशल ताबूत में अंतिम यात्रा के लिए भी केवल ‘शव-परिवहन शुल्क’ अदा करना होता है। एक मरीज की जिद्दी साँसें किसी को नहीं रुलाती; केवल उसका बिल रुलाता है। डॉक्टर अब जीवनदायी गुंजन नहीं, जीवनदायी इनकम-रसीद बन गए हैं। चिकित्सकीय कौशल की जगह, बीमा कंपनी के क्रेडेंशियल्स की कीमत पर सौदा होता है। और जब बीमारी हिम्मत हार जाती है, तो अस्पताल भी ‘फ्री डिस्चार्ज’ का विज्ञापन ऑफ़र कर देता है — ग़रीबों के आखिरी ‘मोक्ष’ का प्रचार। चिकित्सा: इलाज नहीं, मर्ज का मॉल चिकित्सा शब्द का अर्थ होता है बीमारी का निवारण, पर अब मिक्स-फेक्स का बाज़ार सजीव हो गया है।
जनरल प्रैक्टिशनर अब बहुराष्ट्रीय फार्मास्युटिकल कंपनियों के एजेंट की भूमिका निभाते हैं। हर खांसी पर टेबलेट, हर दर्द पर इंजेक्शन; मर्ज मायाजाल बनता चला जाता है। बिना एमआरआई या सीटी—स्कैन के कोई डॉक्टर अब मर्ज का अंदाज़ा नहीं लगाता। कटघरे में तब मरीज आता है, जब उसकी जेब से दवा का डिब्बा गायब हो जाता है। जॉइंट पेन के इंजेक्शन से ‘मेरुदण्ड का व्यापार’ फल-फूल रहा है, और किडनी ट्रांसप्लांट का ‘वॉर रूम’ हड्डियों की चिमत्कार कर रहा है। हर दिन नए मर्ज की लिस्ट एप्रूवल के लिए सीईओ के टेबल पर जमा होती है। यहाँ तक कि आयुर्वेद और यूनानी भी ‘लक्ज़री-ब्रांडेड’ काउंटर में बिकने लगे हैं। प्रभावी हर्बल फ़ॉर्मूलों की जगह, चाय-पत्ती का ढेर और ‘SUV के चक्के’ तुल्य कीमतों में दवा बिक रही है। मरीज तो बस ‘फलता प्रमाणपत्र’ बन कर रह जाता है, जिसकी असली कीमत उसे तब पता चलती है, जब वह बैंक शाखा में ‘सुसाइड नोट’ लिखने बैठता है।
★थाने: न्याय नहीं, नोट छापने की मशीन हमारी कल्पना में पुलिस ‘न्याय का प्रहरी’ थी, पर अब वह ‘प्रहार का दूत’ बन चुकी है। थानों में धूल नहीं, बल्कि रिश्वत का आयोजन होता है। मोल-भाव के बाद मुकदमा दर्ज होता है या ठुकरा दिया जाता है। शिकायतकर्ता को पहले परमिशन लेनी पड़ती है — और यदि रुपये नहीं दिए, तो परमिशन के साथ ‘खामोशी’ भी थमा दी जाती है। मारूति गाड़ी से टकरा भी जाओ, तो कोर्ट-कचहरी की झकझोराहट से पहले चार्जशीट का पेपर वसूली होती है। फास्ट-ट्रैक की जगह, फास्ट-पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम चालू हो गया है। भारी भरकम बजट मिलने के बावजूद, पुलिस स्टेशन का एकमात्र फ़ंड ‘मुझबक़ों की रकम’ बन चुका है। इंसान इतना छोटा हो गया है कि दर्ज शिकायत से पहले उसका ‘राशन कार्ड’ पूछा जाता है। केस फ़ास्ट-ट्रैक की हकीकत एफआईआर के लिए रिश्वत बरी होने के लिए और रिश्वत डीटेंशन में खाने के लिए रिश्वत और जब इंसाफ़ नसीब हो, तब भी वह ‘याचिका शुल्क’ में डूबकर मर जाता है। एक बार पुलिस की अक्षुण्ण मशीन में फँस गए तो पत्ते नहीं, रुपए उड़ते हैं।
★ तहसील: लोकतंत्र का कागज़ी जंगल तहसील एक ऐसा महल है, जहाँ दस्तावेज़ों की भीड़ में इंसान गुम सा हो जाता है। भूमि का बंटवारा हो या जाति-प्रमाण-पत्र, हर चीज़ के लिए ‘पर्ची’ की महफ़िल सजती है। सरकारी स्टांप पेपर, ई-सिग्नेचर, ऑनलाइन पोर्टल — सब आधुनिकता के नाम पर जंजाल हैं। कागज़ी जंगल में सफ़र करते हुए, आदमी भूल जाता है कि उसका मकान है या कागज़ों का ‘ब्रोकरेज’। लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में पसीना सुखता है, लेकिन ‘कमेटी शुल्क’ नहीं सूखता। जाति प्रमाण पत्र के लिए ‘बैकडेटेड’ दस्तावेज़ों का जादूगर हीरो बन जाता है। एक भूल से दस्तावेज़ रद्द, और फिर ‘नया दस्तावेज़’ यानी नया बिल। यहाँ ‘नवाचार’ नाम पर फ्लिपकार्ट-पोशाक की तरह ‘डिजिटल इमेजिंग’ बिक रही है — पर असल में मोबाइल पर मैसेज चेक कराते-कराते आदमी की आत्मा सूख जाती है। ‘ऑनलाइन आवेदन’ में करंसी के बजाय ‘क्रेडिट कार्ड’ रोल करता है। और जो भारी-भरकम फीस भरता है, वही असली ‘अदालत’ में दर्शक बनकर रह जाता है।
★ कब बदलेंगी कीलें? ये पाँचों स्तंभ, जो हमारे विश्वास के आधार थे, आज ताबूत की कीलें बन चुके हैं। हर समाज में विकार होते हैं, पर जहाँ विकार व्यवस्था की आत्मा बन जाए, वहाँ परिवर्तन की पुकार गूँज उठती है। पर क्या हमारी पुकार चुप्पी तोड़ पाएगी?
★हमारी ज़िम्मेदारी है: शिक्षा के निजी कोचिंग मॉल के बजाय सामुदायिक ज्ञान-केन्द्रों का निर्माण करें। स्वास्थ्य सेवाओं को मुनाफ़े के बजाय मानवता के सिद्धांत पर पुनर्निर्मित करें। चिकित्सा व्यावसायीकरण को विनियमन के जरिए रोके—लाभ का नहीं, इलाज का मानदंड बनाए। पुलिस सुधार अधिनियमों को लागू करें—न्याय के प्रहरी को रिश्वत की मशीन न बनने दें। तहसील और प्रशासनिक सेवाओं में पारदर्शिता लाकर ‘कागज़ी जंगल’ को ‘सुनहरे बग़ीचे’ में बदल दें। तब तक तक़दीर की ठोकरें चलेंगी, पर हम खेती की कलम से अंकुरित करेंगे न्याय, सेवा और गरिमा के बीज। तभी शायद ये कीलें ताबूत से जुदा हों, और देश की आत्मा फिर से फड़फड़ाए।