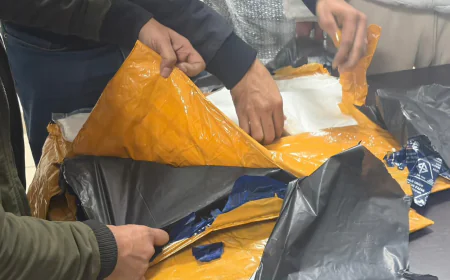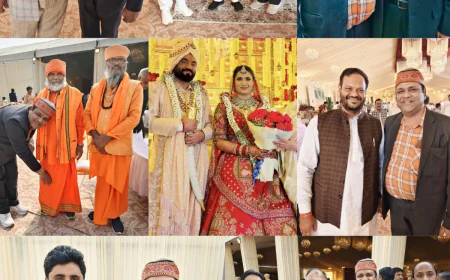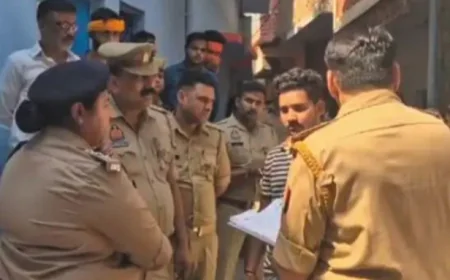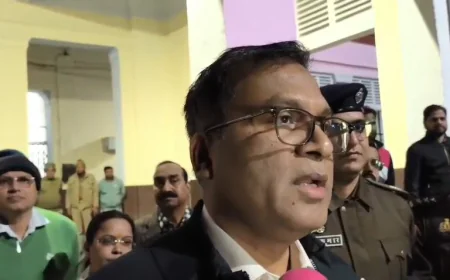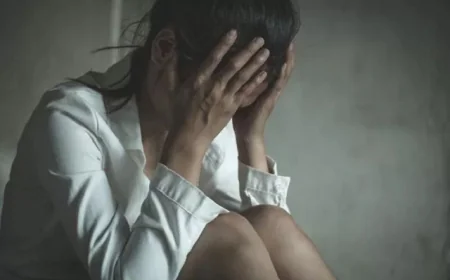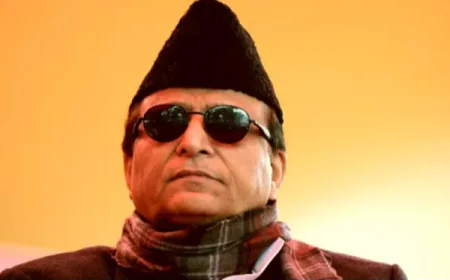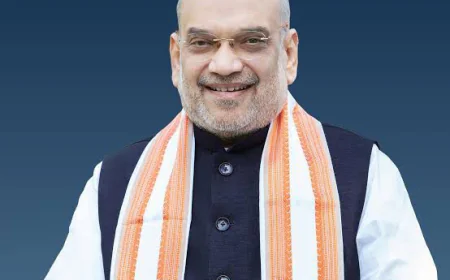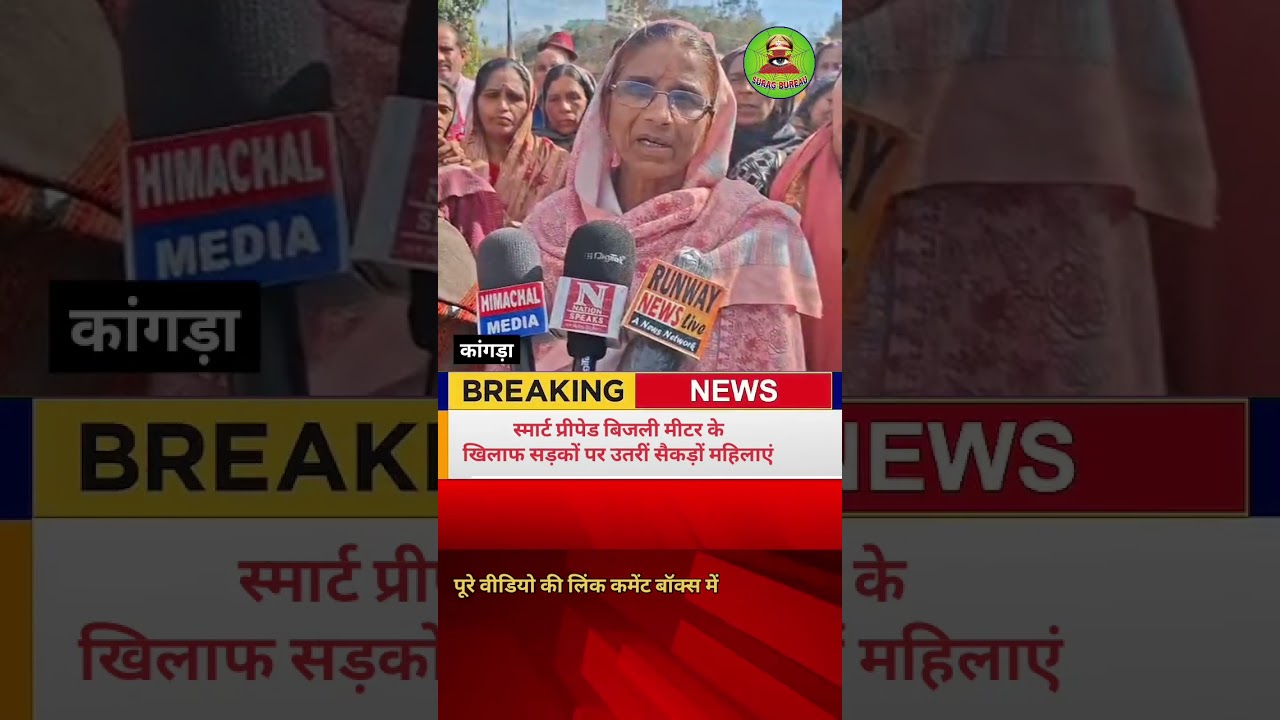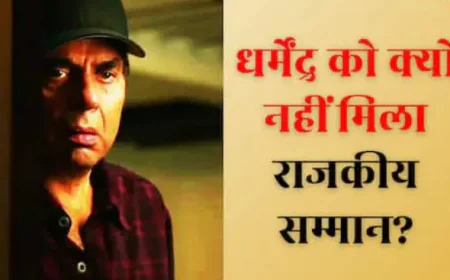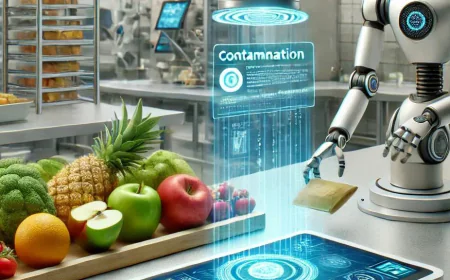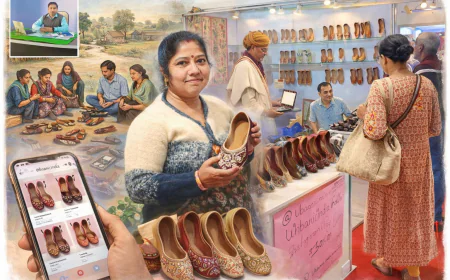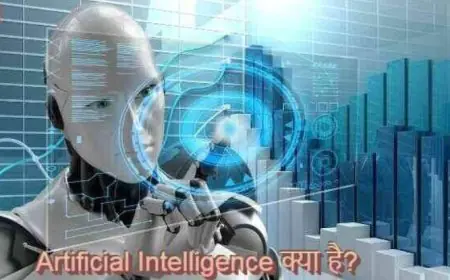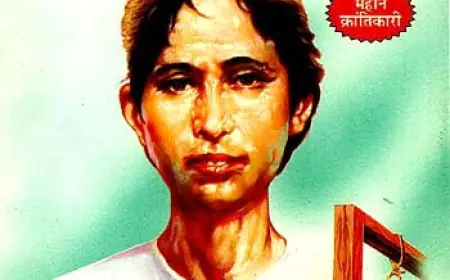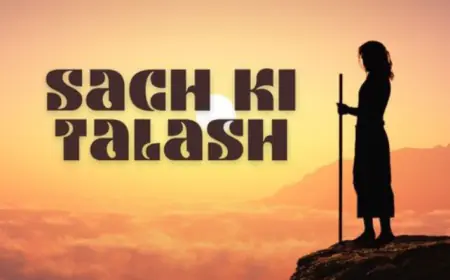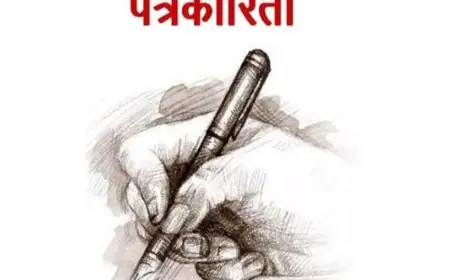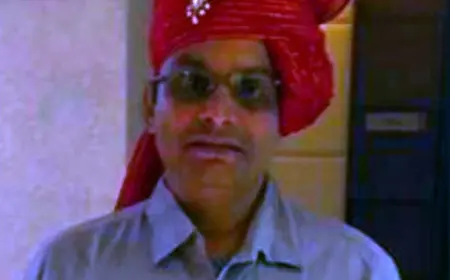चिकित्सा में आत्मनिर्भरता के कदम

चिकित्सा में आत्मनिर्भरता के कदम
विजय गर्ग
केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के साथ आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कई पहल की है। इन कोशिशों से दुनिया में भारत की साख बेहतर हुई है। चंद्रयान 3 3 की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने अब स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों को नया 'काम' सौंपा है। इससे भारत चिकित्सा के क्षेत्र में छलांग लगाने में कामयाब हो सकता है। यह ऐसी योजना है, जो आजाद भारत में पहली बार एक चुनौती के के रूप में पूरी की जानी है। इस तरह की योजना को दुनिया में पहले कभी किसी देश ने नहीं लागू किया। यानी जिन बीमारियों का इलाज कोई नहीं ढूंढ पाया, उसे भारतीय वैज्ञानिक ढूंढेंगे। इसके लिए सरक ने विश्व में प्रथम चुनौती लक्ष्य भी तय किया है, जिसकी जिम्मेदारी नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आइसीएमआर) को सौंपी है। इससे दुनिया में चिकित्सा क्षेत्र में देश की साख एक नए भारत के रूप में बनेगी और यह यह अमेरिका, पेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, जापान और जर्मनी के साथ आगे बढ़ सकेगा। जिन विकसित देशों ने चिकित्सा क्षेत्र में नए और मौलिक शोध के जरिए आश्चर्यजनक परिणाम हासिल किए हैं, वहां के वैज्ञानिकों को सभी जरूरी सुविधाए दी गई भारत भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हमारी जो वैज्ञानिक मेधा, धन, सुविधाएं और उदारीकरण के कारण विदेश चली जाती थी, वह अब भारत में रह कर अपनी विलक्षण प्रतिभा का लोहा मनवाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार शोधार्थी वैज्ञानिकों को सभी कुछ मुहैया करा रही है, जिससे चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हो सकें। सरकार की इस नई योजना को पूरा करने के लिए देश के चिकित्सा संस्थानों को मिल कर काम करना होगा।
कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरे चंद्रयान 3 से प्रेरित होकर दुनिया में पहली बार चिकित्सा के क्षेत्र में भारत एक ऐसी पहल करने जा रहा है, जिससे उसके वैज्ञानिकों को नए और लीक से हट कर विचारों पर काम करने का 1 मौका मिलेगा। गौरतलब है कि देश में वैज्ञानिकों ने कोरोना के दौरान कोविड 19 के टीके तैयार करने अपनी पूरी शोध शक्ति लगा दी थी। केंद्र सरकार ने तीन तरह के टीके तैयार करवाए थे, जो दुनिया के अनेक देशों को सहयोग के रूप में भेजे गए थे। इससे भारत की दुनिया में प्रशंसा हुई। । केंद्र सरकार शोध के जरिए दवा खोजने और उपचार करने के मद्देनजर आगे बढ़ रही वष्य में हो सकने वाली नई बीमारियों के उपचार के लिए शोध वास्ते केंद्र सरकार की तरफ से धन मुहैया कराया जा रहा है निश्चित है कि इससे चिकित्सा जगत में भारत विकसित देशों में शुमार होने की कतार में खड़ा हो सकेगा। यदि भविष्य में हो सकने वाली नई बीमारियों का बेहतर उपचार हमारे चिकित्सा वैज्ञानिकों ने खोज लिया, तो भारत दुनिया का महत्त्वपूर्ण चिकित्सा शोधार्थी के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने आइसीएमआर के जरिए सबसे जटिल बीमारियों के उपचार के लिए वैज्ञानिकों को तैयार करने का निश्चय किया है। इससे वे जटिल बीमारियों का उपचार करने के लिए प्रेरित होंगे। इस पहल का उद्देश्य लीक से हट कर भविष्य की तैयारियों, नए ज्ञान सृजन और खोज को बढ़ावा देना है। इससे बेहतर औषधियां और नए टीके मिलेंगे। लोगों का आसानी से उपचार हो सकेगा। आइसीएमआर के मुताबिक, अगले कुछ सप्ताह में सभी प्रस्तावों को एकत्रित करने के बाद समिति इनका मूल्यांकन करेगी और उसके बाद अंतिम प्रस्तावों पर शोध होंगे, जिन्हें अधिकतम तीन साल में पूरा करना होगा। इस पहल में सभी सरकारी मेडिकल कालेज, देश के सभी शीर्ष चिकित्सा संस्थानों के साथ दिल्ली सहित सभी एम्स, आइसीएमआर के सभी संस्थानों के अलावा यूजीसी, एआइसीटीई और एनएमसी में पंजीकृत संस्थानों के शोधकर्ता शामिल हो सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों और शिक्षा संस्थाओं एवं संगठनों के जरिए आजादी के बाद चिकित्सा क्षेत्र में गंभीर पहल की गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत प्रत्येक नागरिक को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में अभी बहुत पीछे है। ऐसे में लाइलाज, असंभव लगने वाली बीमारियों का इलाज करने के मद्देनजर केंद्र सरकार की यह यह पहल स्वागतयोग्य है।
मगर सवाल है कि क्या सरकार कैंसर, पक्षाघात, मधुमेह, हृदयघात और अस्थमा जैसी बीमारियों का बेहतर इलाज, खासकर गांवों में आम आदमी को, उपलब्ध करा पाई है। केंद्र की नीतियां इस वक्त बेहतर योजनाओं के जरिए सबको समुचित सहूलियतें | मुहैया कराने 1 की है। है। इनका | उद्देश्य हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाते हुए कामयाबी की उन बुलंदियों को हासिल करना है, जो विकासशील देशों के देशों के लिए करीब नामुमकिन माना जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में नए शोध कराने और बेहतर परिणाम हासिल कर उसे मानवता के उपयोग के लिए देने की नीति निश्चय ही भारत की सर्वजन हिताय वाली नीति का ही हिस्सा है। भारत में सात दुर्लभ रोगों में से महज पांच फीसद बीमारियों का इलाज ही ही संभव है। अभी देश में देश में हालत यह है कि बीस में से एक व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित है और उसका उपचार समुचित तरीके से नहीं हो पा रहा है। आइसीएमआर के मुताबिक, देश में सात करोड़ और दुनिया में 35 में 35 करोड़ लोग दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त हैं। भारत में ऐसी अनेक बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, जिनके लक्षण देख कर डाक्टर समझ पाते कि यह बीमारी' है क्या! मिसाल के तौर पर ‘एसेंथामोएबा केराटाइटिस' 'ऐसी बीमारी है जिससे आदमी अंधा हो जाता है। इसका समुचित इलाज भारत में उपलब्ध नहीं है। | इसी तरह 'क्रुत्जफेल्ट-जैकब' ऐसी लाइलाज बीमारी है, जिसकी वजह से घातक मस्तिष्क घात हो जाया लक्षण के आधार पर समुचित तरह हजारों बीमारियां हैं, जिनके लिए सस्ता, सहज और कारगर इलाज खोजने की जरूरत है। केंद्र सरकार को चाहिए कि लाइलाज
● बीमारियों । और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए सबसे पहले गौर करे, जिस पर अभी शोध की बहुत जरूरत है। वर्तमान में केंद्रीय तकनीकी समिति (सीटीसीआरडी) की सिफारिश पर असाध्य रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत 63 रोगों को ही शामिल किया गया है। इसमें प्रति रोगी 50 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। भारत में चिकित्सा उपचार केंद्रों की संख्या जरूरत से बहुत कम कम है। गांवों में तो स्थिति और खराब है। इसलिए इस तरफ समुचित ध्यान जरूरत है। इसी तरह आबादी के मुताबिक चिकित्सकों की संख्या बहुत कम है। गांवों में एक लाख आबादी पर एक डाक्टर ही उपलब्ध है। । इसलिए अब भविष्य में होने वाली बीमारियों के नए उपचार की खोज करनी होगी। वहीं, वर्तमान में लाइलाज, दुर्लभ और अति गंभीर बीमारियों के सहज और सबको समुचित उपचार उपलब्ध कराने पर भी सोचने की जरूरत है।
◆ समान शिक्षा के उत्प्रेरक के रूप में एक राष्ट्र एक सदस्यता -
गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, खासकर भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण संसाधन सामग्री तक पहुंच छात्रों और अनुसंधान विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, खासकर भारत के दूरदराज के इलाकों में। जबकि डिजिटल युग ने सूचना प्रसारित करने के तरीके को बदल दिया है, भौतिक पुस्तकालय अकादमिक उत्कृष्टता की आधारशिला बने हुए हैं। फिर भी, ये आवश्यक ज्ञान केंद्र तेजी से अतीत के अवशेष बनते जा रहे हैं, जो केवल राष्ट्रीय संस्थानों और चयनित विश्वविद्यालयों से जुड़े कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए ही सुलभ हैं। अब तक, देश की प्रत्येक एजेंसी ने अपने डिजिटल लाइब्रेरी संसाधनों के लिए सदस्यता ले ली है, यूजीसी के पास इनफ्लिबनेट है, जो चयनित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उपलब्ध है, सीएसआईआर और डीएसटी संस्थानों के पास राष्ट्रीय ज्ञान संसाधन कंसोर्टियम (एनकेआरसी) है; आईसीएआर संस्थानों को सीईआरए आदि करोड़ों रुपये का भुगतान करना पड़ता है। कई मामलों में, ये ई-संसाधन केवल मेजबान संस्थान के उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित हैं, हालांकि इन्हें सार्वजनिक धन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। यदि महत्वाकांक्षी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो इस असमानता को दूर करने और शैक्षिक परिदृश्य को पुनर्जीवित करने की क्षमता है। तकनीकी प्रगति के बावजूद, भारत में अब तक गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण नहीं किया जा सका है। अधिकांश कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों को विभिन्न कारणों से चिंताजनक गिरावट का सामना करना पड़ रहा है।
पुस्तकालयों में जाने के प्रति युवा पीढ़ी की रुचि की कमी और घटती निधि ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। दुर्भाग्य से, कई सार्वजनिक संस्थानों में, मुख्य रूप से राष्ट्रीय संस्थानों से जुड़े पुस्तकालयों में, पुस्तकालय कर्मचारियों में अक्सर पाठकों के लिए स्वागत योग्य वातावरण बनाने के लिए उत्साह और पारस्परिक कौशल का अभाव होता है। यह, बदले में, सबसे वास्तविक पाठकों को भी अलग-थलग कर देता है, जो बाधाओं के बावजूद, पुस्तकालयों में जाने का प्रयास करते हैं। समर्थन की कमी और एक अनामंत्रित माहौल छात्रों और शोधकर्ताओं को शैक्षणिक और बौद्धिक गतिविधियों के लिए पुस्तकालयों को अपना पसंदीदा स्थान बनाने से रोक सकता है, जिससे पुस्तकालय संस्कृति और भी नष्ट हो रही है जो पहले से ही खतरे में है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल का उद्देश्य एक केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रव्यापी उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके इन चुनौतियों का समाधान करना है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं, डेटाबेस और ई-पुस्तकों के लिए थोक सदस्यता पर बातचीत करके, पहल यह सुनिश्चित कर सकती है कि भौगोलिक या आर्थिक बाधाओं की परवाह किए बिना प्रत्येक छात्र के पास समान ज्ञान है। एक राष्ट्रीय संस्थान में एक छात्र या विद्वान को जो मिलता है वह देश के सुदूर कोने में स्थित विश्वविद्यालय में एक छात्र को मिलेगा। यह ज्ञान संसाधन का लोकतंत्रीकरण कर रहा है। हालाँकि, इस पहल की सफलता केवल पहुंच से कहीं अधिक पर निर्भर करती है। भारत को अपने पुस्तकालय पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए एक समानांतर प्रयास की आवश्यकता है। डिजिटल युग में भी, भौतिक पुस्तकालय प्रतिबिंब और सहयोग के स्थान के रूप में अपूरणीय हैं। सरकार को पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए और कुशल, प्रेरित पुस्तकालयाध्यक्षों की भर्ती के लिए भी कदम उठाना चाहिए जो पाठकों की बढ़ती जरूरतों को समझते हैं और प्रभावी ढंग से डिजिटल और भौतिक संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं। समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को प्रत्येक पंजीकृत छात्र और विद्वान को व्यक्तिगत लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करना होगा, जिससे किसी भी समय, कहीं भी संसाधनों तक सीधी पहुंच सक्षम हो सके। यह पारंपरिक संस्थागत को दरकिनार कर देगागेटकीपिंग और अधिक पाठक-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना।
नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यान्वयन की कमी या पूरक उपायों की उपेक्षा के कारण यह महत्वाकांक्षी योजना विफल न हो। ज्ञान प्रगति की आधारशिला है और इस तक पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, न कि विशेषाधिकार के रूप में। इस पहल की क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए, यह आवश्यक है कि सरकार प्रत्येक छात्र के लिए इन संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करे।
◆ तकनीक बनाम इंसानियत -
आज की दुनिया एक बड़े परिवर्तन के दौर गुजर रही है। डिजिटल तकनीक के व्यापक प्रसार ने हमारी दिनचर्या और सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमता और सोशल मीडिया ने न केवल हमें एक नए युग में प्रवेश कराया है, बल्कि हमारी इंसानियत पर भी सवाल खड़े किए हैं। आज जब अपने चारों ओर की दुनिया को देखा जाए तो कोई भी संवेदनशील व्यक्ति यह सोचने पर मजबूर हो सकता है कि क्या यह तकनीकी क्रांति हमें वास्तव में जोड़ कर रख रही है या हमें और भी अलग-थलग कर रही है ! एक श्लोक है- 'असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय ।' यानी हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यह श्लोक इस बात की याद दिलाता है कि सच्चा मार्ग वही है, जो अंधकार और असत्य से मुक्त हो। इसी तरह, आज हमें तकनीक के उजाले में खोते हुए उन मूल्यों को याद रखना होगा, जो हमें मानवता की ओर ले जाते हैं । तकनीक ने भले ही हमें वैश्विक स्तर पर जुड़ने का अवसर दिया हो, लेकिन वास्तविकता में हमने अपनी आसपास की दुनिया से दूरी बना ली है। आभासी दुनिया में जुड़ने के सुख की हकीकत यह है कि सोशल मीडिया पर हजारों लोग दोस्ती की सूची में हो सकते हैं, उन्हें हमारा लिखा हुआ या कोई और सामग्री पसंद आती है, मगर वास्तव में कोई हमसे जुड़ा नहीं होता। हमारा पड़ोसी तक हमारे दुख शामिल नहीं होना चाहता। ज्यादातर लोग एक ही घर में रह कर अपने स्मार्टफोन में डूबे रहते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि इस डिजिटल दुनिया में हम और भी अकेले होते जा रहे हैं। उन दिनों को याद किया जा सकता है, जब में परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर हम वास्तविक बातचीत किया करते थे। आज वह आपसी संवाद एक 'कमेंट' या 'इमोजी' तक सीमित हो गया है। खुद में सिमटने के उदाहरण अपने आसपास हर जगह देखे जा सकते हैं। किसी व्यावसायिक माल में जमा लोगों को देख कर उनके भी संवेदनशील होने के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ समय पहले एक बुजुर्ग एक जगह असहाय बैठे थे। शायद उन्हें मदद की जरूरत थी। चारों ओर से लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी अपने-अपने स्मार्टफोन या बाजार से खरीदारी में व्यस्त ।
एक व्यक्ति ने जब उनसे बात की, तब पता चला कि उन्हें अपने बेटे से संपर्क करने में परेशानी हो रही थी । उस व्यक्ति ने उनकी मदद की, तब उनकी आंखों में राहत और आभार का भाव उभरे। तकनीक ने हमें भले ही एक नई दुनिया दी हो, लेकिन हम अपनी इंसानियत और आपसी जुड़ाव से कहीं दूर हो गए यह विडंबना है कि जब हमारे पास इतनी तकनीकी प्रगति है, तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी उसी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं। तनाव, अवसाद और अकेलापन जैसे मुद्दे अब आम हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल युग में इन समस्याओं की वृद्धि इस बात का संकेत है कि हम अपने वास्तविक मानवीय रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। अब वह समय नहीं रहा जब हम अपनों के साथ समय बिताने से आत्मिक शांति पाते थे । एक दौर था जब इंसानियत, प्यार और देखभाल हमारे रिश्तों की नींव हुआ करती थी । अब यह सब डिजिटल संकेत और स्क्रीन पर उभरते 'नोटिफिकेशन' या सूचनाओं और संदेशों में बंधकर रह गया है। 'विज्ञान ने संसार को एक बहुत बड़ी चीज दी है- तथ्यों को पहचानने की शक्ति । लेकिन प्रेम ही वह तत्त्व है, जो मानव हृदय को सही दिशा देता है।' प्रेमचंद की ये पंक्तियां हमें इस बात का अहसास कराती हैं कि तकनीक और विज्ञान कितनी भी उन्नति कर लें, आखिरकार मानवीय संवेदनाएं ही हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं और जीवन को सार्थक बनाती हैं। इस बात को लेकर चिंतित होना चाहिए कि क्या हम वाकई सही दिशा में जा रहे हैं। हालत यह हो गई है कि कोई हादसा हो जाता है, कोई अपराध हो रहा होता है, उस समय भी कुछ लोग मदद पहुंचाने या उसके लिए दौड़ पड़ने के बजाय अपने स्मार्टफोन निकाल कर झट से वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं ।
सवाल है कि क्या तकनीक हमारी संवेदनाओं और सोचने-समझने की दिशा को भी प्रभावित कर रही है। तकनीकी प्रगति ने जीवन को सरल बना दिया है, लेकिन इसने हमारे दिलों को जटिल भी कर दिया है। क्या हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं, जहां इंसानियत और मानवीय संवेदनाओं को तकनीक से परे एक नया आयाम देना होगा ? इस प्रश्न का उत्तर हम सभी को मिलकर खोजना होगा। तकनीक का सही उपयोग तभी संभव है, जब यह हमारे मानवीय मूल्यों को संजोए रखे। तकनीकी के उपयोग का उद्देश्य हमारी जिंदगी को आसान बनाना था, लेकिन कहीं न कहीं यह हमें आपस में जोड़ने के बजाय भावनात्मक रूप से दूर कर रही है । हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तकनीक का प्रयोग इंसानियत को मजबूत करने के लिए हो, न कि इसे कमजोर करने के लिए ।
◆ क्यों किताबें पढ़ना आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए
1. ज्ञान का राजमार्ग: किताबें लगभग किसी भी विषय पर ज्ञान का एक विशाल भंडार प्रदान करती हैं। इतिहास, विज्ञान, दर्शन में गहराई से गोता लगाएँ या नए शौक और रुचियों का पता लगाएँ। 2. बढ़ी हुई शब्दावली: नियमित रूप से पढ़ने से आपको शब्दावली की एक विस्तृत श्रृंखला का पता चलता है, जिससे आपके संचार कौशल और समझ में सुधार होता है। 3. याददाश्त बढ़ाता है: अध्ययनों से पता चलता है कि पढ़ना आपकी याददाश्त और संज्ञानात्मक कार्य को तेज करने में मदद कर सकता है, जिससे आपका दिमाग सक्रिय और व्यस्त रहता है। 4. तनाव में कमी: एक अच्छी किताब के साथ आराम करना मानसिक पलायन का एक रूप हो सकता है, जो दैनिक चिंताओं से अस्थायी राहत और आराम करने का मौका देता है। 5. बेहतर फोकस और एकाग्रता: आज की तेज़-तर्रार दुनिया में जो विकर्षणों से भरी हुई है, पढ़ना आपकी ध्यान केंद्रित करने और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को मजबूत करता है। 6. सहानुभूति और परिप्रेक्ष्य: काल्पनिक पात्रों के जूते में कदम रखने से आपको सहानुभूति विकसित करने और विभिन्न दृष्टिकोणों की गहरी समझ हासिल करने की अनुमति मिलती है। 7. रचनात्मकता में वृद्धि: पढ़ने से आपको नए विचार और विचार प्रक्रियाएँ मिलती हैं, जो संभावित रूप से आपकी खुद की रचनात्मकता और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देती हैं। 8. मजबूत लेखन कौशल: अच्छी तरह से लिखे गए गद्य में खुद को डुबोने से आपकी लेखन शैली, वाक्य संरचना और समग्र संचार स्पष्टता में सुधार हो सकता है। 9. बेहतर नींद की गुणवत्ता: सोने से पहले स्क्रीन टाइम की जगह किताब पढ़ें। पढ़ने की शांत प्रकृति आपको आराम करने और तनावमुक्त होने में मदद कर सकती है, जिससे बेहतर नींद की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है।
कहानी ◆ !! अनोखा दोस्त कौआ !! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
एक कौआ था। वह एक किसान के घर के आँगन के पेड़ पर रहता था। किसान रोज़ सुबह उसे खाने के लिए पहले कुछ देकर बाद में खुद खाता था। किसान खेत में चले जाने के बाद कौआ रोज़ उड़ते-उड़ते ब्रह्माजी के दरबार तक पहुँचता था और दरबार के बाहर जो नीम का पेड़ था, उस पर बैठकर ब्रह्माजी की सारी बातें सुना करता था। शाम होते ही कौआ उड़ता हुआ किसान के पास पहुँचता और ब्रह्माजी के दरबार की सारी बातें उसे सुनाया करता था। एक दिन कौए ने सुना कि ब्रह्माजी कह रहे हैं कि इस साल बारिश नहीं होगी। अकाल पड़ जायेगा। उसके बाद ब्रह्माजी ने कहा - "पर पहाड़ो में खूब बारिश होगी।" शाम होते ही कौआ किसान के पास आया और उससे कहा - "बारिश नहीं होगी, अभी से सोचो क्या किया जाये"। किसान ने खूब चिन्तित होकर कहा - "तुम ही बताओ दोस्त क्या किया जाये"। कौए ने कहा - "ब्रह्माजी ने कहा था पहाड़ों में जरुर बारिश होगी। क्यों न तुम पहाड़ पर खेती की तैयारी करना शुरु करो?" किसान ने उसी वक्त पहाड़ पर खेती की तैयारी की। आस-पास के लोग जब उस पर हँसने लगे, उसे बेवकूफ कहने लगे, उसने कहा - "तुम सब भी यही करो। कौआ मेरा दोस्त है, वह मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाता है" - पर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। उस पर और ज्यादा हँसने लगे। उस साल बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। वह किसान ही अकेला किसान था जिसके पास ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया।
देखते ही देखते साल बीत गया इस बार कौए ने कहा - "ब्रह्माजी का कहना था कि इस साल बारिश होगी। खूब फसल होगी। पर फसल के साथ-साथ ढेर सारे कीड़े पैदा होगें। और कीड़े सारी फसल के चौपट कर देंगे।" इस बार कौए ने किसान से कहा - "इस बार पहले से ही तुम मैना पंछी और छछूंदों को ले आना ताकि वे कीड़ों को खा जाये।" किसान ने जब ढेर सारे छछूंदों को ले आया, मैना और पंछी को ले आया, आसपास के लोग उसे ध्यान से देखने लगे - पर इस बार वे किसान पर हंसे नहीं। इस साल भी किसान ने अपने घर में ढेर सारा अनाज इकट्ठा किया। इसके बाद कौआ फिर से ब्रह्माजी के दरबार के बाहर नीम के पेड़ पर बैठा हुआ था जब ब्रह्माजी कर रहे थे - "फसल खूब होगी पर ढेर सारे चूहे फसल पर टूट पड़ेगे।" कौए ने किसान से कहा - "इस बार तुम्हें बिल्लियों को न्योता देना पड़ेगा - एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी बिल्लियाँ"। इस बार आस-पास के लोग भी बिल्लियों को ले आये। इसी तरह पूरे गाँव में ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। कौए ने सबकी जान बचाई।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब